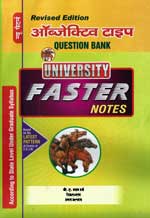|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
प्रश्न- भारतीय जनतन्त्र में शिक्षा के उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।
अथवा
भारत देश के विशेष सन्दर्भ में प्रजातान्त्रिक शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर-
जनतन्त्र तथा शिक्षा के उद्देश्य
(Democracy and Aims of Education)
जनतन्त्र में शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो कि इस प्रकार हैं-
(1) उत्तम अभिरुचियों का विकास (Development of Worthy Interests ) - जनतन्त्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है बालकों के चरित्र एवं रुचियों का निर्माण करना तथा उनके जीवन को सम्पन्नता प्रदान करना जिससे कि बालकों में उत्तम अभिरुचियों का विकास हो पाये। हरबर्ट ने बहुमुखी रुचियों के विकास पर बल दिया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बालकों को अनेकों प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए अवसर प्रदान किये जाने चाहिए जिससे बालकों में कार्य करने की रुचि उत्पन्न हो। बालकों में जितनी अधिक श्रेष्ठ अभिरुचियाँ जागृत होंगी उतना ही वह सुखी एवं कुशल जीवन को व्यतीत कर पायेगा।
(2) अच्छी आदतों का विकास (Development of Sound Habits) - आदतों से ही बालकों में अच्छे व बुरे कार्यों की नींव पड़ती है। इसीलिए जनतन्त्र शिक्षा का उद्देश्य बालकों के अन्दर अच्छी आदतों का विकास करना है। जनतन्त्र को सफल व उत्तम बनाने के लिए शुरूआत से ही बालको में अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए।
(3) जनतन्त्र के मूल्यों का विकास (Development of Democratic Values) जनतन्त्र की सफलता उन नागरिकों से होती है जो कि जनतन्त्र मूल्यों का पालन करते है। जनतन्त्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों में जनतन्त्र के मूल्यों का विकास करना है। जब तक बालकों को विद्यालय में उचित अवसर नहीं दिये जायेंगे तब तक कोई भी पुस्तकीय ज्ञान उस उद्देश्य तक प्राप्त नहीं कर पायेगा। बालक को जब जनतन्त्रीय ढंग से रहने के अवसर उपलब्ध होंगे तभी वह जनतन्त्रीय ढंग से रहना सीख सकता है। अतः इसी के अनुसार स्कूल का वातावरण प्रत्येक पाठ्यक्रम सम्बन्धी क्रिया, हर प्रकार से सम्बन्ध चाहे वह सम्बद्ध बालकों से हो अथवा शिक्षकों से जनतन्त्रीय मूल्यों के अनुसार होना चाहिए।
(4) व्यावसायिक कुशलता का विकास (Development of Vocational Effeciency) - व्यक्ति अब आर्थिक रूप से हीन होता है तो वह अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है और विचलित होकर वह धनवानों के हाथों का खिलौना बनकर अपने बहुमूल्य वोट को अवाछनीय व्यक्ति को दे सकता है। इसलिए जनतन्त्र की सफलता हेतु नागरिकों का आर्थिक रूप से सम्पन्न होना आवश्यक है। जनतन्त्रीय शिक्षा बालकों को व्यंवसायिक कुशलता से निपुण करती है जिससे बालक शिक्षा प्राप्ति के बाद किसी भी श्रेष्ठ व्यवसाय को अपनाकर अपना भार स्वयं उठा सकता है तथा राष्ट्र की यथाशक्ति सेवा कर सकता है।
(5) सामाजिक दृष्टिकोण का विकास (Development of Social Outlook) जनतन्त्रीय शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक दृष्टि का विकास हो जिससे प्रत्येक बालक में यह धारणा उत्पन्न हो कि वह समाज का एक अंग है तथा उसका जीवन समाज के लिए मुख्य भूमिका रखता है जिससे वह समाज हित के लिए अपने निजी हित को भी त्यागने से संकोच नहीं करे। बालकों में सामाजिक अभिरुचियाँ विकसित होने के साथ-साथ अपने दायित्व को समझने के लिए इस उद्देश्य को शिक्षा में महत्व दिया जाना चाहिए।
(6) विचार-शक्ति का विकास (Development of Thinking Power) - आज के बालक कल का भविष्य हैं तथा इन्हीं बालकों को भविष्य में राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं पर विचार करना है। अतः जनतन्त्रीय शिक्षा का उद्देश्य बालकों में अच्छी आदतों का विकास करना है। शिक्षा के द्वारा अनेक प्रकार की समस्याओं पर स्वतन्त्रतापूर्वक विचार करने का निजी निर्णय लेने की आदत डालनी चाहिए।
(7) नेतृत्व का विकास (Development of Leadership) - जनतन्त्र शिक्षा बालकों में नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहन देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वर्तमान समय के बालक भविष्य के शासन की बागडोर सम्भालेंगे। जनतन्त्र की सफलता को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक बड़े होकर नागरिक के रूप में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत नेतृत्व कर सकें।
(8) व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास (Development of Harmonious Personality) - वर्तमान समय का संसार देखा जाए तो संघर्ष एवं कटुताओं से भरा हुआ है। इस संसार में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो सामंजस्यपूर्ण हो। जनतन्त्रीय शिक्षा व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास करती है। अतः शिक्षा को बालक के व्यक्तित्व का सामजस्यपूर्ण विकास करना चाहिए जिससे कि वो एक अच्छे नागरिक के रूप में स्वयं का तथा समाज का कल्याण कर सकें।
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।