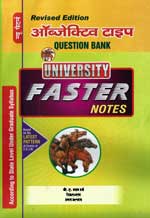|
बी ए - एम ए >> फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र फास्टर नोट्स-2018 बी. ए. प्रथम वर्ष शिक्षाशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्रयूनिवर्सिटी फास्टर नोट्स
|
|
||||||
बी. ए. प्रथम वर्ष (सेमेस्टर-1) शिक्षाशास्त्र के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-प्रश्नोत्तर
प्रश्न- जीवन मूल्यों की स्थापना में विद्यालय का क्या महत्व है?
उत्तर-
विद्यालय और मूल्य शिक्षा
(School and Value Education)
अधिकांश विद्वानों का यह मत रहा है कि विद्यालयों में मूल्य शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए लेकिन शिक्षा का विधान पृथक क्रिया अथवा विषय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए बल्कि विद्यालयों की सभी क्रियाओं एवं विषयों को एक साथ किया जाना चाहिए। बच्चों के उचित विकास हेतु विद्यालयों को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए -
1. मूल्य प्रधान वातावरण बच्चे विद्यालय- में प्रवेश लेने से पूर्व अपने परिवारों एवं समुदायों के मध्य रहे होते हैं, जहाँ पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के माध्यम से वे अनेक आदर्शों, सिद्धान्तों, विश्वासों एवं व्यवहार मानदंडों को ग्रहण करते हैं। विद्यालयों का कार्य यह होता है कि इस प्रकार के ग्रहण किये गये विश्वासों, आदर्शों एवं व्यवहार मानदंडों को काट-छांट कर उसे सही दिशा प्रदान करें। इसके लिए सर्वप्रथम मूलभूत आवश्यकता यह है कि विद्यालय का सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मूल्य प्रधान होना चाहिए। यहाँ पर सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार, समान अधिकार व उचित न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए।
2. पाठ्यक्रम सहगामी क्रियायें और मूल्य शिक्षा - बच्चों के विकास में सहपाठ्यचारी क्रियाओं का भी अत्यधिक महत्व है। सहपाठ्यचारी क्रियायें उन क्रियाओं को कहा जाता है जो विद्यालय में विद्यालयी
विषयों के अतिरिक्त होती है। मूल्य शिक्षा की दृष्टि से इनमें सबसे अधिक महत्व प्रातःकालीन सभा और साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सभाओं का होता है जोकि निम्नलिखित हैं-
(i) मूल्य शिक्षा और प्रातःकालीन सभा - प्रायः सभी विद्यालयों की दैनिक शुरूआत प्रात कालीन सभा के साथ होती है। यदि शिक्षकों द्वारा इसे महत्व दिया जाता है और स्वयं अनुशासित रहकर ईश्वर का ध्यान किया जाता है तो बच्चों में अच्छे गुणों का विकास आसानी से होता है। प्रातः कालीन सभा में भगवान की प्रार्थना के बाद 5 मिनट का समय प्रेरक प्रसंगों के लिए दिया जाना चाहिए। इन प्रेरक प्रसंगों में बुद्ध और हंस, राम और शबरी, कृष्ण और सुदामा तथा महावीर और सर्प आदि प्रसंग सुनाये जा सकते हैं।
(ii) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम - साहित्यिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत कवि सम्मेलन, कवि दरबार व साहित्यिक वाद-विवाद आदि को शामिल किया जाता है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत संगीत, गायन व लोकगीत आदि को शामिल किया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों में हमारी सभ्यता एवं संस्कृति परिलक्षित होती है। शिक्षकों को यह चाहिए कि वे इन कार्यक्रमों का दायित्व बच्चों पर छोड़ दे क्योंकि वे इसके माध्यम से प्रेम व सत्यता की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों की विषय सामग्री अच्छी तथा मानव मूल्यों की अभिव्यक्ति से मुक्त होनी चाहिए।
(iii) खेलकूद ये दो प्रकार के कार्यक्रम होते हैं - वैयष्टिक और सामूहिक। वैयष्टिक खेलकूदों के अन्तर्गत आसन, व्यायाम आदि को शामिल किया गया है। इसके द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य का महत्व बताया जा सकता है तथा उत्तम स्वास्थ्य के प्रति सौन्दर्य की भावना को जाग्रत किया जा सकता है। आसन और व्यायाम करने वालों के शरीर सुडौल व स्वस्थ होते हैं।
(iv) राष्ट्रीय उत्सव - आज हमारे देश में मुख्य रूप से तीन राष्ट्रीय उत्सव मनाये जाते हैं - स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गणतंत्र दिवस 26 जनवरी एवं गाँधी जयन्ती 2 अक्टूबर। इन उत्सवों को मनाने की रीति हम सभी जानते हैं। विद्यालय के बच्चे प्रभात मे जयकारे लगाते हुए आगे निकलते हैं। कुछ खेलकूद व कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं। आज कोई भी व्यक्ति राष्ट्र ध्वज के सम्मान में 1 मिनट सावधान खड़ा नहीं रहता है, राष्ट्रहित की बात तो बहुत दूर की बात है।
(v) महापुरुषों के जन्मोत्सव - विद्यालयों में बच्चों को प्रेरणा देने के लिए महापुरुषों के जन्मोत्सव मनाया जाते हैं किन्तु आजकल इन उत्सवों को मनाने की केवल औपचारिकताएँ निभाई जाती हैं क्योंकि इन उत्सवों में न तो प्रधानाचार्य और शिक्षक रुचि लेते हैं और न ही छात्र अध्यापकों को इन महापुरुषों के जीवन में प्रकाश डालना चाहिए तथा प्रेरक प्रसंग सुनाये जाने चाहिए। शिक्षकों द्वारा बच्चों को अपने प्रेरक प्रसंग में यह बताना चाहिए कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति कभी नहीं मरते हैं अर्थात वे अमर हो जाते हैं।
3. विद्यालयी विषयों के शिक्षण के साथ मूल्य शिक्षा - विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले लगभग सभी विषयों से छात्रों में उचित मूल्यों का विकास किया जा सकता है। लेकिन इनमें भाषा और इतिहास दो ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से बच्चों का विकास आसानी से किया जा सकता है।
(i) मूल्य शिक्षण और भाषा- भाषा के अन्तर्गत महापुरुषों की जीवनी एवं वीर्य और शौर्य के प्रसंगों को शामिल किया जाता है। वास्तव में इसमें समाज के समस्त विश्वासों, आदर्शों और सिद्धान्तों का समावेश होता है और इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हृदय पर पड़ता है। अध्यापको को पाठ पढ़ाते समय उसमें निहित आदर्शों एवं सिद्धान्तों को बालको के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
(ii) मूल्य शिक्षा और इतिहास - इतिहास का सम्बन्ध केवल राजाओं महाराजाओं के उत्थान पतन से न होकर इसमें जाति-समाज अथवा राष्ट्र विशेष की सभ्यता एवं संस्कृति का दिग्दर्शन व मूल्यों का दिग्दर्शन होता है। इतिहास देखने पर यह पता चलता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तथा महाभारत का युद्ध हुआ। अकबर के दरबार में भाट ने राणा प्रताप द्वारा दी गयी पगड़ी को उतारकर सर झुकाया था। अतः इतिहास के माध्यम से बच्चों को जानकारी के रूप में लाभान्वित किया जा सकता है।
(iii) मूल्य शिक्षा और भूगोल - भूगोल के माध्यम से बच्चों को देश विदेश की प्राकृतिक स्थिति से अवगत कराया जाता है। एक शिक्षक थोड़ी सी सावधानी बरतकर भूगोल के माध्यम से बच्चों की अन्योन्याश्रित का ज्ञान करा सकता है तथा उनमें विश्वबन्धुत्व की भावना जाग्रत कर सकता है।
(iv) मूल्य शिक्षा और नागरिकशास्त्र - नागरिकशास्त्र के अन्तर्गत मूल रूप से नागरिकों के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को शामिल किया जाता है। इसके शिक्षण के साथ राजनैतिक मूल्यों का विकास बड़ी ही आसानी के साथ किया जाता है। इसमें अपने हित के साथ राष्ट्र हित की भी चिन्ता की जाती है। अध्ययन से यह पता चलता है कि नागरिकों के हित में ही राष्ट्र का हित होता है। यह युग अंतर्राष्ट्रीय युग है अतः हमें इसी पर जोर देना चाहिए।
(v) मूल्य शिक्षा और अर्थशास्त्र - अर्थशास्त्र के अन्तर्गत आय के साधनों और स्रोतों की चर्चा की जाती है, उत्पादन में श्रम और साहस के महत्व को स्पष्ट किया जाता है, मांग और पूर्ति के नियम बताये जाते हैं तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के भयंकर परिणाम में सतर्क किया जाता है। शिक्षक द्वारा शिक्षण के साथ जीवन साहस और सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। यदि शिक्षक द्वारा थोड़ी सी सावधानी बरती जाती है तो वह यह भी स्पष्ट कर सकता है कि जीवन प्रत्येक क्षेत्र में इनका अत्यधिक महत्व है।
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जीवन मूल्यों में विद्यालयों का भी अत्यधिक महत्व है।
|
|||||
- प्रश्न- वैदिक काल में गुरुओं के शिष्यों के प्रति उत्तरदायित्वों का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्धों का विवेचनात्मक वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु यह किस सीमा तक प्रासंगिक है?
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा के कम से कम पाँच महत्त्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य गुण एवं दोष बताइए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा के प्रमुख गुण बताइए।
- प्रश्न- प्राचीन काल में शिक्षा से क्या अभिप्राय था? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य एवं आदर्श क्या थे?
- प्रश्न- वैदिककालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समावर्तन और उपनयन संस्कारों का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान का विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति करना था। स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- आधुनिक काल में प्राचीन वैदिककालीन शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक शिक्षा में कक्षा नायकीय प्रणाली के महत्व की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- वैदिक कालीन शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न सम्प्रत्ययों का उल्लेख करते हुए उसके वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा के दार्शनिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के समाजशास्त्रीय सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के राजनीतिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के आर्थिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सम्प्रत्यय की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के वास्तविक सम्प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- क्या मापन एवं मूल्यांकन शिक्षा का अंग है?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए। आपको जो अब तक ज्ञात परिभाषाएँ हैं उनमें से कौन-सी आपकी राय में सर्वाधिक स्वीकार्य है और क्यों?
- प्रश्न- शिक्षा से तुम क्या समझते हो? शिक्षा की परिभाषाएँ लिखिए तथा उसकी विशेषताएँ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का संकीर्ण तथा विस्तृत अर्थ बताइए तथा स्पष्ट कीजिए कि शिक्षा क्या है?
- प्रश्न- शिक्षा का 'शाब्दिक अर्थ बताइए।
- प्रश्न- शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी अपने शब्दों में परिभाषा दीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
- प्रश्न- शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की दो परिभाषाएँ लिखिए।
- प्रश्न- शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- आपके अनुसार शिक्षा की सर्वाधिक स्वीकार्य परिभाषा कौन-सी है और क्यों?
- प्रश्न- 'शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है।' जॉन डीवी के इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं?
- प्रश्न- 'शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन् जीवन-यापन की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के इस कथन को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा विज्ञान है या कला या दोनों? स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा की प्रकृति की विवेचना कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ को स्पष्ट कीजिए तथा शिक्षा के व्यापक व संकुचित अर्थ में अन्तर स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षा और साक्षरता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इन दोनों में अन्तर व सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
- प्रश्न- शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या, ज्ञान, शिक्षण प्रशिक्षण बनाम शिक्षा पर प्रकाश डालिए।
- प्रश्न- विद्या और ज्ञान में अन्तर समझाइए।
- प्रश्न- शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर को स्पष्ट कीजिए।