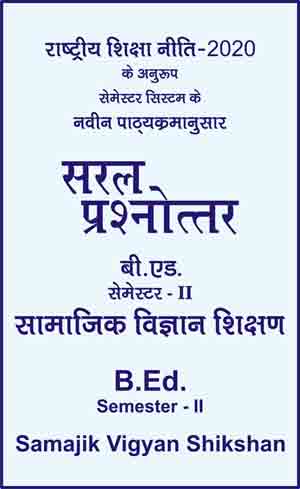|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- निदानात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? निदान के विभिन्न स्तरों को बताते हुए निदानात्मक परीक्षा की रचना को स्पष्ट कीजिए।
अथवा
निदानात्मक मूल्यांकन से क्या आशय है? इसके विभिन्न स्तर व विशेषताओं को बताइए! निदानात्मक परीक्षा की रचना करते समय किन-किन पदों का अनुकरण किया जाता है?
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
- निदानात्मक मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए।
- निदानात्मक मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों को बताइए।
- निदानात्मक मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताओं सम्बन्ध में बताइए।
- एक निदानात्मक परीक्षा की निर्माण प्रक्रिया पर संक्षेप में लिखिए।
उत्तर -
निदानात्मक मूल्यांकन
(Diagnostic Evaluation)
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपलब्धियों एवं परीक्षा परिणामों से कमजोरियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है; परंतु इससे यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि उनकी कमजोरियों के कारण क्या हैं अथवा उनकी अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयाँ क्या हैं? इस प्रकार की जानकारियाँ कराना ही निदानात्मक मूल्यांकन (Diagnostic Evaluation) कहलाता है।
शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, “निदान उपयुक्त उपचारात्मक अथवा उच्च अध्ययन कार्यों को निर्धारित करने के द्वारा उसके अध्ययन की सुविधा बनाने के उद्देश्य से एक विशेष विषय में आवश्यक कार्यों के पदानुक्रम की उसकी विशिष्टता करके एक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।”
सामाजिक विज्ञान शिक्षण अध्ययन में जब किसी छात्र को कठिनाई होती है अथवा परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाता है तब यह जानकारी करनी आवश्यक हो जाती है कि छात्र विषय के किस खण्ड अथवा अनुभव में कठिनाई कर रहा है अथवा असफल हो रहा है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षक उस छात्र की किसी क्षेत्र/खण्ड विशेष में व्यवहारिक समस्या अथवा असफलता के कारणों का खोजता है। तत्पश्चात उनका निराकरण करके अध्ययन पथ पर उन्नयन होने के लिए उसका सहयोग देता है।
निदान के स्तर
(Level of Diagnosis)
निदान के निम्नलिखित स्तर हैं –
-
समस्याग्रस्त छात्र की पहचान करना (Identifying the Student who Face Difficulty) – सर्वप्रथम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समस्या या कठिनाइयाँ छात्रों की पहचान की जाती है।
-
कठिनाई की प्रकृति (Nature of Difficulty) – इसके अन्तर्गत छात्रों द्वारा कृत त्रुटियों के क्षेत्रों की जानकारी की जाती है।
-
समस्या या कठिनाई के कारण (Causes of Difficulty) – छात्रों द्वारा कृत त्रुटियों के क्षेत्रों की जानकारी को जानने के उपरान्त उनके कारणों का पता लगाया जाता है।
-
उपचार (Remedy) – समस्या या कठिनाई के कारण की जानकारी हो जाने के उपरान्त उपचार किया जाता है। चूँकि इसके कोई निश्चित नियम नहीं हैं, इसलिए यह समस्या की प्रकृति पर निर्भर करता है।
निदानात्मक परीक्षण की रचना (Construction of a Diagnostic Test)
वैसे तो विद्यार्थियों की अध्ययन कठिनाइयों तथा कमजोरियों का निदान करने हेतु आज अपने देश तथा विदेशों में निर्मित बहुत-से प्रमाणिक निदानात्मक परीक्षण (Standardized Diagnostic Tests) उपलब्ध हैं परंतु एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में यदि आप भी एक निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कर सकने की नियुक्ति अथवा ही अपेक्षा रखते हैं। इस प्रकार के परीक्षण के निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यों को प्रायः निम्नांकित तीन चरणों में पूरा किया जाता है –
(अ) निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए नियोजन करना (Planning for the Construction of the Diagnostic Test)
एक निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित नियोजन की काफी जरूरत होती है। इस प्रकार के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है –
(1) अध्ययन कठिनाइयों तथा कमजोरियों से सम्बन्धित क्षेत्रों से अवगत होना (Knowing about the Areas of Weakness or Learning Difficulties) – निदानात्मक परीक्षण के निर्माण की शुरुआत उसके निर्माण की जरूरत पर ही आधारित होती है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में कौन कितना कमजोर है या किसकी क्या कठिनाइयाँ हैं, इस बात की पूरी जानकारी हेतु उपलब्ध परीक्षणों के परिणाम, कक्षा में किया जाने वाला अभ्यास कार्य, विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार आदि को जीवन सहायक ली जा सकती है। इस तरह विद्यार्थी विशेष की उपलब्धि तथा नियत कठिनाई मूल्यांकन करने हेतु जो भी तकनीक या साधन काम में लाये जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों तथा निष्कर्षों से ऐसे संकेत अवश्य मिल जाते हैं कि विद्यार्थी विशेष या कक्षा और सम्पूर्ण विशेष में कठिनाई सम्बन्धी लक्षण स्पष्ट हो जायें, यह पता लग जाता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन सम्बन्धी अध्ययन में विद्यार्थी कठिनाइयों अथवा कमजोरियों का अनुभव कर रहा है। इस प्रकार की कठिनाइयाँ तथा कमजोरियों का आभास से उसी के निदानात्मक परीक्षण का विषय बनाया जा सकता है।
(2) कठिनाई क्षेत्र को निर्धारित तथा सीमित करना (Specifying and Limiting the Difficulty Area) – निदानात्मक परीक्षण जिस इकाई या प्रकारण विशेष पर बनाया जाता है उसे जितना भी सीमित कर दिया जाये उतना ही अच्छा होता है। यदि किसी विद्यार्थी विशेष सामाजिक विज्ञान के किसी उपलब्धि परीक्षण में बहुत कम प्राप्त किये हैं तो वहीं उसके इस मूल्यांकन परिणामों की और अधिक गहराई से विश्लेषण करना होगा। यह विश्लेषण बता सकता है कि विद्यार्थी इतिहास के अध्ययन में नहीं बल्कि भूगोल में कमजोर है। आगे वह यह भी संकेत करता है कि भूगोल के अन्तर्गत मिट्टियों के प्रकार तथा उनके उपयोग के सन्दर्भ में वह कठिनाई का अनुभव कर रहा है। मिट्टियों के प्रकार तथा उसके उपयोग को हम निदानात्मक परीक्षण का विषय बना सकते हैं। इस तरह हम निदानात्मक परीक्षण निर्माण हेतु किसी एक इकाई, उप-इकाई, अवयव विशेष को चुन लेते हैं जिससे उसका गहराई और विस्तार से निदान किया जा सके। इस हेतु निम्न-निम्न इकाइयाँ, उप-इकाइयाँ या अवयवों विशेष पर निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करके फिर उन्हें एक इकाई रूप दे देना चाहिए ताकि एक बड़े क्षेत्र, शाखा या पूरे विषय के लिए निदानात्मक परीक्षण तैयार हो सके।
(3) विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) – सामाजिक विज्ञान की एक उप-इकाई (Sub-unit) या किसी एक अवयव या सम्बन्धित विषय-वस्तु की इकाई का विश्लेषण करके यह जानना हमें प्रयत्न करना चाहिए कि:
(i) इस उप-इकाई तथा अवयवण का अधिगम हेतु किस प्रकार के ज्ञान, कौशल आदि की आवश्यकता है अर्थात प्रारम्भिक व्यवहार कैसा होना चाहिए।
(ii) इस उप-इकाई तथा अवयवण के अधिगम के अर्जन के उपरान्त विद्यार्थी के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है अर्थात अन्तिम व्यवहार कैसा होना चाहिए।
(4) परीक्षण प्रश्नों के प्रकार में निर्णय लेना (Deciding about the Nature of the Item of the Test) – विषय-वस्तु के विश्लेषण तथा प्रारम्भिक तथा अन्तिम व्यवहार की जानकारी लेने के बाद निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, निर्णय लेना पड़ता है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या प्रायः ज्यादा ही रखी जाती है क्योंकि यह समस्या विशेष की खोज करना इसका उद्देश्य होता है। अतः ऐसे परीक्षण में निरवचनात्मक प्रश्नों की तुलना में लघु उत्तरीय तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बहुत ही विवश स्थितियों में विशेष रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में विद्यार्थियों की दृष्टियों तथा उनके मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न उतना प्रभावी कार्य नहीं कर सकते अतः निदानात्मक परीक्षण के अध्ययन में जिस प्रकार के ज्ञान, कौशल तथा समझ के व्यवहारणों की जरूरत होती है वे उनमें हैं या नहीं, इस बात का पता चल सके।
(5) परीक्षण लेने सम्बन्धी निर्णय लेना (Taking Decision about Test Administration) – निदानात्मक परीक्षण कैसे लिया जायेगा, इस बारे में भी आवश्यक निर्णय निदानात्मक परीक्षण के निर्माण सम्बन्धी नियोजन स्तर पर ही ले लिया जाना चाहिए, जैसे – परीक्षा के लिए समय-सीमा (time limit) क्या रहेगी, परीक्षा देने से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश विद्यार्थियों को क्या दिये जायेंगे, परीक्षण प्रश्नों के अंकन तथा परीक्षण परिणामों की व्याख्या करने में क्या प्रक्रिया अपनानी होगी इत्यादि।
(ङ) निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना
(Construction of the Diagnostic Test)
इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें ध्यान रखी जाती हैं –
(1) नियोजन स्तर पर जो निर्णय लिये गये हैं उनके ध्यान में रखते हुए परीक्षण के निर्माण हेतु उपर प्रश्नों का चयन कर लिया जाता है। यह चयन मुख्यतः निम्नलिखित तीन बातों पर केन्द्रित होता है –
(i) उप-इकाई या अवयवण विशेष की विषय-वस्तु की प्रकृति।
(ii) उप-इकाई या अवयवण विशेष के अधिगम हेतु आवश्यक प्रारम्भिक व्यवहार (पूर्वज्ञान, कौशल आदि के सन्दर्भ में)।
(iii) उप-इकाई या अवयवण विशेष के अधिगम के पश्चात् विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार (अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग आदि के सन्दर्भ में)।
(2) उपर्युक्त तीन बातों का ध्यान में रखते हुए लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्नपत्र में आवश्यक निर्देश देने एवं समय अवधि आदि दिये जाने की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। प्रश्नों की उत्तर-कुंजी (Scoring Key) तथा आदर्श उत्तरों (Model Answers) का निर्माण उत्तरों की यथोचित व्याख्या और उनसे सही उत्तर प्राप्त करने हेतु भी यहाँ किया जाना चाहिए।
(3) इस प्रश्नपत्र/परीक्षण द्वारा अब विद्यार्थियों के एक समूह विशेष की परीक्षा लेकर इसकी उपयोगिता की जाँच करने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस जाँच के आधार पर इसमें आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं और फिर इसे एक निदानात्मक परीक्षण के रूप में अग्रे प्रस्तुत करने के बारे में सोचा जा सकता है।
(ङ) निदानात्मक परीक्षण लेना और उसकी व्याख्या करना
(Administration and Interpretation of the Diagnostic Tests)
इस प्रकार से बनाये गये निदानात्मक परीक्षण से अब किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह विशेष/कक्षा की परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा लेते समय परीक्षा से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देश विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझा दिये जायेंगे। जब वे अपना कार्य समाप्त कर लेंगे तो उनके उत्तर-पत्रों को प्रश्नपत्र सहित इकट्ठा कर लिया जायेगा। यहाँ अब उनके उत्तरों के अंकन के लिए उत्तर-कुंजी तथा आदर्श हल की सहायता ली जा सकती है और उसके आधार पर विषयविशेष के विशेषज्ञ उन उत्तरों का विश्लेषण करते हैं। उनका विश्लेषण कर वे यह निर्णय लिया जा सकता है कि उनके द्वारा दी जाने वाली गलतियाँ, अनुभव की जाने वाली कठिनाइयाँ तथा कमियों की वास्तविक प्राप्त क्या है? इन्हीं कमियों तथा कठिनाइयों का यथार्थ निदान इस आधार के उपरान्त ही किया जाता है। इसी दृष्टिकोण से परीक्षा से प्राप्त उत्तरों की सही दृष्टि से व्याख्या करके विद्यार्थियों के अधिगम तथा कठिनाइयों के अनुसार उन्हें उपयुक्त सहायता देने की दिशा में अग्रसर होना बहुत जरूरी होता है।
|
|||||