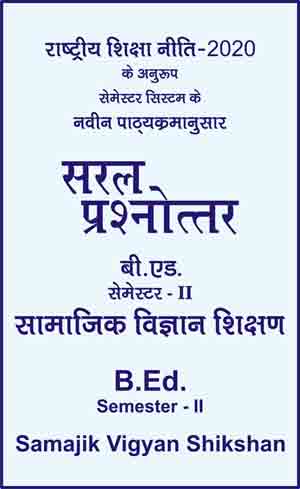|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का क्या प्रयोजन है? इसकी प्रमुख प्रविधियों का वर्णन कीजिए।
अथवा
सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को बताते हुए इसकी प्रमुख प्रविधियों एवं उपकरणों को स्पष्ट कीजिए।
सामान्यतः लघु उत्तरीय प्रश्न
- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के प्रयोजनों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रविधियों तथा उपकरणों का विवेचन कीजिए।
- सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
उत्तर -
सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन का प्रयोजन/उद्देश्य
(Purpose of Evaluation in Social Studies)
मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह तय करती है कि छात्र ने एक नियत अवधि में कितना कुछ सीखा तथा कितनी प्रगति की। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण की समस्त क्रियाएं मूल्यहीन बन सकती हैं, क्योंकि मूल्यांकन द्वारा समस्याओं, असफलताओं, कमजोरियों आदि का यथोचित रूप से निर्धारण हो जाता है जिससे परिणामस्वरूप छात्र भविष्य को लिये सतर्क हो जाते हैं।
सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन के प्रयोजन/उद्देश्य के निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
-
इस बात की जानकारी करना कि शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक ज्ञान बालकों ने किस सीमा तक प्राप्त किया है।
-
बालक के व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तनों की जानकारी हेतु।
-
शिक्षण में वांछित सुधार लाने हेतु।
-
शिक्षण के विभिन्न अंगों (बालकों) की कमियों या त्रुटियों की जानकारी तथा निदान हेतु आधार प्राप्त करने हेतु।
-
छात्रों को अच्छे ढंग से सीखने की प्रेरणा देने हेतु।
-
छात्रों को सीखने या परिश्रम करने प्रति प्रेरित करने के लिए।
-
शिक्षण हेतु उद्देश्यों को स्पष्ट करने तथा उनकी उपयोगिता को स्पष्ट करने हेतु।
-
छात्रों को उचित शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देश प्रदान करने में सहायता देने हेतु।
-
छात्रों की योग्यताओं, मानसिकताओं, रुचियों, कुशलताओं एवं निहित क्षमताओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु।
-
शिक्षक-शिक्षार्थी विधि, पाठ्यवस्तु, पुस्तकें और अन्य शैक्षिक साधनों की उपयुक्तता को परखने हेतु।
-
शिक्षण पाठ्य-वस्तु, पाठ्यक्रम आदि में सुधार लाने के उद्देश्य से।
-
परिवर्तन आवश्यकताओं के अनुसार सफलता को मापने के आधार पर पाठ्यक्रम व शैक्षिक कार्यों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से।
-
बालक की भावी उपलब्धियों के सम्बन्ध में भविष्यवाणी अथवा अनुमान लगाने हेतु।
-
बालकों का वर्गीकरण व उनकी उन्नति के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने हेतु।
-
शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करके बालकों की उपलब्धियों को परखने हेतु।
-
बालकों के व्यवहार सम्बन्धी परिवर्तन, निर्माण और कठिनाइयों की पहचान करने हेतु।
सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन की प्रविधियाँ एवं उपकरण
(Techniques and Tools of Evaluation in Social Studies)
सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन की प्रविधियों से तात्पर्य उन प्रविधियों से है जिनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का पता लगाया जाता है। इन प्रविधियों द्वारा शिक्षण के तीनों – ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाता है। ये प्रविधियाँ प्रमुखतः निम्नलिखित प्रकार की होती हैं –
(1) संख्यात्मक प्रविधियाँ (Quantitative Techniques) – ये निम्नलिखित हैं –
1. मौखिक परीक्षा (Verbal Test) – इस परीक्षा में मौखिक प्रश्न, वाद-विवाद, प्रतिस्पर्धात्मक-वर्णन, नाट्य आदि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग छात्रों में प्रत्यास्मरण, चिन्तन विश्लेषण आदि योग्यताओं के मापन के लिए किया जाता है।
2. लिखित परीक्षा (Written Test) – इस परीक्षा में छात्र लिखित प्रश्नों के उत्तर भी लिखित रूप में देते हैं। इन परीक्षाओं का उपयोग छात्रों की स्मरण-शक्ति, विश्लेषण, भाषा आदि के मापन करने के लिए किया जाता है। ये परीक्षाएँ भी दो प्रकार की होती हैं –
(i) निबन्धात्मक परीक्षाएँ (Essay Type Test),
(ii) वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ (Objective Type Test)।
इन परीक्षाओं का प्रयोग विद्यालयों के प्रत्येक विषय के परीक्षण के लिए किया जा सकता है।
3. प्रयोगात्मक परीक्षा (Practical Test) – प्रयोगात्मक परीक्षा मौखिक, लिखित तथा क्रियात्मक तीनों प्रकार से ली जा सकती है। इसका प्रयोग-प्रयोगात्मक विषयों जैसे- विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीव), मनोविज्ञान, भूगोल, गृह विज्ञान, हस्तशिल्प, ड्राइंग, संगीत, कृषि इत्यादि में किया जाता है। इसमें छात्र अपने विषय से सम्बन्धित कोई क्रियाकलाप, मौखिक या लिखित कार्य परीक्षण के समक्ष प्रस्तुत करता है।
(2) गुणात्मक प्रविधियाँ (Qualitative Techniques) – ये प्रविधियाँ सामान्यतः निम्न प्रकार की होती हैं –
1. निरीक्षण (Observation) – इसका प्रयोग मुख्य रूप से छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इससे उनके वास्तविक व्यवहार का पता चलता है। बड़े छात्र स्वयं अपना आत्म-निरीक्षण का विकास करते हैं। निरीक्षण के द्वारा बालकों के सामाजिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास के बारे में पता लगाया जाता है। यदि निरीक्षण सावधानी से किया जाये तो छात्रों के वास्तविक व्यवहार का सन्तोषजनक पता लगाया जा सकता है।
2. साक्षात्कार (Interview) – साक्षात्कार द्वारा छात्रों की भाषा-शैली, मनोवृत्ति, विश्लेषण शक्ति, रुचि, तकनिकीता एवं मनोबल का पता चलता है।
3. चेक सूची (Check List) – इसमें कुछ कथन छात्रों को दिये जाते हैं। इन प्रश्नों के सम्बन्ध में छात्रों को हाँ अथवा नहीं में उत्तर अंकित करना पड़ता है। इस प्रकार के कथन तैयार करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य होने चाहिए। चेक लिस्ट (मतपत्र) का प्रयोग छात्रों की अनुभूतियों एवं भावनाओं तक के मापन के लिए किया जाता है।
4. प्रश्नावली (Questionnaire) – प्रश्नावली में छात्र प्रश्नों की संख्या की दृष्टिकोण के प्रति अनुरूप व्यवहार करते हैं। इससे छात्रों से अनेक प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।
5. रेटिंग स्केल (Rating Scale) – रेटिंग स्केल में कुछ कथन दिये होते हैं। उनका तीन, पाँच, सात बिन्दुओं तक समान्य निर्णय करना होता है। इसका प्रयोग उच्च कक्षा के छात्रों के लिए किया जाता है। रेटिंग स्केल के कथन स्पष्ट होने चाहिए।
6. अभिलेख (Records) – अभिलेख भी मूल्यांकन की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें छात्रों के महत्वपूर्ण व्यवहार एवं जटिल परिस्थितियाँ आदि का वर्णन होता है।
7. संचयी अभिलेख (Cumulative Records) – इसमें विद्यालय के प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में जानकारी को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है। इसके अन्तर्गत छात्रों की डायरीयाँ आदि आती हैं।
|
|||||