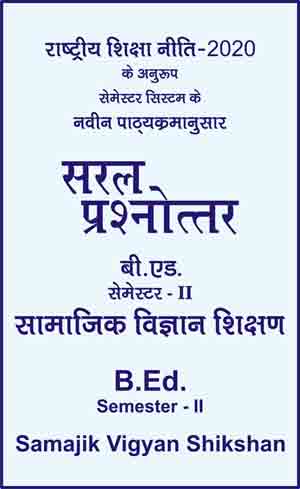|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- श्रव्य-दृश्य (सामाजिक विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री) सामग्री की आवश्यकता तथा महत्त्व का विवेचन कीजिए।
उत्तर -
श्रव्य-दृश्य सामग्री की आवश्यकता तथा महत्व पर जोर देते हुए कोठारी आयोग ने कहा है, ‘इन्हींसिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक विद्यालय को शिक्षण सहायक-सामग्री प्रदान करना आवश्यक है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे देश में शैक्षिक क्रांति उत्पन्न होगी।।’
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1९८६) ने भी शिक्षण-अभिगम के ज्यादा प्रभावशाली, स्पष्ट एवं वास्तविक बनाने के लिए शिक्षण व सहायक सामग्री विशेषकर स्वनिर्मित सामग्री के प्रयोग पर जोर दिया है।
निम्नलिखित बिन्दुओं से श्रव्य-दृश्य सामग्री की आवश्यकता, महत्त्व एवं उपयोगिता को स्पष्ट किया गया है :
1. स्पष्टता - निम्न-स्पष्ट बिन्दुओं तथा अवधारणाओं को स्पष्ट करने में श्रव्य-दृश्य साधनों की अच्छी उपयोगिता एवं महत्त्व सिद्ध होता है।
2. ध्यान तथा रुचि - श्रव्य-दृश्य साधन विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते तथा उनमें पाठ के प्रति रुचि पैदा करके अध्ययन में सहायक होते हैं।
3. शिक्षण-कृत्यों पर आधारित - श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोग से अध्यापक के लिए शिक्षण-सूत्रों को अनुकरणीय बनाना आसान हो जाता है। इससे वह जटिल की ओर, मूर्ख से अमूर्ख की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर, रुचि से सीखना इत्यादि।
4. अनुप्रेरक अभिगमों - श्रव्य-दृश्य साधन हमारी संवेदनाओं के अनुप्रेरक अभिकर्ता हैं। यह अधिगम में रुचि को उत्पन्न करते हैं।
5. ज्ञानेन्द्रियों का अधिकतम प्रयोग - ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। श्रव्य-दृश्य साधन ज्ञानेन्द्रियों के अधिक से अधिक प्रयोग में सहायता प्रदान करते हैं तथा इस तरह से विद्यार्थियों के लिए ज्ञान-प्राप्ति को सुगम बनाते हैं।
जोसेफ जे. वेबर के अनुसार हमारी 40% धारणाएँ दृश्य अनुभवों पर, 25% श्रव्य अनुभवों पर 17% स्पर्श, 3% स्वाद तथा गंधों पर और 15% विविध इन्द्रियों के अनुभवों पर आधारित होती हैं।
6. ज्ञान को स्थिर करना तथा प्रत्यारोपण करना - श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग विद्यार्थियों को सहायता में मदद करता है इस तरह उन्हें विचारों के प्रत्यारोपण में सहूलियत प्राप्त होती है। विचारों के सहायता से ज्ञान को स्थिरता प्राप्त होती है। अध्ययन सहायक तथा प्रत्यारोपण से प्रेरित होता है।
7. समय और श्रम की बचत - श्रव्य-दृश्य साधन समय एवं श्रम की बचत में मदद करते हैं। इनका प्रयोग करने से अनेक मुश्किल अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। इस तरह से विद्यार्थियों तथा अध्यापक के समय एवं श्रम की काफी बचत होती है।
8. व्यैक्तिक भिन्नताओं के अनुकूल - विद्यार्थियों में विस्तृत व्यैक्तिक भिन्नताएँ होती हैं, बहुत से विद्यार्थी श्रवण से ज्यादा सीखते हैं, अनेकोंने के प्रदर्शन से मदद की जाती है तो अनेक करने से सीखते हैं। विभिन्न किस्म के श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक साबित होता है।
9. सामाजिक दृष्टिकोण का विकास - श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग विद्यार्थियों में होता है। सुनने हुए वस्तुओं पर सहमत होने के बजाय वे श्रव्य-दृश्य साधनों की सहायता से वस्तुओं को देखकर तथा उन्हें प्रकट करते हैं। वास्तविक अवलोकनों तथा साधनों की सहायता से वस्तुओं को देखकर वे तथा उन्हें प्रकट करते हैं। वास्तविक अवलोकनों तथा प्रयोगों द्वारा उनमें सामाजिकरण की भावना का विकास होता है।
10. विध्यार्थी को लगाव - श्रव्य-दृश्य साधन क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ, में विद्यार्थियों उत्पन्न करते हैं। जब विद्यार्थियों को कुछ करने की मदद से पढ़ाया जाता है वे नवीनता का अनुभव करते हैं। विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है तथा शिक्षण-अधिगम को अभिप्रेरित करती है।
11. विचारों के संगठन में सहायक - जब इस सामग्री का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थी को अपने विचार स्मरण करता अथवा उन्हें अन्य विचारों से संगठित करता सुगम हो जाता है। इनकी मदद से अभिव्यक्ति की योग्याता का विकास होता है।
12. प्रत्यक्ष अनुभवों का विकल्प - विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय-सामग्री के लिए प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना प्रयास के योग्य नहीं है। इस प्रकार से प्रत्यक्ष अनुभवों के प्रतिरूपण के रूप में चार्ट, स्लाइड आदि के अनेक तरीके से किया जा सकता है।
13. नवीन अनुभव तथा नवीन ऊर्जा की पूर्ति - जो भी ज्ञान विद्यार्थियों ने अपने पूर्व अनुभवों से प्राप्त किया होता है वह उन्हें अधिगम के अनुकूल दोहराया जाता है, लेकिन यह चित्र, चार्ट आदि गतिविधियों में उनके अनुभवों की सीमा को विस्तृत करता है। विवेचन, तुलना, सामान्यीकरण तथा संकल्पनों की योग्याता अनुभवों के विस्तृत आधार पर निर्भर करती है।
14. सक्रियता को प्रोत्साहन - श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोग से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया उत्तेजित एवं सक्रिय बन जाती है। श्रव्य-दृश्य साधनों के प्रयोगों कक्षा के निष्क्रिय वातावरण को सक्रिय एवं सजीव बना देता है। इनका प्रयोग किया जाता है तो विद्यार्थी बोलते, हस्तें प्रश्न पूछते, टिप्पणी करते आदि में स्वतन्त्रता महसूस करते हैं।
15. अधिगम के स्थानांतरण में सहायक - कक्षा में सीखा गया ज्ञान अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने से स्थायी होता है। इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। सहायक सामग्री से यह स्थानांतरण ज्यादा होता है।
16. अंतर्राष्ट्रीय बोध का विकास - श्रव्य-दृश्य साधनों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय बोध के विकास में मदद करता है। चलचित्रों, स्लाइडों, रेडियों, दूरदर्शन, चित्रों आदि की मदद से दूसरे देशों की सभ्यता एवं संस्कृति कक्षा में ऐसे उजागर हो जाती हैं जैसे हमारे अपने राष्ट्र की हो। यह अनुभव विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों तथा विश्व के विविध राष्ट्रों की जीवन-पद्धतियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी विकसित करती है। इस तरह से ये साधन अंतर्राष्ट्रीय बोध के विकास में मददगार सिद्ध होते हैं।
17. विद्यार्थियों के शब्द ज्ञान एवं वृद्धि करने में सहायक - अनुसंधानात्मक सामग्री की मदद से विद्यार्थी नये शब्द सीखते हैं। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करके जब विद्यार्थी अन्य व्यक्तियों के सम्पर्क में आते हैं तो वे उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं और काफी सारे नये अनुभव प्राप्त करते हैं।
18. अनुशासनहीनता पर नियंत्रण - श्रव्य-दृश्य साधनों का कक्षा में प्रयोग विद्यार्थियों को व्यस्त कर देता है। इससे खाली बैठे विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पैदा करने का मौका ही नहीं मिलता। नियमित रूप से मीनारों एवं मूल्य उद्धरण करते रहने से, श्रव्य-दृश्य साधन, यदि तर्कपूर्ण बुद्धिपरक चयन एवं प्रयोग किया जाये, विद्यार्थियों में गहन एवं लाभदायक शिक्षण ज्ञान एवं विकास करते हैं और इस तरह उनके अधिगम को अभिप्रेरित करते हैं। अतः स्पष्ट है कि अभिप्रेरित अधिगम का अर्थ है, क्रियात्मक अनुभूतियाँ, दृश प्रभाव, संवेद अनुभव और अंततः अधिक, परिपूर्ण ज्ञान।
सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातें विशेष ध्यान देना चाहिए :
1. सहायक सामग्री शिक्षण के स्तर को बदलने के लिए नहीं, अपितु इसके पूरक बनाने के लिए और इन्हें योजनाबद्ध करना चाहिए।
2. साधारण सहायक सामग्री अधिक उपयुक्त है - सहायक सामग्री जहाँ तक सम्भव हो सरल होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक जटिलता न हो विद्यार्थियों उसे पूरी प्रकार से सहज समझें।
3. सहायक सामग्री सजीव होनी चाहिए।
4. सहायक सामग्री कम से कम इतनी बड़ी अवश्य हो कि- कक्षा-कक्ष के सभी ओर से विद्यार्थी इसे भली-भाँति देख सकें।
5. सहायक सामग्री रोचक हो - सहायक सामग्री का रोचक होना बड़ा आवश्यक है तभी विद्यार्थियों में रोचकता तथा मनोयोग आएगा।
6. सहायक सामग्री प्रयोजनवादी तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए।
7. सहायक सामग्री विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर के अनुसार होनी चाहिए।
8. जहाँ सहायक सामग्री का उपयोग करना उपयुक्त है वहीं बहुत अधिक सामग्री का प्रयोग करना भी गलत है। ऐसा करने पर पाठ, गड़बड़ रहता है। सहायक सामग्री की प्रस्तुति ही बन्द हो जाएगी।
9. सहायक सामग्री का चुनाव जीवन्त हो।
10. विद्यार्थी सहायक सामग्री के प्रयोगों में सक्रिय रूप से भाग लें।
|
|||||