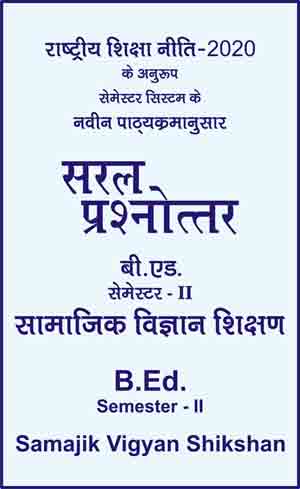|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 9 - पाठ्यक्रम : अर्थ, अवधारणा और
पाठ्यवर्ग के सिद्धान्त निर्माण और मौजूदा
सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की आलोचना
(Curriculum : Meaning, Concept and Principles
of Curriculum Construction, and Criticism
of Existing Social Science Curriculum)
प्रश्न- पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए। इसके निर्माण के लिये आप किन सिद्धान्तों का पालन करेंगे?
अथवा
सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के निर्माण के लिये कौन-कौन-से सिद्धान्त हैं?
अथवा
सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय आप किन सिद्धान्तों की ध्यान रखेंगे?
अथवा
सामाजिक विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।
संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न
- पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है ? स्पष्ट कीजिए।
- पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए।
- पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों को बताइए।
उत्तर-
पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Curriculum)
पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में “करीकुलम” (Curriculum) कहते हैं। लैटिन भाषा में ‘करीकुलम’ का अर्थ है - दौड़ का मैदान (Race Course)। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम छात्रों के लिए एक दौड़ का मैदान ही है। जिस प्रकार एक दौड़ने वाला दौड़ के मैदान को पार करके विजय प्राप्त कर सकता है उसी प्रकार छात्र भी पाठ्यक्रम रूपी दौड़ के मैदान को पार करके शिक्षा रूपी दौड़ जीत सकता है। अतः शाब्दिक अर्थ में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए विद्यार्थी शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है।
ध्यान देने की बात यह है कि संकुचित अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य केवल पाठ्य सूची (Syllabus) अथवा अध्ययन का कोर्स (Course of Study) है जिसमें अनुसार विभिन्न विषयों के तथ्यों की सीमाएँ निश्चित कर दी जाती हैं, परन्तु व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उन सभी अनुभवों (Experience) से है जिन्हें विद्यार्थी अपनी रुचियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न क्रियाओं तथा कक्षा के अन्दर अध्ययन कक्षा के बाहर इस समय प्राप्त करता रहता है।
पेन के अनुसार - “पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वे सभी परिस्थितियाँ आती हैं जिनका प्रधान संगठन और चयन बालकों के व्यक्तित्व के विकास लाने हेतु तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु विद्यालय करता है।”
"Curriculum consists of all the situations that the school may select and consciously organize for the purpose of developing the preasonality of its pupils and for making behaviour change in them."
–Payne
क्रो तथा क्रो के अनुसार - “पाठ्यक्रम में सीखने वाले या बालक के वह सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वह विद्यालय या उसके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित होने से जो अनुभव मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक व नैतिक रूप में विकसित होने में सहायता देता है।”
"Curriculum includes all the learner’s experience in or outside school that are included in a programme which has been devised to help his to develop, mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally."
–Crow and Crow
कनिंघम के अनुसार - “पाठ्यक्रम कलाकार (शिक्षक) के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने पदार्थ (शिष्य) को अपने आदर्श (उद्देश्य) के अनुसार अपने कलाालय (स्कूल) में ढाल सके।”
"The Curriculum is the tool in the hand of the artist (Teacher) to mould his material (Pupil) according to his ideal (Objective) in his studio (School)."
–Cunningham
पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्त
(Principles of Curriculum Construction)
पाठ्यक्रम सम्बन्धी विविध आधारों का पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धान्तों से घनिष्ट सम्बन्ध होता है। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धान्तों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है :
(1) रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धान्त (Principle of Utilizing Creative and Constructive Power) - पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक की रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर सके। मैक्डग महोदय का कथन है - “जो पाठ्यक्रम वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए।”
(2) बाल-केंद्रीयता का सिद्धान्त (Principle of Child-Centrism) - इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम बाल-केंद्रीय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि एवं आयु आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
(3) अनुभवों की पूर्णता का सिद्धान्त (Principle of the Totality of Experience) - पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मानव जाति के अनुभवों की सम्पूर्णता निहित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सैद्धान्तिक विषयों के साथ साथ व्यवहारिक तथा सहायक अनुभवों को विशेष स्थान मिलना चाहिए जिन्हें विभिन्न स्कूल में, खेल के मैदान में, कार्यशाला में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में तथा शिक्षकों के मार्गनिर्देशन सम्बन्धी अन्य शिक्षण स्थलों में प्राप्त किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी यही भावना थी। आयोग के अनुसार “माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य जब तक जीवन मूल्यों की प्राप्ति तथा नैतिक विकास नहीं हो जाता तब तक शिक्षा अधूरी है।” इसलिये शिक्षा में ऐसे अनुभवों को स्थान दिया जाना चाहिए जिनमें अनुभवों की सम्पूर्णता निहित होती है।”
(4) जीवन से सम्बन्धित होने का सिद्धान्त (Principle of Relation with Life) - इस सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन्हीं विषयों को स्थान देना चाहिए जिनका बालक के जीवन से सीधा सम्बन्ध हो। परम्परागत पाठ्यक्रम की आलोचना मात्र इसलिए हो रही है क्योंकि इसका बालकों के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है।
(5) स्वस्थ-आवश्यक आदतों को विकसित करने का सिद्धान्त (Principle of Achievement of Wholesome Behaviour Patterns) - पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालक दूसरों के साथ प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करना सीख जाये। क्रो और क्रो के अनुसार - “पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता कर सके।”
(6) खेल और कार्य की क्रियाओं के अन्तर का सिद्धान्त (Principle of Interrelation of Play and Works Activities) - पाठ्यक्रम तैयार करते समय ज्ञान प्राप्त करने की क्रियाओं को इतना रोचक बनाना का प्रयास करना चाहिए कि बालक ज्ञान को रोचक समझकर प्रभावशाली ढंग से ग्रहण कर ले। क्रो और क्रो के अनुसार - “जब लोग सीखने की प्रक्रिया को निर्देशित करते हैं उनका उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनायें कि खेल के दृष्टिकोण को स्थान प्राप्त हो।”
(7) संस्कृति तथा सभ्यता के ज्ञान का सिद्धान्त (Principle of the Knowledge of Culture and Civilization) - पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उन क्रियाओं, वस्तुओं तथा विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके द्वारा बालकों को अपनी संस्कृति तथा सभ्यता का ज्ञान हो जाये।
(8) विविधता का सिद्धान्त (Principle of Variety and Elasticity) - पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक बालकों को अपने भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सामना हो जाये तथा उनके साथ वे समायोजन कर सके। दूसरे शब्दों में, ऐसा हुआ पाठ ऐसा होना चाहिए जो बालकों को अनुकूलन तथा आवश्यकतानुसार पढ़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन के योग्य भी बना दे।
(9) अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धान्त (Principle of Training for Leisure) - वर्तमान युग में अवकाश काल का सदुपयोग करना एक शिक्षण समस्या है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम इतना व्यापक होना चाहिए कि जहाँ एक ओर वह बालकों को कार्य करने की प्रेरणा दे वहीं दूसरी ओर उनमें ऐसी शक्तियाँ भी उत्पन्न करे कि वे अपने अवकाश काल का सदुपयोग करना सीख जायें।
(10) जनतान्त्रिक भावना के विकास का सिद्धान्त (Principle of Developing Democratic Spirit) - भारत में जनतन्त्र के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालकों में जनतान्त्रिक भावनाओं एवं दृष्टिकोणों का विकास हो जाये।
|
|||||