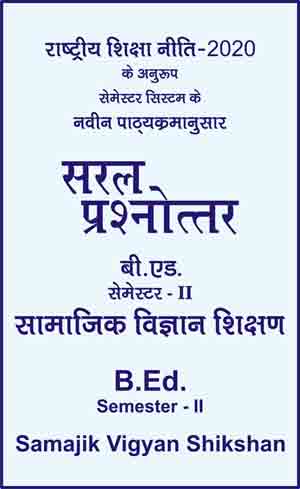|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान शिक्षण की स्रोत विधि से आप क्या समझते हैं ? इस विधि से क्या लाभ हैं ?
अथवा
स्रोत विधि क्या है ? इसके गुण तथा दोष बताइए।
अथवा
स्रोत विधि को स्पष्ट कीजिए और इसके गुण-दोष लिखिए। (कानपुर 2018)
समन्वित लघु उत्तरीय प्रश्न
- स्रोत विधि से क्या तात्पर्य है ? सन्दर्भ में बताइए।
- सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में स्रोतों के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए।
- स्रोत विधि का प्रयोग किस प्रकार करते हैं ? उल्लेख कीजिए।
- स्रोत विधि के गुण व दोष बताइए।
उत्तर -
स्रोत विधि
(Source Method)
ज्ञानार्जन क्रिया में प्रत्यक्ष अनुभव का बहुत महत्व है। हम किसी वस्तु को अपनी आँखों से देखकर या स्पर्श करके जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उतना ज्ञान उस वस्तु या कार्य के विषय में पढ़कर शायद ही प्राप्त करते हैं। किसी नदी, पहाड़, शिलालेख, ध्वज आदि के विषय में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से उक्त विषयों को सुनने अथवा पढ़ने की अपेक्षा उन्हें प्रत्यक्षतः रूप से जाकर देखने से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अतः किसी अन्य द्वारा बताये गये अनुभवों की अपेक्षा स्वयं प्राप्त अनुभव सदैव लाभप्रद एवं महत्वपूर्ण होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा ज्ञानार्जन की स्पष्ट विधि स्रोत विधि है। ये अनुभव प्रत्यक्ष एवं ज्ञान की सहायता प्रदान नहीं करते, क्योंकि अनेकों वस्तुओं एवं घटनाओं से साक्षात्कार सम्भव नहीं है। उदाहरणतः यदि हम अशोक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अशोक के समय का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि न तो उस समय की घटनाएँ घटेंगी और न हमें देखने को देंगी। अतः उस काल सम्बन्धी ज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा, परन्तु इस अप्रत्यक्ष ज्ञान को विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से प्रत्यक्ष बनाया जा सकता है। इन गुतियों में स्रोतों (Sources) का महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक के सिक्कों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, विभिन्न प्रकार मूर्तियाँ, दस्तावेज़ आदि के माध्यम से अशोक सम्बन्धी का मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्रोतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष का मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है।
मूल स्रोतों के विभिन्न रूप (Various Forms of Fundamental Sources) - मूल स्रोत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :
-
भौतिक वस्तुएँ (Material Object) जैसे - खण्डहर, प्रतिमाएँ (Statues), यन्त्र, शस्त्र, वस्त्र आदि।
-
भौतिक विवरण (Oral Accounts) जैसे - गीत, विवरण, दन्त कथाएँ, परम्पराएँ आदि।
-
लिखित या मुद्रित अभिलेख (Written or Printed Record) जैसे- जर्नल, हस्तलेख, डायरी, पत्र, सन्धियाँ, कानून, प्रतिवेदन आदि।
सामाजिक विज्ञान शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग
(Use of Sources in Teaching Social Science)
सामान्यतः स्रोतों का उपयोग इतिहास शिक्षण में होता है परन्तु सामाजिक अध्ययन भी अपनी विषय-वस्तु पर्याप्त मात्रा में इतिहास से प्राप्त करता है। इस कारण स्रोतों का प्रयोग, उसके शिक्षण के हेतु किया जा सकता है। जैसेकि हम जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन वर्तमान परिस्थितियों, घटनाओं आदि पर बल देता है। इन वर्तमान परिस्थितियों, घटनाओं आदि के शिक्षण में स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। जानकारी, तथ्यात्मक सामग्री, किसी विचारधारा विशेष की मूल बातें, विचार की व्याख्याओं के मूल रूप, विदेशी विचारों की भौतिक सामग्री, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाओं में दिये गये भाषण, पंचवर्षीय योजनाओं की मूल प्रतियाँ, पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख आदि सामग्रियाँ ऐसी हैं जिनका उपयोग वर्तमान समस्याओं, घटनाओं एवं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में किया जा सकता है।
सामान्यतः स्रोत विधि का निम्नलिखित दो प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है -
-
छात्रों को मौलिक स्रोतों का अध्ययन करने तथा उनके आधार पर अपना विचार व्यक्त करने के लिये कहा जा सकता है, तथा
-
पाठ्य-पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को विस्तृत या समृद्ध बनाने के लिये स्रोतों के अध्ययन के लिये छात्रों से कहा जा सकता है।
उपर्युक्त दोनों प्रकारों के अतिरिक्त मूल स्रोतों का प्रयोग प्रदर्शन कार्यों की किया जा सकता है।
अध्यापक इनका प्रयोग विवादास्पद तथ्यों की जाँच के लिये भी करवा सकता है। अध्यापक कक्षा-शिक्षण में स्रोतों को निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है -
अध्यापक प्रस्तुत प्रकारण से सम्बन्धित स्रोत के किसी सजीव अवसर की कक्षा में प्रस्तुति करे।
इसके पश्चात् वह स्रोतों के व्याख्याओं के सम्बन्ध में सन्दर्भ में बताये। इसके अतिरिक्त उन्हें छात्रों से पढ़ने को कहे और उन पर प्रश्न पूछे जिससे उनका विश्लेषण करके वे अपना निर्णय लेने में समर्थ हो सकें।
स्रोत विधि के गुण (Merits of Source Method) - स्रोत विधि के गुण अथवा लाभ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है -
-
यह विधि छात्रों को परीक्षण, तुलना या विश्लेषण करने का प्रशिक्षण प्रदान करती है।
-
इस विधि के द्वारा छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास होता है।
-
इस विधि के द्वारा छात्रों में प्रमाणिक बातों को पहचानने की क्षमता विकसित की जाती है।
-
यह विधि पाठ्य-पुस्तकों की विषय-वस्तु को समृद्ध बनाने में सहायता प्रदान करती है।
-
इस विधि के द्वारा छात्रों में प्रमाणों पर आधारित तथ्यों को ग्रहण करने की आदत का विकास किया जाता है।
स्रोत विधि के दोष अथवा सीमाएँ (Demerits/Limitations of Source Method) - स्रोत विधि के दोष अथवा सीमाएँ निम्नलिखित हैं -
-
इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं में नहीं किया जा सकता है।
-
इस विधि को अपनाने समय ऐसी स्रोत-पुस्तकों का अभाव प्रतीत होता है जिसमें सभी स्रोतों का संकलन हो और जो माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिये उपयुक्त हो।
-
विभिन्न विधाओं की विदेशी भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण छात्र इनका उचित उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें विदेशी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है।
प्राचीन काल के स्रोत संस्कृत, पाली, प्राकृत, मध्यकालीन स्रोत उर्दू, अरबी, फारसी तथा आधुनिक काल स्रोत अंग्रेज़ी, हिन्दी व विभिन्न भारतीय भाषाओं में पाये जाते हैं। आज का छात्र भाषा की कठिनाई के कारण इन स्रोतों का उपयोग कुशलता से नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं होता है। अतः छात्रों की सुविधा के लिये सभी स्रोतों का जनसाधारण की भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए।
|
|||||