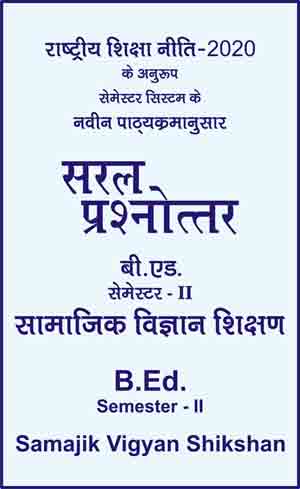|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी के अन्तर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए।
उत्तर -
भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी के अन्तर्गत पाँच शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। ये उद्देश्य इस प्रकार हैं -
-
आग्रण (Receiving),
-
प्रतीक्रिया करना (Responding),
-
मूल्यन (Valuing),
-
व्यवस्थापन (Organization),
-
चरित्रीकरण (Characterization)
इन उद्देश्यों के सम्बन्ध में डॉ० मेघा मार्था ने लिखा है - "शैक्षिक उद्देश्यों को भावात्मक क्षेत्र की टैक्सोनॉमी मुख्यतः बालकों के व्यवहार के भावात्मक पक्षों, रुचियों, मूल्यों, सन्दर्भों तथा अभिवृत्तियों से सम्बन्धित होती है। जब बालक के अन्तर्गत क्रिया नहीं होती है अथवा उसे अधिगम द्वारा सीखे गये व्यवहारों के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिकोण होता है तो यह परिवर्तन उसमें भावात्मक पक्ष से सम्बन्धित माने जाते हैं। मान्यताएँ, मूल्य, रुचि तथा सन्दर्भ सभी हमारे व्यक्तित्व की कसौटियाँ होते हैं तथा शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार को जन्म देते हैं।"
"भावात्मक पक्ष की टैक्सोनॉमी के अन्तर्गत उक्त शैक्षिक उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है -
(1) आग्रण (Receiving or Attending) - यह भावात्मक स्तर से सम्बन्धित सर्वप्रथम उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि यह भावात्मक विकास का प्रथम सोपान है। भावात्मक विकास की दृष्टि से इस उद्देश्य को सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य माना जाता है। इस उद्देश्य के अन्तर्गत अधिगम करने वाला शिक्षार्थी किसी क्रिया की रूपरेखा में अपनी उपस्थिति प्रदर्शित करता है अथवा जो कुछ भी वह सुनता है अथवा देखता है उसकी क्रिया में अपना ध्यान लगाता है। उसके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न व्यवहार ध्यान अथवा उपस्थिति की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं।
सन्दर्भ में, आग्रण की योग्यता का सम्बन्ध व्यक्ति की संवेदनशीलता से होता है। यह संवेदनशीलता तब उत्पन्न होती है जब कोई उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है अथवा किसी क्रिया को होते हुए देखा जाता है। इसी संवेदनशीलता को आग्रण के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। क्रियाओं की आग्रण की प्रक्रिया निम्नलिखित स्तरों से होकर गुजरती है -
(i) क्रिया की जागरूकता (Awareness of the Phenomena),
(ii) क्रिया प्राप्ति की इच्छा (Willingness to Receive Phenomena),
(iii) क्रिया का नियंत्रित ध्यान (Controlled of Selected Attention)
(2) अनुक्रिया (Responding) - यह भावात्मक विकास से सम्बन्धित द्वितीय सोपान होता है। इस स्तर का सम्बन्ध उत्तर-अनुक्रिया या प्रतीक्रिया से होता है। प्रथम स्तर के अन्तर्गत बालक की संवेदनशीलता का ही परिव्यय प्राप्त होता है। इस स्तर पर बालक अपना ध्यान अथवा उपस्थिति से सम्बन्ध व्यवहारों को प्रदर्शित करता है जबकि दूसरे स्तर पर वह आग्रण से आगे बढ़ जाता है। उद्दीपन अथवा क्रिया की प्रतीक्रिया में सहभागिता के व्यवहार स्तर पर प्रतीक्रिया करते हैं। वह सक्रिय होकर क्रिया में भाग लेने लगता है तथा इन क्रियाओं के प्रति अपनी अनुक्रिया भी व्यक्त करने लगता है। यह अनुक्रिया बाह्य क्रियाओं अथवा आन्तरिक उद्दीपन की भी हो सकती है।
अनुक्रिया के समान अनुक्रिया की भी तीन स्तर होते हैं। प्रथम स्तर पर वह अनुक्रिया हेतु सहमत होता है, दूसरे स्तर पर अनुक्रिया की इच्छा करता है तथा तीसरे स्तर पर अनुक्रिया में सतत् व्यवहार करता है।
(3) अनुकूलन (Valuing) - यह भावात्मक विकास से सम्बन्धित तीसरा स्तर होता है जिसका व्यक्तिगत जीवन में विशेष महत्व होता है। इसके अन्तर्गत व्यक्ति के उन मूल्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होती है जिन्हें उसके द्वारा महत्व दिया जाता है अथवा जिन मूल्यों में उसकी आस्था होती है। डॉ० मेघा मार्था के अनुसार - "तीसरे स्तर के इस उद्देश्य के अन्तर्गत बालकों के उन व्यवहारों को वर्गीकृत किया जाता है जिससे द्वारा वह किसी वस्तु, घटना, अथवा व्यवहार के गुण श्रेष्ठता अथवा मूल्य के सम्बन्ध में स्वयं ही भाव प्रकट करता है। वह सबसे पहले उन मूल्यों को स्वीकार करता है, फिर उन्हें प्राथमिकता प्रदान करता है तथा इसके बाद इन मूल्यों में अपना विश्वास प्रकट करता है।"
(4) व्यवस्थापन (Organization) - भावात्मक विकास से सम्बन्धित इस स्तर के अन्तर्गत उन मूल्यों पर विचार किया जाता है जो पहले से ही निश्चित होते हैं अथवा जिनमें व्यक्ति की आस्था होती है। विचार करने के उपरान्त इन मूल्यों को व्यवस्थित किया जाता है जिसका जिन सिद्धान्तों में से होकर गुजरना पड़ता है। विशेष सोपान मूल्यों की अवधारणाओं को समझकर तथा विभिन्न मूल्यों का समुचित विश्लेषण करके यह ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न मूल्यों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध क्या है तथा उनके मध्य कौन-कौनसी भिन्नताएँ हैं? यह ज्ञान ग्रहण करने के उपरान्त ही विभिन्न मूल्यों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यह व्यवस्था से सम्बन्धित दूसरा सोपान होता है। मूल्यांकन की व्यवस्था के नाम से सम्बोधित किया जाता है।
(5) चरित्रीकरण (Characterization) - यह भावात्मक पक्ष का अन्तिम तथा सर्वोच्च स्तर होता है। इस स्तर पर किसी भी व्यक्ति में निहित मूल्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस स्तर पर विभिन्न मूल्य व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं तथा विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से इन मूल्यों की विविधता का दर्शन होता है। व्यक्ति की सोच में विभिन्न मूल्यों का गहन सम्बन्ध एवं समन्वय होती है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि इस व्यवहारिक मूल्यों का व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्देश्यों के माध्यम से बालक के भावात्मक विकास करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यक्ति के चरित्र, मूल्य, अभिवृत्ति आदि के विकास की दृष्टि से इनका अत्यधिक महत्व होता है। डॉ० मार्था के शब्दों में - "शिक्षा में व्यवहार के भावात्मक पक्ष का विकास करने के लिए इन सभी स्तरों से क्रमिक ढंग से गुजरना पड़ता है। इसके द्वारा बालक में रुचियों (Interest), गुणगान (Appreciation), अभिवृत्तियाँ एवं मूल्य (Attitudes and Values) में परिवर्तन होता है और जो उसके समान्यीकरण में अत्यन्त सहायक होते हैं। इस प्रकार से व्यवहार के ये भावात्मक पक्ष उसके व्यक्तित्व निर्माण में भी काफी सहायक होते हैं। इसके माध्यम से बालक के व्यवहार के सम्बन्ध में सरलता से भविष्यवाणी की जा सकती है।"
|
|||||