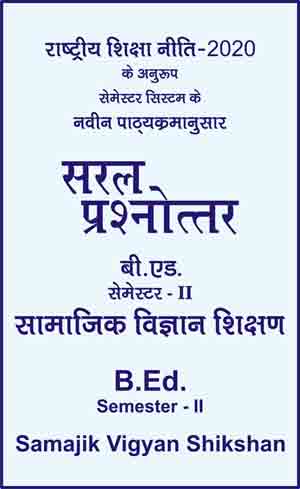|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 सामाजिक विज्ञान शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 4 - माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान
शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य (ब्लूम और संशोधित ब्लूम
टैक्सोनॉमी पर आधारित)
[Aims and Objectives of Pedagogy of Social Science
at Secondary Level (based on Bloom and revised Bloom’s Taxonomy)]
प्रश्न- ज्ञानात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित ब्लूम के समस्त उद्देश्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
अथवा
ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए एवं उचित उदाहरणों के आधार पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में इसकी उपयोगिता बताइए।
उत्तर -
ब्लूम टैक्सोनॉमी के अन्तर्गत 06 शैक्षिक उद्देश्यों को निरूपित किया गया है जो निम्न प्रकार से हैं -
(1) ज्ञान (Knowledge) - यह ज्ञानात्मक क्षेत्र अथवा बौद्धिक योग्यताओं के विकास से सम्बन्धित सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित शेष उद्देश्यों की प्राप्ति इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्भव हो पाती है। दूसरे शब्दों में, जब तक ज्ञान योग्यता का विकास नहीं किया जाता है, तब तक कोई अन्य ज्ञानात्मक, बौद्धिक योग्यताओं का विकास सम्भव नहीं किया जाता। इस योग्यता का सम्बन्ध बालकों की स्मृति स्तर से होता है। विज्ञान एवं विषयों को समझने के लिए बालकों की प्रत्याभरण शक्ति तथा अभिसरण शक्ति का विकास आवश्यक होता है। इसके लिए ऐसी शिक्षण परिस्थितियों का सृजन किया जाता है जिसके माध्यम से बालकों की स्मरण-शक्ति तथा पहचान-शक्ति का विकास हो सके।
बालकों के स्मृति स्तर से सम्बन्धित इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के अधिगम अनुभव अथवा पाठ्य-वस्तु को प्रमुखता किया जाता है। तथ्य, शब्द, नियम, सिद्धान्त, परिभाषाएं आदि से सम्बन्धित हो। उदाहरण के लिए, यदि बालक गुरुत्वाकर्षण के नियम को स्मरण करते उस नियम को व्याख्या सुना देते हैं, सम्भावन के सूत्र को याद करके परीक्षा में उसका उसका प्रत्याभरण कर लेते हैं; किसी विज्ञान की परिभाषा को स्मृति के आधार पर सुना देते हैं अथवा कई विज्ञानों की परीक्षाओं में पूछे गये विज्ञान की परिभाषा को पहचान लेते हैं तो यह माना जाता है कि बालक ने ज्ञानात्मक स्तर से सम्बन्धित इस प्रथम योग्यता का विकास उनमें हो चुका है।
(2) बोध (Comprehension) - यह ज्ञानात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित दूसरा उद्देश्य है। उद्देश्य की प्राप्ति से पूर्व बालकों की प्रत्याभरण शक्ति तथा अभिसरण शक्ति का विकास होना आवश्यक होता है। इसके विकास से पूर्व इस योग्यता का विकास निरन्तर आवश्यक है। इसी प्रकार यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक बालक की इस योग्यता का विकास नहीं किया जायेगा तब तक प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण आदि योग्यताओं का विकास भी सम्भव नहीं हो सकेगा। यह योग्यता, बालक के अवबोधन स्तर से सम्बन्धित सबसे निम्न योग्यता के रूप में स्वीकार की जाती है। विश्लेषण, संश्लेषण आदि योग्यताओं को अवबोधन स्तर उच्चतम योग्यताओं की कोटि में स्वीकार किया जाता है।
बोध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्न प्रकार की पाठ्य-वस्तु को प्रमुखता किया जाता है –
-
तथ्य, शब्द, नियम आदि का उल्लेख करना।
-
दी गई पाठ्य-वस्तु का अनुबोध करना।
-
तथ्य, शब्द, नियम, सिद्धान्त आदि की व्याख्या करना।
-
आकृतियों, साक्षात्कार आदि से सम्बन्धित गुणतत्त्व करना।
-
नियम, सिद्धान्त आदि का प्रतिपादन करना।
(3) अनुप्रयोग (Application) – प्रथम दो उद्देश्यों अर्थात ज्ञान एवं बोध उद्देश्यों की प्राप्ति के उपरान्त ही इस उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव हो पाती है। यह उद्देश्य भी बालक के अवबोधन स्तर से सम्बन्धित होता है। दूसरे शब्दों में, इस उद्देश्य की प्राप्ति के माध्यम से बालकों की अवबोधन शक्ति का विकास होता है। जिस स्तर पर बालक प्रप्त ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तथा उस ज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का बोध भी उन्हें हो जाता है, उस स्तर विशेष उपयुक्त परिस्थितियों के माध्यम से नये परिस्थितियों के विकास होने पर यह माना जाता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हो चुकी है।
इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जिस पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है, उसका उल्लेख निम्न प्रकार से है –
-
किसी विधि अथवा सीखी गई प्रक्रिया का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में करना।
-
किसी भी सामाजीकरण की योग्यता का प्रयोग दी गई परिस्थिति में करना।
-
किसी नियम अथवा सिद्धान्त का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने की दक्षता प्राप्त करना।
(4) विश्लेषण (Analysis) – विश्लेषण की योग्यता का विकास करने के लिए ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग उद्देश्यों की प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब इन योग्यताओं का विकास छात्रों में हो जाता है, तभी विश्लेषण उद्देश्य की प्राप्ति सम्भव होती है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान के बोध एवं उसका प्रयोग करने की दक्षता के उपरान्त ही विश्लेषण उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जाता है। बोध एवं अनुप्रयोग की अपेक्षा यह उद्देश्य अधिक उच्च स्तर का होता है। परन्तु पुनः यह भी अत्यन्त विश्लेषण सम्बन्धी मानसिक योग्यताओं का विकास करने के लिए निम्न प्रकार की पाठ्य-वस्तु को प्रमुख किया जाता है –
-
तथ्यों, प्रयोगों, सिद्धान्तों आदि के तत्वों में विश्लेषण करना।
-
व्यावहारिक सिद्धान्तों का विश्लेषण करना।
-
तथ्य, उदाहरण आदि में निहित पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण करना।
(5) संश्लेषण (Synthesis) – विश्लेषण उद्देश्य की प्राप्ति के उपरान्त इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जाता है। विश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत संश्लेषण, नवीन तत्वों अथवा नव-निर्माण आदि योग्यताओं का विकास किया जाता है। यह उद्देश्य सर्वाधिक बौद्धिक स्तर से सम्बन्धित सृजनात्मक स्तर से सम्बन्धित होता है। मौलिकता अथवा विविधतापूर्ण तत्वों को एकत्र प्रस्तुत करना इस उद्देश्य का प्रमुख विशेषता होती है। विविधताएं, तथ्यों आदि को संयोजन कर एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास इसी उद्देश्य के अन्तर्गत किया जाता है। तथ्यों की संश्लेषण प्रदान करने के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि ये समस्त वस्तुएं पाठ्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित हों।
इस योग्यता के विकास हेतु किसी नवीन योजना का निर्माण अथवा किसी समस्या का समाधान करने की योग्यताओं का विकास आवश्यक है। निम्न प्रकार की पाठ्य-वस्तु को इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया जाता है -
-
विभिन्न प्रकार का समपेक्षण करना।
-
विभिन्न तत्वों का संश्लेषण करते हुए किसी नवीन योजना को प्रस्तुत करना।
-
विभिन्न तत्वों के अनुसार सम्बन्धों की व्युत्पत्ति (Derivation) करना।
(6) मूल्यांकन (Evaluation) - यह ज्ञानात्मक पक्ष से सम्बन्धित सबसे अन्तिम उद्देश्य होता है। संश्लेषण के समान इस उद्देश्य का सम्बन्ध भी मूल्यांकन स्तर से होता है। अतः मौलिकता इस उद्देश्य की प्रमुख विशेषता होती है। इसे ज्ञानात्मक क्षेत्र से सम्बन्धित सर्वोच्च उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस योग्यता के विकास के लिए नियमों, तथ्यों, सिद्धान्तों आदि के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है। परन्तु निर्णय लेते समय आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक होता है। साथ ही यह ध्यान रखना होता है कि विषय-सामग्री के विषय में जो निर्णय लिया गया है वह आन्तरिक तथा बाह्य प्रमाणों के आधार पर लिया जाये। इस प्रकार किसी भी प्रकार की पाठ्य-वस्तु के सम्बन्ध में निर्णय लेने अथवा उसका मूल्य निर्धारण करने की दृष्टि से मूल्यांकन प्रक्रिया का विशेष महत्त्व है। मूल्यांकन के आधार पर लिया जाने वाला निर्णय गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही दृष्टियों से लिया जा सकता है। इस योग्यता का विकास करने हेतु आन्तरिक एवं बाह्य प्रमाणों से सम्बन्धित पाठ्य-वस्तु को आधार बनाना जाता है। ये प्रमाण जितने अधिक शुद्ध एवं विस्तृत होंगे मूल्यांकन के आधार पर लिया गया निर्णय भी उतना ही अधिक विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ सिद्ध होगा।
ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से निम्नलिखित लाभ हैं -
-
इससे शिक्षण में जनबोधात्मक भावनाओं की स्थिति से बचा जा सकता है।
-
इससे शिक्षण की क्रियाएं सीमित तथा सुनिश्चित हो जाती हैं।
-
इससे अधिगम के अनुभवों की विशेषताओं की निर्धारण किया जा सकता है तथा मापन सम्भव होता है।
-
छात्र तथा शिक्षक दोनों विभिन्न प्रकार के व्यवहारों में अन्तर कर लेते हैं जिससे शिक्षण व्यूह रचना के चयन में आसानी होती है।
-
उद्देश्यों के निर्धारण से शिक्षण के लिए दुर्गम-श्य सामर्थ्य सामग्री के चयन में सुविधा होती है।
-
ज्ञानात्मक पक्ष को व्यवहारिक रूप से लिखने में छात्र किसी घटना या प्रकरण के सम्बन्ध में प्रत्याभरण या प्रतिमानिका कर सकते हैं। जैसे कि छात्र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का अध्ययन करते समय ब्रिटिश शासन से सम्बन्धित घटनाओं तथा सिद्धान्तों का प्रत्याभरण कर सकते हैं या किसी ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थान को देखकर प्रतिमानिका कर सकते हैं।
-
इससे छात्र किसी घटना जैसे- स्वतन्त्रता संग्राम, बाढ़, भूकम्प इत्यादि के कारणों की व्याख्या कर सकते हैं।
-
इससे छात्र किसी घटना एवं प्रकरण की सफलता के सम्बन्ध में तर्क कर सकते हैं तथा किसी अन्य प्रकरण से तुलना कर सकते हैं।
-
ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को लिखने में छात्र किसी घटना या प्रकरण जैसे स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित तथ्यों का विश्लेषण करने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं।
|
|||||