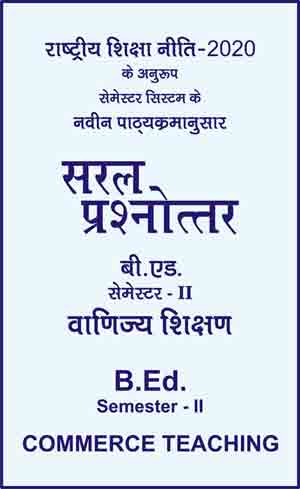|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं ? उपचारात्मक शिक्षण की कठिनाइयों के स्वरूप को स्पष्ट करते हुये इसके महत्व को समझाइये।1)
अथवा
उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ बताते हुये इसकी कठिनाइयों के स्वरूप व महत्व का वर्णन कीजिये।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है?
2. उपचारात्मक शिक्षण की कठिनाइयों के स्वरूप को बताइये।
3. उपचारात्मक शिक्षण के महत्व को बताइये।
4. उपचारात्मक शिक्षण क्या है? आप पिछड़े बालकों के लिये उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था किस प्रकार करेंगे?
उत्तर-
(Meaning of Remedial Teaching)
निदानात्मक परीक्षण द्वारा इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं।उपचारात्मक शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षक शिक्षक छात्रों की त्रुटियों के बारे में कितने विस्तार से जानकारी रखता है। त्रुटियों की प्रकृति देखकर व्यक्तिगत एवं सामूहिक त्रुटियों के उपचार की योजना बनाई जानी आवश्यक है। त्रुटियों का उपचार तत्परता एवं शीघ्रता से किया जाना आवश्यक होता है अन्यथा त्रुटियाँ स्थाई हो जाती हैं। उपचार करने के लिए छात्रों को विभिन्न वर्गों - मन्दबुद्धि, सामान्य बुद्धि एवं प्रखर बुद्धि आदि में विभक्त कर लिया जाता है। इन वर्गों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक त्रुटियों के उपचार की योजना भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न बनाई जाती है।उपचारात्मक कार्य का स्वरूप शिक्षक निश्चित करते हैं लेकिन यह कार्य तुरन्त होना आवश्यक होता है। पिछड़े बालकों का ध्यान किसी भी कार्य में बहुत कम लगता है तथा उनके विचारों में व्यापकता का अभाव रहता है। इस प्रकार के छात्रों के लिये व्यक्तिगत अनुदेशन काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ये बालक किसी आसान से कार्य को सफलतापूर्वक कर लेने पर यह अपेक्षा करते हैं कि अन्य लोग उनकी प्रशंसा करें। कक्षा के वर्ग बनाते समय ऐसे बालकों को एक ही वर्ग में रखा जाये। कक्षा में ऐसे बालकों की संख्या 20-25 से अधिक नहीं होनी चाहिये। ऐसे बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिये निम्नलिखित उपाय करने चाहिये -
(1) कमजोर छात्रों को कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए।
(2) कक्षा में विषय-वस्तु का विकास उदाहरणों एवं दृष्टान्तों द्वारा करना चाहिए।
(3) कक्षा में किसी भी विषय-वस्तु को पढ़ाते समय छात्रों का ध्यान विशेष रूप से उन प्रत्ययों, सिद्धान्तों एवं क्रियाओं आदि की ओर खींचा जाना चाहिए जिनमें छात्र त्रुटियाँ करते हैं।
(4) गणित एवं अन्य विषयों के आधारभूत सम्प्रत्ययों यथा—दशमलव, प्रतिशत, एकक नियम, वर्गमूल, समीकरण आदि को अत्यन्त सावधानी से पढ़ाना चाहिए।
(5) छात्रों को कक्षा में सोचने एवं हल करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने चाहिए।
(6) कमजोर छात्रों के लिए मॉडल, चार्ट एवं अन्य दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर प्रत्ययों आदि को स्पष्ट करना चाहिए।
(7) श्यामपट्ट पर लिखी हुयी सामग्री स्पष्ट, शुद्ध, व्यवस्थित एवं उपयोगी होनी चाहिए।
(8) प्रत्येक उपविषय के अभ्यास प्रश्न ऐसे हों जिनके उत्तरोंको छात्र स्वयं सोच सकें।
(9) छात्रों के लिखित कार्य में सुधार उनके सामने ही करना चाहिए।
(10) छात्रों को कक्षा के बाद भी आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत परामर्श देकर उन्हें त्रुटि सुधार एवं सीखने में सहायता देनी चाहिए।
इस प्रकार शिक्षक को शैक्षिक निदान के लिए निदानात्मक परीक्षण बनाना होता है और निदान के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण करना होता है।
(Forms of Difficulties for Remedial Teaching)
उपचारात्मक शिक्षण हेतु कठिनाइयों का स्वरूप निम्नलिखित हैं-
1. सामान्य कठिनाइयाँ और उनके विवरण हेतु उपाय (General Difficulties and Measures for their Removal) -
यदि छात्र शिक्षण को प्राप्त करने में किसी कठिनाई का अनुभव करते हैं तो इसे सामान्य कठिनाई कहते हैं। इसके निवारण हेतु निम्नलिखित उपाय हैं-
1. यदि सामान्य कठिनाई विषय से सम्बन्धित है तो उसके लिये शिक्षण अधिगम हेतु अतिरिक्त कक्षायें लगाकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।
2. शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने में श्रव्य दृश्य उपकरणों, अभ्यास कार्य एवं प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जा सकता है।
3. शिक्षण को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अधिगम की अन्य शिक्षण विधियों का उपयोग किया जा सकता है।
4. कक्षा में उदाहरणों का चयन विषयवस्तु की प्रकति एवं कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाये।
2. विशिष्ट कठिनाइयाँ और उनके निराकरण हेतु उपाय (Specific Difficulties and Measures for their Removal) - यदि किसी छात्र को शिक्षण अधिगम में व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो उन्हें विशिष्ट कठिनाइयाँ कहते हैं। जैसे किसी छात्र को विषय-क्षेत्र से सम्बन्धित ज्ञान की कमी हो तो छात्र इस ज्ञान की कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। छात्र अपनी अधिगम क्षमता के विकास के लिए अतिरिक्त शिक्षण की सहायता ले सकता है। इससे वह किसी विषय विशेष के मूल प्रत्ययों, प्रक्रियाओं, नियमों सिद्धान्तों आदि पर आधारित प्रश्न हल कर सकता है।
3. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित कठिनाइयाँ (Difficulties related with Physical and Mental Health) - यदि किसी विद्यार्थी को शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में कमी के कारण शिक्षण में कठिनाई आती है तो उसे ठीक करने के लिये उसका उपचार संही प्रकार से कराया जाता है।
4. अन्य कठिनाइयाँ और उनके निवारण हेतु उपाय (Other Difficulties and Measures for their Removal) - यदि विद्यार्थी को विषयगत कठिनाइयों जैसे समय पर विद्यालय का गृहकार्य न कर पाना, अपने विषय को किसी प्रकार से न दोहराना, स्वाध्याय न करना का सामना करना पड़ता है तो इनके निवारण हेतु विद्यार्थी को अभिभावक से सम्पर्क करके उनका सहयोग लिया जाता है एवं उनकी कमजोरियों के अनुरूप उनकी शिक्षा पर अतिरिक्त समय एवं ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाता है।
(Importance of Remedial Teaching).
शैक्षिक निदान का सम्बन्ध विद्यार्थियों की व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं की जाँच से ही नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं, कमजोरियों एवं कठिनाइयों के उपचार से भी है। विशिष्ट बालक कमजोरी एवं कठिनाई को दूर करने के लिए अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक अपनी योग्यतानुसार अधिकतम अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। यह अध्यापन प्रक्रिया निदानात्मक शिक्षण (Remedial Teaching) कहलाती है जिस प्रकार एक सफल चिकित्सक किसी रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व उसके रोग का निरीक्षण करता है तत्पश्चात् चिकित्सा आरम्भ करता है ठीक उसी प्रकार एक सफल अध्यापक भी सर्वप्रथम यह ज्ञात करता है कि बालक किन कारणों से विषय को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहा है वह इन कठिनाइयों का पता लगाता है।
निःसन्देह अध्यापक का यह कार्य चिकित्सक के कार्य से अत्यन्त जटिल है, क्योंकि किसी रोग का कारण जीवाणु हो सकता है लेकिन शिक्षा सम्बन्धी कारण इतने जटिल होते हैं कि उनका विश्लेषण करना कठिन हो जाता है जिसके लिये अध्यापक विभिन्न प्रकार की विधियों, परीक्षणों एवं उपकरणों का सहारा लेता है।
शिक्षण करते समय शिक्षक का कर्त्तव्य है कि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर छात्रों का निदान किया जाये ताकि शीघ्र ही उनकी कमजोरी का पता लगाकर उसका उपचार किया जाये
बालक की कमजोरी का इस प्रकार निदान कर चुकने के पश्चात् वह पुनः विविध उपचारिक विधियों की सहायता से उपचार करता है और बालक की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है।
|
|||||