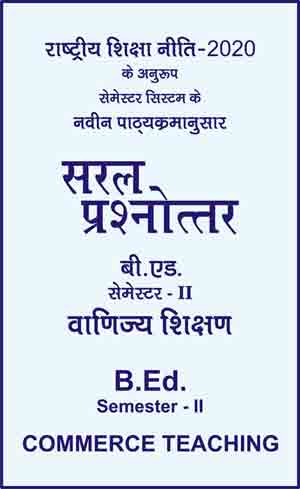|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 6 - निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण
(Diagnostic Testing and Remedial Teaching)
प्रश्न- निदानात्मक परीक्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी निर्माण प्रक्रिया का विवरण देते हुये व्याख्या कीजिये ।
अथवा
निदानात्मक परीक्षण का अर्थ बताते हुये इसकी निर्माण प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिये।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. निदानात्मक परीक्षण क्या है?
2. निदानात्मक परीक्षण की निर्माण प्रक्रिया बताइए।
3. निदानात्मक परीक्षण की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
(Meaning of Diagnostic Testing)
शाब्दिक रूप में निदानात्मक परीक्षण का अर्थ होता है एक ऐसा परीक्षण या मूल्यांकन कार्यक्रम जिसे किसी प्रकार के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे किसी-न-किसी प्रकार के निदानात्मक परीक्षण से अपनी अस्वस्थता सम्बन्धी समस्या के निवारण हेतु गुजरना ही पड़ेगा। आप भी जब बीमार होने पर किसी डॉक्टर या अस्पताल में गये होंगे तो आपकी बीमारी के कारणों की तलाश करने के लिए आपको किसी-न-किसी प्रकार के परीक्षण जैसे- रक्त परीक्षण, मूत्र व मल परीक्षण, रक्तचाप, ई.सी.जी., एक्स-रे चैकिंग आदि से गुजरने की सलाह दी गई होगी। इन सब परीक्षणों के जरिए ही डॉक्टर को यह पता चलता है कि आपकी बीमारी या अस्वस्थता की असली वजह क्या है और इसी आधार पर वह आगे बढ़कर आपको उस बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए औषधि तथा अन्य उपचारात्मक उपाय अपनाने की सलाह देता है। बिल्कुल ऐसी ही बात शिक्षण के क्षेत्र में प्रयुक्त निदानात्मक परीक्षणों और उपचारात्मक शिक्षण पर लागू होती है।
विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने हेतु उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए ही शिक्षा का आयोजन किया जाता है। शिक्षा देने के इन प्रयत्नों में कई बार इच्छित सफलता नहीं मिल पाती और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विद्यार्थी विशेष इन प्रयत्नों से ठीक तरह लाभान्वित नहीं हो पाता।परिणामस्वरूप वह या तो बार-बार फेल होता रहता है या फिर किसी-न-किसी प्रकार की व्यवहारजन्य समस्या का शिकार बन जाता है। हमें चिन्ता तब होती है जब उसकी यह समस्या काफी बढ़ जाती है और हमें यह सोचने को मजबूर कर देती है कि अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाये? इस स्थिति में ही उसके समस्यात्मक व्यवहार तथा शौक्षिक असफलता के पीछे हुए कारणों का निदान करने की आवश्यकता अनुभव होती है।
(Construction of a Diagnostic Test)
वैसे तो विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का निदान करने हेतु आज अपने देश तथा विदेशों में निर्मित बहुत-से प्रामाणिक निदानात्मक परीक्षण (Standardized Diagnostic Tests) उपलब्ध हैं परन्तु एक भौतिक विज्ञान अध्यापक को अपने आप भी एक निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कर सकने की निपुणता अवश्य ही अर्जित करनी चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण के निर्माण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यों को प्रायः निम्नांकित तीन चरणों में पूरा किया जाता है-
(अ) निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के लिए नियोजन करना (Planning for the Construction of the Diagnostic Test) - एक निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित नियोजन की काफी जरूरत होती है। इस प्रकार के नियोजन में कुछ निम्न बातों पर ध्यान देना ठीक रहता है-
(1) अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों से सम्बन्धित क्षेत्रों से अवगत होना (Knowing about the areas of Weakness or Learning Difficulties) - निदानात्मक परीक्षण के निर्माण के शुरूआत उसके निर्माण की जरूरत पर ही आधारित होती है। भौतिक विज्ञान के अधिगम में कौन कितना कमजोर है या किसकी क्या कठिनाइयाँ हैं, इस बात की पूरी जानकारी हेतु उपलब्ध परीक्षणों के परिणाम, कक्षा में किया जाने वाला अभ्यास कार्य, विद्यार्थियों से कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर-, गृहकार्य का निरीक्षण तथा विद्यार्थियों के कक्षा व्यवहार आदि की उचित सहायता ली जा सकती है। इस तरह विद्यार्थी विशेष की उपलब्धि या नि पत्ति का मूल्यांकन करने तथा उसके व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु जो भी तकनीक या साधन काम में लाये जाते हैं उनसे प्राप्त परिणामों तथा निष्कर्षों से ऐसे संकेत अवश्य मिल जाते हैं कि विद्यार्थी विशेष या कक्षा और समूह विशेष में कठिनाई तथा कमजोरी का आभास हो जाये, यह पता चल जाये कि भौतिक विज्ञान के इस क्षेत्र से सम्बन्धित अधिगम में विद्यार्थी कठिनाई या अक्षमता का अनुभव कर रहा है। जिस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की कठिनाई तथा कमजोरी का आभास हो उसी को अब निदानात्मक परीक्षण का विषय बनाया जा सकता है।
(2) कठिनाई क्षेत्र को और अधिक सीमित करना (Specifying and Limiting the Difficulty Area) - निदानात्मक परीक्षण जिस इकाई या प्रकरण विशेष पर बनाया जाना है उसे जितना भी सीमित कर दिया जाये उतना ही अच्छा रहता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान के किसी उपलब्धि परीक्षण में बहुत कम अंक लिये हैं तो हमें उसके इस मूल्यांकन परिणाम को और अधिक गहराई से विश्लेषण करना होगा। यह विश्लेषण बता सकता है कि विद्यार्थी रसायन शास्त्र अध्ययन में नहीं बल्कि भौतिक शास्त्र में कमजोर है। आगे वह यह भी संकेत करता है कि भौतिक शास्त्र में भी वह प्रकाश के आवर्तन तथा उसे उपयोग में लाने के सन्दर्भ में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। प्रकाश के आवर्तन तथा उसके उपयोग को अब निदानात्मक परीक्षण का विषय बनाया जा सकता है। इस तरह हम निदानात्मक परीक्षण निर्माण हेतु किसी एक इकाई, उप इकाई, अवधारणा विशेष को चुन लेते हैं जिससे उसका गहराई और विस्तार से निदान किया जा सके। इस तरह भिन्न-भिन्न इकाइयों, उप इकाइयों या अवधारणा विशेषों पर निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण करके फिर उन्हें एक इकट्ठा रूप दे देना चाहिए ताकि एक बड़े क्षेत्र, शाखा या पूरे विषय के लिए निदानात्मक परीक्षण तैयार हो सके।
(3) विषय-वस्तु विश्लेषण (Content Analysis) – भौतिक विज्ञानों की एक उप इकाई (Sub-unit) या किसी एक अवधारणा से सम्बन्धित विषय-सामग्री का अब ठीक तरह विश्लेषण करके यह जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि-
(i) इस उप इकाई तथा अवधारणा के अधिगम हेतु किस प्रकार के ज्ञान, कौशल आदि की आवश्यकता है अर्थात् प्रारम्भिक व्यवहार (Entry behaviour) कैसा होना चाहिए।
(ii) इस उप-इकाई तथा अवधारणा के अधिगम के अर्जन के उपरान्त विद्यार्थी के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है अर्थात् अन्तिम व्यवहार (Terminal behaviour) कैसा होना चाहिए।
(4) परीक्षण प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना (Deciding about the Nature of the item of the Test) - विषय-वस्तु के विश्लेषण तथा प्रारम्भिक और अन्तिम व्यवहार की जानकारी लेने के बाद निदानात्मक परीक्षण में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए, यह निर्णय लिया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या प्रायः ज्यादा ही रखी जाती है और कठिनाई तथा समस्या विशेष की खोज करना इनका उद्देश्य होता है। अतः ऐसे परीक्षण में निबन्धात्मक प्रश्नों की तुलना में लघु-उत्तर-ात्मक तथा अति लघु उत्तर-ात्मक प्रश्नों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भौतिक विज्ञान के अध्ययन में विद्यार्थियों की त्रुटियों या कमजोरियों का पता लगाने हेतु इस प्रकार के प्रश्नों की रचना करना अच्छा रहता है जिससे विषय-वस्तु के अध्ययन में जिस प्रकार के ज्ञान, कौशल तथा वैज्ञानिक ज्ञान सम्बन्धी अवधारणाओं की जरूरत होती है वे उनमें हैं या नहीं, इस बात का पता चल सके।
(5) परीक्षण लेने सम्बन्धी निर्णय लेना (Taking Decision about test Ad ministration) - निदानात्मक परीक्षण कैसे लिया जायेगा इस बारे में भी आवश्यक निर्णय निदानात्मक परीक्षण के निर्माण सम्बन्धी नियोजन स्तर पर ही ले लिया जाना चाहिए, जैसे परीक्षण के लिए समय सीमा (time limit) क्या रहेगी, परीक्षण देने से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश विद्यार्थियों को क्या दिए जायेंगे, परीक्षण प्रश्नों के अंकन तथा परीक्षण परिणामों की व्याख्या करने में क्या प्रक्रिया अपनानी होगी आदि-आदि।
(ब) निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना (Construction of the Diagnostic Tests)-
(1) नियोजन स्तर पर जो निर्णय लिये जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन कर लिया जाता है। यह चयन मुख्यतया निम्न तीन बातों पर केन्द्रित होता है-
(i) उप-इकाई या अवधारणा विशेष की विषय-वस्तु की प्रकृति।
(ii) उप-इकाई या अवधारणा विशेष के अधिगम हेतु आवश्यक प्रारम्भिक व्यवहार ( पूर्व ज्ञान, कौशल आदि के सन्दर्भ में)।
(iii) उप-इकाई या अवधारणा विशेष के अधिगम के पश्चात् विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार ( अर्जित ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग आदि के सन्दर्भ में )।
(2) उपरोक्त तीन बातों को ध्यान रखते हुए अब लघु-उत्तर-ात्मक, अति लघु उत्तरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रश्न-पत्र में आवश्यक निर्देश देने एवं समय अवधि आदि दिये जाने की भी व्यवस्था कर देनी चाहिए। प्रश्नों की उत्तर- कुंजी (scoring key) तथा आदर्श उत्तरों (model answers) का निर्माण भी, उत्तरोंकी उचित व्याख्या और उनसे सही उत्तर- प्राप्त करने हेतु भी, अब यहाँ किया जाना चाहिए।
(3) इस प्रश्न-पत्र / परीक्षण द्वारा अब विद्यार्थियों के एक समूह विशेष की परीक्षा लेकर इसकी उपयोगिता की जाँच करने का प्रयत्न किया जा सकता है। इस जाँच के आधार पर इसमें आवश्यक सुधार किये जा सकते हैं और फिर इसे एक निदानात्मक परीक्षण के रूप में आगे प्रस्तुत करने के बारे में सोचाजा सकता है।
(स) निदानात्मक परीक्षण लेना और उसकी व्याख्या करना (Administration and Interpretation of the Diagnostic Tests) - इस प्रकार से बनाये गये निदानात्मक परीक्षण से अब किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह विशेष / कक्षा की परीक्षा ली जा सकती है। परीक्षा लेते समय परीक्षण से सम्बन्धित सभी आवश्यक निर्देश विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझा दिये जायेंगे। जंब वे अपना कार्य समाप्त कर देंगे तो उनसे उत्तर--पत्रों को प्रश्न-पत्र सहित इकट्ठा कर लिया जायेगा। यहाँ अब उनके उत्तरोंके अंकन के लिए उत्तर- कुंजी तथा आदर्श हल की सहायता ली जा सकती है और उनके उत्तरोंके विश्लेषण के आधार पर (विशेषकर जो त्रुटियाँ वे करते हैं उनका उचित विश्लेषण कर) यह निर्णय लिया जा सकता है कि उनके द्वारा की जाने वाली गलतियों, अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों तथा * कमजोरियों की वास्तविक प्रकृति क्या है ? इन्हीं कमजोरियों तथा कठिनाइयों का उचित निदान ही आगे के उपचारात्मक उपायों या शिक्षण का आधार बनता है। इसलिए परीक्षण से प्राप्त उत्तरोंकी सही दृष्टि से व्याख्या करके विद्यार्थियों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों से अवगत होना अपने आप में बहुत अधिक महत्त्व रखता है।
|
|||||