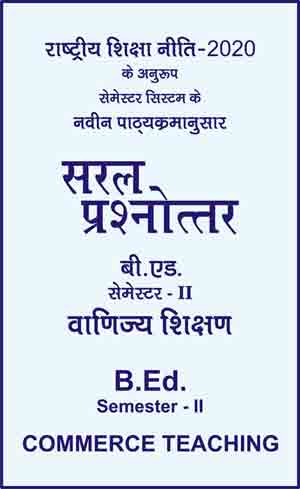|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- पाठ-सूत्र निर्माण करते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगे? उदाहरण सहित उत्तर- दीजिए।
अथवा
पाठ-सूत्र के निर्माण में किन बातों का समावेश किया जाता है।
उत्तर-
पाठ सूत्र के निर्माण में निम्न बातों का समावेश किया जाता है-
1. पाठ-सूत्र संख्या
2. दिनांक
3. विषय
4. कक्षा
5. समय-चक्र
6. छात्र अध्यापक
7. विद्यालय का नाम
8. प्रकरण
9. पाठ के उद्देश्य - (क) सामान्य उद्देश्य, (ख) प्रमुख उद्देश्य
10. सहायक सामग्री
11. पूर्व ज्ञान
12. प्रस्तावना
13. उद्देश्य कथन
14. प्रस्तुतीकरण
15. बोध-प्रश्न
16. श्यामपट्ट सारांश
17. पुनरावृत्ति या प्रयोग
18. गृह-कार्य।
छात्राध्यापक को अपने पाठ सूत्रों का निर्माण यथासंभव पूर्वोक्त क्रम से ही करना चाहिए। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पाठ-सूत्र के निर्माण में पूर्वोक्त बातों को यंत्रवत् स्वीकार कर लिया जाए। अध्यापक आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार-उसमें हेर-फेर भी कर सकते हैं। पूर्वोक्त क्रम में संकेत सात तक बालकों को समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। नीचे हम संकेत आठ से प्रकाश डालेंगे ।
(1) प्रकरण या शीर्षक - प्रकरण को दूसरे शब्दों में शीर्षक कहा जाता है। अध्यापकों को चाहिए कि सुविधा के लिए पाठ्य-वस्तु को विभिन्न अध्यायों में विभाजित कर लें। छोटे अध्यायों को एक घंटे में पढ़ाया जा सकता है।परन्तु लंबे अध्यायों की सुविधा के लिए दो भागों में बाँटा जा सकता है। अध्यापक को चाहिए कि जिस भाग में विचार-प्रधान रूप में प्रकट होता है, उसी के आधार पर प्रकरण का शीर्षक निर्धारित करे। एक घंटे में एक भाग को ही पढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए, आर्थिक विकास के निर्धारक का परिचय छात्रों को देना है तो इसको सुविधानुसार कुछ भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग का शीर्षक आर्थिक विकास के आर्थिक कारक तथा दूसरे भाग का आर्थिक विकास के अनार्थिक कारक रखा जा सकता है। भाषा शिक्षण में प्रत्येक पाठ का शीर्षक उसके विभिन्न भागों में प्रयोग किया जा सकता है। भूगोल, इतिहास, गणितं तथा विज्ञान अदि विषयों के पाठों में शीर्षक स्थिर न रहकर आवश्यकतानुसार बदलता रहता है। इन विषयों का चुनाव अध्यापक को अत्यन्त सावधानी के साथ करना चाहिए। प्रकरण का अधिक लम्बा होना अनुचित है तथा साथ ही प्रकरण अस्पष्ट न हो।
(2) सामान्य उद्देश्य तथा प्रमुख उद्देश्य – प्रत्येक पाठ के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-
(अ) सामान्य उद्देश्य - जो कि उस विषय से सम्बन्धित रहते हैं। ये स्थिर रहते हैं. क्योंकि इनका सम्बन्ध विषय से रहता है, न कि प्रकरण से।
(ब) प्रमुख उद्देश्य - प्रमुख उद्देश्य तकनीकी पाठ से सम्बन्धित रहते हैं, वे अस्थिर हैं। दूसरे शब्दों में, परिवर्तन प्रकरण के आधार पर होता रहता है जबकि सामान्य उद्देश्य प्रायः स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए, वाणिज्य के शिक्षण में सामान्यं उद्देश्य छात्रों में वाणिज्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना तथा उनमें कल्पना शक्ति का विकास करना आदि हो सकता है, परंतु मुख्य उद्देश्य प्रकरण के आधार पर ही निर्धारित किये जायेंगे, जैसे- छात्रों को बेरोजगारी के प्रभावों के बारे में बताना।"
(3) सहायक सामग्री - शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए सहायक सामग्री का विशेष महत्त्व है। अध्यापक को यथासम्भव सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए परंतु आवश्यकता से अधिक सहायक सामग्री का प्रयोग भी अनुचित है, जहाँ उसकी आवश्यकता हो वहीं उसका प्रयोग किया जाए।
(4) पूर्व ज्ञान - पूर्व ज्ञान के आधार पर ही मूल पाठ का प्रस्तुतीकरण किया जाता है। अध्यापक का कर्त्तव्य है कि मूल पाठ को प्रस्तुत करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगा ले। वास्तव में नूतन पाठ को पढ़ाने के लिए उसे पूर्व-ज्ञान के ऊपर निर्भर करना चाहिए। छात्रों के पूर्व - ज्ञान का पता लगाने के लिए अध्यापक को कुछ प्रश्न करने चाहिए। पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रस्तावना निर्भर करती है।
(5) प्रस्तावना - प्रस्तावना से अध्यापक, बालकों को नये पाठ से परिचित कराता है।पाठ की सफलता के लिए आवश्यक है कि उसकी तैयारी अध्यापक ठीक प्रकार से करे। इसके लिए आवश्यक है कि वह नवीन ज्ञान को पूर्व-ज्ञान के आधार पर दे।जितनी सफलता के साथ वह छात्रों के पूर्व-ज्ञान को जाग्रत कर सकेगा, उतना ही वे नवीन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे। इसी कारण पाठ के आरम्भ में बालकों से कुछ प्रश्न किये जायें या कोई रोचक समस्या प्रस्तुत की जाए जिसका सम्बन्ध नवीन पाठ से हो।
प्रस्तावना के विषय में विद्वान् वाल्टन लिखते हैं, 'वशिक्षक को बहुत ही संक्षेप में बालकों के पूर्व - ज्ञान को जाग्रत करना चाहिए, जिससे वे प्रस्तुत पाठ के लिए शीघ्र ही तैयार हो जायें। बालकों की स्थिति में अपने को डालकर शीघ्रता से पाठ को प्रारम्भ कर देना कुशल शिक्षक का चिह्न है। यह जानना कि छात्र कहाँ है और कहाँ पहुँचने के लिए उसे प्रयत्न करना चाहिए, अच्छे अध्यापक के दो आवश्यक लक्षण हैं।"
एक उत्तम प्रस्तावना के लक्षण हैं-
(i) प्रस्तावना में व्यर्थ के प्रश्न न किये जायें।
(ii) प्रस्तावना जहाँ तक सम्भव हो, न अधिक लम्बी हो और न अधिक संक्षिप्त।
(iii) प्रस्तावना के प्रश्न यथासम्भव पूर्व - ज्ञान के आधार पर किये जाएँ।
(iv) प्रश्न मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार-व्यवस्थित किये जाएँ।
दूसरे शब्दों में, प्रश्नों का असम्बन्धित होना उचित नहीं है, प्रत्येक प्रश्न को एक-दूसरे से सम्बन्धित होना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट हों।
(6) उद्देश्य कथन - प्रस्तावना के अन्त में ही बालक को पाठ के उद्देश्य का आभास मिल जाता है परंतु फिर भी अध्यापक को नवीन पाठ के मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट कर देना चाहिए। उद्देश्य का स्पष्टीकरण हो जाने से छात्रों में उत्साह आ जाता है और वे उसे प्राप्त करने के लिए अपने को तैयार कर लेते हैं।
(7) प्रस्तुतीकरण - प्रस्तुतीकरण में बालक के सामने विषय उपस्थित किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस पद में बालकों को नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। अध्यापक को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि नये ज्ञान को सिखाने के साथ-साथ बालक जो सीख चुका है, उसके साथ ही सम्बन्ध स्थापित किया जाय। उद्देश्य कथन के समाप्त हो जाने के पश्चात् बालक का अवधान नवीन पाठ पर केन्द्रित हो जाता है। अतः अब अध्यापक का कार्य ज्ञान का प्रस्तुतीकरण करना हो जाता है; अर्थात् उसक सामने यह समस्या आती है कि वह बालकों के सामने नूतन ज्ञान किस प्रकार तथा किसी भाषा में प्रस्तुत करे।
नवीन ज्ञान को उचित प्रकार से प्रस्तुत करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह 'न्वयन तथा विभाजन' के सिद्धान्त को अपनाकर चले।सुविधा के लिए सम्पूर्ण पाठ का विभाजन दो या तीन अन्वितियों में कर दिया जाये। इस विभाजन में भी अध्यापक को कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसा कि एस.के. अग्रवाल लिखते हैं कि व्यह विभाजन इस ढंग से होना चाहिए कि प्रत्येक सोपान स्वयं में पूर्ण इकाई हो और साथ-साथ आगे आने वाले सोपान से सम्बन्धित हो; अर्थात् प्रत्येक सोपान अपने पूर्व के सोपान से उत्पन्न होता प्रतीत हो।” दूसरे शब्दों में, प्रत्येक सोपान के अन्त में आने वाले सोपान का आभास अथवा संकेत मिलता रहे।
(8) बोध प्रश्न - प्रत्येक सोपान के पश्चात् अध्यापक को इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिये जिनसे कि यह पता लग सके कि पढ़ाया गया विषय छात्रों की समझ में आ रहा है अथवा नहीं। इसी प्रकार के प्रश्नों को बोध प्रश्न कहा जाता है। वाणिज्य, भूगोल आदि विषयों के शिक्षण में प्रश्नों द्वारा अध्यापक, सोपान के मुख्य तथ्य - बिन्दुओं की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। भाषा शिक्षण में ये प्रश्न भाषा सम्बन्धी तथा विषय-वस्तु सम्बन्धी दोनों प्रकार के लिए जा सकते हैं। छात्रों द्वारा बोध - प्रश्नों के उत्तरोंकी सहायता से श्यामपट्ट पर सारांश तैयार कराया जाए।
(9) श्यामपट्ट सारांश - बोध - प्रश्नों के उत्तरों की सहायता से श्यामपट्ट सारांश तैयार कराया जाता है। अध्यापक का कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक अन्विति या सोपान के पश्चात् बोध - प्रश्न करे तथा छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरोंकी सहायता से श्यामपट्ट सारांश लिखे।अध्यापक को सदा इस बात का ध्यान रखना है कि श्यामपट्ट सारांश, जहाँ तक सम्भव हो, छात्रों की सहायता से ही तैयार किया जाए। अध्यापक स्वयं कभी भी श्यामपट्ट सारांश तैयार न करे।
(10) पुनरावृत्ति - छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान को जाँचने तथा पाठ के मुख्य तथ्या को छात्रों के मस्तिष्क में दृढ़ करने के लिए पाठ के अन्त में प्रश्नों द्वारा महत्त्वपूर्ण तथ्यों की पुनरावृत्ति की जाए। इस कारण ही इस पद को स्थानीयकरण पद भी कहा जा सकता है। पुनरावृत्ति के प्रश्नों से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इनस अध्यापक को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे अपने शिक्षण में कहाँ तक - सफलता मिली है और छात्र ने किस सीमा तक नवीन ज्ञान ग्रहण किया है। छात्र को भी अपनी प्रगति का आभास मिल जाता है। इस प्रकार इस पद की अत्यधिक प्रमुखता है। अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि गणित तथा विज्ञान के पाठों में पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से न की जाए। इन पाठां में बालकों से प्रयोग मात्र ही कराये जायें।
(11) गृह कार्य - यह अन्तिम पद है जिसका प्रमुख उद्देश्य पाठ की समाप्ति के पश्चात् को घर के लिए कार्य प्रदान करना है। गृह कार्य के लाभ तथा गुणों के ऊपर अलग से प्रकाश डाला गया है। यहाँ हम गृह कार्य प्रदान करने में जिन आवश्यक सावधानियों की आवश्यकता है, उनका उल्लेख करेंगे-
(i) अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को जो गृह कार्य प्रदान करे, वह मात्रा में अत्यधिक न हो।गृह कार्य उतना ही प्रदान किया जाए जितना कि छात्र सरलता तथा रुचि के साथ कर सके।
(ii) गृह-कार्य प्रदान करते समय अन्य विषयों का भी ध्यान रखा जाए।
(iii) गृह-कार्य प्रदान करने में छात्रों की मानसिक योग्यता का भी ध्यान रखा जाए।
(iv) गृह-कार्य प्रदान करने में विभिन्नता का होना परम आवश्यक है।सदा एक-सा प्रदान किया जाने वाला गृह-कार्य छात्रों में नीरसता उत्पन्न करता है।
(v) जो गृह कार्य छात्रों को प्रदान किया जाए, उसका निरीक्षण अवश्य होना चाहिए। बिना निरीक्षण के गृह कार्य व्यर्थ है।
(vi) छात्रों को प्रदान किया जाने वाला गृह कार्य स्वाध्याय को प्रोत्साहन देने वाला हो।आवश्यकतानुसार छात्रों को गृह कार्य से सम्बन्धित पुस्तकें भी बता दी जायें।
|
|||||