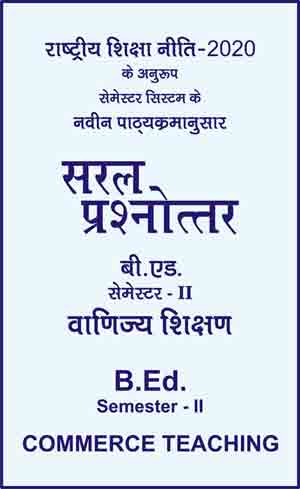|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 वाणिज्य शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय 4 - वाणिज्य शिक्षण की विधियाँ
(Methods of Commerce Teaching)
प्रश्न- एक अच्छी पाठ-योजना किसे कहते हैं? हरबर्ट के पाँच पदीय उपागमों की विवेचना कीजिए।
अथवा
एक अच्छी पाठ योजना की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? हरबर्ट के पाँच पदीय उपागम का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
पाठ योजना अध्यापक के लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। एक अच्छी पाठ - योजना से शिक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। पाठ योजना विस्तृत होनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए-
(i) भली-भाँति सोची समझी योजना हो - यदि पाठ योजना को सोच-समझ कर बनाया जाए तो अधिक उपयुक्त होता है। क्योंकि इससे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुविधा होती है। विशिष्ट विषयों को यदि उपविषय और इकाइयों में बाँटकर विशिष्ट सामग्री, विधि तथा प्रविधियों का सोच - कर चयन करके बनाया जाए तो शिक्षक अपने पाठ में विभिन्नता ला सकता है।
(ii) पाठ योजना के क्रियान्वयन में विचलन नहीं - यह अच्छी पाठ योजना की एक विशेषत- है।पूर्व नियोजित पाठ-योजना लागू करते समय वास्तविक पाठ योजना से विचलित नहीं होनी चाहिए। अच्छी पाठ योजना ऐसा नहीं होने देती। अतः यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के निर्णय कक्षा में प्रवेश करने से पहले तथा पाठ योजना बनाते समय ही ले लेने चाहिए। ताकि कोई भी शिक्षक इस पाठ योजना से कम विचलित हो।
(iii) अच्छी पाठ-योजना - कक्षा-कक्ष गतिविधियों की सूचक अच्छी पाठ योजना इन बातों का पहले से संकेत दे देती है कि कक्षा में क्या कुछ होने वाला है। जैसे किस पक्ष पर प्रश्न पूछे जाने हैं? ब्लैकबोर्ड पर कब स्क्रैच बनाने हैं? बच्चे नक्शे कब बनायेंगे? अध्यापक कब कैसा कथन करेगा ? पाठ-योजना की यह विशेषता तब बहुत ही सहायक होती है जब कोई दूसरा शिक्षक पाठ योजना को पढ़कर शिक्षण कार्य करता है तथा शिक्षक कार्य उसी स्तर का होता है जैसा कि पाठ-योजना वाला शिक्षक करता है।
(iv) अच्छी पाठ-योजना - सहायक सामग्री की आवश्यकता की ओर संकेत करती है- एक अच्छी पाठ योजना हमें यह भी स्पष्ट संकेत देती है कि कक्षा में शिक्षक कार्य के लिए कौन-कौन सी सहायक सामग्री तथा शाब्दिक सामग्री चाहिए। यदि माठ योजना पहले से ही बना ली जाती है तो इस तरह की सामग्री एकत्रित करना आसान हो जाता है।
(v) बच्चों की निरन्तर रुचि बनाए रखना - एक सर्वोत्तम पाठ योजना बच्चों की रुचि को पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बनाए रखती है। इस प्रक्रिया में विभिन्न विधियों और प्रविधियों का प्रयोग आवश्यक है जिनमें बच्चे सक्रियता से भाग ले सके। इस संदर्भ में यह कहना उपयुक्त होगा कि पाठ - योजना की इस विशेषता को बनाए रखने के लिए शैक्षिक सिद्धान्त और शैक्षिक मनोविज्ञान व ज्ञान अति आवश्यक है।
(vi) अच्छी पाठ-योजना के विभिन्न पक्ष - एक अच्छी पाठ योजना के विभिन्न पक्ष होते हैं जो निम्नलिखित हैं-
(क) उद्देश्यों की विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति।
(ख) विषय-वस्तु के विवरण और विधि की विस्तृत रूपरेखा।
(ग) पूर्व ज्ञान के संकेत के आधार पर नए पाठ में विस्तार करना ।
(घ) बच्चों की क्रियाओं की सुझावात्मक सूची जिसमें अधिगम का मूल्यांकन भी शामिल हो।
(च) सन्दर्भ पुस्तकों और सामग्री की जानकारी।
(vii) अच्छी पाठ-योजना शिक्षा में मनोविज्ञान और अधिगम सिद्धान्त का प्रतिबिम्ब होना चाहिए - एक अच्छी पाठ योजना में शिक्षा मनोविज्ञान और अधिगम सिद्धान्तों का आधार होना अति आवश्यक है। शिक्षक पाठ योजना बनाने में इतना निपुण हो कि पाठ योजना में विद्यार्थी की विशेषताओं और विकास की झलक स्पष्ट दिखाई दे।
(viii) अच्छी पाठ योजना शिक्षण शैली की खोज में सहायक - एक अच्छी पाठ-योजना में शिक्षक अपनी विशेषताओं और कमियों की ओर विशेष ध्यान दे सकता है। इससे शिक्षक को सृजनात्मक शिक्षण में सहायता मिलती है तथा उसको एक विशेष शिक्षण शैली की खोज करने में सुविधा रहती है।पाठ का निरीक्षण करने वालों को इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि सभी अध्यापकों या छात्र - अध्यापकों के शिक्षण का एक ही प्रकार के सांचे से मूल्यांकन न किया जाए।
(ix) भविष्य के लिए उत्तम नियोजन - एक अच्छी पाठ योजना में इस बात की गुंजाइश रहती है कि शिक्षक या छात्र अध्यापक कक्षा के बाद यह जान सके कि उसकी पाठ योजना किस प्रकार से और अच्छी तरह स्थिति का सामना कर सकती है। इससे भविष्य में शिक्षण के लिए उत्तम नियोजन का रास्ता मिलेगा।
पाठ-योजना के उपागम
पाठ-योजना बनाने के लिए किसी एक प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। इसे लिखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता रहा है। पाठ योजना के विभिन्न उपागमों में शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न पक्षों पर बल दिया है।पाठ योजना के लिए कौन-सा उपागम अधिक उपयुक्त है, इसके बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। विषय तथा उद्देश्यों के आधार पर विभिन्न उपागमों का प्रयोग किया जाता है। ब्लूम तथा मार्सिया ने शिक्षण के उद्देश्यों को तीन भागों में बाँटा है जो ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक कहलाते हैं। उसके आधार पर पाठ - योजना के मुख्य उपागम इस प्रकार हैं-
(i) हरबर्ट का पाँच पदीय उपागम
(ii) मौरीसन का इकाई उपागम
(iii) ब्लूम का मूल्यांकन उपागम
(iv) आर. सी. ई. एम. उपागम
(च) हरबर्ट उपागम - इस उपागम का प्रतिपादन जर्मन के विख्यात शिक्षाशास्त्री जॉन फ्रेड्रिक हरबर्ट ने किया था।
इस उपागम के पाँच सोपान है-
(क) उद्देश्य कथन या तैयारी,
(ख) प्रस्तुतीकरण,
(ग) तुलना और संबंध या स्पष्टीकरण,
(घ) सामान्यीकरण ए
(ङ) प्रयोग।
(छ) मौरीसन का इकाई उपागम - इस उपागम का प्रतिपादन प्रो. एस. सी. मौरीसन ने 1929 ई. में अपनी पुस्तक "सैकेन्डरी स्कूल में अध्यापन अभ्यास' में की है जिसका प्रयोग अमेरिका में किया जा रहा है। इस उपागम के भी पाँच सोपान हैं-
(क) अन्वेषण,
(ख) प्रस्तुतीकरण,
(ग) संगठन,
(घ) आत्मीयकरण और
(ङ) अभिव्यक्तिकरण।
(ज) ब्लूम का मूल्यांकन उपागम - इस उपागम के तीन सोपान हैं-
(क) शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण,
(ख) अधिगम अनुभव प्रदान करना एवं
(ग) अधिगम परिणामों का मूल्यांकन।
(झ) आर. सी. ई. एम. उपागम - इस उपागम का विकास क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर ने किया। इस प्रणाली उपागम के तीन पद अदा, प्रक्रिया और प्रदा हैं।
हरबर्ट का पाँच पदीय उपागम
हरबर्ट जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री एवं दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने शिक्षण को पांच पदों में बाँटा है। इन पाँचों पदों के आधार पर पाठ योजना बनाई जाती है। उनका यह उपागम सबसे पुराना है लेकिन अधिकांश शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण संस्थाओं में पाठ योजना के लिए हरबर्ट के उपागम का ही प्रयोग किया जाता है।
हरबर्ट के इस उपागम में विषय-वस्तु के प्रस्तुतीकरण पर ही अधिक बल दिया जाता है तथा विद्यार्थी की रुचियों, अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा संबंधों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस उपागम में स्मृति स्तर के शिक्षण को महत्त्व दिया जाता है। इसलिए यह रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। हरबर्ट के निम्न पाँच पद हैं-
(i) प्रस्तावना तथा उद्देश्य कथन,
(ii) प्रस्तुतीकरण
(iii) स्पष्टीकरण,
(iv) सामान्यीकरण
(v) प्रयोग।
(i) प्रस्तावना - अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने पर जाते ही नहीं पढ़ा सकता, उसे पढ़ाने से पहले कुछ क्रियाएँ ऐसी करनी पड़ती हैं जिनसे विद्यार्थी का ध्यान कक्षा में पढ़ने के लिए बनाया जा सके। अध्यापक कक्षा में आने पर सबसे पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर पाठ प्रस्तावना करता है। इसके लिए वह कई तरीका अपनाता है, जैसे-सीधे प्रश्न पूछकर, कविता की पंक्तियाँ पढ़कर, कोई चित्र या चार्ट दिखाकर अथवा कहानी सुनाकर। इस प्रकार पूर्व ज्ञान के आधार पर पूछे गए प्रश्नों से नवीन ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार करना है। इसके पश्चात् अध्यापक उद्देश्य कथन की घोषणा करता है। उसके बाद ही वह पाठ को शुरू करता है।
(ii) प्रस्तुतीकरण - हरबर्ट उपागम में प्रस्तावना के पश्चात् पाठ योजना में प्रस्तुतीकरण आता है।अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष नई विषय-वस्तु को प्रस्तुत करता है। शिक्षण कार्य का आरंभ प्रस्तुतीकरण से ही होता है। इस पद में अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार-पाठ को तीन भागों में बाँट लेता है-
(1) विषय-वस्तु,
(2) शिक्षण विधि
(3) श्यामपट्ट कार्य।
विषय-वस्तु की छोटी-छोटी इकाइयों के माध्यम से विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से सुव्यवस्थित तथा सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। इनमें वह विभिन्न सिद्धान्तों तथा सूत्रों को ध्यान में रखता है।
(iii) स्पष्टीकरण - हरबर्ट उपागम का यह तीसरा पद है। इस पद में अध्यापक मौखिक स्पष्टीकरण करता है। वह उदाहरणों, चित्रों, मानचित्रों, चार्ट आदि का प्रयोग करके विषय-वस्तु को स्पष्ट करता है। इससे आवश्यक हुआ तो वह तुलना तथा संबंध का भी प्रयोग करता है। इससे विद्यार्थियों का मानसिक विकास करने और पर्याप्त ज्ञान प्रदान करने में मदद मिलती है।
(iv) सामान्यीकरण - किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद कुछ न कुछ निष्कर्ष अवश्य निकाला जाता है। इसके आधार पर ही कुछ सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से ही नियमों, सिद्धान्तों तथा सूत्रों का जन्म होता है। इस कार्य में अध्यापक को विद्यार्थियों से अधिक सहायता लेनी चाहिए।
(v) प्रयोग - हरबर्ट के इस उपागम में पाँचवें पद का बहुत महत्त्व है। इस पद में विद्यार्थियों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करने से ज्ञान स्थायी हो सकता है।
|
|||||