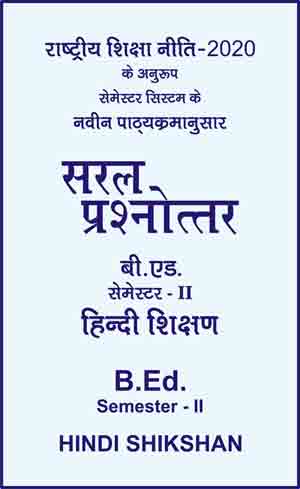|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- कविता-शिक्षण की कौन-कौन सी प्रमुख विधियाँ हैं?
अथवा
कविता शिक्षण की कौन-सी विधियाँ हैं? प्रत्येक का विवरण दीजिए। प्रशिक्षण काल में कौन-कौन सी विधियाँ शिक्षण के लिये उपयुक्त मानी जाती हैं?
अथवा
माध्यमिक स्तर पर कविता पढ़ाने की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
उत्तर-
कविता-शिक्षणकी विधियाँ
भाषा और शिक्षाशास्त्रियों ने कविता-शिक्षण हेतु अनेक विधियों का उल्लेख किया है। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियों का विवरण यहाँ दिया गया है-
(1) गीत व अभिनय विधि - यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सीखने में जितनी अधिक ज्ञानेन्द्रियाँ प्रभावित व सक्रिय होंगी, उसमें छात्र अधिक रुचि लेंगे और सीखने में स्थायीपन होता है। रेडियो की अपेक्षा दूरदर्शन अधिक रुचिकर होता है। दृश्य एवं श्रव्य से इन्द्रियाँ प्रभावित तथा सक्रिय होती हैं। इसीलिए कविता को गाकर तथा अभिनय से सिखाया जाता है।
ढोल बजाता मेढक आया, ढम ढम ढम ढम ढम ढम।
इस विधि का प्रयोग प्रारम्भिक कक्षाओं में होता है। बच्चे स्वभाव से ही संगीत प्रेमी होते हैं। इसी कारण बाल-गीत एवं छन्दबद्ध लय वाले गीत बच्चों को बहुत प्रभावित करते हैं। इन गीतों या लयात्मक पद्यों को पढ़ाने की प्रणाली गीत-प्रणाली है। शिक्षक स्वयं स्तर एवं ताल के साथ गीत पढ़ता है और बच्चे फिर अनुकरण करते हैं।
बालकों को सस्वर पाठ भी कराया जाता है। सस्वर पाठ में अनावश्यक हाव-भाव एवं अंग संचालन नहीं होना चाहिए और उचित रीति से पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए।
इन गीतों या पद्यों की शब्दावली बड़ी सरल और ध्वनात्मक होती है। बालक सरलतापूर्वक इन्हें कण्ठस्थ कर लेते हैं और लय एवं ताल के साथ पढ़ने में आनन्द की अनुभूति करते हैं। यही इस प्रणाली का विशेष गुण हैं। यह प्रणाली केवल प्राथमिक स्तर पर ही प्रयुक्त होती है।
(2) नाट्य विधि - प्रारम्भिक स्तर पर अनेक गीत ऐसे पढ़ने होते हैं जिनमें क्रियात्मकता अधिक होती है। ऐसे गीतों को नाट्य या अभिनय प्रणाली से पढ़ाया जा सकता है। कार्य अथवा भाव-प्रदर्शन के लिए बालक उचित भाव-भंगिमा और अंग संचालन के साथ कविता पढ़ते हैं। इसे प्रणाली से कक्षा में बड़ा ही सजीव और सरल वातावरण बन जाता है और बच्चे आनन्द मग्न बने रहते हैं। इस प्रणाली के प्रयोग में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक अनावश्यक उछल-कूद न करने लगे और कविता में निहित क्रिया एवं भाव के सूचक रूप में ही अभिनयात्मक या नाटकीयता का प्रदर्शन करे। यह प्रणाली भी केवल प्राथमिक स्तर पर ही प्रयुक्त होती है।
(3) अर्थ बोध विधि या शब्दार्थ कथन विधि - कविता शिक्षण में इस विधि का अधिक प्रचलन है। शिक्षण कविता का अर्थ समझाकर अपने कर्त्तव्य की पूर्ति कर लेता है। शिक्षक अपने कर्त्तव्य को भली प्रकार नहीं समझते हैं। कविता की पंक्तियों का शब्दार्थ या भावार्थ बता देना कविता के प्रति अन्याय है।
इस विधि का प्रयोग कक्षा 4-5 से ही प्रारम्भ हो जाता है और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक चलता रहता है। यह प्रणाली परम्परागत प्रचलित प्रणाली है और आज भी शिक्षक इसका अनुसरण करते जा रहे हैं पर इससे कविता शिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।
इस विधि में शिक्षक किसी छात्र से कविता पढ़ने को कहता है और कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुये पद्य का अर्थ भी बताता जाता है। कभी-कभी छात्रों से भी अर्थ पूछ लेता है, पर सामान्यतः शिक्षक ही पूरी कविता का अर्थ स्पष्ट करता है।
कविता पढ़ने की यह विधि सर्वथा दोषपूर्ण है। शब्दार्थों पर बल देने से कविता का पाठ शुष्क एवं गद्यवत् हो जाता है। इस प्रणाली में छात्रों को शब्दार्थ का ज्ञान तो हो जाता है पर कविता में सौन्दर्य तत्त्वों का बोध नहीं हो पाता और वे आनन्द भी नहीं ले पाते। शिक्षक को माध्यमिक कक्षा में कविता पाठ पढ़ाते समय छात्रों को सक्रिय सहयोग लेना चाहिए, पर शब्दार्थ कथन प्रणाली में इसका अवसर नहीं मिल पाता। कविता सुपाठ का भी अवसर इस प्रणाली में नहीं मिलता है।
(4) प्रश्नोत्तर अथवा खण्डान्वय विधि - कविता की एक-एक पंक्ति एवं उसमें एक-एक खण्ड पर प्रश्न पूछते हुये बालकों से उत्तर- प्राप्त करते हुये और यथावश्यक स्वयं स्पष्ट करते हुये कविता अर्थ बताने की विधि प्रश्नोत्तर अथवा खण्डान्वय प्रणाली कहलाती है। यह प्रणाली भी बहुत कुछ गद्य शिक्षण प्रणाली की ही भाँति जिसमें पद्यांश के खण्ड-खण्ड करके प्रत्येक तथ्य, भाव या विचार के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते हैं और अभीष्ट उत्तर- प्राप्त करते हुये सम्पूर्ण विषय-वस्तु का परिचय छात्रों को करा दिया जाता है। यह विधि अपनाने से कविता की विषय-सामग्री तो स्पष्ट हो जाती है पर उसके सौन्दर्य-बोध छात्रों को नहीं हो पाता। सम्पूर्ण पाठ-विकास प्रश्नों का ही क्रमोत्तर विकास जैसा प्रतीत होता है। अत- यह प्रणाली कविता के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है क्योंकि कविता में मुख्य बात ही उसके रागात्मक तत्त्वों से तादात्म्य स्थापना की क्रिया जो खण्डान्वय प्रणाली द्वारा ही सम्भव नहीं हो पाती है।
इस शिक्षण विधि में कविता के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न किये जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तरों में कविता' का मूल भाव प्रकट होता है, जैसे-
प्रीति कर काहू सुख न लहो,
प्रीति पतंग करी दीपक सौं,
सम्पुट माछ लहो।
प्रश्न 1.प्रेम करने का क्या परिणाम होता है?
प्रश्न 2. पतंगा किस को प्रेम करता है?
प्रश्न 3. उसका क्या परिणाम होता है?
इन प्रश्नों की सहायता से खण्डों में विभाजित कर देते हैं और प्रश्नों के उत्तरों से छात्रों को कविता का अर्थ बोध कराया जाता है।
|
|||||