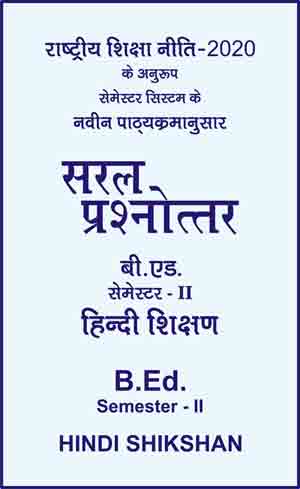|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- मातृभाषा का अन्य विषयों से सह-सम्बन्ध का अर्थ बताइए तथा इसकी आवश्यकता भी बताइए।
अथवा
"मातृभाषा केवल एक विषय ही नहीं है, परन्तु वह सब विषयों की नींव है।" इस सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कीजिये। यह बताइये कि इस सिद्धान्त को पढ़ाने की पद्धति पर कौन-सा असर पड़ता है?
उत्तर-
मातृभाषा का अन्य विषयों से सह-सम्बन्ध
आधुनिक शिक्षा का प्रमुख दोष उसका समन्वय रहित होना है। पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों में किसी भी प्रकार का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जाता है। हिन्दी भाषा का शिक्षण करते समय इतिहास तथा भूगोल की चर्चा व्यर्थ समझी जाती है।
सह-सम्बन्ध का अर्थ
समन्वय का अर्थ है विद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न विषयों में परस्पर सह-सम्बन्ध स्थापित करना। सह-सम्बन्ध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से निम्नलिखित परिभाषाएँ दी. हैं-
1. डमविल के अनुसार- "एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धान्त को सामान्यतः समन्वय के नाम से उल्लेख किया जाता है।"
2. बरनार्ड के अनुसार- "समन्वय विद्यालय के विषयों को यथासम्भव एक-दूसरे से सम्बन्धित करने की कोशिश करता है। "
3. शाह के अनुसार- "सानुबन्ध शिक्षण विद्यार्थी को उसके अनुभवों के स्तर के अनुसार- शिक्षा देने के अलावा कुछ नहीं है।"
मातृभाषा का अन्य विषयों से सम्बन्ध
1. क्षितिजीय सम्बन्ध - इसमें विषयों के बीच में सम्बन्ध किया जाता है। यदि शिक्षक भाषा का शिक्षण कर रहा है, तो वह इतिहास तथा भूगोल, विज्ञान आदि विषयों का भी वर्णन करेगा। दूसरे शब्दों में, वह अन्य विषयों की सामग्री का प्रयोग भाषा के पाठ के समझाने के लिए करेगा।
2. ऊर्ध्वाकार सम्बन्ध - ऊर्ध्वाकार समन्वय में एक ही प्रकार के विभिन्न उपविषयों में सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार भाषा का शिक्षण करते समय गद्य के साथ तथा पद्य के साथ समन्वय किया जाता है। ऊर्ध्वाकार समन्वय पाठ को आकर्षक और रोचक बनाता है।
3. मातृभाषा का विज्ञान से सम्बन्ध - आधुनिक युग विज्ञान का युग है। इसलिए भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में विज्ञान से सम्बन्धित पाठों को रखना आवश्यक है। बेतार का तार, परमाणु शक्ति तथा अणु शक्ति आदि इस प्रकार के ही पाठ हैं, इसलिए शिक्षक का कर्त्तव्य है कि वह इन पाठों को पढ़ाने से पहले इनके विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करे।
4. मातृभाषा का भूगोल से सम्बन्ध - व्यक्ति का जीवन भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है, इसलिये भाषा का शिक्षण करते समय उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गद्य के अनेक पाठ भूगोल से सम्बन्धित होते हैं जैसे हिमालय पर्वत आदि ऐसे पाठों को इस प्रकार के स्थलों का उल्लेख प्रभावशाली तथा भावयुक्त शब्दों में करना चाहिए और उसकी भौगोलिक व्याख्या करनी चाहिए।
5. मातृभाषा का कला से सम्बन्ध - नृत्य कला, चित्रकला तथा संगीत कला से सम्बन्धित पाठ भाषा की पाठ्य-पुस्तक में सम्मिलित किए जा सकते हैं। शिक्षक को इन कलाओं के विषय में यथासम्भव जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कविता में वर्णित दृश्य विद्यार्थियों से बनवाने चाहिए।
6. मातृभाषा का इतिहास से सम्बन्ध - अनेक ऐतिहासिक काव्य लिखे गए हैं। 'झाँसी की रानी', 'मृगनयनी 'आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए हैं। रक्षाबन्धन, अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त तथा स्कन्दगुप्त आदि ऐतिहासिक नाटक हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि 'झाँसी की रानी' नामक कविता का पाठ कराकर विद्यार्थियों को 1857 के ऐतिहासिक महत्त्व को समझाया जाए तथा चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त आदि नाटकों के माध्यम से विद्यार्थियों को ऐतिहासिक महत्त्व समझाया जाए। क्षत्रिय के अनुसार-, "साहित्य समाज के भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का दर्शन कराता है। उन घटनाओं को ज्यों-की-त्यों अंकित न करके साहित्यकार उसमें अपनी कल्पनाओं के सहारे कुछ नवीन रंग अवश्य भर देता है, परन्तु होता वह सत्य ही है।" अतः साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का स्पष्ट दर्शन होता है।
मातृभाषा का अन्य विषयों से समन्वय
मातृभाषा का विकास करने के लिए अन्य भाषाओं की अच्छाइयों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाओं के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद मातृभाषा में करवाया जायें। इस प्रकार के अनुवादों से मातृभाषा के साहित्य भण्डार की आसानी से अभिवृद्धि हो सकती है। अंग्रेजी की कविता को पढ़ाते समय उसी से सम्बन्धित हिन्दी को भी पढ़ाया जाए। अन्य शब्दों में, अंग्रेजी के शब्दों के अर्थों का ज्ञान कराते समय हिन्दी के शब्दों के अर्थों का ज्ञान कराया जाए। समन्वय करते समय ही ध्यान रहे कि वह स्वाभाविक हो, उसमें व्यर्थ की बातों पर जोर न दिया जाए तथा समन्वय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। समन्वय में आवश्यकता से अधिक विषयों का समन्वय न किया जाए। समन्वय का प्रयोग साधन के रूप में किया जाना चाहिए न कि साध्य के रूप में।
|
|||||