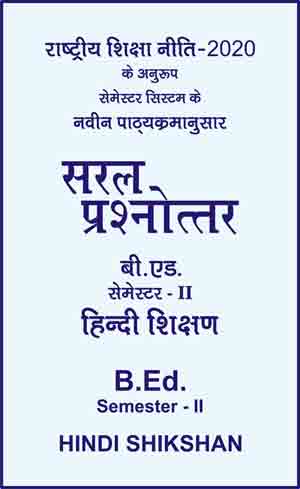|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- भाषा शिक्षण की क्षेत्रीय एवं अंग्रेजी भाषा शिक्षण से तुलना कीजिये।
उत्तर-
भाषा के रूप में क्षेत्रीय एवं विदेशी भाषा के रूप में - हिन्दी शिक्षण में पर्याप्त अन्तर है। पिछली शताब्दी तक बहुभाषी होना व्यक्ति की सांस्कृतिक सम्पन्नता का द्योतक था किन्तु आज की स्थिति सर्वथा भिन्न है। अब वह एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई है, बीसवीं शताब्दी में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषा की जानकारी के इस लक्ष्य परिवर्तन को समझना अत्यन्त आवश्यक है। आज हम एक-दो प्रमुख भाषाओं की जानकारी केवल इसलिये नहीं करना चाहते हैं कि उस भाषा में उचित उच्च साहित्य का रसास्वादन कर सके अपितु इसलिए भी करना चाहते हैं कि अन्य भाषा-भाषी व्यक्तियों के जीवन को व्यापक स्तर पर समझें, उनके साथ हम जीवनगत उपलब्धियों का आदान-प्रदान कर सकें। साहित्यिक उपलब्धि से हटकर जब भाषा शिक्षण को जन सामान्य की सामाजिक एवं व्यावहारिक आवश्यकता के स्तर पर उतारा तो फिर परिवर्तन के फलस्वरूप परम्परागत रूप से चली आ रही उसकी प्रणाली में भी आधारभूत परिवर्तन अनिवार्य हो उठा। वस्तुत- यह परिवर्तन भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में एक नूतन क्रान्ति के रूप में अवतरित हुआ।
अन्य भाषा शिक्षण का तात्पर्य भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीखना है। यह अन्य भाषा विद्यार्थी के ही देश की कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा हो सकती है या किसी दूसरे देश की भाषा भी हो सकती है। हमारे देश में हिन्दी शिक्षण के दो रूप हैं एक तो हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में जिनकी अपनी मातृभाषा के रूप में (प्रथम भाषा) और दूसरे अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में जिनकी अपनी मातृभाषा कुछ और है वहाँ अन्य भाषा के रूप में (द्वितीय भाषा)। आजकल विदेशों में भी हिन्दी भाषा के अध्ययन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है।
(1) अहिन्दी भाषी राज्य - असम, बंगाल, उड़ीसा, नागा प्रदेश, आन्ध्र, मद्रास, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर।
क्षेत्रीय भाषाएँ - आसामी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलगू, उर्दू, भारतीय संविधान आठवीं अनुसूची।
उपरोक्त तथ्यों के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है वह निम्नलिखित प्रकार से है-
भाषा व अंग्रेजी भाषा में अन्तर
(1) उद्देश्य में अन्तर - भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण का उद्देश्य ग्राह्यात्मक, अभिव्यंजनात्मक, सराहनात्मक एवं सृजनात्मक भी होता है किन्तु राजभाषा या विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के केवल दो ही उद्देश्य पर्याप्त हैं- ग्राह्यात्मक एवं अभिव्यंजनात्मक।
(2) मातृभाषा एवं अन्य भाषा शिक्षण के प्रयोजन में अन्तर - हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में मातृभाषा सीखने का प्रयोजन जीवन की मौलिक आवश्यकताओं के रूप में लोगों द्वारा उक्त भाषा को सीखना है किन्तु अन्य भाषा के रूप में हिन्दी सीखने का प्रयोजन अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में है सामुदायिक जीवन की कुछ विशेष आवश्यकता की पूर्ति।
इलपावुलुरि पांडुरंग राव के शब्दों में - घरेलू जीवन के सीधे-सीधे वार्तालाप से लेकर साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और अध्यात्मिक जीवन के ऊँचे-ऊँचे और जटिल से जटिल विचारों तक को व्यक्त करने की क्षमता मातृभाषा ही में और अपेक्षित प्राप्त होती है।
(3) चारों क्षमताओं के क्रम में अन्तर - मातृभाषा सीखते समय सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यही क्रम अपनाया जाता है। यही क्रम स्वाभाविक भी है किन्तु अन्य भाषा के रूप में हिन्दी सीखते समय जो क्रम अपनाया जाता है वह इससे कुछ भिन्न होता है।
1. पुस्तक के आधार पर भाषा सीखने की प्रवृत्ति |
2. सरल से कठिन सूत्र पर आधारित!
3. वातावरण का अन्तर।
(4) पाठ्य पुस्तक की रचना में अन्तर - हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों में हिन्दी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ायी जाती है इसलिये पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी पाठ्य पुस्तक अलग-अलग होनी चाहिए।
(5) अन्य भाषा शिक्षक के लिये द्वि-भाषी होना आवश्यक - मातृभाषा शिक्षक यदि केवल एक भाषा का ही ज्ञाता है तो भी शिक्षण समुचित ढंग से चल सकता है। किन्तु अन्य भाग (विदेशी) के रूप में हिन्दी शिक्षण के लिये शिक्षक का द्वि-भाषी होना आवश्यक है इसलिये अन्य भाषा-शिक्षण मातृभाषा शिक्षण से अधिक कठिन माना जाता है।
(6) शिक्षण विधि में अन्तर - मातृभाषा अध्यापन विधि एवं अन्य भाषा अध्यापन विधि में पर्याप्त अन्तर होता है। मातृभाषा बोलना तो बालक सामाजिक वातावरण से ही सीख लेता है किन्तु अन्य भाषा सिखाते समय इस कमी को दूर करने के लिये ऐसी विधियों का आश्रय लेना पड़ता है जिससे भाषा सीखने के लिये कक्षा में ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर दिया जाये ताकि बालक भाषा को बार-बार सुनकर भाषा के गठन से परिचित हो जाये।
(7) मातृभाषा व विदेशी भाषा के रूप में हिन्दी-शिक्षण के स्तर में अन्तर - अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी का जो स्तर होगा, यह हिन्दी भाषी प्रदेशों में नहीं होगा। मातृभाषा के रूप में हिन्दी का स्तर ऊँचा होगा और अन्य भाषा के रूप में हिन्दी का स्तर अपेक्षाकृत उतना ऊँचा होगा। साधारणत- अहिन्दी प्रदेशों में चौथी कक्षा से हिन्दी पढ़ना प्रारम्भ किया जाता है जबकि मातृभाषा के रूप में हिन्दी सिखाना हिन्दी-भाषी प्रदेशों में पहली कक्षा से ही प्रारम्भ कर दिया जाता है।
|
|||||