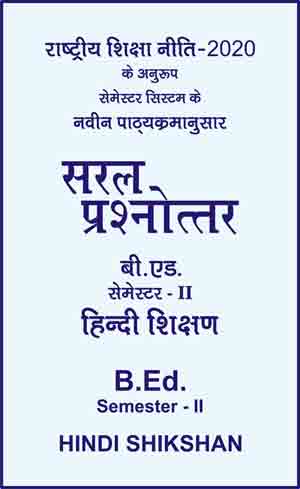|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- राबर्ट मेगर विधि को समझाइये। कुछ उदाहरणों से हिन्दी शिक्षण के उद्देश्यों के व्यावहारिक रूप को समझाइये |
उत्तर-
राबर्ट मेगर ने 1962 में अभिक्रमित अनुदेशन के लिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने की विधि का विकास किया। शिक्षण के अनुदेशन के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए राबर्ट मेगर विधि को उत्तम माना जाता है क्योंकि इसका विकास ही मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन के लिए किया है। मेगर तथा स्किनर दोनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। मेगर की विधि का शिक्षण तथा अनुदेशन के उद्देश्यों और मिलर की विधि का शिक्षण तथा अनुदेशन के उद्देश्यों और मिलर की विधि का प्रशिक्षण के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए अधिक प्रयोग होता है।
मेगर विधि (Method of Megar) से उद्देश्यों को लिखना
मेगर के विचार में उद्देश्यों की व्यावहारिक रूप में निम्नलिखित रूप से लिखा जाना चाहिए-
1. सर्वप्रथम, अन्तिम व्यवहार (Terminal Behaviour) को उनके नाम से परिभाषित करना चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार को स्पष्ट करना चाहिए जिसे इस बात के साक्षी के रूप में स्वीकार करेंगे कि सीखने वाले ने उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है।
2. दूसरे, वांछित व्यवहार को उन महत्त्वपूर्ण दशाओं में जिनके अन्तर्गत वांछित व्यवहार उत्पन्न होने की सम्भावना हो परिभाषित करना चाहिए।
3. तीसरे, स्वीकार किये जाने योग्य व्यवहार को परिभाषित करना चाहिए।
यद्यपि उपरोक्त दोनों कथन सदैव आवश्यक नहीं होते, किन्तु नये अध्यापकों को इनका अनुसरण करना चाहिए।
राबर्ट मेगर की विधि से उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना
उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए मेगर ने भी ब्लूम के वर्गीकरण का ही उपयोग किया है। मेगर ने उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप देने के लिए 'कार्य सूचक क्रियाओं' (Action Verbs) की सूची तैयार की है।
ज्ञानात्मक उद्देश्यों की क्रियाओं की सूची अग्रलिखित तालिका में प्रस्तुत की गई है-
ज्ञानात्मक उद्देश्यों की क्रियाओं की सूची
| उद्देश्य | कार्य सूचक क्रियाएँ (Action Verbs) | ||
| 1. ज्ञान | परिभाषित करना कहना सुनना नाम देना |
लिखना प्रत्यास्मरण करना अभिज्ञान करना चिपकाना |
रेखांकित करना चयन करना पुन-उत्पन्न करना मापन करना |
| 2. बोध | सिद्ध करना उचित कारण बतलाया चुनना प्रकट करना |
व्याख्या करना चित्र में लाना नाम देना सूत्र रूप में कहना |
व्याख्या करना निर्णय करना वर्गीकरण करना |
| 3. प्रयोग | भावी बातें बतलाना चुनना मूल्यांकन करना व्याख्या करना |
चुनना पाना दिखाना प्रदर्शित करना |
रचना करना गणना करना प्रयोग करना निष्पादन करना |
| 4. विश्लेषण | विश्लेषित करना सिद्ध करना निष्कर्ष निकालना भेद करना |
चयन करना पृथक करना तुलना करना अन्तर करना |
उचित कारण बताना हल करना आलोचना करना |
| 5. संश्लेषण | मिलाना दोबारा वर्णन करना सारांश करना संक्षेप करना |
सिद्ध करना वाद-विवाद करना संगठित करना एकीकरण करना |
चुनना सम्बन्ध रखना सामान्यीकरण निष्कर्ष करना। |
| 6. मूल्यांकन | निर्णय करना मूल्यांकन करना निश्चय करना आलोचना करना |
सहारा देना बचाना धावा करना |
सिद्ध करना त्याग करना चुनना |
पाठ्य-वस्तु तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस सूची में से समुचित क्रिया का चयन किया जाता है। पाठ्य-वस्तु के विशिष्ट तत्त्व के लिए उद्देश्य की समुचित क्रिया को प्रयुक्त करने के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप दिया गया है।
इस प्रकार व्यावहारिक उद्देश्य के तीन प्रमुख तत्त्व होते हैं-
(1) पाठ्य-वस्तु के तत्त्व का स्वरूप निश्चित करना।
(2) उद्देश्यों का निर्धारण करना।
(3) समुचित क्रिया का सूची में से चयन करना।
उदाहरणार्थ- अनुदेशन की पाठ्य वस्तु' अभिप्रेरणा' और उसका तत्त्व' अभि-प्रेरणा का अर्थ ' है। उद्देश्य ज्ञान तथा बोध उद्देश्य के लिए समुचित क्रिया परिभाषित करना है।
इन तत्त्वों के मिलने के उद्देश्य का व्यावहारिक रूप निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है-
(1) छात्र अलंकार की परिभाषा कर सकते हैं। (ज्ञान उद्देश्य)
(2) छात्र अलंकार की पहचान कर सकते हैं। (बोध उद्देश्य)
इसी प्रकार अभिक्रमक अपने 'प्रकरण' के अनुदेशन के निर्माण के लिए उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिख सकता है। अर्थशास्त्र में आवश्यकता के अनुदेशन के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में निम्न प्रकार से लिख सकते हैं-
| क्र. सं. | उद्देश्य | व्यावहारिक रूप |
| 1. | ज्ञान | छात्र'अलंकार' की परिभाषा कर सकते हैं। |
| 2. | बोध | छात्र 'अलंकार' का वर्गीकरण कर सकते हैं। |
| 3. | प्रयोग | छात्र अलंकार की पहचान कर सकते हैं। |
| 4. | विश्लेषण | छात्र अलंकार में भेद कर सकते हैं। |
| 5. | संश्लेषण | छात्र अलंकार का चयन कर सकते हैं। |
| 6. | मूल्यांकन | छात्र अलंकार का आकलन कर सकते हैं। |
संज्ञा तथा सर्वनाम के लिए उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है-
| क्र. सं. | उद्देश्य | व्यावहारिक रूप |
| 1. | ज्ञान उद्देश्य | छात्र 'संज्ञा' तथा 'सर्वनाम' के सम्बन्ध में कथन दे सकते हैं। |
| 2. | बोध उद्देश्य | छात्र संज्ञा तथा सर्वनाम का उदाहरण दे सकते हैं। |
| 3. | प्रयोग उद्देश्य | वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम उपयोग कर सकते हैं। |
| 4. | विश्लेषण उद्देश्य | छात्र संज्ञा तथा सर्वनाम की वाक्यों में पहचान कर सकते हैं। |
| 5. | संश्लेषण उद्देश्य | छात्र संज्ञा तथा सर्वनाम का अपने वाक्य में उपयोग कर सकते हैं। |
| 6. | मूल्यांकन उद्देश्य | छात्र संज्ञा तथा सर्वनाम के उपयोग के सम्बन्ध में निर्णय ले सकते हैं। |
मेगर विधि की सीमायें
उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने में मेगर विधि की निम्नलिखित सीमायें हैं-
1. मेगर विधि को क्रियात्मक उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
2. मेगर की क्रियाओं की सूची में समान क्रियाओं को विभिन्न उद्देश्यों के लिए सम्मिलित किया गया है। इससे उद्देश्यों में विभेदीकरण नहीं किया जा सकता है।
3. मेगर के व्यावहारिक रूप मानसिक क्षमताओं की अपेक्षा क्रियाओं को ही महत्त्व दिया जाता है।
4. मेगर की ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उद्देश्यों की क्रियाओं की सूचियों में अधिकांश क्रियायें दोनों में एक ही हैं इसलिए ज्ञानात्मक तथा भावात्मक उद्देश्यों के व्यावहारिक रूप में भेद नहीं किया जा सकता है।
5. मेगर अधिगम की उद्दीपन तथा अनुक्रिया के रूप में व्याख्या करता है जबकि मानव अधिगम को उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है।
|
|||||