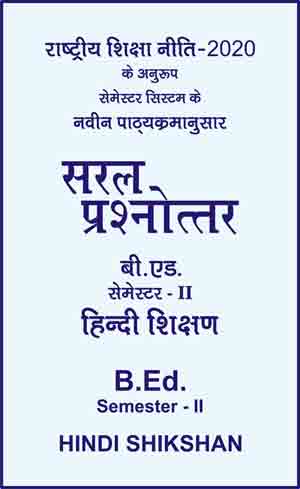|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- शब्द रचना से क्या अभिप्राय है? हिन्दी में शब्दों की रचना करने में किन-किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? विस्तृत विवेचन कीजिए।
अथवा
हिन्दी शब्द रचना पर एक लेख लिखिए।
उत्तर-
भाषा का निर्माण सीधे ही ध्वनियों द्वारा नहीं हो जाता। सबसे पहले अनेक ध्वनि समूह से सार्थक शब्दों की रचना की जाती है और फिर उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते समय कुछ परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है और वे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर पद कहलाते हैं तथा पदों को व्यवस्थित क्रम से प्रयोग किये जाने पर वाक्य बनता है जो कि किसी की भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होता है। वाक्यों के समूह से भाषा को आकार व रूप प्रदान होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ध्वनियों से शब्द, शब्दों से पदों, पद से वाक्यों का निर्माण करते समय व्याकरण की कुछ सुनिश्चित प्रक्रियाएँ होती हैं।
व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट उत्पत्ति। कोई शब्द किसी धातु में कौन-सा प्रत्यय लगने से बना है- इसका विवेचन करना ही व्युत्पादन है। जिस धातु से कोई शब्द बनता है उसे प्रकृति' कहते हैं। इस प्रकार संस्कृत के सभी शब्द प्रकृति तथा प्रत्यय के योग से बनते हैं। उदाहरण के लिए 'वेद' शब्द 'ज्ञान' अर्थ में प्रयुक्त विद् धातु में अच् प्रत्यय लगने से बना है। वेदना, विद्या, विद्यार्थी शब्द इसी विद् धातु से बने हैं।
भाषा की पूरी व्याकरणिक प्रक्रिया शब्द-रचना और रूपायन पर आधारित हैं। अतः यहाँ इन दोनों का भेद समझना आवश्यक है। व्युत्पादन केवल शब्दों की व्युत्पत्ति या शब्द निर्माण प्रक्रिया तक सीमित है। शब्दों की संरचना कृदन्त और तद्वित प्रत्ययों के योग से होती है। जो प्रत्यय क्रियाओं के मूल धातु रूप में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का निर्माण करते हैं, वे कृदन्त प्रत्यय कहलाते हैं, यथा संस्कृत की 'दा' धातु का अर्थ है देना। इसमें 'ता' (तृच्) कृदन्त प्रत्यय लगने से दा + ता = दाता शब्द बनता है। दृश् धातु का अर्थ है देखना। इसमें अनीय प्रत्यय लगने से दृश् + अनीय = दर्शनीय शब्द बनता है।
तद्धित प्रत्यय वे हैं जो मूल धातुओं में नहीं लगते। वे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम शब्दों में लगकर नये शब्द बनाते हैं। इस प्रकार कृदन्त प्रत्यय धातुओं से शब्द बनाते हैं और तद्वित प्रत्यय शब्दों से शब्दों का निर्माण करते हैं, यथा पुष्प + इत= पुष्पित, कुशल + ता = कुशलता। स्पष्ट है। कृदन्त क्रियाओं के संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का निर्माण होता है और तद्वित प्रत्ययों से शब्दों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार जहाँ कृदन्त का कार्य समाप्त होता है, वहाँ से तद्धित का कार्य प्रारम्भ होता है। उदाहरण के लिये संस्कृत की 'दय्' धातु का अर्थ है दया करना। दय्' धातु है अर्थात् क्रिया का मूल रूप है। इसमें कृदन्त प्रत्यय आलु' लगने से दय् + आलु = 'दयालु' विशेषण बनता है। अब इस 'दयालु' विशेषण में तद्धित प्रत्यय 'ता' जोड़ने से दयालु + ता = 'दयालुता' भाववाचक संज्ञा - शब्द बनता है।
इस प्रकार धातुओं से कृदन्त प्रत्यय लगाकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाने और फिर शब्दों में तद्धित प्रत्यय लगाकर संज्ञा, विशेषण आदि नये शब्द बनाने की सारी शब्द- निर्माण प्रक्रिया व्युत्पादन के क्षेत्र में आती है। ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुए बिना भाषा नहीं बनते, क्योंकि भाषा केवल शब्दों का ढेर नहीं है। शब्दों को भाषा बनने के लिए वाक्यों में प्रयुक्त होने योग्य बनना पड़ता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। 'पद' बनने पर शब्द में लिंग, वचन, पुरुष के अनुरूप विभक्तियाँ और प्रत्यय लगते हैं तभी शब्दों के रूप बनता है। छात्रा, पाठशाला, पढ़ाना शब्द तो हैं, किन्तु भाषा या वाक्य नहीं। वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए लिंग, वचन के अनुरूप इनके रूप बनाने होंगे, यथा छात्राओं को पाठशालाओं में पढ़ाया जाता है। यह पद निर्माण और वाक्य रचना का कार्य क्षेत्र रूपायन के अन्तर्गत आता है। अतः जहाँ व्युत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण होती है वहाँ से रूपायन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है।
हिन्दी शब्दों के व्युत्पादन के कृदन्त और तद्धित प्रत्ययों के अतिरिक्त उपसर्गों का भी विशेष योग है। यह ध्यान देने योग्य है कि हिन्दी के शब्द भंडार का बहुत बड़ा भाग संस्कृत शब्दावली से सम्पन्न है, किन्तु साथ ही देशज, विदेशी शब्दों से विकसित हिन्दी की अपनी शब्दावली भी विपुल है। अतः हिन्दी शब्दों के व्युत्पादन में संस्कृत के उपसर्गों तथा कृदन्त और तद्धित प्रत्ययों के अतिरिक्त हिन्दी के अपने उपसर्ग और कृदन्त तथा तद्वित प्रत्यय भी प्रचुर हैं।
1. उपसर्ग और शब्द- रचना हिन्दी में चार प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। हिन्दी शब्दों के व्युत्पादन में इन चारों प्रकार के उपसर्गों की उल्लेखनीय भूमिका है। यहाँ इन चारों के कुछ नमूने प्रस्तुत हैं-
(क) संस्कृत से लिए गये उपसर्ग और शब्द रचना - संस्कृत में अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत्, उद्, उप, परि, दुर्, प्र, वि, सम्, सु, प्रति, दुस्, नि, निर्, निस, परा 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों के योग से संज्ञा और विशेषण शब्द निर्मित हुए हैं।
संज्ञा शब्द-रचना-
(1) अधि - 'अधि उपसर्ग से 'अधिकार, अधिनायक, अध्यक्ष, अधिपति, अधिष्ठाता, अधिकरण, आदि संज्ञा शब्द बनते हैं।
(2) अनु - 'अनु' उपसर्ग से अनुशासन, अनुग्रह, अनुवाद, अनुराग, अनुसन्धान, अनुकरण, अनुमान, अनुचर, अनुशीलन आदि संज्ञा-शब्द बनते हैं।
(3) अप - इससे अपवाद, अपयश, अपकार, अपहरण, अपशब्द, अपव्यय, अपमान, अपशकुन आदि संज्ञा-शब्द बनते हैं।
(4) अभि - 'अभि' उपसर्ग से अभिमत, अभिमान, अभिलाषा, अभ्युदय, अभियोग, अभिभावक, अभियान, अभिशाप आदि संज्ञा शब्द बनते हैं।
(5) आ - इससे आरम्भ, आगमन, आकाश, आकर्षण, आक्रमण, आदान, आकार, आरोह, आक्रोश आदि संज्ञा शब्द निर्मित होते हैं।
विशेषण- शब्द रचना-
(1) सु - 'सु' उपसर्ग से सुकर्म, सुशील, सुयश, सुमंगल, सुडौल, सुकन्या, सुशिक्षित, सुपुत्र सुगम आदि अनेक विशेषण बनते हैं। -
(2) दुर् - 'दुर्' उपसर्ग से दुर्जन, दुर्गम, दुर्बल, दुर्बुद्धि, दुर्लभ, दुर्मति, दुराचारी, दुर्भेद्य आदि विशेषण बनते हैं।
(ख) हिन्दी के उपसर्ग और शब्द रचना - हिन्दी के उपसर्ग प्रायः संस्कृत के उपसर्गों से बिगड़कर बने हैं। इसके साथ ही हिन्दी के अपने भी उपसर्ग हैं। हिन्दी के संज्ञा शब्दों के निर्माण में तो अधिकांशतः संस्कृत उपसर्गों का ही आश्रय लिया गया है, किन्तु संस्कृत उपसर्गों पर आधारित विशेषणों के अतिरिक्त कुछ नये विशेषण बनाने की दिशा में हिन्दी के उपसर्गों का विशेष योगदान है।
(1) अ - 'अ' उपसर्ग से अलग, अटल, अडिग, अमर, अजर, अपढ़, अमोल अशान्त, अनाथ, अबला आदि विशेषण बनते हैं।
(2) अन् - 'अन' उपसर्ग से अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनदेखी, अनहोनी, अनमेल आदि विशेषण निर्मित होते हैं।
(3) अध - 'अध उपसर्ग से अधपका, अधमरा, अधजला, अधखिला, अधकचरा, आदि विशेषण बनते हैं।
(4) बिन - 'बिन' उपसर्ग से बिनदेखा, बिनचखा, बिनब्याहा आदि विशेषण बनते हैं।
(5) भर - 'भर' उपसर्ग से भरपूर, भरपेट, भरमार, भरसक विशेषण बनते हैं।
(ग) उर्दू (अरबी-फारसी) के उपसर्ग और शब्द रचना - हिन्दी में अरबी-फारसी के लगभग 20 उपसर्ग व्यवहार में लाये जाते हैं। इन उपसर्गों से हिन्दी के अनेक संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है।
संज्ञा शब्द-रचना-
(1) हर - 'हर' उपसर्ग से हरघड़ी, हररोज, हरसाल, हरहाल, हरकाम, हरइंसान आदि संज्ञा शब्द बनते हैं।
(2) बद - 'बद' उपसर्ग से बदबू बदहज्मी, बदनामी, बदकिस्मती, बदतमीजी, बदमाशी आदि संज्ञा - शब्द निर्मित होते हैं।
विशेषण शब्द रचना-
(1) बे - 'बे' उपसर्ग से बेईमान, बेइज्जत, बेरहम, बेकसूर, बेवकूफ, बेकार, बेचारा, बेअक्ल आदि अनेक विशेषण बनते हैं।
(2) गैर - 'गैर' उपसर्ग से गैरहाजिर, गैरकानूनी, गैरजिम्मेदार आदि विशेषण बनते हैं। (3) ना 'ना' उपसर्ग से नापसन्द, नालायक, नासमझ, नाराज, नाबालिग आदि विशेषण बनते हैं।
(घ) अंग्रेजी उपसर्ग और शब्द रचना - अंग्रेजी के अनेक उपसर्ग व्यावहारिक हिन्दी में प्रचलित है। इन प्रत्ययों में Deputy (हिन्दी में डिप्टी ) Vice (वाइस), Head (हैड), Sub (स्नान), Semi (सेमी) आदि विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं।
(1) डिप्टी - डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलक्टर।
(2) वाइस - वाइस चान्सलर, वाइस प्रिंसिपस, वाइस प्रेसिडेण्ट।
(3) हैड - हैड क्लर्क, हैड - मास्टर।
(4) सब - सब जज, सब-इंस्पैक्टर।
(5) सेमी - सेमी-फाइनल, सेमी- गवर्नमैन्ट।
2. प्रत्यय और शब्द - रचना जो अक्षर या अक्षर-समूह शब्द के अन्त में लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर एक नये शब्द की रचना करता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। हिन्दी में प्रत्यय को दो वर्गों में बांटा जा सकता है.
(अ) कृदन्त प्रत्यय और शब्द रचना - कृदन्त प्रत्यय मूल धातुओं के पश्चात् लगते हैं। हिन्दी में तीन प्रकार के कृदन्त प्रत्यय प्रचलित हैं-
(क) संस्कृत के कृदन्त प्रत्यय और शब्द रचना - हिन्दी शब्द-भंडार की अधिकांश शब्दावली संस्कृत भाषा से आयी है। इनमें से अधिकतर संज्ञा तथा विशेषण शब्द कृदन्त प्रत्ययों के योग से ही निर्मित हैं। यहाँ संज्ञा व्युत्पादन और विशेषण व्युत्पादन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-
संज्ञा शब्द-रचना -
(1) क्तिन् (ति) - कृ + क्तिन् = कृति, भज् + क्तिन् = भक्ति।
(2) इन् (इ) कृष् + इन = कृषि, रुच् + इन् = रुचि।
विशेषण शब्द-रचना-
(1) अनीय - दृश् + अनीय दर्शनीय, रम् + अनीय = रमणीय।
(2) चर - वन + चर = वन चर, नभ + चर = नभचर।
(ख) हिन्दी के कृदन्त प्रत्यय और शब्द रचना - हिन्दी के कृदन्त प्रत्ययों से हिन्दी के अनेक संज्ञा विशेषण शब्दों का निर्माण हुआ है। क्रिया पदों के निर्माण में भी इनकी महती भूमिका है।
संज्ञा शब्द-रचना-
(1) आई - चढ़ना + आई = चढ़ाई, पढ़ना + आई = पढ़ाई, लिखना + आई = लिखाई
(2) आहट - चिल्लाना + आहट = चिल्लाहट, घबराना + आहट = घबराहट
( 3 ) औती - मनाना + औती = मनौती, छुड़ाना + औती = छुड़ौती, चुनना + औती = चुनौती।
विशेषण शब्द रचना-
(1) अवना - सुहाना + अवना = सुहावना, लुभाना + अवना = लुभावना, डराना + अवना = डरावना
(2) यल - अड़ना + यल = अड़ियल, सड़ना + यल सड़ियल, मरना + यल = मरियल
(3) आऊ - टिकना + आऊ = टिकाऊ, बिकना + आऊ = बिकाऊ, चलना + आऊ = चलाऊ।
क्रिया शब्द रचना - हिन्दी की क्रियाओं के वर्तमानकालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक रूप भी कृदन्त प्रत्ययों के योग से ही बनते हैं, यथा-
(1 ) ता - पीता, खाता, पढ़ता, लिखता, आता, जाता आदि।
(2) आ - पढ़ा लिखा, भोगा, त्यागा, जला मिला, खिला आदि।
(3) या - लिया, दिया, पिया, बोया, सोया, खोया आदि।
( 4 ) एगा - जाएगा, खाएगा, पिएगा, लिखेगा, पढ़ेगा आदि।
(ग) उर्दू (अरबी-फारसी) के कृदन्त प्रत्यय-
(1) इश - कोशिश, मालिश, फरमाइश, परवरिश आदि।
(2) ई - आमदनी, खुशी, नेकी, दोस्ती।
( 3 ) इन्दा - शर्मिन्दा, बाशिन्दा, जिन्दा, परिन्दा आदि।
(आ) तद्धित प्रत्यय और शब्द रचना - तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में लगते हैं, धातुओं में नहीं लगते हैं। ये निम्नलिखित रूपों में मिलते है-
(क) संस्कृत के तद्वित प्रत्यय और शब्द रचना - हिन्दी का विपुल शब्द भंडार संस्कृत के तद्वित प्रत्ययों के योग से निर्मित है। यहाँ नमूने के रूप में कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-
संज्ञा शब्द-रचना-
(1 ) ता - कुशलता, लघुता, गुरुता, मधुरता, सुन्दरता, समता, निजता आदि।
(2) त्व- गुरुत्व, सतीत्व, पुरुषत्व, विप्रत्व, निजत्व आदि।
विशेषण शब्द रचना-
(1) इक - वार्षिक, हार्दिक, मासिक, दैनिक, सैनिक, शारीरिक आदि।
(2) इल - पंकिल, फेनिल, तन्द्रिल, जटिल, कुटिल आदि।
(ख) हिन्दी के तद्वित प्रत्यय और शब्द रचना - हिन्दी के तद्वित प्रत्ययों के योग से अनेक प्रकार के संज्ञा, विशेषण शब्द निर्मित होते हैं।
संज्ञा शब्द-रचना-
(1) आई - भलाई, बुराई, चतुराई, सच्चाई आदि।
(2) पा - बुढ़ापा, मुटापा, रंडापा आदि।
(3) ई - तोली, माली, धोबी आदि
(4) पन - बचपन, लड़कपन, पागलपन, छुटपन, कालापन आदि।
विशेषण शब्द रचना-
(1) आ - भूखा प्यासा, प्यारा, न्यारा, मैला, थैला, कसैला।
( 2 ) वन्त - गुणवन्त, शीलवन्त दयावन्तं ज्ञानवन्त धनवन्त आदि।
(3) ईला - संजीला, लजीला, रंगीला, नशीला, रसीला आदि।
(ग) उर्दू (अरबी-फारसी) के तद्धित प्रत्यय और शब्द रचना - उर्दू के तद्धित प्रत्ययों का हिन्दी भाषा के शब्द भंडार के निर्माण में विशेष योगदान है। उर्दू के लगभग तीस तद्वित प्रत्यय हिन्दी भाषा के शब्दों के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। इनसे संज्ञा शब्द भी निर्मित होते हैं और विशेषण भी। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-
संज्ञा शब्द रचना
(1) आना - नजराना, हर्जाना, दस्ताना, जुर्माना आदि।
(2) कार - काश्तकार सलाहकार, पेशकार।
(3) गार - मददगार, यादगार, गुनहगार।
(4) दार - तीमारदार, थानेदार, वफादार, जमींदार, ईमानदार। विशेषण शब्द रचना -
(1) वार - उम्मीदवार, माहवार, तारीखवार आदि।
(2) आना - मर्दाना, रोजाना, जानना, सालाना आदि।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी शब्दों के व्युत्पादन में संस्कृत, हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्गों का महत्वपूर्ण योग है। संस्कृत के कृदन्त प्रत्ययों के साथ हिन्दी और उर्दू (अरबी-फारसी) कृदन्त प्रत्ययों के योग से हिन्दी की बहुत-सी शब्दावली निर्मित हुई है। इस प्रकार संस्कृत हिन्दी और उर्दू के तद्धित प्रत्ययों के योग से हिन्दी के कितने ही संज्ञा और विशेषण शब्द निर्मित हुए हैं।
समस्त पद - 'समस्त पद का अर्थ है समास से युक्त पद। समास का अर्थ है संयोजन या मेल। परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मूल को समास कहते हैं। अधिकतर समस्त पद दो पदों के मेल से बनते हैं। दो पदों के मेल का उदाहरण है 'राजपुरुष' अर्थात् राजा का पुरुष। इसमें राजा और पुरुष के मेल में तीसरा शब्द बना है राजपुरुष। राजपुरुष बनने में 'राजा' का 'राज' बन गया है तथा राजा और पुरुष के मध्य का 'का' लुप्त हो गया है। आशय यह है कि नये शब्द के निर्माण में कुछ आन्तरिक परिवर्तन घटित हुआ है।
वास्तविकता यह है कि सन्धियों की भाँति समास भी शब्द व्युत्पादन प्रक्रिया के अंग हैं। समस्त पद दो या तीन पदों के योग से निर्मित होने पर भी एक ही पद के रूप में अपने व्याकरणिक दायित्व का निर्वाह करते हैं। उदाहरण के लिए पुरुष जा रहा है' और 'राजपुरुष जा रहा है' में व्याकरणिक दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। यही बात 'यह संघ का कार्यालय है' और 'यह विश्वविद्यालय अध्यापक संघ का कार्यालय है' पर लागू होती है।
समास के मूल प्रयत्न लाघव की प्रेरणा निहित है। 'समास' का एक अर्थ संक्षेपीकरण भी है। अतः समास में लाघव की प्रवृत्ति निहित है।
समास की प्रवृत्ति सभी भाषाओं में पायी जाती है। अंग्रेजी में The boy of the school' कहने के स्थान पर 'School boy' कहना सुविधाजनक है। 'English-speaking course', 'Uni- versity - students welfare-association', 'poverty-line' अग्रेजी समस्त पदों के उदाहरण हैं। हिन्दी शब्द-भंडार में संस्कृत के अधिकतर समस्त पद तो समाहित हैं ही, साथ ही नये समस्त पदों की संख्या भी अत्यधिक है। 'मुँहतोड़', 'घुड़दौड़, अनपढ़, अछूता, दहीबड़ा, दुरंगा, दाल-भात, चौराहा, भरपेट, डाकगाड़ी, अमचूर, सिरदर्द, रेखांकित, बीचो-बीच, मनचाहा आदि हिन्दी के अपने समस्त पद हैं।
1. तत्पपुरुष समास - जिस समास में अर्थ की दृष्टि से पूर्वपद गौण और उत्तरपद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के मध्य आने वाले परसर्गों (विभक्तियों) का लोप हो जाता है। इस समास में कर्त्ता और सम्बोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्तियाँ पूर्वपद और उत्तरपद के मध्य लुप्त रहती है। जिस कारक की विभक्ति लुप्त होती है, उसी के नाम पर तत्पुरुष का नामकरण होता है, यथा-
1. कर्म तत्पुरुष - दिवंगत (दिव को गत ), गिरहकट (गिरह को काटना)
2. करण तत्पुरुष - ईश्वर प्रदत्त (ईश्वर द्वारा प्रदत्त )
3. सम्प्रदान तत्पुरुष - सत्याग्रह (सत्य के लिए आग्रह )
4. अपाद्यन तत्पुरुष - पथभ्रष्ट (पथ से भ्रष्ट )
5. सम्बन्ध तत्पुरुष - गंगाजल (गंगा का जल)
6. अधिकरण तत्पुरुष - आनन्दमग्न ( आनन्द में मग्न)
(क) नञ् तत्पुरुष-
जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, उसे नञ् समास कहते हैं, यथा-
अभाव (न भाव)
असम्भव ( न सम्भव )
अपूर्ण (न पूर्ण)
अज्ञान (न ज्ञान)
अनन्त (न अन्त)
(ख) अलुक तत्पुरुष - जिस समस्त पद में प्रथम पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, वह अलुक तत्पुरुष कहलाता है। यथा युधिष्ठिर में युधि ( युद्ध में) में सप्तमी विभक्ति लुप्त नहीं है, अतः युधिस्थिर = युधिष्ठिर ( युद्ध में स्थिर रहने वाला)। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं-
वाचस्पति = वाचस् (वाणी का ) + पति (स्वामी)
विश्वम्भर = विश्वम् (विश्व को ) + भर (पोषित करने वाला)
मृत्युञ्जय = मृत्युम् (मृत्यु को) + जय ( जीतने वाला)
खेचर = खे (आकाश में) + चर (विचरने वाला)
मनसिज = मनसि (मन में) + ज ( जन्म लेने वाला)
सरसिज = सरसि (सर में) + ज ( जन्म लेने वाला)
(ग) मध्यम पदलोपी तत्पुरुष - जिस तत्पुरुष समास में पूर्वपद और उत्तरपद के मध्य के पद लुप्त हो जाते हैं, उसे मध्यमपद लोपी तत्पुरुष कहते हैं, यथा-
पर्णकुटीर = पर्ण ( पत्तों) से बना कुटीर
बैलगाड़ी = बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी
रेलगाड़ी रेल (Rails = पटरी) पर चलने वाली गाड़ी
गोबरगणेश = गोबर से बना हुआ गणेश
दहीबड़ा = दही में डूबा हुआ बड़ा
पनचक्की = पानी से चलने वाली चक्की
2. कर्मधारय समास - जिस समास में उत्तरपद प्रधान हो तथा पूर्वपद और उत्तरपद में उपमान- उपमेय अथवा विशेषण- विशेष्य सम्बन्ध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है।
(क) विशेषण - विशेष्य सम्बन्ध-
नील गाय = नीली है जो गाय.
पीताम्बर = पीत (पीला) है जो अम्बर (वस्त्र)
सद्धर्म = सत् (सच्चा) जो धर्म
महादेव = महान है जो देव
(ख) उपमान - उपमेय सम्बन्ध-
कमलनयन = कमल के समान नयन
चन्द्रमुख = चन्द्र के समान मुख
घनश्याम = घन (मेघ) के समान श्याम
कुसुमकोमल = कुसुम के समान कोमल
(ग) उपमेय-उपमान सम्बन्ध-
देहलता = देहरूपी लता
मुखचन्द्र = मुखरूपी चन्द्र
विद्याधन = विद्यारूपी धन
चरणकमल = चरणरूपी कमल
ग्रन्थरत्न = ग्रन्थरूपी रत्न
3. द्विगु समास - जिस समास में पूर्वपद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूहवाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं, यथा-
चौमासा = चार मासों का समूह
सतसई = सात सौ (दोहों) का समूह
चौराहा = चार राहों का समूह
पंचवटी = पाँच वटों का समूह.
त्रिभुवन = तीन भुवनों का समूह
नवग्रह = नौ ग्रहों का समूह
4. द्वन्द्व समास - जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तथा दोनों के मध्य के अव्यय पद का लोप हो, उसे द्वन्द्व समास कहते हैं, यथा-
माता-पिता = माता और पिता
नर-नारी = नर और नारी
गंगा-यमूना = गंगा और यमुना
राजा-प्रजा = राजा और प्रजा
देश-विदेश = देश और विदेश
5. बहुब्रीहि समास - जिस समास में पूर्वपद और उत्तरपद में से कोई भी पद प्रधान न हो, वरन् कोई न अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहतें हैं, यथा-
चन्द्रशेखर = चन्द्र है शेखर पर जिसके (शिव)
दशानन = दश हैं आनन जिसके (रावण)
गजानन = गज का है आनन जिसका (गणेश)
चक्रधर = चक्र को धारण करता है जो (विष्णु)
लम्बोदर = लम्बा है उदर जिसका (गणेश)
गिरिधर = गिरि को धारण करने वाला (कृष्ण)
6. अव्ययीभाव समास - जिस समास में पूर्वपद प्रधान हो तथा अव्यय हो तथा जिसके योग से समस्त पद अव्यय का रूप ले ले, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं, यथा-
यथाशक्ति = शक्ति के अनुसार
प्रतिदिन = दिन-दिन
हररोज = रोज-रोज
भरपेट = पेट भरकर
आजन्म = जन्म से लेकर
आजीवन = जीवनपर्यन्त
समासों के स्वरूप से स्पष्ट है कि भाषा में कसाव और संक्षिप्तता की क्षमता लाने की पद्धति है। समासों से भाषा की अनेक शब्दों को एक शब्द में समेटने की समाहार शक्ति बढ़ती है, पदों में तो पूरा पदबन्ध या उपवाक्य ही समाया रहता है। 'लम्बोदर' कहते ही उन गणेश जी का बोध होता है 'लम्बा है उदर जिसका। इसी प्रकार 'बैलगाड़ी' कहने से 'बैलों' द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी का बोध होता है। 'यथाशक्ति' में शक्ति के अनुसार- क्रिया विशेषण पदबन्ध समाया हुआ है।
जैसे-जैसे किसी लेखक की भाषा का स्तर ऊंचा होता जाता है उसके लेखन में सन्धि और समास से युक्त शब्दों की संख्या बढती जाती है तथा वाक्यों में पदबन्धों अथवा उपवाक्यों के संयोजन की प्रवृत्ति और क्षमता में विकास होता जाता है। सन्धि और समास का क्षेत्र शब्द व्युत्पादन है तो उपवाक्यों और पदबन्धों का क्षेत्र वाक्य रचना हैं।
|
|||||