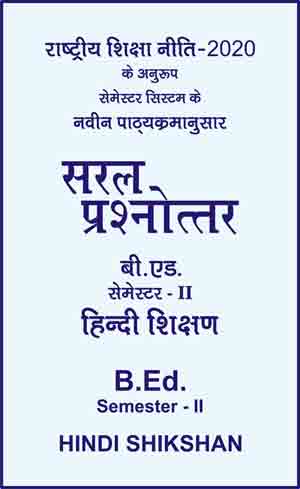|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षणसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 हिन्दी शिक्षण - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- विराम चिन्हों के प्रकारों की विवेचना कीजिये।
उत्तर-
विराम चिन्हों के प्रकार - हिन्दी भाषा में विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है या अनुकरण किया गया है।
प्रमुख विराम चिन्हों के प्रकार या रूप निम्नलिखित हैं-
(1) पूर्ण विराम = ।
(2) अल्प विराम = ,
(3) अर्द्ध विराम = ;
(4) प्रश्न चिन्ह = ?
(5) सम्बोधन या विस्मयादि = !
(6) कोष्ठक = ( )
(7) निर्देशक (डैश) = -
(8) अवतरण चिन्ह = '-'
(9) विवरण चिन्ह = : -
(10) योजनक का विराम =-
(1) पूर्ण विराम (।) अथवा, या का प्रयोग - जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तब उसके अन्त में पूर्ण विराम लगाया जाता है। एक वाक्य के अन्तर्गत कई उपवाक्य भी होते हैं परन्तु विराम चिन्ह मुख्य वाक्य के अन्त में ही लगाया जाता है, जैसे-
आज विद्यालय में शिक्षकों की एक सभा होगी, जिसमें आपको भी आना है। कविता में दोहे की प्रथम पंक्ति के अन्त में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, चौपाई के आधे भाग के बाद पूर्ण विराम तथा चौपाई के अन्त में दो पूर्ण विराम प्रयुक्त किये जाते हैं। पूर्ण विराम के बाद पाठक को कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है यह अन्तराल सबसे अधिक होता है।
(2) अल्प-विराम (,) का प्रयोग - यह न्यूनतम विराम का द्योतक है। अन्य विरामों की तुलना में इसका प्रयोग अधिक होता है। इसका प्रयोग प्रायः नीचे लिखे स्थानों पर किया जाता है- वाक्य में समान पादी शब्दों को पृथक करने के लिए; जैसे- श्याम अपनी भूमि, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा और मान-मर्यादा सभी कुछ खो बैठा।
वाक्यों में प्रयुक्त युग्म शब्दों को एक-दूसरे से पृथक करने के लिए अर्द्ध विराम जैसे पाप पुण्य, और सर्दी और गर्मी, हर्ष और विषाद, रात और दिन, सब ईश्वर की देन हैं।
जब एक ही शब्द भेद के दो शब्दों के बीच समुच्चय बोधक न हो तो उन्हें पृथक करने के लिए; अर्द्ध विराम जैसे आजकल अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में लोग घास, पात से पेट भर रहे हैं।
समानाधिकरण शब्दों के मध्य में; जैसे- पं. मोतीलाल के पुत्र भारत के प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनतन्त्रातिक राज्य व्यवस्था के संस्थापक थे।
यदि उद्देश्य बहुत अधिक लम्बा हो तो उसके पश्चात् ; जैसे चारों ओर से आने वाले घुड़सवारों के घोड़ों की हिन-हिनाती हुई आवाजें, दूर-दूर तक फैल रही थीं।
पढ़ते समय वाक्य में जिस स्थान पर अल्प समय के लिए रुकना पड़े; जैसे वह चुपचाप शान्त लेटा हुआ था, न कुछ बोलता था, न आँखें खोलता था और न किसी बात का उत्तर- देता था।
यदि सम्बोधन शब्द वाक्य के प्रारम्भ में हो तो सम्बोधन शब्द के बाद और यदि सम्बोधन शब्द वाक्य के मध्य में हो तो उसके पूर्व और पश्चात् दोनों स्थलों पर ; जैसे-
उदाहरण- राम, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है, यहाँ आओ, राम तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
जब एक ही वर्ग के तीन या अधिक शब्द आयें और उनके मध्य विकल्प से समुच्चय बोधक रहे, तो अन्तिम शब्द को छोड़कर शेष शब्दों के पश्चात् ; जैसे-
उदाहरण- मुझे वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, पुष्कर और द्वारिकापुरी की तीर्थ यात्रा करनी है।
जब एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति है; जैसे आओ-आओ, शीघ्र आओ, वहाँ नहीं वहाँ नहीं, तुम यहाँ बैठो।
एक ही क्रिया की पुनरावृत्ति न कर उक्त क्रिया के स्थान पर ; जैसे-
उदाहरण- तुम इलाहाबाद होकर दिल्ली गये, मैं आगरा होकर।
उद्धरण चिन्ह के पूर्व ; जैसे श्याम ने कहा, राम, मैंने समाज सेवा का अब व्रत ले लिया है। उपाधियों को अलग करने के लिए; जैसे- शास्त्री, साहित्याचार्य, एम. ए.।
किसी वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए; जैसे तीन-तीन भाषाओं के समावेश से, मैं समझता हूँ, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम बहुत बोझिल हो जायेगा।
हाँ या नहीं के पश्चात् ; जैसे- हाँ, तुम्हारा कहना सही है। नहीं, तुम्हारा कहना सही नहीं है।
क्रिया विशेषण या वाक्यांशों को अलग करने के लिए; जैसे भारतीय मनीषियों ने, समय-समय पर, विचार के क्षेत्र में विश्व का पथ-प्रदर्शन किया है।
संज्ञा उपवाक्य को छोड़कर मिश्रित उपवाक्य के शेष बड़े उपवाक्यों के बीच में; जैसे- विद्यार्थी को स्वर्ण पदक मिला, क्योंकि उसने इस विश्वविद्यालय की एम. ए. परीक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था।
(3) अर्द्ध विराम (;) का वाक्यों में प्रयोग - अर्द्ध विराम का प्रयोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकने के लिए होता है ये पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह होता है।
इसी नियम के पश्चात् आने वाले उदाहरण सूचक 'जैसे' शब्दों के पहले; जैसे- स्त्रियों के नामों के साथ प्राय- देवी शब्द का प्रयोग करते हैं; जैसे- गायत्री देवी।
जब संयुक्त वाक्य के मुख्य या प्रधान उपवाक्यों में परस्पर विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है उन्हें पृथक करने के लिए; जैसे- आज जिसे हम मित्र समझते हैं कल वही हमारा शत्रु हो सकता है; आज जिसे हम चाहते हैं, कल उससे घृणा कर सकते हैं।
समानाधिकरण वाक्यों के मध्य में; जैसे महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन को नया मोड़ दिया; उन्होंने सत्याग्रह का एक नया अस्त्र दिया; उन्होंने ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया।
मिश्रित अथवा संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच में; जैसे लोग उसे गालियाँ देते; वह उन्हें अपना प्यार देता; लोग उस पर पत्थर फेंकते; वह उनके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता।
(4) प्रश्न सूचक (?) चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग - इसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के अन्त में होता है; जैसे- तुम कहाँ जा रहे हो?
यदि एक वाक्य में कई प्रश्नवाचक उपवाक्य हों और वे एक ही प्रधान उपवाक्य पर अवलम्बित हों तो ऐसे प्रति उपवाक्य के अन्त में अल्प विराम के चिन्ह का प्रयोग करके सबसे अन्त में अर्थात् प्रधान उपवाक्य के पश्चात् इसका प्रयोग होता है; जैसे तुमने, यह कार्य क्यों किया, तुम कहाँ चले गये थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम किन लोगों के साथ खेल रहे थे, तुम अपना जीवन नष्ट करने पर क्यों तुले हो?
यदि वाक्य के अन्त में कहीं सन्देहात्मक या व्यंग्यात्मक भाव प्रकट किया जाये तो कभी-कभी कोष्ठक के भीतर प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग होता है; जैसे- 'गरीबी हटाओ' का संकल्प पूरा होगा (?)
(5) विस्मय सूचक (!) चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग - हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, भय, प्रार्थना, आज्ञा आदि मनोवेग सूचक वाक्यों, शब्दों के अन्त में; जैसे- हाय!बेचारा कुचल गया!वाह!क्या बात है!छी!धोखा देते हो!
प्रश्नवाचक वाक्यों के अन्त में, जहाँ मनोवेग प्रदर्शित होता है; जैसे- सुनते क्यों नहीं, क्या बहरे हो!
मनोवेग की क्रमशः वृद्धि दिखाने के लिए दो या तीन विस्यमयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं; जैसे - ऐ लड़के!मित्रों!
(6) निर्देशक (-) चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग - समानाधिकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में; इन कविताओं से नैतिक मूल्यों, राष्ट्र प्रेम, बलिदान, कर्त्तव्यपालन आदि की शिक्षा मिलती है।
किसी वाक्य के प्रवाह में अवरोध होने पर अथवा भाव निर्देशक चिन्ह परिवर्तन होने पर जैसे- मैंने तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया पर अब यह सब करने से क्या लाभ!
किसी के वाक्य को उद्धृत करने के पूर्व, जैसे-
शिक्षक किन छात्रों ने काम पूरा कर लिया है?
निम्नांकित है या निम्नलिखित है के बाद; जैसे हमारे देश के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी निम्नांकित हैं- भगत सिंह, चन्द्रशेखर, बिस्मिल, राजगुरु आदि।
किसी शब्द की व्याख्या करने के लिए; जैसे- ईश्वर सब कुछ देता है- जीवन, संतति, सुख, सम्पत्ति आदि।
किसी अवतरण के बाद और उसके लेखक के पूर्व; जैसे- 'देखिए रूप नाम अधीनां' तुलसीदास।
(7) कोष्ठक ( ) चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग - क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ; जैसे-
(i) संज्ञा,
(ii) सर्वनाम-
(क) भारत,
(ख) पाकिस्तान।
समानार्थी शब्द या वाक्यांश के साथ; जैसे- अफ्रीका में नीग्रो (हब्शी) अधिकतर उन्हीं की सन्तान है। ज्ञान राशि (विचारों का समूह) के संचित कोष का नाम ही साहित्य है।
किसी रचना का रूपान्तर करने में बाहर से लगाये गये शब्दों के साथ; जैसे इन्द्र (आनन्द से) अच्छा, देव सेना सज्जित हो गयी।
(8) अवतरण या उद्धरण (" ") चिन्ह का वाक्यों में प्रयोग - किसी का कथन उद्धृत करने में अथवा कहावतों में; जैसे ऋषियों ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी ऊँचा पद दिया था - "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादीप गरीयसी"। उस बालक की कुशाग्रता देखकर लोग यही कहते थे कि "होनहार बिरवान के होत चिकने पात"। तुलसीदास ने सत्य ही लिखा है-
"जासु राज पिय प्रजा दुखारी। सो नृप अवसि नरक अधिकारी। "
कभी-कभी पुस्तकों के नाम अथवा व्यक्तिवाचक नाम भी एकहरे अवतरण चिन्हों के भीतर लिखे जाते हैं; जैसे- नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'हिन्दी व्याकरण' भाषा के छात्रों के लिए उपयोगी पुस्तक है।
जब किसी अक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयोग अक्षर या शब्द के अर्थ में होता है; जैसे - हिन्दी में 'ल' का प्रयोग नहीं होता। चारों ओर से 'पकड़ो-पकड़ो' की आवाज आ रही थी।
(9) विवरण चिन्ह (--) का वाक्य में प्रयोग - किसी विषय अथवा बातों को समझाने के लिए . अथवा निर्देशन के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है; जैसे- क्रिया दो प्रकार की होती है-
(अ) अकर्मक,
(ब) सकर्मक।
(10) योजक या विभाजक चिन्ह' - ' का वाक्य में प्रयोग - उन तत्पुरुष एवं द्वन्द्व समासों में जब सन्धि या रूप परिवर्तन के कारण दोनों शब्द एक नहीं हो पाते; जैसे वर्णन-भेद, रूप-ज्ञान।
मध्य के अर्थ में; कालका-हावड़ा मेल, राम-रावण युद्ध। अक्षरों में लिखी जाने वाली संख्याओं और उनके अंशों के बीच में; जैसे एक-तिहाई, तीन-चौथाई।
पुनरुक्ति अथवा युग्म रूप में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है ऐसे शब्द संज्ञा विशेषण, क्रिया, क्रिया-विशेषण आदि पदों के रूप में हो सकते हैं।
संज्ञा - घर-घर, बच्चा-बच्चा।
विशेषण - काले-काले, लाल-लाल। क्रिया- पढ़ते-पढ़ते, हँसते-हँसते।
क्रिया-विशेषण - धीरे-धीरे, जल्दी-जल्दी।
विस्मय बोधक - छिः-छः, अरे-अरे, हाय-हाय!
अतिशय बोधक - पानी-पानी, बाग-बाग।
विराम चिन्हों के उचित प्रयोग के लिए छात्रों को लिखित रचना, शिक्षण के समय विविध अभ्यास दिये जा सकते हैं। विराम चिन्ह रहित वाक्यों एवं अनुच्छेदों को देकर उपयुक्त स्थलों पर विराम चिन्ह लगाने के लिए उन्हें कहना चाहिए। उनकी रचना-पुस्तिकाओं में अशुद्ध विराम चिन्ह प्रयोगों का संशोधन अवश्य करना चाहिए और उन्हें कक्षा में स्पष्ट कर देना चाहिए कि किस स्थान पर कौन-सा विराम चिन्हं शुद्ध और उपयुक्त है।
|
|||||