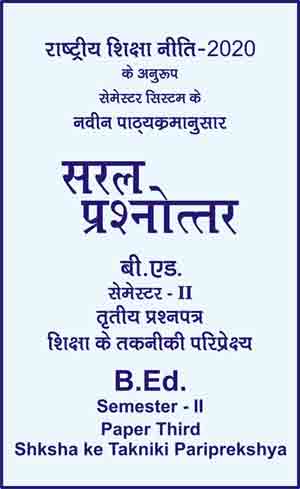|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्यसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- ई-लर्निंग के विभिन्न उपागमों, विभिन्न शैलियों, उपयोगिता एवं सीमाओं पर प्रकाश डालिए।
अथवा
'कम्प्यूटर सहायतित अधिगम' पर टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
ई-लर्निंग के विभिन्न उपागम
जिन-जिन क्षेत्रों में कम्प्यूटर ने प्रवेश कर लिया है, वहाँ वहाँ हर कार्य के नये उपागमों ने जन्म लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कम्प्यूटर के प्रवेश ने विभिन्न उपागमों से परिचित कर दिया है ई-लर्निंग के मुख्य उपागमों का वर्णन निम्नलिखित है-
(1) कम्प्यूटर आधारित अधिगम - आज के शैक्षिक वातावरण में कम्प्यूटर एक अनिवार्य सेवा मानी जा रही है। इस प्रणाली से अर्थ यह हैं कि वह शैक्षिक वातावरण जिसमें कम्प्यूटरों का प्रयोग विभिन्न शिक्षण कार्यों के लिए किया जाता है, परन्तु इस प्रणाली में कम्प्यूटर अनुभव जैसे खेल, इंटरनेट आदि का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत छात्र अपने-अपने विषयों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रोग्रामों में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि का प्रयोग किया जाता है।
(2) कम्प्यूटर समर्पित अधिगम - इसमें विभिन्न शैक्षिक कम्प्यूटर उपयोग शामिल हैं, जैसे ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटरिंग, सिमूलेटिंग तथा समस्या समाधान आदि। CAL का प्रचलन 1959 से हुआ। शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक अनुदेशन की तुलना में CAL अधिक प्रभावशाली है। CAL में कम्प्यूटर विद्यार्थी के साथ सीधे अन्तर्क्रिया करता है। यह विद्यार्थी को सीधे अनुदेशन प्रदान करता है। CAL से निम्न प्रकार के पाठों को प्रदान किया जा सकता है-
(i) ड्रिल और अभ्यास - CAL में यह सबसे सरल प्रकार्य है, जिसे सीखा जाता है। इसमें अधिगमकर्ताओं को समस्याएँ और प्रश्न प्रस्तुत किये जाते हैं तथा उनकी अनुक्रिया प्राप्त की जाती है। अधिगमकर्ताओं की प्रतिक्रियाएँ तत्काल सही की जाती हैं।
(ii) ट्यूटोरियल प्रकार - इसमें सूचना को छोटी-छोटी इकाइयों में प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थी के उत्तर का कम्प्यूटर विश्लेषण करता है तथा आवश्यक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। यदि कम्प्यूटर में अधिक कार्यक्रम होंगे तो वे व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से उतने ही अधिक उपयोगी होंगे।
(iii) अनुकरणीय प्रकार - इसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के लघु रूप का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इसमें वास्तविक अभ्यास का बिना किसी खतरे के अभ्यास का अवसर मिलता है। अधिगमकर्ता के सामने विभिन्न आँकड़े किसी वास्तविक परिस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा इन्हें देखकर विभिन्न निर्णय लेने के लिये कहा जाता है।
(iv) खोज प्रक्रिया - इसमें आगमनात्मक उपागम का उपयोग किया जाता है। परन्तु समस्या को विद्यार्थी मूल और प्रयास विधि द्वारा उसे हल करने का प्रयास करता है।
(v) खेल प्रकार - यह प्रकार अनुदेशनात्मक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यह अधिकतर मनोरंजनात्मक उद्देश्य के लिए होता है। कई बार खेलों के द्वारा शिक्षण किया जाता है।
(vi) समस्या समाधान प्रकार - इस उपागम में अधिगमकर्ता समस्या समाधान के लिए उत्पन्न कार्यक्रम स्वयं बनाता है तथा शैक्षिक मूल्य को अधिगमकर्ता अर्जित करता है। समस्या का हल ही अंतिम पृष्ठपोषण होता है।
इस प्रकार CAL में सूचनाएँ एवं संचार तकनीकी के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
(3) अधिगम प्रबन्धन प्रणाली - इस अधिगम प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयरों का निर्माण किया जाता है, जिनका प्रयोग शिक्षा के विस्तार एवं प्रबन्धन में किया जाता है। किसी नये विषय या कोर्स के निर्माण के दौरान सभी आवश्यक तत्वों के प्रबन्धन, उनके संचालन, मूल्यांकन तथा सम्बन्धित आँकड़ों को सुरक्षित रखने को महत्व प्रदान किया जाता है। इस कार्य के लिए विभिन्न भंडारण यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- सी.डी., फ्लॉपी, पेन ड्राइव, डी.वी.डी. आदि। इनका प्रयोग विद्यार्थी अपने कम्प्यूटरों पर करके सीखते हैं।
अधिगम प्रबन्धन विद्यार्थियों संसाधन प्रदान करने से तथा मूल्यांकन करने से संबंधित है। अभ्यास के लिए विद्यार्थियों को तैयार कर लिया जाता है। इस प्रकार का पृष्ठपोषण अलग-अलग विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं।
(4) कम्प्यूटर समर्थित मूल्यांकन - कम्प्यूटर समर्थित मूल्यांकन को ई-मूल्यांकन का नाम भी दिया जाता है। जब कम्प्यूटर यह अनुदेशन और अधिगम प्रचलित हो चुके हैं तब उन परिस्थितियों में कम्प्यूटर समर्थित मूल्यांकन या ई-मूल्यांकन का होना भी आवश्यक हो जाता है। इस ई-मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों के विषय एवं स्तर के अनुसार विभिन्न बहु-विकल्पी प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। छात्र इन प्रश्नों के कम्प्यूटर के मॉनीटर पर देखता है तथा अपनी अनुक्रिया रिकॉर्ड करता है। इसमें मूल्यांकन के परिणाम भी तत्काल प्राप्त हो जाते हैं तथा तत्काल ही प्रतिपुष्टि हासिल हो जाती है।
ई-लर्निंग की सम्प्रेषण प्रणालियाँ - ई-लर्निंग की विभिन्न शैलियाँ निम्नलिखित होती है-
(1) समकालिक सम्प्रेषण शैली - सम्प्रेषण की इस प्रकार की शैली में शिक्षण और विद्यार्थी दोनों को ही शिक्षा-अधिगम प्रक्रिया के सम्पादन हेतु आवश्यक सम्प्रेषण के लिए एक समय विशेष में एक साथ इंटरनेट पर मौजूद रहना पड़ता है। इस प्रकार का सम्प्रेषण अध्यापक और विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की आवश्यक सूचना तथा अधिगम सामग्री की भली-भाँति भागेदारी करने के अत्यधिक अवसर प्रदान करता है। इस दौरान छात्र अपनी शंकाओं के निवारण हेतु प्रश्न पूछ सकता है। इस प्रकार अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में छात्रों से प्रश्न पूछ सकता है।
(2) अतुल्यकालिक सम्प्रेषण शैली - इस शैली के अंतर्गत कोर्स या पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचनाएँ तथा अधिगम अनुभव सीखने वाले को ई-मेल द्वारा भेजे जाते हैं। ये सूचनाएँ सी.डी., डी.वी.डी., ब्लॉग्स या वेब पेज के रूप में उपलब्ध रहती है। इस दृष्टि से सम्प्रेषण के लिए अध्यापक और विद्यार्थी का एक समय विशेष पर, एक स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। इसके अंतर्गत अध्ययन सामग्री पहले से ही मौजूद रहती है। अधिगमकर्ता इस सामग्री का अपनी सुविधानुसार तथा अपनी गति से और किसी भी समय अध्ययन कर सकता है। वह उत्पन्न कार्य ई-मेल द्वारा अध्यापक को भेज सकता है तथा अध्यापक भी अपनी सुविधानुसार विद्यार्थी को पृष्ठपोषण भेज सकता है।
ई-लर्निंग की उपयोगिता ई-लर्निंग की उपयोगिताएँ निम्नलिखित होती हैं-
(1) लचीलापन - ई-लर्निंग में लचीलापन होता है, जो कि इसकी विशेषता एवं उपयोगिता है। ई-लर्निंग में विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे- सीडी, डीवीडी, मोबाइल फोन इत्यादि।
(2) स्वगति - विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकता है। इसके लिए ई-लर्निंग में विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं ऐसे अवसरों की उपलब्धता जिनमें विद्यार्थी विषय-वस्तु की जितनी बार चाहे उतनी बार ही पुनरावृत्ति करना, पाठ्य-वस्तु के किसी भी हिस्से पर जितनी देर चाहे वह रुक सके।
(3) गुणात्मक अधिगम सामग्री - ई-लर्निंग के द्वारा सबसे उत्तम अधिगम सामग्री विद्यार्थियों तक पहुँचायी जा सकती है। कई बार तो यह सामग्री परम्परागत सामग्री से भी बढ़िया होती है। इसमें बढ़िया सामग्री का भंडारण होता है, जिसका लाभ असंख्य विद्यार्थी उठा सकते हैं ।
(4) सार्वभौमिकरण - ई-लर्निंग उच्च कोटि का अनुदेशन तथा अधिगम अनुभव दुनिया के हर कोने में बैठे असंख्य विद्यार्थियों तक पहुंचाने का उत्तम उपागम माना जाने लगा है। इस उपागम द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों का तथा संसाधनों के अभाव का सामना करने में सहायता मिलती है।
(5) एक जैसी शिक्षण - ई-लर्निंग उपागम के द्वारा सभी विद्यार्थी समान अधिगम एवं प्रशिक्षण के अवसर प्राप्त करते हैं चाहे वे किसी भी स्थान, संस्कृति, प्रांत या देश से जुड़े हों।
(6) आवश्यकताओं के अनुसार सीखना - ई-लर्निंग में सीखने वालों की आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, दक्षता, स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप अधिगम अनुभव प्रदान करने की क्षमता पर्याप्त मात्रा में होती है।
(7) करके सीखने में सहायक - अनुकरणीय शिक्षण तथा करके सीखने में ई-लर्निंग का विशेष योगदान रहता है। ई-लर्निंग में जब तक विद्यार्थी स्वयं कुछ नहीं करता है तब तक वह कुछ भी नहीं सीख पाता। ई-लर्निंग अधिगम प्रक्रिया को जीवंत रूप प्रदान करने की क्षमता रखती है।
(8) सुविधानुसार सीखना - आज के व्यस्त समय में ई-लर्निंग की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है - उन विद्यार्थियों के लिये जो परम्परागत कक्षा - शिक्षण से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते, कारण चाहे कुछ भी हो सकता है। साधन-विहीनता की स्थिति में ई-लर्निंग अधिगम में बहुत सहायक सिद्ध होती है।
(9) अवसरों की विभिन्नता - ई-लर्निंग के दौरान विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा अभिप्रेरणा को उनके अधिगम में ठीक प्रकार से बनाये रखने में ई-लर्निंग बहुत उपयोगी है। ई- लर्निंग उनके अधिगम से अनुभव प्राप्त करने के अवसरों में पर्याप्त विभिन्नता ला सकती है
(10) उचित मूल्यांकन में सहायक - ई-लर्निंग में अधिगम का मूल्यांकन करने का भी उचित प्रावधान होता है। इस जाँच को अधिगमकर्ता स्वयं भी कर सकता है तथा अध्यापक द्वारा भी यह जाँच की जा सकती है। इस मूल्यांकन से विद्यार्थियों को उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण प्रदान करने में भी मदद मिल सकती है।
ई-लर्निंग के दोष या सीमाएँ - जैसा कि सर्वविदित है कि ई-लर्निंग अभी अपनी शैशवावस्था में ही है, अतः इसके दोष एवं सीमाएँ भी स्वाभाविक हैं। ये सीमाएँ निम्नलिखित हैं-
(1) प्रत्यक्ष अन्तःक्रिया का अभाव - ई-लर्निंग में परम्परागत कक्षा शिक्षण की भाँति मेल-जोल के अवसर नहीं होते। विद्यार्थी न तो अपने साथियों से मिल पाते हैं और न ही अपने माता-पिता से। अधिगमकर्ता अलग-थलग पड़ जाते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता।
(2) आधुनिक सुविधाओं का अभाव - ई-लर्निंग का तभी लाभ हो सकता है यदि अधिगमकर्ताओं को सभी सुविधाएँ प्रदान की जायें, जैसे- लैपटॉप, कम्प्यूटर, मल्टीमीडिया, इंटरनेट आदि। ये सुविधाएँ स्कूल तथा घर में मिलनी चाहिए। लेकिन ये सभी सुविधाएँ पर्याप्त नहीं।
(3) कुशलता का अभाव - ई-लर्निंग में विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इंटरनेट, कम्प्यूटर तथा वेब टेक्नोलॉजी को उपयोग करने की कुशलता रखते हैं। तभी ई-लर्निंग का वे लाभ उठा पायेंगे। लेकिन इस कुशलता का पर्याप्त अभाव देखने को मिलता है।
(4) प्रशासनिक उदासीनता - प्रशासनिक स्तर पर भी उदासीनता देखने को मिलती है। स्कूलों में तथा घरों में ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं हो पातीं। कुछ गिनती के चुने हुए पब्लिक स्कूलों में ही ऐसी व्यवस्थाएँ हो पाई हैं जिनमें ई- लर्निंग की व्यवस्था संभव हो सकी।
(5) नकारात्मक दृष्टिकोण - ई-लर्निंग का सम्प्रत्यय नया-नया होने के कारण इसके समर्थन में अभी अधिकतर लोगों का दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाया है। अधिकतर लोग इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही रखते हैं जो कि ई-लर्निंग को अपनाने में बाधक सिद्ध होता है।
(6) शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव - ई-लर्निंग नवीन सम्प्रत्यय होने के कारण इससे पूर्णरूप से परिचित होने में कुछ समय लगेगा। इस सम्बन्ध में वांछित कौशलों का भी अभाव है। इन अभावों के होते हुए ई-लर्निंग को लोकप्रिय बनाना किस प्रकार से संभव हो सकता है।
|
|||||