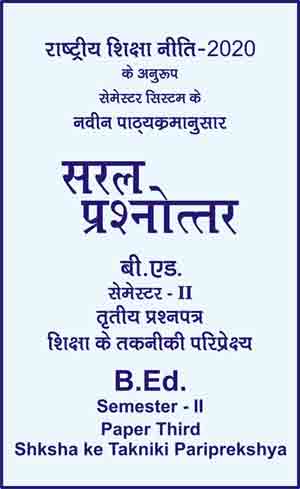|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्यसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 तृतीय प्रश्नपत्र - शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता एवं सीमाओं की विवेचना कीजिये।
उत्तर-
सूचना और सम्प्रेषण तकनीकी से आजकल आमतौर पर अभिप्राय है- विचारों या आँकड़ों का कम्प्यूटर आधारित प्रबन्धन।
विस्तृत अर्थ में, सम्प्रेषण और सूचना तकनीकियाँ वे आधार हैं, जिनकी सहायता से मानव जाति ने दूसरे जानवरों से स्वयं को अलग किया है।
सूचना और सम्प्रेषण तकनीकी की कोई सर्वसम्मति से स्वीकार्य कोई परिभाषा नहीं क्योंकि इसमें प्रयुक्त तकनीकियाँ आदि नित दिन बदल रही हैं। यह परिवर्तन बहुत ही तेज गति से हो रहे हैं। ICT का सम्बन्ध डिजिटल आँकड़ों से तथा इनके भंडारण, पुनःप्राप्ति, संचारण तथा प्राप्ति से होता है।
ICT में 'C' से अभिप्राय है - आँकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दूर तक सम्प्रेषण। इसे हम आँकड़ों को भेजने और प्राप्त करने हेतु विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने वाले नेटवर्क के प्रयोग द्वारा इस उद्देश्य को अर्जित किया जाता है। ये नेटवर्क भी विभिन्न वर्गों में बाँटे जा सकते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क जिसे ऑफिस बिल्डिंग के भीतर ही लिंक किया जाता है, वाईड एरिया नेटवर्क जैसे इंटरनेट जिसे बहुत विस्तृत क्षेत्र से जोड़ा जाता है।
LAN में जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें ऑफिस में सम्बद्ध कर दिया जाता है। जैसे इनपुट और आऊटपुट यंत्र एवं कम्प्यूटर प्रोसेसिंग। LAN का उद्देश्य होता है - हार्डवेयर सुविधाओं को आपस में बाँटना। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एवं आँकड़े। ऐसा नेटवर्क बहुत ही उपयोगी होता है, जिसमें ऑफिस में सभी सहयोगी सामान्य आँकड़ों या कार्यक्रम तक पहुँचना चाहते हैं।
ICT व्यापक संदर्भ में - ICT को विस्तृत या व्यापक संदर्भ में प्रयोग करने के लिए हमें निम्न शब्दों पर ध्यान देना होगा-
(1) सूचना की प्रकृति - ICT में 'I' से अभिप्राय है। सूचना जिसमें शामिल है, सूचना का अर्थ एवं मूल्य सूचना को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ICT की सीमाएँ आदि।
(2) सूचना का प्रबंधन - इसमें शामिल किया जाता है- आँकड़ों को कैसे प्राप्त किया जाता है, प्रभावशाली प्रयोग के लिए उसका कैसे सत्यापन और भंडारण किया जाता है, व्यवस्था, प्रोसेसिंग और सूचना का वितरण। सूचना को सुरक्षित रखना, सूचना को बाँटने के लिए नेटवर्क डिजाइन करना।
(3) सूचना प्रणालियों की व्यूह रचना - इससे यह विचार किया जाता है कि ICT का व्यापार या संगठन में लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किया जाये। इस प्रकार हम देखते हैं कि ICT में वह कोई भी उत्पाद शामिल होगा जो सूचना को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल रूप में भंडारण, पुनः उत्पादन, व्यवस्थित, स्थानान्तरण या ग्रहण करेगा। जैसे - व्यक्तिगत कम्प्यूटर, डिजिटल टेलीविजन, ई-मेल, रोबोट, वीडियो तथा ऑडियो कान्फ्रेंसिंग, डिजिटल लाइब्रेरी आदि।
शिक्षा में सूचना एवं सम्प्रेषण की उपयोगिता - शिक्षा के क्षेत्र में ICT की उपयोगिता निम्नलिखित है-
(1) भंडारण - ICT के प्रयोग द्वारा सूचनाओं का भंडारण करना सुगम हो गया है। इस भंडारण के कारण सूचनाओं की प्राप्ति भी सुगम हो गई है। सूचनाओं की प्राप्ति एवं भंडार के परिणामस्वरूप समस्याओं के समाधान में भी सहायता मिलती है। उदाहरणार्थ इंटरनेट का प्रयोग। इंटरनेट तो आजकल सूचनाओं का भंडार सिद्ध हो रहा है। सी.डी., डी.वी.डी., फ्लॉपी आदि भी सूचनाओं के भंडारण में योगदान करती हैं। इन सभी साधनों के विकास के परिणामस्वरूप पुस्तकालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। विभिन्न पुस्तकालयों की पुस्तकों को ई-पुस्तकों के रूप में बदलकर इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक इन पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं।
(2) विदेशी भाषाओं का अधिगम - विदेशी भाषाओं को सीखने के लिये केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसके लिये ICT का प्रयोग प्रभावी सिद्ध हो रहा है। इस सम्बन्ध में भाषा - प्रयोगशालाएँ, दूरसंचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया स्पीकरों आदि का प्रयोग संभव हो पाया है। इस दृष्टि से भाषाओं को सीखना, विशेषकर विदेशी भाषाओं को सीखना अब उतना कठिन नहीं रह गया।
(3) शैक्षिक अनुसंधान - आजकल ICT ने अनुसंधान कार्य को अधिक सरल बना दिया है। हर, अनुसंधान कार्य में विशेष प्रकार की तथा विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ तथा आवश्यकताएँ बाधित होती हैं। शर्त यह भी है कि ये सूचनाएँ वास्तविक और विश्वसनीय होनी चाहिये। क्योंकि अनुसंधान कार्य में से परिणाम निकालने में इन सूचनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ICT द्वारा इन सूचनाओं को प्राप्त करके अनुसंधान कार्य को शीघ्रता से अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है। अतः अनुसंधान के क्षेत्र में ICT का सहयोग दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है।
(4) प्रबन्धन - आजकल प्रबन्धन, नियोजन किसी भी क्षेत्र का हो, ICT के सहयोग के बिना निसहाय से दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबन्धन ICT पर आधारित हो रहा है तथा इसका प्रयोग प्रबंधकों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। प्रबंधन में भी विभिन्न सूचनायें चाहिए कि ICT द्वारा क्षेत्रों में उपलब्ध हो जाती हैं। जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधन का कार्य अधिक सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलती है। स्कूलों में प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ, पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचनाएँ, शोध कार्य सम्बन्धी सूचनाएँ तथा अध्यापकों के वेतन आदि सम्बन्धी सूचनाएँ ICT के माध्यम से कुछ ही क्षणों में आँखों के सम्मुख आ जाती हैं।
(5) शिक्षण प्रक्रिया - ICT द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों द्वारा अध्यापक पाठ्य वस्तु को अधिक जीवन्त बना कर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी की सहायता से दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग बहुत ही सजीव ढंग से किया जा सकता है। कम्प्यूटर के प्रयोग से अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को बेहतर ढंग से विद्यार्थियों तक पहुँचा सकता है। इस दृष्टि से अध्यापक बाल-केंद्रित शिक्षा के उद्देश्य को इस माध्यम में प्राप्त कर सकता है।
(6) विशिष्ट बालकों की शिक्षा - विशिष्ट बालकों को शिक्षा प्रदान करना इतना सरल कार्य नहीं है, क्योंकि ये बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। विशेषकर अधिगम की दृष्टि से। लेकिन ICT के बढ़ते हुए प्रयोग ने इन बालकों की शिक्षा को एक नया मोड़ दिया है। सम्प्रेषण की नई विधियों व उपकरणों की सहायता से विशिष्ट बालकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रक्रिया कुछ हद तक सरल हो गई है और प्रभावशाली भी। मूक व बधिर बालकों के लिये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अच्छा तरीका है। नेत्रहीन बच्चों के लिए ब्रेल लिपि पर आधारित कम्प्यूटरों का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार इनके लिये सॉफ्टवेयरों द्वारा भी इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है।
(7) पूर्व-प्राथमिक शिक्षा पूर्व - प्राइमरी स्तर की शिक्षा में ICT का प्रवेश भी प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। इन छोटे बच्चों की शारीरिक गतिशीलता के लिये अनेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर प्रयोग बच्चों को खेल ही खेल में दिखाया जाता है। जिससे ये बच्चे विज्ञान के प्रति अपनी जिज्ञासा के विकास का प्रयत्न करते हैं।
(8) शिक्षा तंत्र में परिवर्तन - ICT ने पूरे शिक्षा तंत्र में क्रांति लाकर उसमें व्यापक परिवर्तन कर दिये हैं, जैसे-
(i) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की बजाय अधिगम प्रक्रिया को मुख्य केंद्र बना दिया है। इससे सक्रिय अन्तः क्रियाओं की संभावनाएँ बढ़ गई हैं।
(ii) कक्षा का वातावरण अरुचिकर और एकतरफा नहीं रह पाया।
(iii) विद्यार्थी सूचनाएँ अपने ढंग से प्राप्त कर सकता है तथा अपनी गति से सूचनाएँ प्राप्त कर सकता है।
(iv) इसमें इंटर-एक्टिव मॉडल का अधिकतम प्रयोग होता है अर्थात् अध्यापक और विद्यार्थी की अन्तर्क्रिया।
(v) विद्यार्थी पर ज्ञान अर्जन का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा अधिक हो गया है।
(vi) शिक्षकों की भूमिका में भी ICT ने परिवर्तन ला दिया है। अध्यापक ज्ञान के स्रोत न रहकर वे विद्यार्थी के साथ सक्रिय ज्ञान प्राप्त करने वाले साथी की भूमिका में आ गये हैं।
(vii) इस तकनीक का योगदान सेवाकालीन तथा सेवा पूर्व दोनों प्रकार की शिक्षण गतिविधियों में देखा जा सकता है।
सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी की सीमाएँ - ICT के उपयोग में कुछ कठिनाइयाँ भी आती हैं, जिनसे इसका उपयोग सीमित हो जाता है। ICT की मुख्य सीमाएँ निम्नलिखित हैं-
(1) ICT सम्बन्धी सूचनाएँ अभी इस देश के स्कूलों में पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि कई स्कूलों के लिये इन्हें खरीद पाना संभव ही नहीं और न ही उनकी देखभाल करना। इन परिस्थितियों में ICT का प्रयोग ऐसे स्कूलों में संभव नहीं।
(2) ICT का प्रयोग संदेह एवं डर पैदा करता है कि इस तकनीकी के प्रयोग से उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा।
(3) कुछ सीमा तक स्कूल के विद्यार्थी भी ICT का प्रयोग करने में रुचि नहीं रखे। ऐसा शायद ICT के ज्ञान के अभाव के कारण तथा उचित मार्गदर्शन के अभाव के कारण है।
(4) शिक्षक भी अपनी पुरानी पद्धति में परिवर्तन नहीं करना चाहते। वे रूढ़िवादिता में जकड़े रहना पसंद करते हैं।
(5) ICT में शिक्षकों के प्रशिक्षण के अभाव के कारण भी इसका प्रयोग स्कूलों में सीमित ही है। इसके लिये अध्यापकों को प्रशिक्षण स्तर पर ही तैयार करके ICT के प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सकता है।
(6) स्कूलों में उपलब्ध सीमित सूचनाओं की पृष्ठभूमि हमें इसी बात की ओर संकेत करती है कि अभी हमारे अधिकतर स्कूल ICT के प्रयोग के लिये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए।
(7) स्कूल प्रशासन, अधिकारी, मैनेजमेंट आदि भी स्कूलों में ICT के प्रयोग के बारे में 'संवेदनशील नहीं हैं। इस बारे में उनकी उदासीनता के परिणामस्वरूप ICT का प्रयोग सीमित - सा दिखाई देता है। इसका प्रचार तो बहुत है, लेकिन इसका प्रयोग अभी हर स्कूल की दहलीज पार नहीं कर पाया।
|
|||||