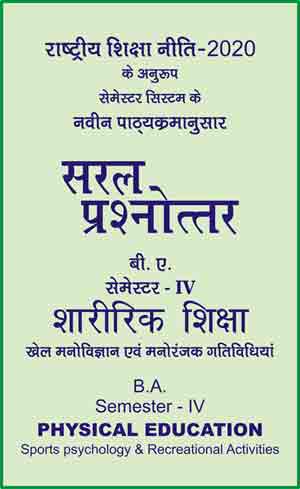|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- अभिप्रेरणा के स्त्रोत एवं सिद्धान्त की विवेचना कीजिए।
उत्तर-
अभिप्रेरणा के स्रोत
अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारम्भ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें अन्तर्नोद और प्रोत्साहन की भी अपनी ही भूमिका होती है। इसलिये अभिप्रेरणा के निम्न स्रोत हैं-
(1) आवश्यकताएँ - आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का द्योतक होती है। जैसे प्राणी के शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता अनुभव होना। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है- शारीरिक अथवा जैविक और मनो- सामाजिक। शारीरिक आवश्यकताओं में मनुष्य की शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकताएँ आती हैं, जैसे - भोजन, जल, वायु व मल-मूत्र विसर्जन आदि और मनो-सामाजिक आवश्यकताओं में मनुष्य में उसके सामाजिक पर्यावरण के कारण उत्पन्न मनो-सामाजिक आवश्यकताएँ आती हैं। जैसे आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर एवं अर्थ आदि। ये आवश्यकताएँ मनुष्य में तनाव उत्पन्न करती हैं और वह इनकी पूर्ति के लिये क्रियाशील हो जाता है और तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। जैसे भूख लगने पर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता अनुभव होती है, यह उसमें एक तनाव उत्पन्न कर देती है और इस तनाव के कारण वह भोजन की प्राप्ति के लिये क्रियाशील हो उठता है और यह तनाव की स्थिति उसमें तब तक रहती है जब तक उसे भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। बोरिंग और लैंगफील्ड ने आवश्यकता को तनाव के रूप में ही परिभाषित किया है। उनके शब्दों में - "आवश्यकता प्राणी के अन्दर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्यलक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है।"
(2) अन्तर्नोद या चालक - आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करती है, यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अन्तर्नोद अथवा चालक कहते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना एवं पानी की आवश्यकता होने पर प्यास लगना आदि। ये चालक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राणी को क्रियाशील करते हैं। जैसे - भूख लगने पर भोजन की तलाश करना और प्यास लगने पर पानी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। शेफर व अन्य के अनुसार "अन्तर्नोद या चालक वह शक्तिशाली एवं सतत् उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की माँग करता है।"
(3) प्रोत्साहन - प्रोत्साहन को उद्दीपन भी कहते हैं। प्रोत्साहन बाह्य वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न अन्तर्नोद अथवा चालक को शांत करती है, जैसे भूख की पूर्ति के लिये भोजन। भोजन भूख प्रेरक को शांत करने के संदर्भ में प्रोत्साहन है। इसी प्रकार काम चालक (Sex-Driver) का उद्दीपन / प्रोत्साहन है - दूसरे लिंग का व्यक्ति क्योंकि उसी से यह चालक संतुष्ट होता है। अतः हम बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बील्ड के शब्दों में यह कह सकते हैं कि - "उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है, जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करती है।"
हिलगार्ड - ने इसे निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है - "सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अन्तर्नोद की तीव्रता कम होती है।"
(4) प्रेरक - प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन/ प्रोत्साहन, चालक, तनाव व आवश्यकता सभी आ जाते हैं। गेट्स के अनुसार - "प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे - आवश्यकताएँ, इच्छाएँ, तनाव, स्वाभाविक स्थितियाँ, निर्धारित प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और स्थायी उद्दीपक आदि।"
प्रेरक क्या है? इस सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। कुछ इनको जन्मजात या अर्जित शक्तियाँ मानते हैं, कुछ इनको व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएँ मानते हैं और कुछ इनको निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियाँ मानते हैं। पर सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिये उत्तेजित करते हैं। वास्तव में प्रेरक ही व्यक्ति को उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं।
अभिप्रेरणा के सिद्धान्त
मानव व्यवहार तथा उसके कारणों का अध्ययन करके मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा के कई विभिन्न सिद्धान्तों को प्रतिपादित किया है। इनमें से कुछ मुख्य सिद्धान्त प्रस्तुत हैं
(1) मूल प्रवृत्ति का सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मैकडुगल ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, उसकी मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग ही अभिप्रेरकों का कार्य करते हैं। इस सिद्धान्त के संदर्भ में पहली बात तो यह है कि मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियों की संख्या के सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं और दूसरी बात यह है कि यह सिद्धान्त अपनी ही कसौटी पर खरा नहीं उतरता। मूल प्रवृत्तियाँ सभी मनुष्यों के समान होती हैं, तब उनका व्यवहार भी समान होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है।
(2) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के दो मूल कारक होते हैं - एक मूल प्रवृत्तियाँ और दूसरा अचेतन मन फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य के मूल रूप से दो ही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं - एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जो उसे क्रमशः संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक व्यवहार की ओर प्रवृत्त करती है। साथ ही उसका अचेतन मन उसके व्यवहार को अनजाने में प्रभावित करता है। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि फ्रॉयड की मूल प्रवृत्ति सम्बन्धी विचार ही मनोवैज्ञानिकों को मान्य नहीं है और दूसरी बात यह है कि मनुष्य का व्यवहार केवल उसके अचेतन मन से नहीं अपितु अर्द्धचेतन एवं चेतन मन से भी संचालित होता है।
(3) शरीर क्रिया सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मार्गन ने किया है। इनके अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपक द्वारा उत्पन्न नहीं होती अपितु उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है। इस सिद्धान्त में मनुष्य के पर्यावरणीय कारकों की अवहेलना की गई है। इसलिये यह भी अपूर्ण है।
(4) अन्तर्नोद सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएँ मनुष्य से कम तनाव पैदा करती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में अन्तर्नोद कहते हैं और ये अन्तर्नोद ही मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिये अभिप्रेरित करते हैं। यद्यपि आगे चलकर मनोवैज्ञानिकों ने इसमें शारीरिक आवश्यकताओं के साथ मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी जोड़ दिया। लेकिन फिर भी यह सिद्धान्त अपने से अपूर्ण ही है क्योंकि यह मानव के उच्च ज्ञानात्मक व्यवहार की व्याख्या नहीं करता।
(5) प्रोत्साहन सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन बोल्स तथा काफमैन ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है। पर्यावरण के इन सभी तत्वों को इन्होंने प्रोत्साहन माना है। इनके अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं-
(i) धनात्मक प्रोत्साहन
(ii) ऋणात्मक प्रोत्साहन
धनात्मक प्रोत्साहन जैसे - भोजन एवं पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिये धकेलते हैं जबकि ऋणात्मक प्रोत्साहन जैसे - दण्ड एवं बिजली का झटका आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। यह सिद्धान्त मनुष्य के केवल बाल कारकों पर ही बल देता है। इसलिये अपने में अपूर्ण है।
(6) माँग सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का प्रतिपादन मैसलो ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। मैसलो ने आवश्यकताओं को एक विशेष क्रम (निम्न से उच्च की ओर) में प्रस्तुत किया है। मैसलो के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर लेता दूसरे स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता। मैसलो की यह बात तो सही है किन्तु मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होते हैं पर उनकी यह बात सही नहीं है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी क्रम विशेष में करते हैं। अतः यह सिद्धान्त भी अपने में अपूर्ण है।
|
|||||