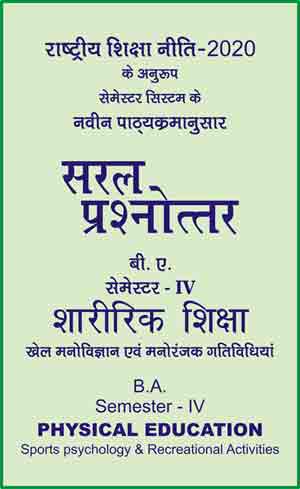|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 6
अभिप्रेरणा
(Motivation)
प्रश्न- प्रेरणा की परिभाषा लिखिए। खेल तथा शारीरिक शिक्षा में विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की विभिन्न प्रविधियों की चर्चा कीजिए।
अथवा
अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिये।
उत्तर-
प्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा
प्रेरणा के शाब्दिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों में अंतर है। 'प्रेरणा' के शाब्दिक अर्थ में हमें 'किसी कार्य को करने' का बोध होता है। इस अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को प्रेरणा कह सकते हैं क्योंकि उत्तेजना के अभाव में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सम्भव नहीं है। हमारी हर एक प्रतिक्रिया या व्यवहार का कारण कोई न कोई उत्तेजना अवश्य होती है। यह उत्तेजना आन्तरिक भी हो सकती है और बाह्य भी।
अंग्रेजी के 'मोटीवेशन' शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा की मोटम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है - मूव मोटर और मोशन।
मनोवैज्ञानिक अर्थ में 'प्रेरणा' से हमारा अभिप्राय केवल आन्तरिक उत्तेजनाओं से होता है, जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। इन अर्थ में बाह्य उत्तेजनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति है, जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह एक अदृश्य शक्ति है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर केवल इसका अनुमान लगाया जा सकता है।
क्रैच एवं क्रचफील्ड ने लिखा है- “प्रेरणा का प्रश्न, 'क्यों' का प्रश्न है ?" हम खाना क्यों खाते हैं, प्रेम क्यों करते हैं, धन क्यों चाहते हैं, काम क्यों करते हैं? इस प्रकार के सभी प्रश्नों का सम्बन्ध 'प्रेरणा' से है।
हम 'प्रेरणा' शब्द के मनोवैज्ञानिक अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ दे रहे हैं, यथा-
(1) गुड - "प्रेरणा, कार्य को आरम्भ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है।"
(2) ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन - "प्रेरणा एक प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाले की आन्तरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएँ उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं।"
(3) वुडवर्थ - "अभिप्रेरणा शक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है।"
(4) ऐवरिल - "प्रेरणा का अर्थ है- सजीव प्रयास। यह कल्पना को क्रियाशील बनाती है, यह मानसिक शक्ति के गुप्त और अज्ञात स्रोतों को जाग्रत और प्रयुक्त करती है, यह हृदय को स्पंदित करती है, यह निश्चय, अभिलाषा और अभिप्राय को पूर्णतया मुक्त करती है, यह बालक में कार्य करने, सफल होने और विजय पाने की इच्छा को प्रोत्साहित करती है।"
(5) लावेल - "अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक या आन्तरिक प्रेरणा है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो उस आवश्यकता को संतुष्ट करेगी।"
(6) ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन - "प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आन्तरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएँ उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है।"
(7) यंग - "प्रेरणा, व्यवहार को जाग्रत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है।"
इसकी परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ये तथ्य उभरते हैं-
(i) प्रेरणा मनोव्यावहारिक क्रिया है।
(ii) यह किसी आवश्यकता से उत्पन्न है।
(iii) इससे किसी विशेष क्रिया करने का संकेत मिलता है।
(iv) प्रेरणा द्वारा प्रसूत क्रिया लक्ष्य प्रगति तक रहती है।
विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने की प्रविधियाँ - विद्यार्थियों का विद्यालय में आना इस बात का द्योतक है कि वे सीखने के लिये अभिप्रेरित है, पर कितने अधिक अथवा कम यह दूसरी बात है। उनकी इस अभिप्रेरणा के पीछे कोई एक अभिप्रेरक भी हो सकता है, दो अभिप्रेरक भी हो सकते हैं और दो से अधिक अभिप्रेरक भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी अपनी इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिये विद्यालय आते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है, हो सकता है कि कुछ शिक्षार्थी इस मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिये विद्यालय आते हों। यह भी हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी मित्रों की संगत के लोभ से विद्यालय आते हों। कुछ विद्यार्थी खेल - कूद की सुविधाओं के कारण भी विद्यालय आ सकते हैं और कुछ शिक्षार्थियों के लिये समाज में पढ़े-लिखे व्यक्तियों का उच्च स्तर होना उनकी अभिप्रेरणा का आधार हो सकता है। कुछ शिक्षार्थी इनमें से किसी एक अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो सकते हैं और कुछ एक से अधिक अभिप्रेरकों से। कोई शिक्षार्थी चाहे एक अभिप्रेरक से अभिप्रेरित हो और चाहे एक से अधिक अभिप्रेरकों से, वह जितना अधिक अभिप्रेरित होगा, सीखने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारु रूप से चलेगी और सीखना भी उतना ही अधिक स्थायी होगा। विद्यार्थियों को सीखने के लिये पूर्ण रूप से अभिप्रेरित करने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों का विकास किया है जो निम्नलिखित हैं-
(i) पढ़ाये जाने वाले विषय अथवा सिखाये जाने वाले कौशल की उपादेयता - उपयोगिता / उपादेयता सबसे अधिक शक्तिशाली अभिप्रेरक होता है। यदि विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि पढ़ाया जाने वाला विषय अथवा सिखाया जाने वाला कौशल उनके जीवन में उनके लिए कितना जरूरी है तो जितना अधिक उन्हें उसकी उपयोगिता का आभास होगा, वे सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होंगे।
(ii) पढ़ाये जाने वाले विषय अथवा सिखाये जाने वाले कौशल के प्रशिक्षण के उद्देश्य - किसी पढ़ाये जाने वाले विषय अथवा सिखाये जाने वाले कौशल के प्रशिक्षण के उद्देश्य भी स्पष्ट करना आवश्यक होता है। ये प्रथम विधि से अभिप्रेरित शिक्षार्थियों को सीखने के लिये और अधिक अभिप्रेरित करते हैं। शिक्षार्थियों को सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने के उद्देश्य जितने अधिक स्पष्ट होते हैं वे सीखने के लिए उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं और उनकी सीखने सम्बन्धी क्रियायें भी उतनी ही अधिक उद्देश्य लक्षित होती है।
(iii) शिक्षार्थियों की आवश्यकतायें - किसी विषय का ज्ञान एवं कौशल व प्रशिक्षण अपने में कितना भी उपयोगी क्यों न हो जब तक वह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं करता जब तक शिक्षार्थी उसे सीखने के लिये अभिप्रेरित नहीं होता। इसलिये कौशल को शिक्षार्थी की आवश्यकताओं से जोड़ा जाना अति आवश्यक है।
(iv) शिक्षार्थियों का आकांक्षा स्तर - कुछ शिक्षार्थी केवल उत्तीर्ण होने भर की आकांक्षा रखते हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने की तो कुछ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की। इसी प्रकार कुछ छोटी- मोटी नौकरियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, कोई व्यवसाय या कोई अफसर श्रेणी की नौकरियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। यह देखा गया है कि जिन विद्यार्थियों का आकांक्षा का स्तर जितना ऊँचा होता है वे तत्सम्बन्धी ज्ञान एवं कौशल सीखने के लिये उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं। अतः हम शिक्षार्थियों का आकांक्षा स्तर उठाकर उनकी अभिप्रेरणा में वृद्धि कर सकते हैं।
(v) कक्षा का वातावरण - कक्षा का वातावरण भी शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने में अभिप्रेरक का कार्य करता है। सुन्दर कक्ष, शुद्ध हवा, पर्याप्त प्रकाश, शान्त वातावरण शिक्षक-शिक्षार्थियों के बीच के सम्बन्ध और शिक्षार्थियों के आपस के सम्बन्ध इन सबसे कक्षा का वातावरण तैयार होता है। जिस कक्षा में सीखने के लिये जितना अच्छा वातावरण होता है उस कक्षा के शिक्षार्थी उतने ही अधिक अभिप्रेरित होते हैं।
(vi) उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग - शिक्षक उपयुक्त शिक्षण विधियों के प्रयोग से भी शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। किसी वर्ग विशेष के छात्रों के लिये उपयुक्त शिक्षण विधि वह होती है जिसमें छात्रों की रुचि होती है और जिसके द्वारा वे शीघ्र सीखते हैं। शीघ्र सफलता से पुनर्बलन मिलता है, सीखने वाले अभिप्रेरित होते हैं और सीखने की क्रिया को और अधिक गति प्रदान होती है।
(vii) शिक्षक का व्यवहार - शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति आत्मभाव एक अचूक रामबाण होता है। वह अपने प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार से शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को सरलता से बढ़ा सकता है। यह कार्य वह छात्रों की भावनाओं का सम्मान करके उन्हें अभिव्यक्ति के स्वतंत्र अवसर प्रदान करके और उनकी समस्याओं का तुरन्त हल करके कर सकता है।
(viii) प्रशंसा एवं निंदा - इस संदर्भ में किये गये मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से दो तथ्य उजागर हुए। प्रथम यह कि औसत बुद्धि वाले शिक्षार्थियों के लिए प्रशंसा अच्छे अभिप्रेरक का कार्य करती हैं और छोटे बच्चों के लिए निन्दा अच्छे अभिप्रेरक का कार्य करती है। दूसरा यह कि निंदा की अपेक्षा प्रशंसा अधिक अच्छा अभिप्रेरक होता है। यह कार्य शिक्षक शिक्षार्थियों की सही अनुक्रिया के लिये प्यार एवं मुस्कान भरी स्वीकृति एवं सुन्दर शाबास, बिल्कुल ठीक आदि शब्दों द्वारा कर सकते हैं। गलत अनुक्रिया पर निन्दा के स्थान पर सहयोग अधिक उत्तम अभिप्रेरक होता है। यदि कोई शिक्षार्थी बार-बार गलत अनुक्रिया करे तो भी उसकी निन्दा प्रेम एवं सहानुभूति के साथ करनी चाहिए।
(ix) पुरस्कार एवं दण्ड - इस संदर्भ में किये गये मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि जिस समूह की प्रशंसा की गई, उसकी निष्पत्ति उस समूह से अधिक थी जिसकी आलोचना की गई थी और जिसे नियंत्रण में रखा गया था। हाँ, कुछ परिस्थितियों में बच्चों को दण्ड देना अभिप्रेरक का कार्य करता है। पर दण्ड बड़ी सावधानी से देना चाहिए, क्रोध की स्थिति में दण्ड देना हानिकारक होता है, विद्यार्थी अभिप्रेरित होने के स्थान पर पलायन कर जाते हैं। पुरस्कार भी बड़ी सावधानी से देना चाहिए, यह लोभ का कारण नहीं बनना चाहिए। पुरस्कार पदक अथवा प्रमाण-पत्र के रूप में देना अधिक प्रभावी होता है।
(x) प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतियोगिता - कभी-कभी स्पर्धा आधारित प्रतिद्वन्द्विता और प्रतियोगिता भी अच्छे अभिप्रेरक का कार्य करती है। यह प्रतिद्वन्द्विता व्यक्तिगत के स्थान पर सामूहिक स्तर की अधिक प्रभावशाली होती है। व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतियोगिता जहाँ अच्छे अभिप्रेरक का कार्य करती है वहाँ शिक्षार्थियों में द्वेष की भावना भी उत्पन्न करती है परन्तु सामूहिक प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतियोगिता शिक्षार्थियों को अपने समूह को विजयश्री दिलाने हेतु अधिक श्रम करने के लिये अभिप्रेरित करती है। शिक्षकों को प्रतिद्वन्द्विता और प्रतियोगिता का उपयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए।
(xi) सफलता का ज्ञान - मनोवैज्ञानिक स्किनर ने अपने प्रयोग में पाया कि यदि सीखने वाले को अपनी सफलता का ज्ञान तुरंत करा दिया जाये तो वह उसके लिये अभिप्रेरक का कार्य करता है, वह उससे आगे के कार्य को और अधिक उत्साह से करता है। स्किनर ने इसे पुनर्बलन की संज्ञा दी। उन्होंने शिक्षार्थियों के इस प्रकार के पुनर्बलन देने हेतु अभिक्रमित अध्ययन का विकास भी किया है।
|
|||||