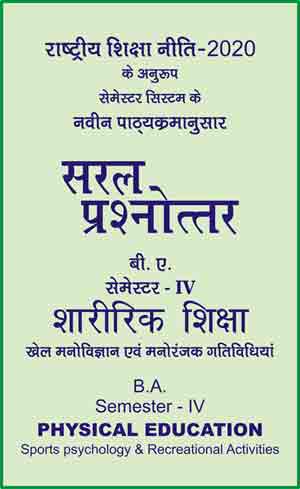|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- सीखने से सम्बन्धित विभिन्न दृष्टिकोणों, प्रकारों तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
सीखने के स्वरूप के बारे में दृष्टिकोण
(1) व्यवहारवादी दृष्टिकोण - व्यवहारवादियों का विचार है कि सीखना अनुभव के परिणाम के तौर पर व्यवहार में परिवर्तन का नाम है। मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं। बच्चा जन्म से ही अपने वातावरण में सीखने का प्रयत्न करता है।
इस विचारधारा के अंतर्गत थॉर्नडाइक का 'भूल और प्रयास का सिद्धान्त' या 'उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धान्त' शामिल हैं। थॉर्नडाइक के भूल और प्रयास के सिद्धान्त या 'सम्बन्धवाद' ने पश्चिमी देशों को बहुत प्रभावित किया है। उसने जानवरों पर कई प्रयोग किए। उसके अनुसार समस्त अधिगम 'सम्बन्धों' पर आधारित है।
(2) गेस्टाल्ट दृष्टिकोण - इस दृष्टिकोण के अनुसार सीखने का आधार गेस्टाल्ट या संगठनात्मक ढाँचे पर निर्भर है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि किसी भी प्रकार के सीखने के लिए हम उसके विभिन्न अंगों की अपेक्षा सम्पूर्ण इकाई पर बल देते हैं। 'गैस्टाल्ट' शब्द 'लैटिन' भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है - 'सम्पूर्ण रूप में देखना। गेस्टाल्टवादियों ने सम्पूर्ण परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना तथा फिर बुद्धिमत्तापूर्ण उचित अनुक्रिया व्यक्ति को अर्न्तदृष्टि मासूम की संज्ञा दी है।
इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सूझ-बूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का आधार जर्मन के वैज्ञानिक कोलहर के प्रयोग हैं जो उन्होंने पशुओं पर किए। उन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया कि पशु भी मनुष्य के समान बुद्धिपूर्ण निरीक्षण द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोहलर ने यह प्रयोग चिम्पैजी पर प्रयोग करके स्पष्ट किया।
(3) होरमिक दृष्टिकोण - यह दृष्टिकोण मैकडुगल की देन है। यह सीखने के लक्ष्य-केंद्रित स्वरूप पर जोर देता है। सीखना लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। मैकडुगल का मानना है कि यदि हम वस्तुनिष्ठ निरीक्षण तक सीमित रहते हैं तो हम किसी जानवर के व्यवहार के यांत्रिक दृश्य को ही प्राप्त कर पाएंगे। व्यक्ति या मानव तो एक मशीन ही लगेगा। परन्तु हम अपने व्यवहार को आन्तरिक रूप से जानते हैं और उसकी उद्देश्यपूर्णता को भी समझते हैं जो कि यांत्रिक नहीं होती। मैकडुगल ने लक्ष्य की खोज करते हुए व्यवहार की कई विशेषताएँ बताई हैं-
(i) व्यवहार स्थायी रहता है-
(ii) इस स्थायीपन के बावजूद क्रिया में भिन्नता होती है
(iii) लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात् क्रिया समाप्त हो जाती ह,
(iv) क्रिया पुनरावृत्ति के साथ सुधरती है
(4) सीखने का फील्ड दृष्टिकोण - कर्टलेविन ने इस दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया है। उसने लिखा है कि सीखना परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है और सीखने में प्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है।
लेविन ने अभिप्रेरणा के अध्ययन को नई दिशा प्रदान की है। लेविन के अनुसार जैसे-जैसे बच्चा विकसित होता है, उसकी व्यक्तित्व प्रणाली में विस्तार होता है और यह पूर्ण रूप से उप प्रणाली में संगठित हो जाता है। बच्चे के मनोवैज्ञानिक वातावरण में दिक और समय में भी प्रसार हो जाता है। वह अपनी वास्तविक और अवास्तविक इच्छाओं में अंतर करने लगता है। इस प्रकार लेविन का क्षेत्र है 'जीवन दिक' जिसमें व्यक्ति और उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण शामिल है।"
मनोवैज्ञानिक पर्यावरण के अंतर्गत निस्संदेह ही वह सब कुछ शामिल होता है, जिसे वह देखता था या समझता है। लेकिन इससे भी अधिक उसकी वर्तमान आवश्यकताएँ उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण में शामिल होती है।
सीखने या अधिगम के प्रकार - मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक दृष्टि से अधिगम को हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं। यह वर्ग है-
A. सीखने वाले प्रकार के अनुसार अधिगम।
B. शरीर के अंगों की संभागिता के अनुसार अधिगम।
C. मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम।
A. सीखने वाले प्रकार के अनुसार - अधिगम सीखने वाले के प्रकार के अनुसार अधिगम निम्नलिखित दो प्रकार का होता है-
(1) जानवरों द्वारा अधिगम - जानवरों के व्यवहार में परिवर्तन को जानवरों का अधिगम कहते हैं।
(2) मानव द्वारा अधिगम - मानव के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे मानव का अधिगम या मानव द्वारा अधिगम कहा जाता है। मानव-अधिगम मानव के विकास की अवस्थाओं के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे शैशवावस्था अधिगम, बाल्यकाल अधिगम, किशोरावस्था अधिगम।
B. शरीर के अंगों की संभागिता के अनुसार - इस प्रकार के अधिगम को अधिगम निम्नलिखित दो उपवर्गों में बाँट जा सकता है-
(1) गत्यात्मक अधिगम - इस प्रकार के अधिगम में मांसपेशियों से युक्त क्रियाओं को शामिल किया जाता है। गत्यात्मक अधिगम भी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है।
(i) संवेदन गति अधिगम - इस प्रकार के अधिगम के अन्तर्गत ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से साधारण आदतों को अर्जित किया जाता है। उदाहरणार्थ- नर्सरी स्कूल के खेल मैदान में कौशलों को सीखना।
(ii) प्रत्यक्षात्मक गत्यात्मक अधिगम - इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आदतों तथा जटिल कौशलों को अर्जित किया जाता है। उदाहरणार्थ नृत्य करना, साइकिल चलाना, हाथ से लिखना, तैरना, संगीत के यंत्र को बजाना इत्यादि।
(2) विचारात्मक अधिगम - इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत विचारों, संप्रत्ययों तथा मानसिक सहचर्यों को अर्जित किया जाता है। यह प्रायः व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति का अधिगम होता है तथा इसमें मांसपेशियों की क्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। विचारात्मक अधिगम निम्न प्रकार का होता है
(i) प्रत्यक्षात्मक अधिगम - यह मुख्यतः या पूर्णतया ज्ञानेन्द्रियों, ठोस पदार्थों, बोले गए शब्दों या लिखित चिन्हों या चित्र बनाकर या प्रकृति के अध्ययन या पठन या भ्रमण करने के परिणामस्वरूप होता है।
(ii) संप्रत्यक्षात्मक अधिगम - इसे अमूर्त अधिगम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत संप्रत्यय और अमूर्त विचारों को सीखा जाता है।
(iii) साहचर्यात्मक अधिगम - यह वह अधिगम होता है जो इत्तेफाक से या अचानक या सम्बन्ध से या प्रयोग द्वारा होता है। इसके अंतर्गत सूचनाओं के एक निर्धारित क्रम में जोड़ना शामिल है। इसमें स्मरण करना तथा मानसिक प्रक्रियाओं में सम्बन्ध बनाना भी शामिल होता है।
(iv) काल्पनिक अधिगम - वह प्रक्रिया जिसमें भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यकाल की बातों को चेतना में एक निश्चित स्वरूप मिल जाए, उसे 'कल्पना' कहते हैं तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन बातों को सीखा जाता है तथा समझा जाता है, उसे काल्पनिक अधिगम कहते हैं। उसमें आकृतियों को 'अर्जित करना तथा उन चीजों को समझना जिनका ज्ञानेन्द्रियों को अनुभव नहीं होता, शामिल है।
C. मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार अधिगम - मानव व्यवहार के मुख्य तीन पक्ष हैं-
ज्ञानात्मक
भावात्मक
क्रियात्मक पक्ष
(1) ज्ञानात्मक अधिगम - इस प्रकार के अधिगम का सम्बन्ध ज्ञान, संप्रत्ययों तथा उनमें आपसी सम्बन्धों से होता है। स्कूल के सभी विषय इसी प्रकार के अधिगम का विकास करते हैं। स्कूल में, अध्यापक विभिन्न विषयों को पढ़ाते समय विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्रदान करता है. विभिन्न प्रत्ययों में सम्बन्ध समझाता है तथा सीखने वालों को अपने अनुभवों के आधार पर किसी सामान्यीकरण पर पहुँचने में सहायता करता है।
(2) अभिवृत्यात्मक या दृष्टिकोण अधिगम - दृष्टिकोण और मूल्य मानव-व्यवहार द्वारा सीखे जाते हैं या अर्जित किये जाते हैं। इनका विकास अपने समूह के साथ सम्बन्धों के विकास के दौरान होता है। इस प्रकार के अधिगम के परिणामस्वरूप संवेग, स्थायी भाव तथा आत्मानुभूति आदि सीखे जाते हैं।
(3) कौशलों द्वारा सीखना - इसमें अभ्यास द्वारा गत्यात्मक प्रकार का अधिगम शामिल है। स्कूल में कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा इस प्रकार का अधिगम होता है, जैसे पढ़ना लिखना, कोई विशिष्ट खेल खेलना। कौशलों के विकास के लिए जो मुख्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, वे हैं प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, प्रतिपुष्टि तथा अभ्यास।
D. कुछ अन्य प्रकार - उपरोक्त प्रकारों के अतिरिक्त कुछ और भी अधिगम के प्रकार हैं, जैसे-
(1) बौद्धिक अधिगम - बालक के मानसिक विकास के साथ-साथ उसमें तर्कशक्ति बढ़ती है। संवेदन गति से प्राप्त होने वाले ज्ञान के विकास का अर्जन ही बौद्धिक है।
(2) अनुशीलनात्मक अधिगम - जब बालक में वस्तुओं एवं घटनाओं के प्रति गुण-दोष, अच्छाई-बुराई, सौन्दर्य आदि का बोध करने की क्षमता पैदा हो जाती है तो वह कविता, इतिहास, नाटक आदि के अध्ययन में अनुशीलनात्मक अधिगम ग्रहण करता है।
(3) अनुकरणात्मक अधिगम - अधिगम का अनुकरण किया जा सकता है। जैसे नृत्य, कला, संगीत आदि का अधिगम अनुकरण द्वारा ही होता है।
(4) समस्या समाधान अधिगम - इस प्रकार के अधिगम के परिणामस्वरूप समस्या का समाधान करने की योग्यता विकसित होती है तथा सही अनुक्रिया का चयन करने की क्षमता का विकास होता है।
(5) संवेगात्मक अधिगम - जन्म के समय बच्चा डर, प्रेम, घृणा की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं कर पाता। लेकिन समय के साथ-साथ वह संवेगों की अभिव्यक्ति करने की योग्यता अर्जित कर लेता है।
(6) सामाजिक अधिगम - व्यक्ति विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सामाजिक कार्य करना सीखता है जिसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है।
(7) शैक्षणिक अधिगम - इस प्रकार के अधिगम के अन्तर्गत वह ज्ञान सम्मिलित होता है जिसे बालक पुस्तकों एवं औपचारिक शिक्षा द्वारा ग्रहण करता है।
(8) एकीकृत अधिगम - इस प्रकार के अधिगम में उपरोक्त सभी प्रकार के अधिगम एक साथ होते हैं।
अधिगम की प्रक्रिया - किसी भी क्रिया को सीखने का अर्थ है- कुछ क्रियाओं को एक साथ सम्पन्न करके सम्पूर्ण रूप से किसी अनुभव को प्राप्त करना। सम्पूर्ण अनुभव अनेक क्रियाओं एवं उप- क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों से बनता है। इस प्रकार अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। डेशिल ने अधिगम प्रक्रिया के कुछ सोपानों का वर्णन किया है जो कि निम्नलिखित हैं-
(i) अभिप्रेरणा - वह हर कार्य जिसे मनुष्य करना चाहे, किसी न किसी अभिप्रेरणा से संचालित होता है। छात्र इसलिए पढ़ते हैं कि परीक्षा में पास होकर अच्छी नौकरी या व्यवसाय हासिल करें। अभिप्रेरणा ही उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करती है। मानव जो भी कार्य करता है, उसके मूल में किसी न किसी प्रकार की अभिप्रेरणा निहित होती है। व्यक्ति की बहुत-सी आवश्यकताएँ होती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए विभिन्न प्रेरक उत्पन्न हो जाते हैं। इन प्रेरकों के कारण व्यक्ति अधिक क्रियाशील हो जाता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति सदा ही अभिप्रेरित रहता है।
(ii) उद्देश्य - किसी कार्य को सीखने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य का भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी क्रिया को सीखने का कोई न कोई उद्देश्य होता है। मनुष्य उस क्रिया को नहीं सीखना चाहता है जो उसके उद्देश्य की पूर्ति न करती हो। अतः व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यविहीन नहीं होना चाहिए। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार करता है तथा उसका व्यवहार एक निश्चित दिशा की ओर केंद्रित होता है। उद्देश्यों की स्पष्टता से व्यवहार को निश्चित दिशा प्राप्त होती है।
(iii) बाधा - उद्देश्य की प्राप्ति के दौरान बाधाओं का उत्पन्न होना निश्चित होता है। इन बाधाओं की उपस्थिति में व्यक्ति अनेकों प्रकार का संभावित व्यवहार करता है। तभी वह इसके पश्चात् किसी - उपयुक्त व्यवहार पर पहुँचता है। उपयुक्त व्यवहार होने पर इन बाधाओं को नियंत्रित किया जा सकता है।
(iv) विभिन्न अनुक्रियाएँ - बाधाओं को दूर करने के लिए तथा परिणामस्वरूप अपने उद्देश्य तक पहुँचने के लिए व्यक्ति विभिन्न अनुक्रियाएँ करता है। लेकिन सभी अनुक्रियाएँ सही नहीं होतीं। उद्देश्य को अर्जित करने के लिए वह कुछ विशेष प्रकार की अनुक्रियाएँ करता है।
(v) पुनर्बलन - पुनर्बलन के अन्तर्गत वे सभी क्रियाएँ तथा तथ्य आ जाते हैं जिनसे विवश होकर विद्यार्थी की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अध्यापक का आदेश, स्वयं की इच्छा, बड़ों के सम्मान तथा सामाजिक मर्यादा से प्रभावित होकर जो कार्य किए जाते हैं, वे सभी पुनर्बलन के अन्तर्गत आता है। जो भी अनुक्रिया संतोषजनक एवं सुखप्रद होती है वह पुनर्बलित हो जाती है। सभी असफल अनुक्रियाओं को भुला देना पड़ता है तथा सफल अनुक्रिया की स्थिति का सामना करने के लिए चुन लेना पड़ता है। उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर व्यक्ति वैसे ही व्यवहार या अनुक्रिया को दोहराता है।
(vi) एकीकरण एवं सामान्यीकरण - अधिगम की क्रिया के विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। जब तक पूर्व एवं नवीन ज्ञान को जोड़ा नहीं जाता तब तक क्रिया सम्पूर्णता प्राप्त नहीं करती। इस प्रकार व्यक्ति नवीन सफल प्रतिक्रिया का पहले सीखी गई क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। इसे नवीन ज्ञान का पूर्व ज्ञान से जोड़ना भी कहते हैं। ऐसा करने से नवीन प्रतिक्रिया उसके ज्ञान का एक अंग बन जाती है और उसका सम्पूर्ण ज्ञान एकीकृत हो जाता है।
अतः यह स्पष्ट है कि अधिगम किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। अधिगम के अंतर्गत अनेक उप-क्रियाएँ होती हैं जो उसे पूर्णता प्रदान करती हैं।
|
|||||