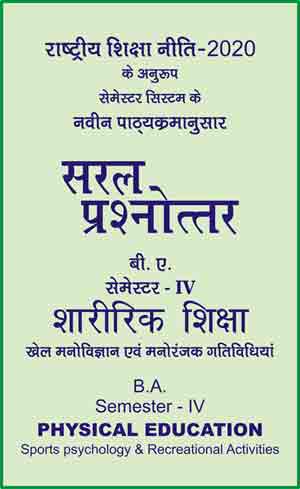|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 4
अधिगम
(Learning)
प्रश्न- सीखने का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।
अथवा
सीखने से आप क्या समझते हैं? सीखने को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
सीखने या अधिगम का अर्थ
हमारे दैनिक जीवन में सीखने का बहुत महत्व है। जन्म के समय व्यक्ति असहाय होता है। धीरे-धीरे वह वातावरण के सम्पर्क में आता है और वातावरण के अनुसार स्वयं को बनाने का प्रयास करता है। इस क्रिया में वह अपने तथा परिवार व समाज के अन्य व्यक्तियों से भी लाभ उठाता है, जिसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। भाषा बोलना, पढ़ना लिखना तथा बहुत-सी अन्य आदतें भी हम सीखते हैं, जिसके कारण हमारा व्यवहार समाज के अनुरूप हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व बहुत से शीलगुणों का निर्माण भी सीखने के आधार पर ही होता है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति या जीव में कुछ जन्मजात संस्करण होते हैं, जो उसकी प्राथमिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करते हैं और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के द्वारा व्यक्ति स्वयं को बाह्य वातावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। बाह्य वातावरण के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया को ग्रहण करना ही मनोविज्ञान में सीखना कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भूख की स्थिति में बन्दर की छीनने की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक होगी, परन्तु एक बालक के माँगने की प्रतिक्रिया सीखने का परिणाम होगा। सीखना एक प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों में अभ्यास का बहुत महत्व है। अभ्यास के प्रभाव में व्यवहार में होने वाले परिवर्तन सीखने से संबंधित नहीं होते। सीखने से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं।
बर्नार्ड का मत है कि - "सीखने की प्रक्रिया आवश्यकता से आरम्भ होती है तथा जो उद्देश्यपूर्ण होती है।"
जब इसे प्रेरणा मिलती है तो इसमें तत्परता आ जाती है और पुनर्बलन द्वारा व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और पूर्व अनुभवों के संगठनों के आधार पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में जो सक्रिय परिवर्तन आ जाता है, इसे ही सीखना कहते हैं।
सीखने को परिवर्तन, सुधार, विकास, उन्नति तथा समायोजन के तुल्य जाना जाता है। यह केवल . स्कूल की शिक्षा, साइकिल चलाने, पढ़ने या टाइप करने तक सीमित नहीं बल्कि यह एक विशाल शब्द है जिसका व्यक्ति पर गहरी छाप या प्रभाव पड़ता है।
परिभाषाएँ -
(1) हेनरी स्मिथ के शब्दों में - "अनुभव के प्रतिफल के रूप में नये व्यवहार का अर्जन अथवा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्बलीकरण अधिगम है।"
(2) वुडवर्थ के अनुसार - "अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं को ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है।"
(3) क्रो एवं क्रो - ने भी अधिगम को आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों को ग्रहण करना बताया है।
(4) जे. पी. गिलफोर्ड - ने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम माना है।
(5) क्रॉनबैक - ने कहा है कि अनुभव के परिमामस्वरूप व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है।
(6) पैवलव - ने अनुक्रिया द्वारा आदतों के निर्माण को ही अधिगम माना है।
(7) गेट्स के अनुसार - "सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार का शोध है।"
(8) किंग्सले तथा गैरी के अनुसार - "शोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार की अभ्यास या ट्रेनिंग द्वारा उत्पत्ति होती है या उसमें परिवर्तन होता है।"
(9) कॉलविन के अनुसार - "पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं।"
(10) जी. डी. बाज के अनुसार - "अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति विभिन्न आदतें, ज्ञान एवं दृष्टिकोण सामान्य जीवन की माँगों की पूर्ति के लिए अर्जित करता है।"
(11) प्रेसी ने कहा है कि - "अधिगम एक ऐसा अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है तथा व्यवहार की नई विधि प्राप्त होती है।"
(12) सी. ई. स्किनर के शब्दों में - "व्यवहार के अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं।"
उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अधिगम के सम्बन्ध में कुछ तथ्य स्पष्ट होते हैं। जैसे-
1. अधिगम व्यवहार परिवर्तन है।
2. अधिगम व्यवहार का संगठन है।
3. अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है।
परन्तु वास्तविकता यह है कि व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार एवं संगठन तथा पुष्टिकरण में कोई भी एक कारण अधिगम के लिए पूरी तरह उत्तरदायी नहीं है।
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक - अधिगम की प्रक्रिया अनेक कारकों से प्रभावित हो सकती है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों का वर्णन निम्न है
(1) पूर्व अधिगम - बालक कितनी शीघ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। नवीन अधिगम की प्रक्रिया प्रायः शून्य से प्रारम्भ नहीं होती है वरन् बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारम्भ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारु ढंग से चलती है। अतः अध्यापकों को 'ज्ञात से अज्ञात की ओर' के शिक्षण सिद्धान्त के अनुरूप शिक्षण कार्य करना चाहिए।
(2) विषयवस्तु - अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषयवस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। कठिन व असार्थक बातों की अपेक्षा सरल व सार्थक बातों को बालक अधिक शीघ्रता व सुगमता से सीख लेता है। विषय सामग्री की व्यक्तिगत उपादेयता भी सीखने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग तथा महत्व रखती है तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। अतः बालक के जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए।
(3) शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता - शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं जिससे वे शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। इसके विपरीत कमजोर, बीमार व अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता का विशेष महत्त्व है जिससे वे पुस्तक, कलम, कापी आदि ठीक ढंग से पकड़ सके। इसलिए बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता के अनुरूप ही उन्हें नवीन बातें सिखानी चाहिए।
(4) मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता - मानसिक रूप से स्वस्थ व परिपक्व बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। अधिक बुद्धिमान बालक कठिन बातों को शीघ्रता से तथा सरलता से सीख लेता है। मानसिक रोगों से पीड़ित या कम बुद्धि वाले बालक प्रायः मन्दगति से नवीन बातों को सीख पाते हैं। बड़ी कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के सीखने में उनकी बुद्धि तथा मानसिक परपिक्वता दोनों का ही विशेष महत्व होता है।
(5) अधिगम की इच्छा - अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि बालक में किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस बात को सीख लेता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक किसी बात को सीखना ही नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता। अतः बालकों को सिखाने से पहले अध्यापकों व अभिभावकों को उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए।
(6) प्रेरणा - प्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है तो वह सीखने के कार्य में रुचि नहीं लेता है। अतः अध्यापकों को चाहिए कि सीखने से पहले बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करे। प्रशंसा व प्रोत्साहन के द्वारा तथा प्रतिद्वन्द्विता व महत्वाकांक्षा की भावना उत्पन्न करके बालकों को प्रेरित किया जा सकता है।
(7) थकान - थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। थकान की स्थिति में बालक पूर्ण मनोयोग से सीखने की क्रिया में रत नहीं हो पाता है तथा उसका ध्यान विकेंद्रित होता रहता है जिससे सीखना संदिग्ध हो जाता है। प्रातःकाल बालक स्फूर्ति से युक्त रहते हैं जिसके कारण प्रातः काल में सीखने में सुगमता रहती है। धीरे-धीरे बालकों की स्फूर्ति में शिथिलता आती जाती है जिसके कारण बालकों की सीखने की गति मंद होती जाती है। अतः बालकों के पढ़ने की समय सारिणी बनाते समय विश्राम की व्यवस्था रखने का भी ध्यान रखना चाहिए।
(8) वातावरण - अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शान्त, सुविधाजनक, नेत्रप्रिय, उचित प्रकाश तथा वायु वाले वातावरण में बालक प्रसन्नता से व एकाग्रचित्त होकर सीखता है। इसके विपरीत शोरगुल वाले अनाकर्षक तथा असुविधाजनक वातावरण में बालक के सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। ऐसे वातावरण में बालक जल्दी ही थकान का अनुभव करने लगता है। अतः अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्रायाचों को घर कक्षा व विद्यालय के अंदर सीखने में सहायक वातावरण तैयार करने का प्रयास करना चाहिए।
(9) सीखने की विधि - सीखने की विधि का भी अधिगम की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कुछ विधियों से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। खेल विधि या करके सीखना विधि जैसी मनोवैज्ञानिक व आधुनिक विधियों से ज्ञान शीघ्रता व सुगमता से प्राप्त किया जाता है तथा यह ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसके विपरीत अमनोवैज्ञानिक विधियों से यदि वालकों को जबरदस्ती सिखाये जाने का प्रयास किया जाता है तो बालक सीखने में रुचि नहीं लेता है। अतः बालकों को सिखाते समय उनकी आयु, क्षमता आदि एवं विषयवस्तु की प्रकृति जैसी बातों को ध्यान में रखकर ही उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए।
|
|||||