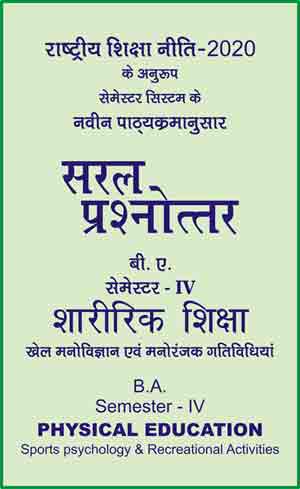|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी सेमेस्टर-4 शारीरिक शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- खेलों में खेल मनोविज्ञान का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए।
अथवा
खेल मनोविज्ञान के महत्व तथा कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
यह धारणा आम है कि खिलाड़ी का प्रदर्शन उसकी शारीरिक दक्षता तथा अनुभव पर निर्भर करता है परन्तु खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी की मानसिक स्थिति उसके प्रदर्शन व व्यवहार को प्रभावित करती है। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों के व्यवहार से जुड़ा हुआ एक विज्ञान है इसमें खिलाड़ी के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। खेल मनोविज्ञान के महत्व को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:
1. भावात्मक पक्ष को मजबूत करने - वैश्वीकरण के दौर में दुनिया भर में खेल में प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है जिनमें विभिन्न देशों से हजारों खिलाड़ी भाग लेते हैं। खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर खिलाड़ी के मन में निराशा, डर और तनाव के भाव आने लगते हैं और जब वह अपना प्रदर्शन करते हैं तो मानसिक स्थिति के कारण उनका खेल प्रभावित होता है। खेल मनोविज्ञान के द्वारा खिलाड़ियों के भावनात्मक पक्ष को मजबूत किया जाता है जिससे वह खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
2. खिलाड़ियों का व्यवहार समझने में - खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी के व्यवहार को समझना आवश्यक होता है। खेल मनोविज्ञान खेल शिक्षक को खिलाड़ी के व्यवहार को समझने में सहायक होता है। इससे खेल शिक्षक खिलाड़ी की उत्सुकता, रुचि, क्षमता व अभिवृत्ति आदि को समझने में सफल होता है। वह खिलाड़ी को अच्छी प्रकार निर्देशन दे सकता है और उसके प्रदर्शन को सुधार सकता है।
3. गति कौशलों को सीखने में - प्रत्येक बालक क्षमता, योग्यता एवं रुचि में एक-दूसरे से भिन्न होता है वह अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार ही खेल का चुनाव करता है। खेल मनोविज्ञान गति कौशलों को सीखने में सहायता देता है।
4. खिलाड़ी की क्रियात्मक क्षमता के विकास में - खेल मनोविज्ञान खिलाड़ी की क्रियात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन मानसिक शक्ति पर निर्भर होता है। खेल मनोविज्ञान के द्वारा खिलाड़ी को शारीरिक तथा मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है जिससे वह खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर सके।
5. तनाव व निराशा को नियंत्रित करने में - खेल प्रतियोगिताओं में अकसर यह देखने को मिलता है कि करीबी मुकाबलों में खिलाड़ी निराश हो जाते हैं या वे तनाव में आ जाते हैं जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। खेल मनोविज्ञान खिलाड़ी की मानसिक स्थिति को दृढ़ करने में सहायक होता है।
6. प्रतियोगिता की तैयारी में - बड़ी खेल प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी काफी लम्बे समय से होने लगती है। इन प्रतियोगिताओं की तैयारी खेल प्रशिक्षकों की देख-रेख में होती है। इनमें एक अच्छे खेल मनोवैज्ञानिक का होना आवश्यक होता है, जो खिलाड़ी की मानसिक दशा को समझ कर उसे निर्देशन देता है। इससे खिलाड़ी का भावनात्मक तथा शारीरिक पक्ष मजबूत होता है।
खेल मनोविज्ञान का क्षेत्र
खेल मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है इसमें समूह की गतिशीलता का अध्ययन, खिलाड़ी के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन, प्रतियोगिता के प्रति दृष्टिकोण, समूह निर्माण, समूह रखरखाव, समूह सामंजस्य, समाजमिति, नेतृत्व, प्रबन्धन, खिलाड़ी पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रभाव आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त खेल मनोविज्ञान का सीधा सम्बन्ध निम्न अनुशासनों से है।
1. शैक्षिक खेल मनोविज्ञान (Educational Psychology of Sports) - राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जा रही है। आज प्रत्येक खिलाड़ी को खेल प्रशिक्षक से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शैक्षिक खेल मनोविज्ञान सीखने, सिखाने से जुड़ा अनुशासन है इसमें, खेल प्रशिक्षक प्रतिधारण, स्मृति, शिक्षण स्थान्तरण में खिलाड़ियों की सहायता करता है।
2. विकासात्मक मनोविज्ञान (Developmental Psychology) - इसमें मानव के विकास से सम्बन्धित विषयों का अध्ययन किया जाता है इसके अन्तर्गत खेल से सम्बन्धित निम्न विषय आते हैं-
1. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी पर आनुवांशिकता का प्रभाव
2. विभिन्न प्रकार के कौशलों को सीखने की उम्र
3. खिलाड़ी के प्रदर्शन का चरम बिन्दु
4. लिंग और आयु
5. प्रतिस्पर्धियों की विभिन्नता
6. व्यक्तिगत भिन्नता का प्रदर्शन पर प्रभाव, आदि।
3. नैदानिक मनोविज्ञान (Chinical Psychology) - यह खिलाड़ी के व्यवहार और मनोवैज्ञानिक विकारों से सम्बन्धित अनुशासन है इसमें प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के दौरान चोटों, किसी विशेष खेल प्रणाली को अपनाने में असमर्थता, फोबिया (भय) और निराशा का कारण और पराजय (नकारात्मकता) के कारणों का अध्ययन किया जाता है।
|
|||||