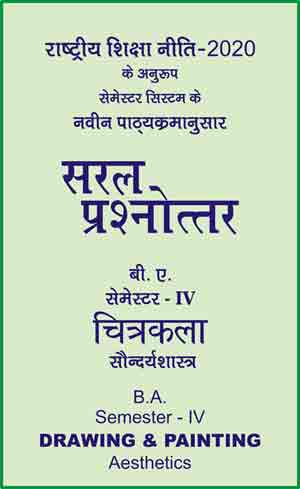|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला बीए सेमेस्टर-4 चित्रकलासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- आनन्द कुमार स्वामी की रस विषयक मान्यताओं के विषय में आप क्या जानते हैं?
अथवा
आनन्द कुमार स्वामी का सौन्दर्य विषयक सिद्धान्त क्या था?
उत्तर-
रस विषयक मान्यता - आनन्द कुमार स्वामी रस-विषयक मान्यताओं का अंग्रेजी, अनुवाद करने में अग्रणी रहे। पूर्व एवं पश्चिम के कला-विषयक तुलनात्मक अध्ययन करने का पूरा श्रेय कुमार स्वामी को ही जाता है। इनका जन्म श्रीलंका में हुआ। इनके पिता तमिल के रहने वाले और माँ अंग्रेज़ थी। इन्होंने अपनी जीवन यात्रा एक भूगर्भशास्त्र से प्रारम्भ की, तत्पश्चात् राजनैतिक सुधारक एवं कला इतिहासकार के रूप में अन्ततः कला में 'शाश्वत दर्शन के व्याख्याकार हुए। ये दस वर्षों तक भारत में रहे। इन्होंने भारतीय कला का अध्ययन किया। ये तीस वर्षों तक अमेरिका में बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में भारतीय कला-कक्ष के संरक्षक रहे। इन्होंने लगभग 341 निबन्ध लिखकर अपने विचारों को प्रस्तुत किया। 'मिरर ऑफ जेस्चर' (1917), 'द डांस ऑफ शिवा (1918), 'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एण्ड इण्डोनेशियन आर्ट (1927 ई.) तथा ट्रांसफार्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट्स (1943 ई.) इत्यादि सुप्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय दृष्टिकोण से रस सिद्धान्त को ही सौन्दर्य का पर्याय माना है।
इनके अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव इत्यादि बाह्य उपादानों से ही रस उत्पन्न होता है। राम और दुष्यन्त के पात्रों से तादात्म्य स्थापित करते हैं उनकी क्रियाओं तथा संवेदनाओं से हमारे संवेग जागृत अवस्था में होते हैं तथा धीरे-धीरे हम नाटक के पात्रों से पूर्ण तादाम्य स्थापित करते हैं, जिसके अन्तर्गत अहं और देशकाल की भावना होती है। यही रसानुभूति है। यह रसानुभूति दर्शक तथा पात्र की समानुभूति का सुखद परिणाम है। यह नैतिकता तथा ऐन्द्रियता से अलग (परे) है। रस आस्वाद्य वस्तु है जिसके आस्वादन में दो प्रमुख तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होते हैं-
1. केवल रसिक ही रसास्वादन कर सकता है - अर्थात् रस की स्थिति मानव-मन में होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त पाषाण प्रतिमा में भी ईश्वर के दर्शन करता है, उसी प्रकार रसिक भी प्रत्येक वस्तु में रसानुभव करता है। रसिक में जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जिज्ञासा के कारण ही हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए व्याकुल होते हैं। इस प्रकार जहाँ जिज्ञासा या रुचि होगी वहीं आनन्द प्राप्त होगा। इस कारण केवल रसिक ही रसानुभूति कर सकता है।
2. रसास्वादन जागृत किया जा सकता है - अर्थात् मानव में भाव जन्मजात होते हैं। उचित वातावरण या कलाकृति द्वारा उनसुप्त भावों को जागृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कल्पना तथा तकनीकी कुशलता को प्राथमिकता दी जाती है। यही इसके प्रमुख तत्व दृष्टव्य हैं। तकनीकी कुशलता बाह्य उत्पादन है या उपादान है। कल्पना सौन्दर्य चेतना को जागृत करने का प्रमुख तत्व है जिसके फलस्वरूप कलाकार द्वारा उसके भावों की अभिव्यक्ति होती है। कल्पना के माध्यम से वह अपने विचारों को प्रकट करने के लिये बिम्ब खोजता है। कलाकार की कल्पना जितनी कुशलपूर्वक सजगतायुक्त होगी, कलाकृति उतनी ही अधिक संवेदनशील होगी। इसी प्रकार दर्शक में भी अनुभूति की तीव्रता का आधार कल्पना की गहनता स्पष्ट परिलक्षित है। दर्शक या रसिक नाटक का पात्रों या कलाकृति से कल्पना द्वारा ही समन्वय स्थापित करता है। रसिक स्वयं को उस भाव या स्थिति में कल्पित करता है जिसमें कलाकार या नाटक के पात्र होते हैं। कल्पना की गहराई समानुभूति जितनी तीव्र होगी, उतना ही रसिक अहं भाव को विस्तृत कर कलाकृति या पात्रों के भावों में तिरोहित हो जायेगा। यही रसानुभूति है जिसे जागृत किया जा सकता है।
उक्त प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। काव्य, नाटक या कलाकृति के प्रत्यक्षीकरण से ही रसिक के संवेग जागृत होते हैं। इसके लिये कला वर्णनात्मक हों, यह आवश्यक नहीं है। कला में एक विचार या पंक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। कला का विषय सदैव विशेष प्रकार से होता है सामान्य रूप में नहीं होता। कलाकार व्यक्ति को प्रस्तुत करता है उसकी सम्पूर्ण जाति को नहीं करता। इस ईश्वरमय सृष्टि से सौन्दर्य को खोजता है। संकलित करके तथा अन्त में अपनीं अनुभूति में समेटकर उसे व्यक्त करते हुए रसिक तक संप्रेषित करता है यद्यपि यह कलाकार का व्यक्तिगत अनुभव होता है तथापि सम्पूर्ण मानव जाति के लिए ग्रहण करने योग्य होता है। यही रसानुभूति या सौन्दर्यानुभूति की सार्वभौमिकता है। सौन्दर्य या रस कलाकार की एक मनोस्थिति है जो व्यक्तिगत होने के कारण सापेक्षिक है। परन्तु जब यह रस या सौन्दर्य कला में व्यक्त होकर मानव जाति के लिये ग्रहण करने योग्य होता है। तब यह निरपेक्ष दृष्टिगत होता है। उदाहरण के लिये, कलाकार की एक कृति कुछ व्यक्तियों को ही सुन्दर लगती है परन्तु अजन्ता की चित्रकला, ग्रीक, गोथिक या रोमनस्क कला सम्पूर्ण मानव के लिए आकर्षक सुन्दरता का केन्द्र बिन्दु है। निष्कर्षतः हम कह सकते है कि आनन्द कुमार स्वामी ने "रस का ज्ञान कलाकार को होता है यह एक सहज ज्ञान है।' इस सहज ज्ञान को वह कलाकृति में अभिव्यक्त करता है। इस अभिव्यक्ति द्वारा वह अपने भावों को रसिक तक संप्रेषित करता है। जिस प्रक्रिया में भाषा, रंग, रेखा आदि के भौतिक उपादान अपेक्षित होते हैं। रसिक के मन में भी वही भावनायें उत्पन्न होनी चाहिये जो कलाकार के मन में उत्पन्न हो चुका है। रसिक, कलाकार तथा कलाकृति तीनों के परस्पर तादात्म्य से ही रस उत्पन्न होता है।
आनन्द कुमार स्वामी रस को अदृश्य मानते हैं। रस रसिक की कल्पनात्मक तथा ऐन्द्रिय चेतना का परिणाम है जो आनन्दमय है। इस प्रकार रस में चेतना व आनन्द का समन्वय है जो हमें सत् के दर्शन कराता है अर्थात् रस सच्चिदानंद है। ये रस को ब्रह्मास्वाद सहोदर मानते हैं। इनके अनुसार कलाकार कलाकृति को प्रस्तुत करता है। कला समीक्षक रसिक की सौन्दर्य दृष्टि को जाग्रत कर देता है। समीक्षक स्वयं भी एक कलाकार ही है जो कलाकार की खोज में कुछ नवीन खोज करता है। रसास्वादन और सौन्दर्यानुभूति की अवस्था में हम एक अलग दूसरी दुनिया में भ्रमण (विचरण) करने लगते हैं। सौन्दर्य या रस ऐसी दृष्टि है जिसके आगोश में हम बँध जाते हैं। इस सौन्दर्य या रस में रचनात्मकता भी होनी चाहिए। यदि कलाकार कला में एक ही अभिव्यक्ति को व्यक्त करता जायेगा तो वह आकर्षित नहीं करेगी। निरन्तर नवीनतापूर्ण आभास होना आवश्यक है। रस या सौन्दर्य दृश्य जगत के कण - कण में विस्तीर्ण है जो परमात्मा के प्रकाश का ही एक अंश है।
कुमार स्वामी ने प्रारम्भ में भारतीय कला के इतिहास पर लेखन प्रारम्भ किया। धीरे - धीरे वे दर्शन की ओर आकर्षित हुए। इससे अनेक कला दर्शन का विकास दृष्टिगत है। आनन्द कुमार स्वामी के सिद्धान्त भारत, चीन, ईरान, अरब, यूनान तथा रोमन सभ्यताओं पर एवं हिन्दू, बौद्ध, जैन, ईसाई इत्यादि की मध्यकालीन धार्मिक परम्पराओं पर आधारित हैं। उन्होंने कोई आदर्श सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की। उनके लिए दर्शन जीवन का ही एक अंग था। वास्तविक दैनिक जीवन से सम्बन्धित सार्वभौमिक सत्य को भारतीय दृष्टि से उन्होंने जिस प्रकार देखा था उसी से उनके कला सिद्धान्त निकले हुए हैं। सृष्टि के पदार्थों को प्रायः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है- सुन्दर और असुन्दर उनका कोई सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। प्लेटों के अनुसार प्रत्येक अपनी रुचि के अनुसार ही सुन्दर वस्तुओं में से किसी को प्रिय समझता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सौन्दर्य का आदर्श अलग होता है किन्तु इसका यह मत नहीं कि दूसरे के आदर्श अच्छे नहीं होते और अपना आदर्श ही सर्वश्रेष्ठ होता है। कला में भी यही तथ्य दृष्टिगत है। विभिन्न कलाकारों के अनेक आदर्श रहे हैं। कलाकारों के समान दर्शक भी विभिन्न रुचियों के होते हैं। इसका प्रमुख कारण रुचि की सापेक्षता है। कहा गया है कि ईश्वर को केवल चरम सौन्दर्य, प्रेम अथवा सत्य के रूप में ही ज्ञात किया जा सकता है। यह स्वीकार किया गया है कि सच्चा रसिक (सौन्दर्य प्रेमी) सरस एवं रस हीन कृति में अन्तर कर सकता है। इस विरोधाभास को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ? किसी वस्तु के सुन्दर कहने से हमारा आशय है कि वह हमें सुख प्रदान करती है, अच्छी लगती है। पर यदि हम किसी कलाकृति को सुन्दर कहते हैं तो या तो हम उसे मन से चाहते हैं या उनके विषय और क्रिया व्यापार का समर्थन करते हैं या उसके रंग, ध्वनि, इत्यादि की मिठास और आकर्षण के कारण वह वस्तु हमें अच्छी लगती है। वास्तव में रसयुक्त कलाकृति को सुन्दर अथवा रसवन्त और अच्छी लगने वाली प्रिय को कहना चाहिए। किसी कलाकृति के पीछे निम्न चार स्थितियाँ होती हैं-
1: कलाकार का सौन्दर्य सम्बन्धी सम्प्रदाय।
2. इस सम्प्रदाय के आधार पर बनी कृति।
3. कलाकार की भाषा, संकेत तथा प्रतीक।
4. रसिकों की प्रतिक्रिया।
इस तरह कलाकृति का सौन्दर्य मुख्यतः कलाकार से ही सम्बन्धित रहता है। सौन्दर्य को भांपा नहीं जा सकता क्योंकि कलाकार से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं है। रसिक भी कलाकार के अनुभव की कल्पना करता है। कला का अनुभव एक सम्पूर्ण अनुभव है। कला में वही सुन्दर है जिसमें विषय और व्यंजना विधि में संगतिपूर्ण सम्बन्ध स्पष्ट परिलक्षित है. इसमें रूप तथा प्रतिपाद्य की एकता हो। जिस प्रकार भक्त के हृदय में भक्ति का उदय अपने में स्वत: होता है वैसे ही सौन्दर्य दृष्टि भी सहज और स्वतः स्फूर्ति होती है। यह किसी एक व्यक्ति में दूसरे के द्वारा उत्पन्न नहीं की जा सकती। जो दर्शक कलाकृति का प्रभाव ग्रहण करने तथा कल्पना में असमर्थ है उसे रस (सौन्दर्य) की अनुभूति नहीं हो सकती। रसास्वादन की प्रतिभा कुछ ईश्वर प्रदत्त और कुछ संस्कार को बढ़ाने वाली होती है। इस प्रकार कलाकार और दर्शक दोनों के लिये ही प्रतिभा की आवश्यकता सौन्दर्य के अनुभव के लिए अनिवार्य मानी गयी है। कलाकृति में किया हुआ तकनीकी परिश्रम ही केवल रस का कारण नहीं है उसमें रसिक की स्वयं की अनुभूति का योग रहता है। रस का आस्वादन ब्रह्मानन्द के समान और लोकोत्तर है। इसीलिए यह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। सौन्दर्य का ज्ञान अलौकिक होता है। इस प्रकार धर्म और कला एक ही अनुभव के दो नाम हैं। जैसे सत्य के अस्तित्व को दार्शनिक ही अनुभव करता है। उसी प्रकार सौन्दर्य की यथार्थता को कलाकार ही अनुभव करता है। ये तीनों एक ही ईश्वर के तीन रूप हैं किन्तु कलाकार अपनी कृतियों के द्वारा ही अपने अनुभव को प्रेषित करता है और विषय के अनुरूप चयन करता है। वह सत्य को छोटे-बड़े, जड़ और चेतन, अच्छे और बुरे सभी में देखता है। किसी उपासना में एक निश्चित आधार अथवा रूप आवश्यक है। हम संसार की प्रत्येक वस्तु में उस असीम के सौन्दर्य का दर्शन करते हैं। भारतीय कला में कृति कामधेनु के समान है जिसमें से दर्शक अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विषय वस्तु ग्रहण करते हैं।
|
|||||