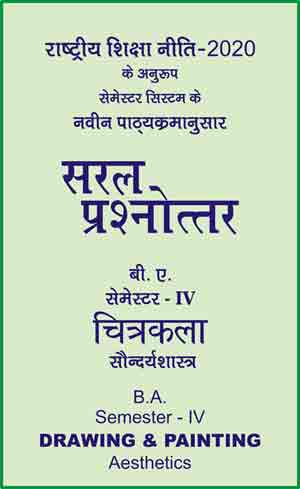|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला बीए सेमेस्टर-4 चित्रकलासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- रवीन्द्रनाथ टैगोर का कला - सौन्दर्य सम्बन्धी चिन्तन क्या था, बताइये?
उत्तर-
रवीन्द्रनाथ टैगोर की कला-सौन्दर्य सम्बन्धी विचारधारा कला ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। ब्रह्म सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है तथा प्रकृति के अंग जब स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं तब वह कला है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचारों पर पाश्चात्य दार्शनिकों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित है। इन्होंने पाश्चात्य व भारतीय दर्शन में संगति लाने का प्रयास किया है। ये सौन्दर्य के प्रत्येक पक्ष के उपासक थे। साहित्यिक पक्ष के अन्तर्गत राजनैतिक स्वतंत्रता आन्दोलन में इनका पूर्णरूपेणं सहयोग रहा। ये शान्तिपूर्वक शांति निकेतन में कलाओं के माध्यम से सौन्दर्य दर्शन एवं उसकी उपासना करते रहे। इन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन एवं समीक्षा की है। भाषाओं में बंगला, हिन्दी व अंग्रेजी भाषाओं पर इनका पूर्ण अधिकार था। नया छंद बंगला में लिखने का कार्य इन्होंने किया। जिस प्रकार हिन्दी गद्य का श्रेय भारतेन्दु जी को है, उसी प्रकार नये बंगला गद्य का श्रेय टैगोर को है। संस्कृत के ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों इत्यादि का गहन अध्ययन इनके चिन्तन में स्पष्ट परिलक्षित है। रवीन्द्रनाथ टैगोर का चिन्तन उपनिषदों से अत्यधिक प्रभावित है। आध्यात्मिक चिन्तन सौन्दर्य का एक अंग माना है। वड्सवर्थ की भाँति ही रवीन्द्रनाथ टैगोर भी प्रकृति में ब्रह्म व सौन्दर्य का दर्शन करते हैं तथा दोनों को एक-दूसरे का पर्याय मानते हैं।
प्रकृति के परिवेश में ये ईश्वर के दर्शन करते हैं। वर्ड्सवर्थ की एक कविता है जिसमें सूर्यास्त में ईश्वर दर्शन की बात बतायी गई। रवीन्द्रनाथ ने पाश्चात्य दर्शन की एक बात का विरोध किया कि धर्म कला की अभिव्यक्ति के लिए हानिकारक है। पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार, जब तक कला की अभिव्यक्ति धर्म पर आधारित है तब तक कला कुण्ठित ही रहती है उसका स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाता। इन्होंने इसके विरोध में कहा कि भारतीय धर्म की परिभाषा पाश्चात्य धर्म से अलग है। धर्म व ईश्वर हमारे जीवन का ही एक अंग है जैसे बुद्ध। उन्हें ईश्वर का रूप देते हुए भी लोक़ का एक अंग माना है। इनकी धर्म सम्बन्धी व्याख्या प्रकृति को देवतुल्य मानती है। आधुनिक कला में भी धर्म का विरोध करने की जरूरत नहीं हुई। इनके अनुसार जो वस्तु धारण की जाये वही धर्म है। बुद्ध, कृष्ण आदि धर्म के प्रतीक थे। इस प्रकार भारत में कला और धर्म का अन्योन्याश्रित सम्बन्धा है। हमारा धर्म एवं धार्मिक काव्य किसी भी प्रकार से हमारी सृजनशीलता में बाधक नहीं। कला में उसकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक है। इस प्रकार दर्शन की विषय वस्तु पर अपनी सशक्त व स्पष्ट विचार दिये। अपने दार्शनिक विचारों में वे कभी उपनिषदों, भगवान बुद्ध, ईसा, महात्मा गाँधी, एवं बर्नार्ड शा के निकट दृष्टव्य हैं। कला बाह्य सृष्टि से भिन्न और स्वतंत्र सृष्टि है, जिसे रवीन्द्र ने मानस सृष्टि या मानसिक जगत् की संज्ञा में परिभाषित किया। कला की उत्पत्ति के संदर्भ में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तीन प्रकार के विचार दिये हैं-
1. कला की उत्पत्ति पूजा से मानी। मनुष्य अपने से अधिक बलशाली प्राकृतिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयत्न करता है एवं परिचय हो जाने पर उनकी अभिव्यक्ति करता है, वही कला है।
2. बेले नृत्य भी कला उत्पत्ति का साधन है। ये वे लोक नृत्य है जो अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े थे। उदाहरण शिकार पर विजय प्राप्त करने पर हर्षोल्लास से नृत्य-गान। इससे चित्रकला का विकास हुआ।
3. मनुष्य की आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यात्मक अनुभूति।
यह कलाकार की व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित है कि मानव सृष्टि का कितना अंश अभिव्यक्त करता है। सौन्दर्य को अभिव्यक्त करने का कार्य युगों से चलता आ रहा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की मान्यता है कि कला के रूप में मानव सृष्टि ज्यों की त्यों हैं। कला और साहित्य सृष्टि की इस प्रक्रिया में रवीन्द्रनाथ तीन बातों पर बल देते हैं-
1. बाह्य-सृष्टि का आन्तरिक प्रवेश।
2. मानसिक जगत की सृष्टि,
3. उसकी अभिव्यक्ति के रूप में कला की सृष्टि।
रवीन्द्रनाथ टैगोर की दृष्टि में कला का उद्देश्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। वे मनुष्य का जगत् के साथ तीन प्रकार का सम्बन्ध मानते हैं-
1. शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए,
2. मन या मस्तिष्क की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
3. व्यक्ति की संतुष्टि के लिए।
सौन्दर्य रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार - आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार कोई अलौकिक शक्ति है जो इस सम्पूर्ण जगत् का नियंत्रण करती है। वास्तविक अलौकिक सौन्दर्य शक्ति का अनुभव करते हैं तो हमें आनन्द की अनुभूति होती है। सत्य और सौन्दर्य एक ही वस्तु है जो सत्य है वही सुन्दर है उसी से आनन्द की प्राप्ति होती है। सत्य में ही सौन्दर्य का बोध तभी होता है, जब हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने सौन्दर्य को शिव से जोड़ा है। सौन्दर्य मंगलमयी एवं कल्याणकारी है। किन्तु सभी प्रकार के सुन्दर मंगलमय नहीं मानते बल्कि जो सौन्दर्य अपनी पूर्णता पर पहुँच जाता है वही मंगलमय होता है। मंगल एक सापेक्षित शब्द है क्योंकि मंगल के साथ ही अमंगल की भावना जुड़ी होती है। सौन्दर्य का स्वरूप निश्चित करते हुए रवीन्द्रनाथ टैगोर ने सौन्दर्य को एक ऐसी शक्ति माना है जो सजीव है और हमारे मन को प्रभावित करती है। सौन्दर्य में आध्यात्मिकता का समन्वय होता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के समान रस सिद्धान्त की व्याख्या नहीं की है। भारतीय सौन्दर्यशास्त्र में सभी रस को संवेगों से सम्बद्ध मानते हैं। संवेग को समझने के लिए भाव तथा विचार को समझना आवश्यक है। भावना में सत्य और असत्य का प्रश्न ही नहीं। कला का सम्बन्ध संवेग या अनुभूतियों से है। अनुभूतियाँ दो प्रकार की मानी जाती है-
1. कलात्मक सौन्दर्यानुभूति
2. व्यावहारिक अनुभूतियाँ।
सौन्दर्यात्मक अनुभूतियों में विलगता होती है। वह निष्प्रयोजन और निरुद्देशीय होती है इसमें प्रयोजन होते हैं। जीवन में संवेग स्पष्ट परिलक्षित है जो प्रेरक का कार्य करती है। संवेग जीवन को चलाने की शक्ति है। संवेगों का सम्बन्ध सौन्दर्यात्मक अनुभूति से नहीं हो सकता क्योंकि इस अनुभूति में लय व्यावहारिकता से ऊपर उठ जाती है। रवीन्द्रनाथ टैगोर पाश्चात्य एवं भारतीय दोनों मतों को अस्वीकार करते हैं और इनकी मान्यता है कि भारतीय विचारकों में महत्वपूर्ण यह दोष है कि रसानुभूति के समय विषय का लोप हो जाता है और यह उचित नहीं है। रसानुभूति के समय चेतना और विषय एक साथ रहते हैं न तो विषय का लोप होता है और न ही चेतना विषय को लुप्त करती है बल्कि विषय और चेतना में एक संगति उत्पन्न करता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कला शैली अलग सृजनात्मकता, परिकल्पना तथा प्रयोग की ऐसी त्रिवेणी प्रवाहित की जो कालान्तर में आधुनिक कला का आधार बनी। शचीरानी गुटु के अनुसार "प्रकृति के अनन्त अभिसार, बासन्तिक उन्माद की आँख-मिचौनी और अपरूप सृष्टि की प्रकाश छाया के इंगित, व्यंजना और क्षणिक स्पर्श से उनमें स्वयमेव व सुप्त कलाकार जागा जिसने बालक से चापल्य और भीतरी कौतुक को. आत्मबद्ध आवेगों और भावातिशयता में उड़ेल दिया। सुमधुर गायक, प्रतिष्ठित कवि, तत्व चिन्तक, अद्भुत साहित्यकार, देशभक्त, धर्म विवेचक इत्यादि विभूतियों से सुशोभित कलाकार रवीन्द्रनाथ टैगोर आज विश्व में कला गुरु के नाम से विख्यात हैं। फ्रेंच कलाकार सेंजा की भाँति किसी भी विषय में तथ्य में पैठने की प्रवृत्ति इनमें भी थी और इस बाह्य निरीक्षण के आधार पर तट पर अभिव्यंजित इनकी कल्पना वैशिष्ट्यपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक रूप में दर्शक के समक्ष उभरकर आती है। इस क्षेत्र में उन्होंने नवीन तकनीक, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति एवं मौलिक प्रयोगों से जिस शैली की नींव रखी उसने आधुनिक भारतीय चित्रकला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यही कारण है कि वनिता बंसल ने रवीन्द्रनाथ टैगोर को-
First Indian modern nature painter of International standard (प्रथम आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय भारतीय प्राकृतिक चित्रकार) कहा है।
रवीन्द्रनाथ टैगोर का मानना है चित्र में, कलात्मक तत्वों की तुलना में भावात्मक तत्वों पर अधिक बल देना चाहिए जिससे कलाकार किसी भी दृष्य को बाह्य वातावरण पर ही विचरण न करके आन्तरिक चक्षु से उस दृश्य की गहराई में पैठ कर विषय की आत्मा को चित्र पद पर साकार कर सके। रवीन्द्रनाथ ने चित्रण कार्य कविताओं की की रम काट से प्रारम्भ किया। इन्होंने पेस्टल, एर्चिंग, ड्राइप्वाइंट, जलरंग, इंक आदि विविध माध्यम अपनाये।
|
|||||