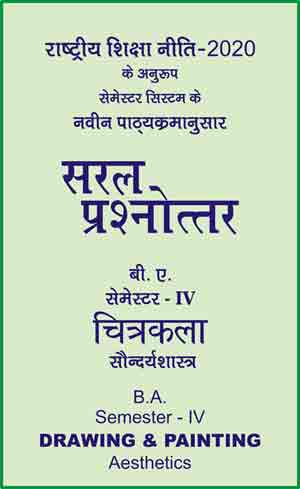|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला बीए सेमेस्टर-4 चित्रकलासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- कला क्या है? हीगेल द्वारा प्रतिपादित कला के वर्गीकरण के विषय में बताइये।
उत्तर -
हीगेल द्वारा कला का वर्गीकरण
(Classification of art by Hegel)
समय 1770 - 1881
कलाकृतियों का विभाजन अन्य सभी की तुलना में हीगेल का विभाजन अधिक उत्कृष्ट माना गया और ललित कलाओं के सन्दर्भ में उसी के आधार पर वास्तु मूर्ति, चित्र, संगीत एवं काव्य आदि कलाओं को महत्व दिया। हीगेल ने कला-विभाजन तीन दृष्टियों से किया है। उनका विचार रहा है कि कला के दो पक्ष हैं-
(1) एकता अर्थात आध्यात्मिक अर्थ, जो कलाकृति की आत्मा है।
(2) गेंदो को अनेकता अर्थात् कलाकृति का भौतिक पक्ष, जिसे इन्द्रियाँ ग्रहण करती हैं। अतएव कलाकृति के तीन पक्ष हैं-
(1) अभिव्यंजना का विषय
(2) रूप अथवा भौतिक सामग्री
(3) उपर्युक्त इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध।
(1) अभिव्यंजना के विषयों के आधार पर कलाएँ तीन प्रकार की होती हैं-
(क) प्रमातृमूलक अथवा कलाकार की आन्तरिक अनुभूति से सम्बन्धित (Subjective)
(ख) प्रमेयमूलक अथवा बाह्य वस्तु पर आधारित (Objective)
(ग) परतत्वमूलक (Absolute ideational)
प्रथम प्रकार की कला उन सुन्दर रूपों को उत्पन्न करती है जो उपयोगी हैं। द्वितीय प्रकार में कला किसी माध्यम की कलात्मक विशेषताओं का ही आधार लेकर अग्रसित होती है। केवल तीसरे प्रकार की ही कला सर्वश्रेष्ठ होती है।
(2) भौतिक सामग्री के आधार पर कलाकृतियों को पाँच भागों में विभक्त कर सकते है -
(1) वास्तुकला
(2) मूर्तिकला
(3) चित्रकला
(4) संगीत कला
(5) काव्य कला
ये पाँच कलाएँ तीन वर्गों में रखी गयी हैं-
(क) प्रतीकात्मक (Symbolic) - वास्तुकला
(ख) शास्त्रीय (Classical) - मूर्तिकला
(ग) स्वच्छन्द (Romantic) - चित्रकला, संगीत कला तथा काव्य।
वास्तुकला यान्त्रिक और अंगहीन पदार्थ (Mass) पर आधारित रहती है और सम्मात्रा (Symmetry) के अनुसार उसे बौद्धिक रूप से व्यवस्थित करती है। इसकी कृतियाँ भाव से केवल बाहरी रूप से सम्बन्धित रहती हैं। अतः यह प्रतीकात्मक होती हैं।
मूर्तिकला के द्वारा आन्तरिक भाव का केवल संकेत मात्र दिया जा सकता है। यह शास्त्रीय स्तर की कला है। यह अन्तर्वस्तु को मानवीय शरीर की सर्वोत्कृष्ट आकृति में परिवर्तित करके उसे शान्त और स्थिर रूप में प्रकट करती है।
चित्र, संगीत तथा काव्य स्वच्छन्द कलाएं हैं। हीगेल का सौन्दर्यात्मक दर्शन त्रयात्मक है। इसे कला दर्शनकला "हीगलीय त्रय" (Hegelian trio) भी कहा गया।
इस विवेचन से यह निष्कर्ष दृष्टिगत है कि स्थापत्य बाह्य कला है, मूर्तिकला वस्तुपरक है, जबकि चित्र संगीत एवं काव्य अन्तर्मुखी हैं। जिस कला में माध्यम जितनी सीमा तक अनिवार्य रहता है वह कला उतनी ही निम्न कोटि की हो जाती है क्योंकि माध्यम की अनिवार्यता के कारण कलाकार स्वयं को स्वच्छन्द रूप में व्यक्त नहीं कर सकता।
हीगेल ने अपने वर्गीकरण में काव्य को ही श्रेष्ठ माना है परन्तु कलाओं को तीन न मानकर पाँच माना है-

हीगेल - (G. W. F. Hegal) - हीगल का जन्म 27 अगस्त, 1770 में हुआ। ये जर्मनी के दार्शनिक थे। हीगेल के विचारों का ही परिणाम मार्क्सवाद था जिसने पाश्चात्य राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया। हीगल को जर्मन दर्शन में अरस्तू कहा जाता है। यह सत्य है कि हीगल काण्ट से प्रभावित था, किन्तु फिर भी दोनों में कुछ अन्तर हैं काण्ट भौतिकी विद्वानों से प्रभावित थे तथा हीगेल समाज दर्शन एवं मानव इतिहास से प्रभावित थे। उनके दर्शन को विकासवादी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा किसी विकास सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया। उनके विचारों में परिवर्तन एवं विकास का स्थान अरस्तू के दर्शन की भाँति था। हीगल के सौन्दर्यशास्त्र ने पहले के समस्त विरोधों को समाप्त करने का प्रयास किया। हीगेल दर्शन में पहले के विचारों को निष्कर्ष कहने का तात्पर्य यह था कि इसमें यूनानी एवं काण्ट के विचारों का समन्वय एवं समिश्रण किन्तु हीगेल के दर्शन का आधार यूनानी है और उसका परिणाम जर्मन है। हीगेल के सम्पूर्ण चिन्तन को हम तीन भागों में बाँट सकते हैं
(1) तर्क - इसमें हीगेल के द्वारा विचार एवं तर्क का सम्बंध बताने का प्रयास किया गया। प्रकृति का दर्शन इसमें प्रकृति के विकास को समझाने हेतु तर्क दिये गये हैं।
(2) प्रकृति का दर्शन - इसमें प्रकृति के विकास को समझाने हेतु तर्क दिये गये है।
(3) आत्मा का दर्शन - इसमें इतिहास, संस्कृति परिवर्तन, कला धर्म एवं दर्शन पर विचार किया। कला धर्म एवं दर्शन को एक - दूसरे से सम्बन्धित बताकर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है।
हीगेल के अनुसार - वर्तमान जगत आभास मात्र है अतः विश्वआत्मा को ही शक्ति एवं मूल तत्व मानते हैं। यह सृष्टि चैतन्य के विकास का परिणाम मात्र है। मनुष्य के रूप में चैतन्य की अभिव्यक्तिवाद हुयी है। विकास का गुण केवल चैतन्य एवं इसीलिए यह चैतन्य विकास मर्यादित रूप में होता है। मानव बुद्धि विकासवाद के स्वरूप को तथा रहस्य को समझने में समर्थ है।
कला धर्म और दर्शन चैतन्य विकासवाद के सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। हीगेल के अनुसार विचार का इन्द्रिय अवतार है। अर्थात् विचारों का संवेदात्मक प्रस्तुतिकरण कला में होता है। कला में विचारों को इस तरह (प्रकार) से कि वे इन्द्रियों द्वारा प्रकट हो सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कला मस्तिष्क की वस्तु है। इनके अनुसार कला मस्तिष्क की वस्तु होने के साथ-साथ अनुभव - एवं ज्ञान की भी वस्तु है यह विचार एवं उसके रूप विचार का इन्द्रिय अभिव्यक्ति है। इन दोनों में विचार ही प्रधान है जो कला विचार को जितनी स्पष्टता एवं प्रधानता के साथ व्यक्त की जायेगी, वह उतनी ही श्रेष्ठ होगी। ललित कलाओं की श्रेष्टता का आधार विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। इनके अनुसार विचार, घृणा, सुख, दुख, प्रेम करना आदि है किन्तु ये विचार अन्तिम नहीं होते हैं। अन्तिम विचार केवल आत्मा हैं। हीगल के अनुसार यह सभी आत्म चेतनाओं में साकार होती है।
इन्होंने विश्वात्मा का कर्ता और चैतन्य माना है। हीगेल के विचार को दो भागों में बाँटा गया है-
(1) शुद्ध विचार - शुद्ध विचार वे हैं जो कि इन्द्रियों द्वारा किसी भी अंश में प्राप्त नहीं किया गया है।
(2) अशुद्ध विचार - अशुद्ध विचार वें कि जो अनुभव द्वारा आश्रित होते हैं।
एक प्रकार से विचार किया जाये तो हम पाते हैं कि कला विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है। विश्वात्मा अभिव्यक्ति कई प्रकार से की जा सकती है। जैसे विचार स्तर पर दर्शन के रूप हैं। अनुभव के स्तर पर धर्म के रूप, यही विचार जब हम अनुभूति के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तब वह कला कहलाती है। हीगेल ने कला को सत्य की अभिव्यक्ति कहा है। इसी प्रकार से मानव की समझ के लिये तीन स्तरों के आधार पर वह तीन रूपों में अभिव्यक्त होती है।
कला धर्म और दर्शन - हीगेल के अनुसार कला वाद है। धर्म प्रतिवाद है और दर्शनवाद यदि हम देखें तो ज्ञात होता है कि कला धर्म और दर्शन की विषय वस्तु विश्वआत्मा ही है। (केवल विश्वात्मा की अभिव्यक्ति करने के माध्यम) अलग-अलग माध्यम होते हैं, इसी प्रकार से हीगेल ने विश्वात्मा की तीन अवस्थाओं या माध्यम के आधार पर निम्न तीन अवस्था बतायी हैं।
प्रतिकात्मक - (वास्तुकला)
शास्त्रीयकला - (मूर्तिकला, चित्रकला)
रोमांटिक कला - (चित्रकला, संगीतकला, काव्य)
इस प्रकार हीगल ने पाँच प्रकार की कला मानी है - वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला।
प्रतिकात्मक कला - प्रतिकात्मक कला का अभिप्राय है कि हमारे विचार सहज रूप से व्यक्त न हो प्रतीक का रूप ले ले। इसका उत्कृष्ट उदाहरण मन्दिर है। प्रतिकात्मकता का प्रतीक केवल साधन होते हैं। त्रिभुज द्वारा ईश्वर को अभिव्यक्त किया जाता है। किन्तु एक वक्त था जिसनें नील नदी कला एवं उर्वक्ता का प्रतीक त्रिभुज माना जाता था। वर्तमान में भारत में इसी प्रकार के त्रिभुज को परिवार नियोजन का प्रतीक माना जाता था। इस प्रकार कला में प्रतीक के अनेक अर्थ भी हो सकते हैं और यही कारण है कि परमतत्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता। किन्तु प्रतीकों से चित्र को संकेत अवश्य मिले हैं।
वास्तु तांत्रिक कला - इसमें प्रतिकात्मक कला एवं शास्त्रीय कला, मूर्तिकला आदि आते हैं।
आत्म तांत्रिक कला - इसमें रोमांसवादी कला अर्थात् चित्रकला, संगीत, काव्य कलायें आती हैं।
शास्त्रीय कला - हीगल के अनुसार, यूनानी कला को उत्तम कला माना गया। इसमें सत्य है कि विश्वात्मा का आभास मानव शरीर द्वारा किया गया है। शास्त्रीय यूनानी कला में देवता तथा देवी पूर्णतया व्यक्तित्व पूर्ण देखने आते हैं जिसके द्वारा चित्र की अभिव्यक्ति पूर्ण होती है।
हीगेल के शब्दों में - "यूनानी शास्त्रीय कला चरोत्तम अवस्था में पहुँच गयी है।"
रोमांस कला - हीगेल के अनुसार शास्त्रीय एवं प्रतिकात्मक कलायें जहाँ आत्मा अथवा चेतना के आस-पास घूमती हैं। वही रोमांसवादी कला आत्मा व चेतना की गहराइयों में उतरकर एक आध्यात्मिक कला बन जाती है। रोमांसवादी कला का मूलतत्व मनोवेग है। इस कला में विचार अधिक संशक्त होते हैं। इस कला को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।
|
|||||