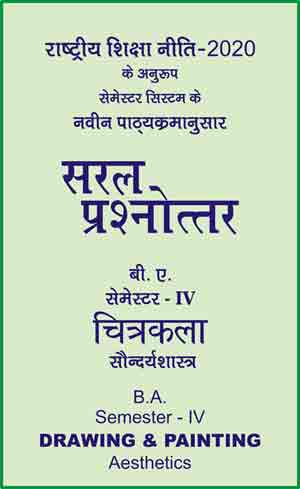|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला बीए सेमेस्टर-4 चित्रकलासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- कला का वर्गीकरण करते हुए उसके विभिन्न पक्षों को समझाइये।
अथवा
कलाओं का भारतीय विभाजन बताइये।
उत्तर - किसी भी कलाकार की कलात्मक अनुभूति को अखण्ड माना गया है एवं बाहरी माध्यम में प्रस्तुत कलाकृति को उसका बाह्य प्रत्यक्षीकरण (External Projection) मात्र कहा जाता है। परन्तु प्राचीन काल में कलाकृति को कला की क्रिया से अलग नहीं समझा गया और बाहरी माध्यम के आधार पर किये गये विभाजन को कलाओं का ही विभाजन माना गया। इसकी दो परम्परायें दृष्टिगत हैं-
(1) पूर्वी (भारतीय परम्परा)
(2) पाश्चात्य (यूरोपीय परम्परा)
कलाओं का भारतीय विभाजन
प्राचीन भारत में कलाओं का कोई स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ। वैदिक साहित्य में कलाकृतियाँ उपयोगी और मौलिक दो प्रकार की दृष्टिगोचर हैं। सामवेद में 64 कलाओं का उल्लेख है परन्तु कलाओं की संख्या उस समय इससे भी अधिक रहीं। कलाओं का सर्वप्रथम विभाजन वभ्रु पुत्र पांचाल ने दो भागों में किया-
(1) मूल
(2) आन्तर
परन्तु इस विभाजन का आधार स्पष्ट नहीं किया गया। वभ्रु पांचाल ने मूल कलाओं की संख्या 64 मानकर इनको चार भागों में विभक्त किया-
(1) कर्माश्रित कलाओं के वर्ग में गीत, नृत्य, वाद्य तथा चित्र को रखा गया।
(2) द्यूताश्रित
(3) शयनोपचारिका
(4) उत्तर कला।
64 कलाओं की संख्या वात्स्यायन के समय में भी प्रचलित रही। इन कलाओं में गीत, वाद्य, नृत्य, चित्र, छन्द रचना तथा समस्या पूर्ति से लेकर गुप्त लिपि पढ़ना, माला गूँथना तथा शय्या सजाना आदि विविध प्रकार की कलात्मक क्रियाओं का समावेश है जिन्हें आज कई अलग- अलग वर्गों में रखा जा सकता है।
भारत ने कला और शिल्प के भेद को एक नवीन मोड़ देने का प्रयत्न किया। नाट्य कला को प्रधान कला माना और अन्य कलाओं तथा शिल्पी को गौणं रूप में माना।
न तद् ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला॥
सन योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते।
सर्व शास्त्राणि शिल्पानि कमाणि विविधानि च ॥
- नाट्यशास्त्र 1/113-114
इसका समर्थन करते हुए आचार्य वामन ने नाटक को सभी प्रकार की प्रबन्ध रचना में सर्वश्रेष्ठ माना किन्तु इसी के साथ नाटक को चित्रपट की भाँति विचित्र भी कहा। चित्रकला के समकक्ष नाटक को खड़ा तो कर दिया परन्तु उनका मत अन्य कला आचार्यों में समर्थन न पा सका। केवल दो उल्लेख दृष्टिगत हैं जिनमें किसी विशेष आधार के कारण काव्य तथा चित्रकला को एक समान माना गया। एक उल्लेख में वामन ने रीति सिद्धान्त को काव्य में उसी प्रकार प्रतिष्ठित किया जिस प्रकार रेखाओं में चित्र की प्रतिष्ठा की जाती है।
दूसरा उल्लेख जयदेव का है जिन्होंने 'चन्द्रालोक में रस के आधार पर बनायी गयी कलाओं का एक साथ उदाहरण दिया-
काव्ये नाटये च कार्ये च विभावाद्यैर्विभावितः।
आस्वाद्यमानैकतनुः स्थायिभावो रसः स्मृतः॥
-चन्द्रालोक 6/3
नाटक तथा रूपक काव्य का ही एक गेंद है। अतएव भरतमुनि के अनुकरण पर भामह ने अन्य समस्त कलाओं को काव्यांग बनाकर गौणता प्रदत्त की।
भरत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रस की सम्पूर्ण अभिव्यंजना है। इसके साथ ही वे नाट्य को नैतिक उपदेशयुक्त, वेदना, पीडा तथा मानसिक थकान से व्याकुल व्यक्ति को शान्ति, यश, पुण्य तथा दीर्घ आयु देने वाला और सभी कलाओं में श्रेष्ठ मानते थे। तत्पश्चात् भट्टनायक ने इसमें अध्यात्म तत्व का समावेश कर दिया। संगीत तथा वास्तु को भी परम तत्व विषयक कलाएँ मान लिया गया।
इसी परम्परा में शार्डगदेव ने संगीत रत्नाकर में 'नाद ब्रह्म' तथा भोज ने समरांगण सूत्रधार में "वास्तु - ब्रह्म" की चर्चा की। दूसरी ओर ॠग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि अपने ही जीवन द्वारा स्पन्दित अनेक सम्भावनाओं से पूर्ण इच्छा आद्य पदार्थ में नया कम्पन उत्पन्न करती है। इसके अन्तर्गत काम एवं सृजन की इच्छा जन्म लेती है।
कुछ बनाने की इच्छा वह कल्पनाशक्ति है जिसमें समस्त कलाकृतियाँ रूप धारण करती हैं। इसी परम्परा में दण्डी ने 64 कलाओं को कामार्थ के आश्रित माना है। किन्तु भरत, भट्टनायक, शार्डगदेव तथा भोज आदि ने जो मत प्रतिपादित किये, उनके आधार पर नाट्य (काव्य) तथा संगीत के तीनों रूपों (गीत, नृत्य एवं वाद्य) को उपेक्षाकृत उच्च स्तर का माना।
आचार्यों ने उक्त मान्यता को अग्रसर करते हुये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला को भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाली कला के रूप में महत्ता प्रदत्त की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार चित्रकला, वास्तुकला का ही अंश है। नृत्य कला की भाँति चित्रकला का उद्देश्य भी तीनों लोकों की अनुभूति करते हुए उनके आदर्श रूपों को प्रस्तुत किया। इस प्रकार किसी कला को गौण और किसी कला को प्रमुखता प्रदत्त की गई।
लक्ष्य के आधार पर भारतीय मनीषियों ने काव्य की विधाओं और अन्य कलाओं को उपविधाओं की श्रेणी में रखा। शुक्राचार्य ने इनका अनुसरण किया और उन्होंने अपने अनुभवों को प्रकट किया। उन्होंने कहा है कि विधायें अनन्त हैं और कलाओं की संख्या भी स्पष्ट नहीं बताई जा सकती। फिर भी इनमें 32 विधाएँ और 64 कलाएँ मुख्य हैं। आचार्यों ने विधाओं को ज्ञानात्मक और कलाओं को क्रियात्मक कहा।
माध्यम के भेद से कलाओं का सर्वप्रथम विचार शुक्राचार्य ने किया, उन्होंने विद्या को (काव्य सहित) वाणी के माध्यम पर आश्रित तथा कलाओं को अन्य माध्यमों (वाणी को छोड़कर) के द्वारा सम्पादित होने वाली कहा है। जिस कला को गंगा भी कर सके।
इस प्रकार भारतीय मत से काव्य कला सर्वश्रेष्ठ है। संगीत कला दूसरे स्थान पर है। काव्य में आध्यात्म तत्व प्रधान होता है। संगीत का स्वरों पर आधारित अनुभव काव्य कला की अपेक्षा निम्नतर है। चित्रकला और मूर्तिकला दोनों ही वास्तुकला के अंग के रूप में मानी जाती हैं। अतः तीसरा स्थान भारतीय मत से वास्तुकला का है। वास्तु मूर्ति और चित्र के साधन आर्विभूत हैं।
कलाकृतियों का भारतीय विभाजन ललित तथा उपयोगी कला के रूप में कभी नहीं रहा। ललित कलाओं को उपयोगी कलाओं से पृथक रखने के सम्बन्ध में भारतीय प्राचीन उल्लेखों का आधार लेकर विचार-विमर्श किया गया, जो प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को सही रूप में प्रस्तुत नहीं करती। मात्र कारीगरी की वस्तुओं से कलात्मक कुशलतापूर्वक निर्मित वस्तुओं में चाहे कुछ अन्तर किया जाता हो फिर भी उनका वर्ग पश्चिमी विचारकों के ललित कला वर्ग के समान नहीं था।
कला का वर्गीकरण
(Classification of Art)
यूरोपीय विभाजन - यूरोपीय कला विभाजन की परम्परा का आरम्भ यूनान से प्रारम्भ हुआ। प्राचीन यूनानी विचारकों की ललित कला जैसी कोई मान्यता नहीं थी परन्तु वे उपयोगी और निरुपयोगी में भेद मानते थे। यूनान में कुछ प्रमुख कलाओं को अन्य कलाओं से अलग करने के लिये अनुकृति का आधार लिया गया। इसके अनुसार काव्य (जिसमें नाटक भी सम्मिलित हैं). संगीत तथा नृत्य, चित्र और मूर्ति को अनुकृतिमूलक कलाओं के वर्ग में रखा गया और भवन निर्माण तथा अन्य कलाओं को ऐसे वस्तुनिरपेक्ष रूपों का सृजन माना गया जिनमें किसी के स्वभाव या चरित्र, दैवी अथवा सांसारिक भावों और चेष्टाओं (क्रिया-कलापों) की अनुकृति नहीं होती। काव्य तथा संगीत की तुलना में चित्रकला और मूर्तिकला को केवल बाहरी यथार्थ की अनुकृति करने वाली कलाएं माना गया। ये स्थिर हैं। अरस्तू के अनुसार कलाओं का निम्न विभाजन किया जा सकता है-
(1) अनुकृति के आधार पर-
अनुकृतिमूलक (Imitative) - काव्य (नाटक सहित), नृत्य एवं संगीत, चित्र एवं मूर्ति ।
अनुकृतिविहीन (Non-Imitative) - वास्तु एवं अन्य उपयोगी कलाएँ।
(2) गति के आधार पर-
गतिशील (Dynamic) - काव्य एवं नाटक, नृत्य एवं संगीत।
स्थिर (Static) - चित्र तथा मूर्तिकला।
अरस्तू ने गतिशील कलाओं में लय की व्यंजना-शक्ति को बहुत महत्व दिया। श्रवणेन्द्रियों को ही इसका प्रमुख माध्यम माना था किन्तु दृष्टि द्वारा लयानुभूति में सहायता मिलने की सम्भावना दृष्टिगत होती है। अरस्तू के इसी विचारधारा पर अग्रसर इन्द्रियों के आधार पर हीगेल, बोसांके, देलाक्रा इत्यादि द्वारा कलाओं के श्रव्य एवं दृश्य वर्गीकरणों का उल्लेख स्पष्टतः परिलक्षित है-
श्रव्य कलाएँ (Auditory Arts) - काव्य तथा संगीत
दृश्य कलाएँ (Visual Arts) - मूर्ति तथा चित्र
श्रृव्य-दृश्य कलाएँ (Audio Visual Arts) - नाटक तथा नृत्य
काण्ट ने कलाकृतियों को ज्ञानेन्द्रियों द्वारा ग्रहण किये जाने वाले पक्ष के आधार के बजाय कर्मेन्द्रियों के आधार पर विभक्त किया-
वाणी की कला (Arts of Speech) - काव्य, संगीत (गायन-वादन)
रूप की कला (Arts of Form) - चित्र, मूर्ति, भवन
संवेदन - क्रीड़ा प्रधान कला (Arts of play of sensation)
वाणी में स्वर और शब्द दोनों का प्रयोग होता है अतएव केवल स्वरों अथवा ध्वनियों पर आधारित होने के कारण संगीत बहुत स्पष्ट नहीं होता, इसलिए अपने विभाजन में काण्ट ने संगीत को स्थान नहीं दिया।.
संवेदन क्रीड़ा में मांसपेशियों के अनुभव अत्यधिक महत्व रखते हैं। बोसांके द्वारा इस विभाजन को नवीन रूप प्रदत्त किया गया-
भाषा की कला (Arts of Speech) - काव्य
स्वरों की कला (Arts of Tones) - 'संगीत' (गायन-वादन)
रूप की कलाएँ (Plastic Arts) चित्र, मूर्ति तथा भवन
गति की कला (Kinetic Art) - नृत्य
कुछ अन्तर से इसी को दूसरे विचारकों ने निम्नवत् है-
(1) रखा रूप की कलाएँ (Plastic Arts) - चित्र,
(2) मूर्ति, भवन स्वर की कलाएँ (Tonal Arts) - संगीत
(3) शरीर की कलाएँ (Bodily Arts) - नृत्य
(4) मौखिक कलाएँ (Verbal Arts) - काव्य
परन्तु कालाओं का विभाजन कुल्पे ने इन्द्रियों के आधार पर तीन वर्गो के अन्तर्गत किया है-
अ- नेत्र से सम्बन्धित (Optic) - इसके अन्तर्गत निम्न तीन भेद हैं-
(1) समतल पर अंकित की जाने वाली कला (Surface Arts)-
(क) वर्णहीन अथवा एकवर्णी (Uncoloured or mono chrome) - रेखाचित्रण (Graphic Arts and Photography)
(ख) रंगीन (Polychrome) - चित्रकला एवं टेपेस्ट्री चित्रण - (मणिकुट्टिम एवं रंगीन कांच (Mosaic and stained glass सहित)।
(ग) गति सहित (With Motion) - यंत्र चालित दृश्य कलाएँ मूक चलचित्र तथा रंग-संगीत (Silent Cinema and Colour music)|
(2) ठोस अथवा त्रिविस्तारात्मक (Solid and three dimensional)-
(क) किंचित ठोस (Semi Solid) - अर्ध चित्र एवं निम्नोत्कीर्ण (Relief and Intaglio)
(ख) पूर्ण ठोस (Completely Solid) - मूर्तियाँ एवं चीनी मिट्टी के खिलौने (Sculpture and Ceramics)|
(ग) गति सहित (With Motion) - अनुकृतिमूलक अभिनय, लयात्मक गति तथा आतिशबाजी (Pantomime, Eurhythmics and Fire works)
(3) सम्मिलित प्रभावयुक्त (Aggregate Arts) - समतल एवं ठोस दोनों का सम्मिलित प्रभाव (Surface and plastic effects)-
(क) ढाँचा निर्मित करने वाली (Tectonic) - घर आदि (Building Arts)
(ख) स्थापत्य (Architecture) - स्मारक, प्रकृति अलंकरण, आन्तरिक भवन सज्जा तथा फूलों की कला। (Monuments, Landscape Design, Interior decoration and flower art)
ब - बकुल्पे ने 'ब' वर्ग में ध्वनि से सम्बन्धित कलाएँ (Acoustic Arts) - इसके अन्तर्गत तीन भेद किये हैं-
(1) स्वाश्रित (of tones) - संगीत (Music)
(2) शब्दाश्रित (of words) - काव्य (समस्त साहित्य एवं सम्भाषण कलाएँ) (Poetry All literature and Speech Arts)
(3) सम्मिलित प्रभावयुक्त (Aggregate) - स्वर-शब्दाश्रित गीत, गीतिनाटय (Song and Melodrama)
स - नेत्र एवं ध्वनि दोनों से सम्बन्धित (दृश्य-श्रव्य कलाएँ) (Optic-Acoustic Arts) - इनमें प्रायः वेशभूषा एवं पृष्ठभूमि में वास्तु आदि के दृश्य भी प्रयुक्त होते हैं।
(1) मुद्राओं एवं स्वरों पर आधारित (of gestures and tones) - गायन-वादन के साथ नर्तन, शब्द सहित बोलता हुआ चलचित्र।
(2) मुद्राओं, शब्दों एवं दृश्यों पर आधारित (of gestures, words and scenery) - नाटक तथा कठपुतली (Drama and Puppetry)
(3) मुद्राओं, स्वरों, शब्दों एवं दृश्यों पर आधारित (of gestures, tones, words and scenery) - संगीत, अभिनय, नृत्य तथा संवादों की कला-आपेरा (opera)।
इन्द्रियों के आधार पर कलाओं का जो वर्गीकरण अथवा विभाजन है उसमें मुख्य रूप से दृष्टि, श्रवणेंद्रिय तथा गति (मांसपेशियों की गति) के संवेदनाओं का ही आधार लिया गया है। कला अभिव्यंजना की भाषा है। भाषा का सम्बन्ध हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं से होता है। प्राकृतिक रूपों के प्रभाव से होता है।
|
|||||