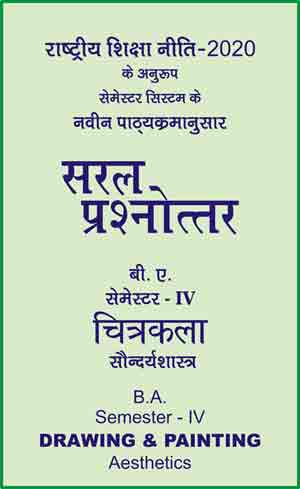|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला बीए सेमेस्टर-4 चित्रकलासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- भारतीय चित्रकला के छः अंगों के बारे में विस्तार से लिखिये।
उत्तर-
भारतीय चित्रकला में आकृति रचना का आधार दो प्रकार का है-
(1) भौतिक
(2) मानसिक।
किसी भी आकृति की रचना करते समय भारतीय चित्रकार आकृति के बाहरी रूप को ही नहीं देखता वरन् उसके गुणों तथा उसके पीछे छिपे भाव को भी देखता है।
प्राचीन भारतीय चित्र की परिभाषा के लिये 11वीं शताब्दी में लिखित कामसूत्र की टीका में एक सूत्र प्राप्त होता है, जो 11वीं शताब्दी और उससे पूर्व के चित्रों के संदर्भ में उचित है। प्रत्येक के लिये यह जानना अति आवश्यक है कि भारतीय शिल्पशास्त्रों में चित्र शब्द का प्रयोग आज से अधिक व्यापक अर्थ में किया गया है।
शिल्पाचार्य पत्थर, लकड़ी, लौह, स्वर्ण आदि में बनाई गई त्रि-आयामी प्रतिमा को चित्र कहते थे। आज हम जिसे चित्र अथवा पेंटिग कहते हैं उसे शिल्पशास्त्रानुसार चित्राभास कहा जायेगा, क्योंकि वह चित्र का आभास मात्र है। दूसरे शब्दों में, ठोस त्रि-आयामी रचना चित्र और द्वि-आयामी धरातल पर छाया प्रकाशादि से उसे दर्शाना चित्राभास ही होगा। क्योंकि चित्र तूलिका आदि से बनाया जाता है और उसमें भाव प्रदर्शन की क्षमता भी है अतः इसे आलेख्य की संज्ञा भी दी गई है। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने भी आलेख्य की व्याख्या करने के लिये ही निम्नलिखित सूत्र दिया है-
सादृश्यं वर्णिका भंग: इतिचित्र षडंगकम्॥
आलेख्य की परिभाषा के लिये चित्रषडंग का प्रयोग स्वयं यह सिद्ध करता है कि चित्र और आलेख्य के गुण मूलतः समान ही हैं। यह जानना भी आवश्यक है कि टीकाकार 'इतिचित्र षड़गकम्' कहकर यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि चित्र के यह छः अंग उसी प्रकार एक - दूसरे से सबद्ध हैं, जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंग।
चित्र और चित्रांग भिन्न न होकर एक ही वस्तु के सृजक अंग हैं। दूसरे चित्रषडंग शिल्पशास्त्र का विषय नहीं है। अतः यह चित्रकार के लिये निर्देशक सिद्धान्त नहीं कहे जा सकते। इसलिये इन्हें चीनी चित्रकला के सिद्धान्त से अलग समझना चाहिये जो कि चित्रकार के चित्र रचना के निमित्त आवश्यक क्रमिक प्रक्रिया का निर्देश देते हैं। कुल मिलाकर भारतीय चित्रषडग चित्र की एक भारतीय परिभाषा है। ये न केवल 11वीं शती एवं पूर्ववर्ती चित्रों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि उन सभी चित्रों पर लागू होती है, जिनका मूल भारतीय संस्कृति और परम्परा रही है। आचार्य अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने जब भारतीय कला के पुनरूत्थान हेतु प्राचीन भारतीय कलारूप और पूर्वी कला शैलियों के आधार पर नवीन सृजन आरम्भ किया तो साथ ही भारतीय विचारधारा को चित्र सम्बन्ध में समझने का प्रयास भी किया। यशोधर के चित्रषडंग सूत्र की पुनर्व्याख्या उन्होंने की तथा उसकी चीनी चित्रकला के नियमों से तुलना की। तभी से षडंग कला लेखक के आकर्षण का केन्द्र बना और उनके लेखकों ने अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की षड़ंग व्याख्या को भारतीय चित्र की व्याख्या के रूप में अपनाया। उन्होंने चित्र के छः अंग बताये-
1. रूपभेदा:
2. प्रमाणा
3. भावलावण्ययोजनम्
4. सादृश्यं
5. वर्णिका
6. भंग।
1. रूपभेदा - चित्र का आधार रूप है। अनेकों रूपाकृति सुनियोजित होकर चित्र का निर्माण करती हैं। इन आकृतियों की विविधता पर चित्र का आकर्षण निर्भर करता है। किसी भी रूप का अपना आकार, रंग व स्वभाव होता है। इन्हीं के आधार पर रूप का रूप से भेद किया जा सकता है। रूप सम्पूर्ण चित्र को भी कहते हैं और चित्र में प्रयुक्त रूपाकृतियों को भी। अतः सम्पूर्ण चित्र को आधार मानकर रूप भेद का अर्थ विभिन्न प्रकार के चित्रों से है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चित्र के चार भेद बताये गये हैं-
1. सत्य
2. नागर
3. वैणिक
4. मिश्र।
इसी प्रकार मानसोल्लास में चित्र के पाँच भेद बताये गये हैं-
1. विद्ध चित्र
2. अविद्ध चित्र
3. भाव चित्र
4. रस चित्र
5. धूलि चित्र।
आचार्य अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के अनुसार - "पहले-पहल रूप से आँखों का परिचय होता है, धीरे-धीरे उससे आत्मा का परिचय होता है - यही रूपमेद की प्रारम्भिक और अन्तिम बात है।"
आँख और आत्मा का योग ही कला रूप के आस्वादन का कारण होता है। एक सा देखने से रूचि का ह्रास होता है। एक ही भाव के बार-बार प्रकट होने से थकान होती है। तब परिवर्तन की आवश्यकता होती है। एक रस अथवा नीरस वस्तुओं के दोष भी दिखाई नहीं पड़ते परन्तु आकर्षक वस्तुओं में कोई दोष हो तो वह तुरन्त दिखाई पड़ता है। कारण यही है कि हम केवल उन्हीं आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं जो आकर्षक होती हैं। अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने सोलह प्रकार के रूप बताये हैं - "ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चतुष्कोण और नानकोण जैसे त्रिकोण, षट्कोण, अष्टकोण आदि। गोलाकृति, अण्डाकृति अथवा श्वेत, कृष्ण, नीलारूण, बैंगनी तथा नानावर्णों से मिश्रित रूपः रक्त पीतादि एक - एक स्वतन्त्र वर्ण, रूपः कठिन, श्लक्षण, पिच्छिल, मृदु, दारुण, छोटे, बड़े, मोटे - पटले, कटे - छटे, गोल, काले सफेद रंग, पंच रंगे इत्यादि।
यहाँ भी रूप के भेद का आधार आकार, वर्ण एवं स्वाभाव ही है। साथ ज्यामितीय, सजीव एवं प्रतीक आदि भेद हैं। अतएव रूपभेद के दो आशय हैं - प्रथम कलाकृति को एकरसता से बचाना, द्वितीय भावाभिव्यक्ति के लिये बनाई गई विभिन्न आकृतियों में अन्तर करना।
2. प्रमाणानि - किसी भी वस्तु का बाहरी आकार तथा उसके अवयवों का अनुपात प्रमाण द्वारा स्थिर किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किये जाते हैं और इनकी निर्धारित परम्परा को आचार्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। आचार्य अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने प्रमाण को प्रमातृ चैतन्य द्वारा प्राप्त ऊँचे - नीच, दूर - निकट, सफेद-काला, जल - स्थल इत्यादि का भेदाभेद बताया। यहीं प्रमातृ चैतन्य जब मानसिक रूप में प्रकट होता है तो प्रमाण चैतन्य कहा जाता है। क्योंकि प्रमाण का सम्बन्ध दर्शक के प्रमाण चैतन्य से है। अतः चित्र के सभी तत्व जिनका सम्बन्ध विषय-वस्तु से पहचान कराने अथवा विषय का मानसिक ज्ञान कराने से है 'प्रमाण' कहलायेंगे।
इस प्रकार चित्र में प्रमाण का अर्थ लक्षण तथा अंगानुपात होता है। प्रमाण को लक्षण, अनुपात, प्रत्यक्ष तथा उपमान जाना जा सकता है। उदाहरण ऋषिगण को जटाजूट धारण, मृगचर्म और तेजस्विता से जाना जाता है। रात्रि के चित्रण में चन्द्र, तारा, उलूक का चित्रण किया जाता है। यहाँ पर अनुमान का सम्बन्ध विभिन्न जाति एवं गुण वाले मानव देह की लम्बाई, चौड़ाई तथा विभिन्न अंगों का सानुपात चित्रण विधान, शिल्प शास्त्रों में वर्णित है। जैसे - हंस पुरुष अपनी ही अंगुली के मान से 108 अंगुल लम्बाई वाला होता है। भद्रपुरुष 106 इत्यादि।
शुक्राचार्य ने पुरुषाकृतियों को 5 प्रकार का माना है - नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार। प्रमाण का एक अंश ताल कहलाता है। एक ताल बारह अंगुल का होता है। अतएव विभिन्न आकृतियाँ निम्न प्रकार अंकित करनी चाहिये-
नर - साधारण आठ ताल, उत्तम नव ताल।
क्रूर - बारह ताल।
असुर - सोलह ताल
वामन एवं कुमार - पाँच ताल।
स्त्रियों को पुरुषों से छोटा अंकित किया जाता है।
नवताल के अनुसार प्रतिमा के 9 भाग किये जाते हैं-
पहला भाग माथे से ठोड़ी तक,
दूसरा कन्धे से छाती तक
तीसरा छाती से नाभि तक
चौथा नाभि से कूल्हे तक
पाँचवा तथा छठा कूल्हे से घुटने तक
सातवां व आठवां घुटने के निचले भाग से टखने तक
नवें भाग का चतुर्थांश केश, गला, घुटनों की टोपी तथा चतुर्थांश पैर का टखने से निचला भाग होता है।
चौड़ाई की दृष्टि से सिर एक ताल, ग्रीवा 1/2 ताल, एक कंधे से दूसरे कंधे तक की चौड़ाई तीन ताल, वक्षस्थल 1 - 1/2 ताल, कटि (नाभि से ऊपर) सवा ताल, कूल्हे लगभग 1 - 3/4 ताल। हाथ की लम्बाई 4 ताल, जिसमें कीं से कुहनी पौने दो ताल, कुहनी से कलाई 1 - 1/4 ताल, हथेली 1 ताल होती है। सम्पूर्ण मुख के तीन बराबर भाग किये जाते हैं। जिनमें एक भाग मस्तक से लेकर आँखों के मध्य तक, दूसरा भाग नासिका की नोंक तथा तीसरा भाग ठोड़ी तक होता है।
3. भाव - भारतीय चित्रकला में भाव का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। चित्र रचना का महत्वपूर्ण उद्देश्य भावाभिव्यक्ति अथवा रसानुभूति है। चित्र की आत्मा (भाव) की उत्पत्ति के संदर्भ में दो आधार मुख्यतः विचारणीय हैं।
1. चित्रकार के वे भाव जिनको वह चित्र में रूपायित करता है
2. दर्शक के हृदय में उत्पन्न होने वाले वे भाव जो चित्र के अवलोकन से उत्पन्न होते हैं।
वस्तुत: दर्शक के हृदय में होने वाले भाव चित्र के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ही रसोत्पत्ति का आधार हैं। चित्र तो मात्र प्रेरक ही रहता है। भरतमुनि ने भाव की व्याख्या करते हुये कहा है कि "भाव वह है जो उसी प्रकार व्याप्त हो जाय जिस प्रकार गन्ध या रस किसी वस्तु में व्याप्त हो जाती है।" रस के सन्दर्भ में भी भाव ही मूल तत्व हैं तथा विभावादि की सहायता से भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है। नाट्यशास्त्र के अनुसार, - "विभाव और अनुभाव आदि से उपचित होकर स्थायी भाव ही रस रूप में उद्भूत होता है।" चित्र के सन्दर्भ में इन स्थायी भावों और रसों का नाम इस प्रकार दिया गया है-
| स्थायी भाव | रसानुभूति |
| रति | श्रृगार |
| हास | हास्य |
| शोक | करूण |
| उत्साह | वीर |
| क्रोध | रौद्र |
| भय | भयानक |
| जुगुप्सा (घृणा) | वीभत्स |
| विस्मय (आश्चर्य) | अद्भुत |
| निर्वेद (शान्ति) | शान्त |
भावों की व्यंजना में रस-दृष्टियों तथा हस्त मुद्राओं का प्रधान रूप से प्रयोग होता है किन्तु शरीर के अन्य अंगों से भी भाव-प्रदर्शन का कार्य अंग कर्म द्वारा सम्पादित किया जाता है। चित्रसूत्र में कहा गया है कि घरों में शृंगार, हास्य तथा शान्त रसों के चित्र लिखने चाहिये किन्तु राजभवन तथा देवालयों में सभी रसों के चित्र लिखे जा सकते हैं।
लावण्य योजना - चित्रकृति भावपूर्ण होने के साथ-साथ लावण्य युक्त भी होनी चाहिये। रायकृष्ण दास के अनुसार "भाव के साथ - साथ लावण्य योजना भी होनी चाहिये। लावण्य बाह्य सौन्दर्य का व्यंजक है।
4. सादृश्यं - सादृश्य का अर्थ है - वस्तु जैसी प्रतीत होती है अथवा जैसी वह मानस को दिखाई देती है। चित्रकला का कार्य इस सादृश्य की रचना है। लक्षणों का सादृश्य आकृति में भावव्यंजना उत्पन्न कर देता है। जैसे "विरहणी और मछली का सादृश्य आकृति का सादृश्य नहीं माना जा सकता परन्तु मछली की तड़फ के लक्षण मानवाकृति में यदि संयोजित कर दिये जायें तो भाव रूप का सादृश्य होगा। आचार्य अवनीन्द्र नाथ ठाकुर ने सादृश्य की व्याख्या इस प्रकार की "सादृश्यस्य भाव इति सादृश्य।' एक का भाव जब दूसरे का उद्रेग कर रहा है तभी सादृश्य होता है।
5. वर्णिका - वर्ण चित्र का प्राण है। चित्र का अर्थ ही 'रंग-बिरंगा' है। चित्र का वह अंग जो सबसे पहले दर्शक का ध्यान आकृष्ट करता है वह वर्ण (रंग) ही है। वर्णिका का एक अर्थ रंग, रोगन, स्याही है तो दूसरा अर्थ रंग भरने का यंत्र कलम या कूची है। शिल्पशास्त्रों में मूल रंगों का उल्लेख मिलता है। सफेद, पीला, हरा, नीला, रक्ताभ, नील कमल जैसा, जामुनी इत्यादि मिश्र वर्णों का उल्लेख है। मिट्टी अथवा धातु पर सोना, चाँदी, ताबाँ, अभ्रक, राजवन्त, सिन्दूर, हरिताल, चूना, लाख, इगुर तथा नील।
वर्ण को विभिन्न रसों के साथ भी सयोजित किया गया है।
6. भंग (भंगिमा) - भारतीय कला मानवाकृति प्रधान होने के कारण इसमें अंग-भंगि का बहुत महत्व है। देह के खडे होने की भंगिमा को चार मुख्य रूप में बताया गया है।
1. समभंग - सीधी खड़ी मानवाकृति जिसमें देह का भार दोनों पैर पर बराबर हो।
2. अभंग - सीधी खड़ी आकृति में यदि देह का भार एक पैर पर थोड़ा अधिक हो जाये तो संतुलन नहीं रह पाता। इस भंगिमा को अभंग कहा गया है।
3. त्रिभंग - यदि आकृति में संतुलन रेखा में तीन मोड़ आ जायें तो मुद्रा में गतिमान संतुलन आ जाता है इसे त्रिभंग कहा गया है।
4. अतिभंग - यदि आकृति में अधिक झुकाव आ जाये जैसे- शिवमजी की ताण्डव नृत्य की मुद्रा, तो इसे अतिभंग कहा गया है।
यदि रूपभेद, प्रमाण, भावलावण्य योजना, सादृश्य और वणिका का अर्थ एक सर्वगुण चित्र के अवयवों से है तो 'भंग' के अभाव में ये सब अपूर्ण ही ठहरते हैं। ये सभी भारतीय कला में सर्वत्र प्रयोग किये गयें हैं।
|
|||||