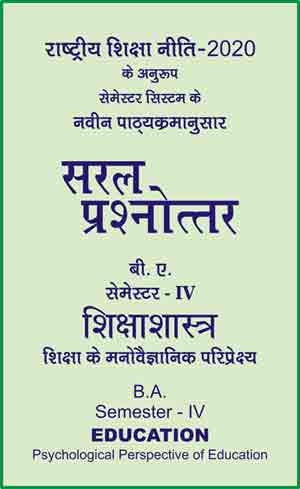|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 शिक्षाशास्त्र बीए सेमेस्टर-4 शिक्षाशास्त्रसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 शिक्षाशास्त्र - सरल प्रश्नोत्तर
स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य
अभिप्रेरणा के शाब्दिक तथा मनोवैज्ञानिक अर्थ में अन्तर है।
अभिप्रेरणा के शाब्दिक अर्थ से केवल किसी कार्य को करने का बोध होता है।
शाब्दिक अर्थ में हम किसी भी उत्तेजना को 'अभिप्रेरणा' कह सकते हैं।
मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से अभिप्राय केवल आन्तरिक उत्तेजना से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है।
वस्तुतः मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा एक आन्तरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।
प्रेरणा एक अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता। इस पर आधारित व्यवहार को देखकर ही इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है।
प्रेरणा का प्रश्न 'क्यों' का प्रश्न है।
गुड के अनुसार - "प्रेरणा कार्य को आरम्भ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है।"
सिम्पसन के अनुसार - "प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आन्तरिक शक्तियां या आवश्यकतायें उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है।"
मैकडोनाल्ड के अनुसार - "अभिप्रेरणा व्यक्ति के अन्दर ऊर्जा परिवर्तन हैं जो भावात्मक जागृति तथा पूर्ण अपेक्षित उद्देश्य एवं अनुक्रियाओं से निर्धारित होता है।"
एटकिन्सन ने अभिप्रेरणा को परिभाषित करते हुए कहा है कि- - "अभिप्रेरणा का संबंध किसी एक अथवा अधिक प्रभावों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति को उद्वेलित करने से होता है।"
वुडवर्थ के अनुसार - " योग्यता + " योग्यता + अभिप्रेरणा से निष्पत्ति प्राप्त होती है।
प्रेरणा से व्यक्ति की योग्यता का विकास होता है।
पी. टी. यंग के अनुसार - "प्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का प्रेषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है।
ऐटरिल के अनुसार - "प्रेरणा का अर्थ है सजीव प्रथा से।"
प्रेरणा एक मनोव्यावहारिक क्रिया है।
प्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है।
प्रेरणा से किसी विशेष क्रिया को करने का संकेत मिलता है।
प्रेरणा द्वारा उत्पन्न- क्रिया लक्ष्य की प्राप्ति तक रहती है।
प्रेरणा दो प्रकार की होती है-
(1) सकारात्मक तथा
(2) नकारात्मक
सकारात्मक प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है।
सकारात्मक प्रेरणा को आन्तरिक प्रेरणा भी कहा जाता है।
शिक्षक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों तथा परिस्थितियों का निर्माण कर बालक को सकारात्मक प्रेरणा प्रदान कर सकता है।
नकारात्मक प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव के कारण करता है।
शिक्षक प्रशंसा, निन्दा, पुरस्कार, प्रतिद्वन्द्विता आदि का प्रयोग करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है।
नकारात्मक प्रेरणा को बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है।
बालक को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक या आन्तरिक प्रेरणा का प्रयोग अधिक उत्तम समझा जाता है।
प्रेसी के अनुसार - "अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा आन्तरिक प्रेरणा से निम्नतर है।"
अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारकों को अभिप्रेरक कहते हैं।
अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं-
(1) आन्तरिक तथा
(2) बाह्य।
पूर्ण रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति के बाद ही शांत होता है।
आन्तरिक अभिप्रेरक का तात्पर्य मनुष्य की शारीरिक अथवा जैविक अभिप्रेरणा से होता है यथा - आत्मरक्षा, भूख, प्यास, काम।
बाह्य अभिप्रेरणा से तात्पर्य मनुष्य के पर्यावरणीय अथवा मनोसामाजिक अभिप्रेरकों से होता है' यथा - आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर, वकील, जज, इंजीनियर नेता आदि बनने की इच्छा से है।
अभिप्रेरणा की उत्पत्ति संबंधी मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं-
(1) मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत ( Instinct Theory)
(2) मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत (Psycho Analytic theory)
(3) अन्तर्नोद सिद्धांत ( Drive Theory)
(4) प्रोत्साहन सिद्धांत ( Incutive Theory)
(5) शरीर क्रिया सिद्धांत ( Psysiological Theory) तथा
(6) मांग सिद्धांत (Need Theory)
मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडुगल ने किया।
इस सिद्धांत की मान्यता है कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है। और उसकी मूलप्रवृत्तियों के पीछे छिपे संवेग ही अभिप्रेरकों का कार्य करते हैं।
मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड हैं।
फ्रायड के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाली अभिप्रेरणा के दो मूल कारक होते हैं-
(1) मूल प्रवृत्तियां
(2) अचेतन मन।
अन्तर्नोद सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक हल (Hull) ने किया था।
प्रोत्साहन सिद्धांत का प्रतिपादन वोल्स तथा काफमैन ने किया था।
वोल्स के अनुसार प्रोत्साहन दो प्रकार के होते हैं-
(1) धनात्मक तथा
(2) ऋणात्मक।
धनात्मक प्रोत्साहन व्यक्ति को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
ऋणात्मक प्रोत्साहन जैसे दण्ड, बिजली का झटका आदि बिजली का झटका आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं।
शारीरिक क्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक मार्गन ने किया था।
मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन अब्राहम मास्लो ने किया था।
मांग सिद्धांत के अनुसार - मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है।
अभिप्रेरण प्रक्रिया तथा परिणाम दोनों है।
अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है।
अभिप्रेरणा व्यक्ति को रुचि के अभाव में भी क्रियाशील रखती है।
व्यक्ति चाहे आन्तरिक अभिप्रेरकों से अभिप्रेरित हो या वाह्य अभिप्रेरकों से, इनसे उत्पन्न अभिप्रेरणा सदैव आन्तरिक होती है।
आवश्कतायें, अन्तर्नोद, प्रोत्साहन, प्रेरक अभिप्रेरणा स्रोत हैं।
हिलगार्ड के अनुसार - आवश्यकता अन्तर्नोद को जन्म देती हैं।
मैस्लो ने प्रेरकों का वर्गीकरण
(1) जन्मजात
(2) अर्जित के रूप में किया है।
थामसन ने प्रेरकों को स्वाभाविक एवं कृत्रिम में बांटा है।
गैरेट ने प्रेरकों को जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक में विभाजित किया है।
जन्मजात प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाये जाते हैं यथ - भूख, प्यास, निद्रा, काम।
अर्जित प्रेरक अर्जित किये जाते हैं या सीखे जाते हैं यथा - रूचि, आदत, सामुदायिकता आदि।
स्किनर के अनुसार - अभिप्रेरणा, सीखने का राजमार्ग है।
सफलता या निष्पत्ति, योग्यता तथा अभिप्रेरणा के योग पर निर्भर करती है।
सीखने का उच्चतम लक्ष्य अधिकतम निष्पत्ति होती है।
शिक्षार्थियों की आकांक्षायें, आवश्यकतायें, कक्षा का वातावरण, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग शिक्षक का व्यवहार, प्रशंसा एवं निन्दा, पुरस्कार एवं दण्ड, प्रतिद्वन्द्विता एवं प्रतियोगिता, सफलता का ज्ञान शिक्षार्थियों की अभिप्रेरणा को बढ़ाने की विधियां है।
|
|||||