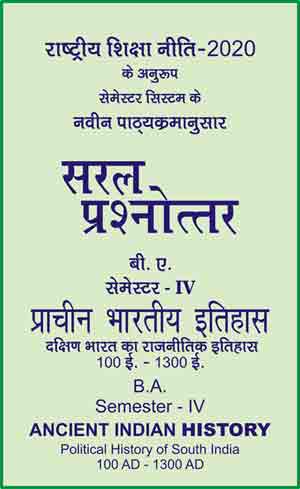|
प्राचीन भारतीय और पुरातत्व इतिहास >> बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृतिसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- राष्ट्रकूटकालीन शासन-प्रणाली पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए।
अथवा
राष्ट्रकूट प्रशासन का वर्णन कीजिए।
अथवा
राष्ट्रकूटों की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए।
अथवा
राष्ट्रकूटों की प्रशासन के विषय में आप क्या जानते हैं?
अथवा
राष्ट्रकूट प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. राष्ट्रकूटकालीन सैन्य संगठन के विषय में बताइए।
2. राष्ट्रकूटों के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ क्या थीं?
उत्तर-
राष्ट्रकूटकालीन प्रशासन
राष्ट्रकूटों के राजनैतिक महत्व का वर्णन करते हुए सुलेमान ने लिखा है, "वे (राष्ट्रकूट) भारत के सर्वशक्तिशाली सम्राट थे तथा देश के अन्य नरेश उनसे भयभीत रहते थे।'
जहाँ तक दीर्घकालीन राजनैतिक स्थायित्व का प्रश्न है, राष्ट्रकूटों ने लगभग 225 वर्षों तक जनिष्कंटक राज्य किया। इतने लम्बे समय तक बहुत कम हिन्दू राजवंशों ने शासन किया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रकूट नरेशों के कठिन परिश्रम द्वारा दक्षिणी भारत का राजनैतिक गौरव श्रेष्ठता की सीमाओं को लाँघ गया था। राष्ट्रकूटों के महत्व तथा स्थायित्व के कारणों में उनके प्रशासन का सराहनीय योगदान था। इस बात पर सभी इतिहासकार एक ही मत रखते हैं।
राष्ट्रकूटों के प्रशासन की रूपरेखा का वर्णन निम्नवत् है -
सम्राट - राष्ट्रकूट सम्राट का सम्पूर्ण साम्राज्य पर एकाधिकार था। शासन की सम्पूर्ण शक्ति उसके हाथ में केन्द्रित थी। निरीक्षण तथा रणाभियान के समय को छोड़कर अन्य सभी अवसरों पर सम्राट राजदरबार में उपस्थित रहता था। सम्राट बहुमूल्य रत्नजड़ित वस्त्राभूषण धारण करता था। सम्राट के राजदरबार में अंगरक्षकों के अतिरिक्त सुन्दर नर्तकियाँ, अनेक अधीनस्थ सामन्त, राजदूत, सैनिक, प्रमुख अधिकारी, कवि, ज्योतिषी, चिकित्सक तथा श्रेणियों के प्रतिनिधि सम्राट की सेवा में उपस्थित रहते थे।
राष्ट्रकूट काल में ही स्वेच्छाचारी राजतन्त्र की स्थापना की गयी थी। साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केन्द्रित रहती थी, वही मुख्य सेनानायक और मुख्य न्यायाधीश होता था, उसको विस्तृत अधिकर प्राप्त थे। अधिकतर राजा का बड़ा पुत्र ही उसकी मृत्यु पर सिंहासनारूढ़ होता था, परन्तु राष्ट्रकूट इतिहास में कहीं-कहीं सिंहासन के लिए गृहयुद्ध के उदाहरण भी मिलते हैं।
युवराज - राजपद की परम्परा वर्षों से चली आ रही थी। साधारणतः राजा का सबसे बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता था। इसी को युवराज की संज्ञा दी जाती थी। कभी-कभी छोटे पुत्र के अधिक योग्य होने पर भी उसे युवराज पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। गोविन्द तृतीय के लिए ऐसा ही किया गया था। देश के शासन में राजा की सहायता करना 'युवराज' का कर्त्तव्य था। युवराज के अतिरिक्त शेष राजकुमारों को प्रान्तीय गवर्नर नियुक्त किया जाता था। राजकुमारियों को भी राष्ट्रकूट प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान दिये जाते थे।
मंत्री - प्रशासन में मंत्रियों की मंत्रणा विशेष महत्व देती थी। मन्त्रियों की योग्यता और उनकी नियुक्ति की विधि से हम परिचित नहीं हैं लेकिन कल्पना की जा सकती है कि राजनीतिक और सैनिक कार्यों में सामर्थ्य और प्रवीणता के लिए ही उन्हें चुना जाता होगा। मंत्री को राजा का दायां हाथ कहा गया है।
राजकीय पदाधिकारी - यह ज्ञात नहीं है कि साम्राज्य के अनेक प्रान्तों और जिलों पर केन्द्र सरकार किस प्रकार निरीक्षण और प्रतिबन्ध रखती थी लेकिन ऐसा लगता है कि राष्ट्रकूटों के अधीन ऐसे अधिकारी थे जो सम्पूर्ण साम्राज्य में निरीक्षण यात्राएँ करते थे। सम्पूर्ण साम्राज्य की देख-रेख के लिए केन्द्रीय सरकार के अपने प्रतिनिधि भी थे। उनका प्रमुख कर्त्तव्य केन्द्रीय सरकार को आवश्यक जानकारी भेजना था।
अधीनस्थ राज्य - राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ भाग तो प्रत्यक्ष शासन द्वारा अनुशासित होते थे और शेष अधीनस्थ राज्य थे। प्रमुख सामन्तों को लगभग पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त थी। राजा की आज्ञा के बगैर वे ग्राम दान दे सकते थे। उनके अपने उपसामन्त होते थे। इन उपसामन्तों के लिए उन्हें राजा कहा जाता था। सामन्तों से सम्राट की आज्ञापालन करने की मांग की जाती थी, उन्हें नियमित शुल्क देना पड़ता था। राजधानी की देख-रेख के लिए उन्हें साम्राज्य की राजधानी में अपने प्रतिनिधि रखने पड़ते थे।
प्रत्यक्ष प्रसारित क्षेत्र - प्रत्यक्ष प्रसारित क्षेत्र के सम्बन्ध में एक विद्वान ने कहा है कि केन्द्र द्वारा सीधे प्रशासित क्षेत्रों को 'राष्ट्रों' और 'विषयों में बांटा गया था। एक 'विषय' में सम्मिलित ग्रामों की संख्या 1000 से 4000 तक थी। प्रत्येक 'विषय' को अनेक 'भुक्तियों का एक नामकरण सम्भवतः उनके मुख्य कार्यालय के नगर के नाम पर किया जाता था । प्रत्येक भुक्ति को 20 ग्रामों में बांटा जाता था। ग्राम सबसे छोटी प्रशासकीय इकाई थी।
राष्ट्र तथा राष्ट्रपति - प्रो. नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार, "राष्ट्र का प्रमुख 'राष्ट्रपति' कहलाता था। उसका अधिकार नागरिक और सैनिक प्रशासन दोनों पर था। अपने अधिकार क्षेत्र में शक्ति और व्यवस्था बनाये रखना उसका प्रथम कर्त्तव्य था। यदि कोई विद्रोह करे तो उसे एकदम दबाने के लिये उससे मांग की जाती थी।' 'राष्ट्रपति के नियंत्रण में पर्याप्त सैनिक शक्ति होती थी। प्रायः वह सैनिक अधिकारी भी होता था। उसे एक सामन्त की स्थिति और उपलब्धियाँ दी जाती थीं। राष्ट्रपति' की तुलना गुप्त प्रशासन के उपरिक से की जा सकती है। 'राष्ट्रपति' आर्थिक प्रशासन के भी अधिकारी थे। भूमि कर वसूल करना भी उनका कर्त्तव्य था। स्थानीय अधिकारियों और विशेषाधिकारियों का ब्योरा रखना उसका कर्त्तव्य था। मन्दिरो और ब्रह्मणों को जिन ग्रामों का राजस्व दे दिया जाता था उनके नाम और संख्या का विवरण भी उन्हें ही रखना पड़ता था। राजा की अनुमति के बिना वे राजस्व दान नहीं दे सकते थे। वे जिलों आदि के उच्चाधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते थे।
विषयपति तथा भोगपति - डॉ. मलिक के अनुसार, “विषयपति और भोगपति अपने-अपने सीमित क्षेत्रों में वही कार्य करते थे जो 'राष्ट्रपति' अपने विस्तृत क्षेत्र में करते थे। इन पदों पर नियुक्ति सैनिक सेवा के लिए उपहार के रूप में था। प्रशासनीय योग्यता की मान्यता के लिए की जाती थी। कभी-कभी ये पद वंशानुगत हो जाते थे। 'विषयपति' और 'भोगपति राजस्व एकत्र करने का अपना कार्य 'नग्दाकुण्ड' या 'देशयामकूट नामक कूलजुगत राजकर्मचारियों की सहायता से करते थे। इन कर्मचारियों को वेतन के रूप में बिना कर के भूमि दी जाती थी।'
ग्राम प्रशासन - डॉ. आर.सी. मजूमदार के अनुसार, "ग्राम और ग्राम कोषाध्यक्ष ग्राम प्रशासन के मुख्य पदाधिकारी थे। ये पद प्रायः कुलानुगत होते थे। ग्राम में कानून एवं व्यवस्था की स्थापना का दायित्व ग्राम प्रमुख पर था। उसके अधिकार में एक स्थानीय सेना होती थी। ग्राम प्रमुखों से सैनिक कप्तान के कर्त्तव्य निभाने की मांग की जाती थी। ग्रामों से कर एकत्र करने का दायित्व उन्हीं पर था। राजस्व को राजकोष में जमा करना होता था या धन्यागार में सुरक्षित रखा जाता था। ग्राम कोषाध्यक्ष एक सहकारी के रूप में कार्य करता था। प्रत्येक ग्राम में एक सार्वजनिक परिषद होती थी जिसमें प्रत्येक वयस्क गृहस्थ होता था। स्थानीय पाठशालाओं, तालाबों, मन्दिरों और सड़कों के प्रबन्ध के लिए उपसमितियाँ बनायी जाती थीं। वे धरोहर सम्पत्ति भी प्राप्त कर सकती थीं और दान देने वाली शर्तों के अनुसार उनकी व्यवस्था कर सकती थी। उपसमितियों को ग्राम प्रमुख के सहयोग से कार्य करना पड़ता था। ग्राम परिषदों, नागरिकों, अभियोगों का निर्णय भी करती थी और उन निर्णयों को सरकार कार्यान्वित करती थी। इसी प्रकार की सार्वजनिक परिषदें नगरों में भी थीं।'
सैन्य संगठन - राष्ट्रकूटों ने सैन्य संगठन पर विशेष बल दिया था। उनके पास एक विशाल सेना थी लेकिन इतिहास में यह निश्चित जानकारी नहीं मिलती कि सैनिकों की संख्या क्या थी। राज्य की प्रमुख सेना राजधानी में रहती थी लेकिन उत्तरी और दक्षिणी ओर भी थोड़ी-थोड़ी सेना तैनात थी।
एक विद्वान के अनुसार "राष्ट्रकूट सम्राट अत्यन्त महत्वाकांक्षी थे। अतः अपनी सेना को शक्तिशाली और कार्यकुशल बनाने की उन्होंने भरसक चेष्टा की। वे विशाल सेनाएँ रखते थे किन्तु सैनिकों की संख्या के विषय में हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। सेना का बहुत बड़ा भाग राजधानी में रखा जाता था। एक दक्षिण की सेना और एक उत्तर की सेना थी। स्थायी सेनाएँ प्रतिरक्षा और विजय के लिए रखी जाती थीं। अपनी पैदल सेना के लिए वे प्रसिद्ध थे लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अश्व सेना महत्वहीन थी। कुछ टुकड़ियां सामन्त और प्रान्तीय गवर्नर दिया करते थे। यह उस समय किया जाता था जब कई प्रमुख अभियान आरम्भ किये जाते थे। सैनिक जातियों का प्रबन्ध धनी व्यापारियों की सहायता और सहयोग से किया जाता था। सेना की भर्ती ब्राह्मणों और जैनियों सहित सभी जातियों में से की जाती थी। बांकेय, श्रीविजय, नरसिंह आदि राष्ट्रकूट सेनानी जैन थे।'
राजस्व के स्रोत - राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि- कर था, जो उपज का 1/4वाँ भाग होता. था। इसे भोग कर भी कहा जाता था। भोग कर के अतिरिक्त राज्य की आय बागों, वनों खानों आदि से भी होती थी। क्रय-विक्रय की वस्तुओं और चुंगी लेने की प्रथा थी । सामन्तों से भी अधिकतर बहुत भेंट प्राप्त होती थी। मन्दिरों से भी कर लेने की व्यवस्था थी लेकिन मन्दिरों पर बहुत कम कर लगाया जाता था।
प्रो. अल्तेकर के अनुसार - "राष्ट्रकूट साम्राज्य के राजस्व के कई स्रोत थे। सामन्तों से शुल्क के रूप में बहुत सा धन प्राप्त होता था। खानों, जंगलों और ऊसर भूमि से भी आय प्राप्त होती थी। 'उद्रंग' या 'भोग कर' के रूप में भूमि कर से भी पर्याप्त आय होती थी। यह पैदावार का लगभग पाँचवां भाग था। इसे पदार्थ रूप में दो या तीन किश्तों में लिया जाता था। फलों सब्जियों आदि पर भी कर लिये जाते थे। बहुत- सी वस्तुओं पर चुंगी और शुल्क लिया जाता था। ग्राम की यात्रा करने वाले अधिकारियों के निवास, निर्वाह और आने-जाने का प्रबन्ध ग्रामवासियों को निःशुल्क करना पड़ता था।'
सुलेमान ने - राष्ट्रकूट नरेशों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वे भारत के सर्वशक्तिशाली सम्राट थे तथा देश के अन्य नरेश उनसे बहुत डरते थे। जहाँ तक दीर्घकालीन स्थायित्व का प्रश्न है, राष्ट्रकूटों ने लगभग 225 वर्षों तक निष्कंटक राज्य किया। इतने दीर्घकाल तक राज्य करने का गौरव बहुत ही कम हिन्दू राजवंशों को प्राप्त हुआ। इस बात में संदेह नहीं है कि राष्ट्रकूट नरेश के कठिन परिश्रम द्वारा दक्षिण भारत की राजनीतिक दशा उत्कर्षता की सीमाओं को पार कर गई थी।
|
|||||