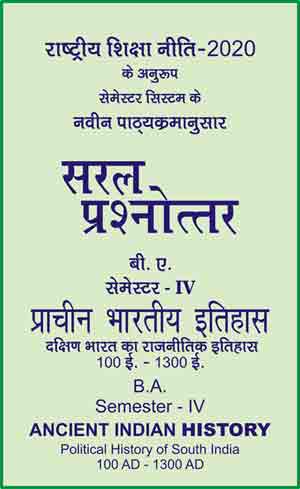|
प्राचीन भारतीय और पुरातत्व इतिहास >> बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृतिसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- राष्ट्रकूट काल की सामाजिक दशा, धार्मिक व्यवस्था, शिक्षा एवं साहित्य का वर्णन करते इस वंश का मूल्यांकन कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. राष्ट्रकूट काल की सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए।
2. राष्ट्रकूट काल की धार्मिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए।
राष्ट्रकूटों के धर्म के विषय में बताइए।
अथवा
3. राष्ट्रकूट काल की शिक्षा व साहित्य का वर्णन कीजिए।
4. राष्ट्रकूट काल की कला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर-
राष्ट्रकूट काल की सामाजिक दशा
विभिन्न जातियाँ - राष्ट्रकूट काल में विभिन्न जातियाँ और उपजातियाँ थीं। इब्न खुदर्दव के अनुसार इस काल में सात जातियाँ थीं-
(1) ब्रह्म
(2) कटारिया
(3) सुदरिया
(4) बेसुरिया
(5) संडालिया
(6) साब्कुफिया
(7) लहूद
ब्रह्म, कटारिया, सुदरिया, बेसुरिया और संडालिया का समीकरण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र और चाण्डाल से किया गया है। साब्कुफिया जाति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉ. अल्तेकर का मत है कि यह संस्कृत के 'सत क्षत्रिय' का रूपान्तर है। लहूद जाति एक प्रमुख जाति है जिसमें जादूगर और मदारी आदि सम्मिलित थे। अल्बरूनी ने सात जातियों के स्थान पर 19 जातियों का उल्लेख किया है। इसमें से 7 प्रमुख वर्ण थे, 5 निम्न जातियाँ और 7 अस्पृश्य ।
समाज में किसी जाति या वर्ण विशेष के लिए कोई निश्चित कार्य न था। ब्राह्मण व्यापार भी करते थे और सेना में भी भरती होते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय अपनी परम्पराओं को छोड़ते जा रहे थे।. वैश्वों की स्थिति अत्यन्त गिर चुकी थी और वे शूद्रों की श्रेणी में आने लगे थे। अल्बरूनी ने लिखा है कि "शूद्रों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी और वेद पाठन करने पर उनकी जिह्वा काट ली जाती थी।'
विवाह - समाज में सजातीय विवाह अच्छे माने जाते थे। परन्तु अन्तर्जातीय विवाहों का भी प्रचलन था। अनुलोम विवाह के भी उदाहरण मिलते हैं। अल्बरूनी का मत हैं कि राष्ट्रकूट काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी और कोई ब्राह्मण 12 वर्ष से अधिक की आयु की कन्या से विवाह नहीं कर सकता था।
स्त्रियों की दशा - राष्ट्रकूट काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी न थी। यद्यपि पर्दा प्रथा न थी परन्तु सती-प्रथा आरम्भ हो चुकी थी। दक्षिण में सती-प्रथा प्रचलित न थी परन्तु स्त्रियाँ अपने प्राचीन गौरव को खो चुकी थी।
रूढ़िवादिता - समाज में रूढ़िवादिता और संकीर्णता का बोलबाला था जिससे स्वतन्त्रता और प्रगतिशीलता समाप्त हो चुकी थी।
राष्ट्रकूट काल की धार्मिक व्यवस्था
हिन्दू धर्म - राष्ट्रकूट काल में हिन्दू धर्म का बोलबाला था। यह धर्म अनेक सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था। यज्ञों की प्रधानता थी और कुछ यज्ञ हिंसात्मक भी होते थे। उज्जयिनी में दन्तिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था।
शंकराचार्य का उत्थान भी इसी युग में हुआ था। शंकराचार्य ने संन्यास सिद्धान्त को प्रचलित किया और भारत के चार धामों में चार मठों की स्थापना की, परन्तु शंकराचार्य का संन्यास सिद्धान्त अधिक प्रचलित नहीं हुआ। कुमारिल ने यज्ञ विधि का विरोध किया।
राष्ट्रकूट काल में शैव और वैष्णव दोनों ही धर्म प्रचलित थे। राष्ट्रकूट नरेशों की मुहरों पर अनेक देवताओं की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। किसी मुहर पर 'विष्णु वाहन' तथा 'गरुड़ वाहन' हैं तो किसी पर देवता की मूर्ति। वैष्णव और शैव धर्म से सम्बन्धित अनेक मन्दिरों का निर्माण भी इसी युग में हुआ था। एक अभिलेख में ऐसे ही एक मन्दिर का उल्लेख हुआ है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की प्रतिमायें एक साथ स्थापित की गयी थीं। ऐलोरा की त्रिमूर्ति भी राष्ट्रकूट काल की है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी। पठारी स्तम्भों के लेखों में सूर्य मन्दिर का उल्लेख है। सलोत्गों में एक दुर्गा का मन्दिर भी था, मनगोलि में सरस्वती का मन्दिर भी स्थापित किया गया था।
जैन मन्दिर - राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, इन्द्र तृतीय और इन्द्र चतुर्थ ने जैन धर्म को प्रोत्साहित किया था। प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन अमोघवर्ष प्रथम का गुरु था, गुणभद्र कृष्ण द्वितीय का गुरु था। कृष्ण द्वितीय ने एक जैन मन्दिर को दान दिया था। इन्द्र तृतीय ने और इन्द्र चतुर्थ ने भी जैन धर्म को मान्यता प्रदान की थी। इन्होंने जैन मन्दिरों और मठों को बहुत अधिक धन दिया था।
बौद्ध धर्म - बौद्ध धर्म की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। बौद्ध आचार्य, जैन आचार्यों से शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके थे, परन्तु फिर भी इस काल में बौद्ध धर्म के कुछ अनुयायी अवश्य विद्यमान थे। अमोघवर्ष प्रथम के शासनकाल में कन्हेरी में एक बौद्ध संघ था। बल्लभी में भी प्रसिद्ध बौद्ध विहार और पुस्तकालय था। इस बात का भी उल्लेख हुआ है कि काम्पिल में भी एक बौद्ध विहार और पुस्तकालय था। बौद्धों में महायानी सम्प्रदाय अधिक प्रचलित था और तारादेवी की पूजा होती थी।
अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि राष्ट्रकूट शासक धार्मिक दृष्टि से अत्यन्त सहिष्णु थे। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था परन्तु फिर भी महालक्ष्मी की पूजा करता था। सलोत्गों के एक मन्दिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती थी। ऐलोरा की त्रिमूर्ति भी इस बात की साक्षी है कि राष्ट्रकूट राजा सभी धर्मों का आदर करते थे। डॉ. अल्तेकर ने लिखा है- "धार्मिक विषयों में राज्य का दृष्टिकोण उदार एवं सहिष्णु था। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म एक-दूसरे के साथ शान्ति और सामंजस्य में पनप रहे थे।'
शिक्षा और साहित्य
राष्ट्रकूट काल में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अनेक अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि राजा शिक्षा संस्थाओं को बहुत अधिक दान दिया करते थे। कहा जाता है कि भद्रविष्णुं ने कन्हेर के बौद्ध विहार को पुस्तकें खरीदने के लिये धन दिया था। सलोगों अभिलेख में एक विद्यालय का उल्लेख हुआ है जिस पर बहुत अधिक व्यय किया जाता था। इस विद्यालय में 27 छात्रावास थे। वल्लभी का बौद्ध विहार भी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। मन्दिरों में भी पाठशालाओं का प्रबन्ध किया जाता था। विद्यालयों में राज्य की ओर से अध्यापक नियुक्त किये जाते थे और गाँव में भी पाठशालाओं की व्यवस्था की गयी थी।
राष्ट्रकूट काल में साहित्य की भी विशेष उन्नति हुई। राष्ट्रकूट अभिलेखों की शब्दावली, वाक्य रचना और अलंकरणों के प्रयोग इस बात के साक्षी हैं कि इस युग के लेखकों को संस्कृत का अच्छा ज्ञान था।
राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष उच्चकोटि का विद्वान था। उसने कन्नड भाषा में 'कविराजमार्ग' नामक ग्रन्थ का सृजन किया जो कन्नड़ भाषा का सर्वप्रथम काव्यशास्त्र है। अमोघवर्ष के गुरु जिनसेन ने 'हरिवंश' और 'पार्श्वभ्युदय' नामक ग्रन्थों का सृजन किया। जिनसेन को भी अमोघवर्ष ने राज्यश्री प्रदान की थी, जिसने 'आदिपुराण' लिखा। अमोघवर्ष की सभा के एक विद्वान शंकटायन ने 'अमोघवृत्ति और एक अन्य विद्वान ने 'महावीराचार्य' व 'गणितसार संग्रह' नामक ग्रन्थों का सृजन किया। डॉ. भण्डारकर का मत है कि इन्द्र तृतीय के शासनकाल में त्रिविक्रम नामक एक विद्वान ने 'नल चम्पू' की रचना की। कृष्ण तृतीय के शासनकाल में हलायुध नामक विद्वान ने 'कविरहस्य' का सृजन किया। इस काल में कन्नड़ भाषा के कवि पम्पा हुए जिसने अनेक ग्रन्थों का सृजन किया। इनके द्वारा रचित ग्रन्थों में 'आदि पुराण और 'विक्रमार्जुनविजय' आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसी युग के एक अन्य विद्वान पोन्ना ने संस्कृत और कन्नड़ दोनों ही भाषाओं में काव्य का सृजन किया, फलस्वरूप उसे उभयकविचक्रवर्तिन' की उपाधि प्राप्त हुई। पोन्ना ने 'शान्ति पुराण' का सृजन किया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा और साहित्य की उन्नति की दृष्टि से राष्ट्रकूट काल दक्षिणी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
राष्ट्रकूटकालीन कला
राष्ट्रकूट काल में कला की अधिक उन्नति नहीं हुई। यद्यपि मौर्यों, गुप्तों तथा पल्लवों ने अपनी कलाकृतियों का विकास यथेष्ट किया था परन्तु राष्ट्रकूट इस क्षेत्र में पिछड़े रहे। इस युग की कला के कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-
एलोरा का कैलाश मन्दिर - एलोरा के कैलाश मन्दिर को राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा मन्दिर इस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है। डॉ. अल्तेकर का कथन है कि कैलाश मन्दिर का निर्माण सम्भवतः पल्लवों की राजधानी काँची से बुलाये गये कलाकारों के द्वारा किया गया था। इसमें गुहा स्थापत्य के दर्शन होते हैं। गुहा मन्दिर पर्वत को गहराई तक खोदकर बनाये जाते थे किन्तु यह. मन्दिर चोटी से तराश कर बनाया गया था। मन्दिर के चारों ओर पत्थर काटे गये हैं। बीच में पर्वत खण्ड जो शेष बचा है उसे सजाया गया है। इस मन्दिर का विमान (Body of the temple) एक समान्तर चतुर्भुज के आकार का है। यह 150 फुट लम्बा और 100 फुट चौड़ा है। यह विमान 25 फुट ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया है। एक सीढ़ी से व्यक्ति मन्दिर में जाते हैं। मन्दिर के ऊपर शिखर की ऊँचाई 95 फीट है। मन्दिर के सामने एक मण्डप 70 फुट लम्बा और 60 फुट चौड़ा बना है जो स्तम्भों पर रुका है।
इस मन्दिर के बाद एक नन्दी मन्दिर है जिसके दोनों ओर 51-52 फीट ऊँचे दो ध्वजस्तम्भ हैं जिन पर त्रिशूल स्थापित किये गये हैं। इस मन्दिर में जिस स्थापत्य के दर्शन होते हैं विद्वानों ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि इस प्रकार की कृतियों में जो अपने सौन्दर्य में एथेन्स और फ्लोरेन्स की कृतियों की तुलना करने के योग्य है, कदाचित भारतीय कला अपनी श्रेष्ठता की उच्चतम शिखर पर पहुँच जाती है।
इस मन्दिर की प्रशंसा करते हुए पर्सी ब्राउन लिखता है कि यह भारत में निर्मित कला का विलक्षण नमूना है।
कैलाश मन्दिर की स्थापत्य - कृतियों में प्रमुख हैं- गजासुर, संहारकशिव, नटराज, कैलाश पर्वत उठाता हुआ रावण आदि।
एलीफेण्टा की त्रिमूर्ति - राष्ट्रकूट काल में एलीफेण्टा की कुछ गुफाओं और उसमें स्थापत्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। इन कृतियों में त्रिमूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें शिव के तीन मुख प्रदर्शित है। भारतीय देव प्रतिमाओं में इनका विशेष महत्व हैं।
राष्ट्रकूट वंश का मूल्यांकन - राष्ट्रकूट वंश बड़ा प्रतिभाशाली वंश था। उसके विषय में एक विद्वान ने लिखा है- दक्षिण का लगभग 753 से 975 ई. तक राष्ट्रकूट वंश की सर्वोच्चता का काल सम्भवतः इसके इतिहास का सर्वाधिक शोभापूर्ण अध्याय है। 18वीं शताब्दी में मराठों के उदय से पहले दक्षिण के किसी अन्य राजवंश ने भारत के इतिहास में ऐसा प्रमुख भाग नहीं लिया। इसके कम से कम तीन शासक ध्रुव, गोविन्द तृतीय और इन्द्र तृतीय अपने विजय अभियान उत्तरी भारत के मध्य तक ले गये और सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों को पराजित करके उन्होंने इतिहास का प्रवाह ही बदल दिया। दक्षिण में भी उनकी सफलताएँ अपूर्व थीं जबकि कृष्ण तृतीय अपनी विजययात्रा में वस्तुतः रामेश्वरम् तक पहुँच गया था। भारत की सभी महान शक्तियों जैसे उत्तर के प्रतिहार और पाल वंश और दक्षिण के पूर्वी चालुक्य और चोल वंश को उन्होंने एक या दूसरे समय में अपने अधीन किया। निस्संदेह कभी-कभी उन्होंने हार भी खाई, किन्तु कुल मिलाकर वे अपने शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध सफल हुए।
दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रकूट शासकों का समय अत्यधिक गौरवपूर्ण रहा। दक्षिण भारत के किसी अन्य राजवंश ने इतने लम्बे समय तक इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया। दक्षिण भारत के इस वंश के शासकों ने सुदूर दक्षिण तक आक्रमण किये और कृष्ण द्वितीय ने रामेश्वर तक पहुँचकर अपने कीर्तिस्तम्भ का निर्माण किया। इसके शासक उत्तर भारत में आक्रमण करने वाले दक्षिण भारत के पहले शासक थे। सम्राट ध्रुव और गोविन्द तृतीय ने उत्तर भारत के शक्तिशाली प्रतिहारों और पालों को पराजित किया तथा उत्तर भारत की राजनीति को गम्भीरतापूर्वक प्रभावित किया। राष्ट्रकूट शासकों ने भारत के तत्कालीन शक्तिशाली शासकों में से सभी को किसी न किसी समय परास्त किया। निस्सन्देह समय-समय पर उनकी पराजय भी हुई। परन्तु उनके शक्तिशाली सम्राटों का समय निर्विवाद सफलता का रहा है और उन्होंने समय-समय पर उत्तर भारत के शक्तिशाली प्रतिहार और पाल शासकों और दक्षिण भारत के चालुक्यों तथा चोल शासकों को परास्त किया। गुप्त शासकों के पश्चात् युद्धों में इतनी सफलता भारत के हिन्दू शासकों में किसी अन्य राजवंश के शासकों ने प्राप्त नहीं की।
राष्ट्रकूट शासकों ने परमेश्वर, परमभट्टारक, महाराजाधिराज आदि पदवियाँ धारण कीं। इस प्रकार वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और शक्तिशाली मानते थे सम्राट का पद पैतृक था और साधारणतया सबसे बड़ा पुत्र अथवा युवराज राज्य का उत्तराधिकारी होता था, परन्तु राजा निरंकुश न थे। वे राजधर्म के आधार पर शासन करते थे तथा प्रजा की भलाई तथा सुरक्षा उनका प्रमुख कर्त्तव्य था। राजा की सहायता के लिए मन्त्री तथा बड़े अधिकारी होते थे सम्राट के आधीन राष्ट्रपति अथवा विरापति होते थे। राज्य राष्ट्रों, भुक्तियों और गाँवों में बँटा होता था। अधीनस्थ शासकों और सामन्तों के पास भी विस्तृत अधिकार होते थे और वे समय-समय पर सम्राट की सैनिक सहायता करते थे।
राष्ट्रकूट शासकों ने संस्कृतिक प्रगति में सहयोग किया। धार्मिक दृष्टि से अधिकांश राष्ट्रकूट शासक हिन्दू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने वैदिक धर्म के अनुसार विभिन्न यज्ञ किये और पौराणिक हिन्दू धर्म के अनुसार विभिन्न हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की। उनके समय में हिन्दू धर्म की अत्यधिक प्रगति हुई। यद्यपि उनमें से कुछ ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया परन्तु राष्ट्रकूट शासक धार्मिक दृष्टि से अधिक उदार थे। उन्होंने जिन मन्दिरों का निर्माण किया उनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देवी- देवताओं की मूर्ति स्थापित की गयी। अन्य धर्मों के प्रति भी उनका व्यवहार सहिष्णुता का था। सम्राट अमोघवर्ष महावीर और लक्ष्मी दोनों को समान रूप से मानता था। कृष्ण द्वितीय के सामन्त पृथ्वीराज और, उसके पुत्र ने जैन मन्दिरों का निर्माण कराया जबकि उनके प्रपौत्र हिन्दू हुए। इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबों के प्रति भी राष्ट्रकूट शासक उदार रहे। उन्होंने अरबों को अपने धर्म को मानने तथा व्यापार करने की पूर्ण सुविधा प्रदान की। निस्सन्देह उनके समय में बौद्ध धर्म अवनति पर था, परन्तु उसका कारण उसकी स्वयं की दुर्बलता थी।
राष्ट्रकूट शासक शिक्षा - साहित्य की प्रगति में भी रुचि लेते थे। उनके समय में संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा की भी प्रगति हुई। राष्ट्रकूट शासकों ने हिन्दू और जैन विद्वानों का सम्मान किया। जिनसेन ने 'हरिवंश' और 'पार्श्वभ्युदय' की रचना की, शंकटायन ने 'अमोघवृत्ति' और महावीराचार्य ने 'गणितसार संग्रह' लिखा। ये सभी विद्वान सम्राट अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में थे जो स्वयं एक विद्वान था और जिसने स्वयं कन्नड़ भाषा में 'कविराजमार्ग' नामक एक ग्रन्थ को लिखा था। इसके अतिरिक्त कन्नड़ भाषा के तीन विद्वान पोन्ना', 'पम्पा' तथा 'रत्ना' भी इसी काल में हुए थे।
राष्ट्रकूट शासकों ने कला के क्षेत्र में किसी नवीन शैली को जन्म नहीं दिया, परन्तु तब भी उनके समय में बहुत से मन्दिर और मूर्तियाँ बनायी गयीं। उनके द्वारा बनवाये गये मन्दिरों में अब केवल एक मन्दिर प्राप्त होता है, वह ऐलोरा का प्रख्यात कैलाश मन्दिर है। पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया यह विशाल मन्दिर वास्तुकला का एक श्रेष्ठ नमूना है। डॉ. स्मिथ ने उसे भारत के वास्तु आश्चर्यों में सर्वाधिक विस्मयजनक माना है। इस मन्दिर के भीत्ति चित्रों में 'गंगावतरण' और रावण द्वारा कैलाश पर्वत के उठाये जाने के चित्र अत्यन्त सुन्दर और सजीव हैं। इस प्रकार राष्ट्रकूट शासकों ने दक्षिण भारत को ही नहीं बल्कि समकालीन उत्तर भारत की राजनीति को भी प्रभावित किया। निस्सन्देह उत्तर भारत की राजनीति में उनका हस्तक्षेप लाभदायक न रहा क्योंकि उत्तर भारत में उनके आक्रमणों के कारण प्रतिहारों के एक शक्तिशाली सार्वभौमिक राज्य के निर्माण में कठिनाई हुई जो देश के लिए हानिकारक रहा। परन्तु तब भी राष्ट्रकूट शासकों ने यश और शक्ति प्राप्त की। दक्षिण भारत की राजनीति और सांस्कृतिक प्रगति में उनका प्रभाव निस्सन्देह अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।
|
|||||