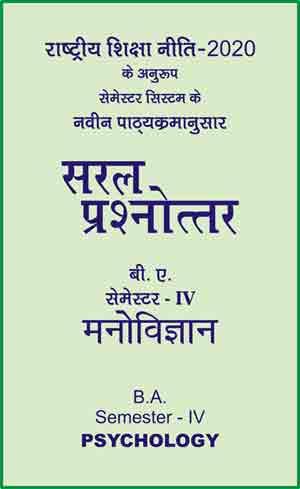|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञानसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- मद्यपानता के प्रमख हैतुकी की व्याख्या करें।
अथवा
मद्यपान के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. मद्यपान के जैविक कारकों का वर्णन कीजिए।
2. मद्यपान के मनोसामाजिक कारकों का उल्लेख कीजिए।
3. मद्यपान के सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
सामान्यतः जिस व्यक्ति को मद्यपान व्यसनी समझा जाता है, वह बहुत अत्यधिक मात्रा में मद्यसार पीता देखा गया है और इसके परिणामस्वरूप उसे अपने जीवन में कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मद्यपान के निम्नांकित प्रमुख कारण हैं-
(1) जैविक कारक - मद्यपान रोगियों के रक्त एवं शरीर की कोशिकाएँ मद्यपान पदार्थों के साथ अनुकूलित एवं अभियोजित हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप मद्यपान इन व्यक्तियों के लिए एक शारीरिक आवश्यकता हो जाती है। ऐसी स्थिति में वे कुछ समय के लिए अपने आपको शराब से वंचित करते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं एवं कई तरह के शारीरिक लक्षण जैसे पसीना आना, चक्कर आना, वमन की इच्छा होना, विभ्रम, ऐंठन आदि मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। इन शारीरिक कष्टों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति पुनः शराब पर टूट जाता है।
अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि मद्यपानता आनुवांशिक रूप से काफी प्रभावित होता है। कॉटन (1979) तथा गोल्डनमैन (1998) ने अपने अध्ययनों में पाया है कि मद्यपानी माता-पिता के बच्चों, भाई-बहनों में सामान्य लोगों की तुलना में तीन से चार गुना मद्यपान होती है। बोहमैन एवं सिगवार्डस्सन (1999) ने एक अध्ययन में पाया कि जब माताएँ मद्यपान करने वाली होती हैं तो उनकी पुत्रियों में मद्यपानता की सम्भावना अन्य ऐसी महिलाओं की तुलना में जिनकी माताएँ मद्यपानी नहीं थीं, चार गुना अधिक होती है।
(2) मनोसामाजिक कारक - मद्यपान की स्थिति में न केवल दैहिक निर्भरता बल्कि रोगी मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी विकसित कर लेता है। मनोवैज्ञानिकों ने तीन मुख्य मनोसामाजिक कारकों का उल्लेख किया है-
(i) व्यक्तित्व कारक - अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि संभाव्य मद्यपानी सामान्यतः सांवेगिक रूप से अपरिपक्व होते हैं, उन्हें दुनिया से काफी उम्मीद होती है, वे अन्य लोगों से अत्यधिक प्रशंसा एवं प्यार की उम्मीद करते हैं, असफलता के प्रति तीव्र हीनता, भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा कुंठा सहनशीलता की क्षमता कम होती है। कैडोरेट तथा उनके सहयोगियों (1996) एवं ड्रेक तथा भाईलैन्ट (1988) द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन व्यक्तियों का समाज-विरोधी व्यक्तित्व होता है, उनके मद्यपान व्यसनी होने की संभावना अधिक होती है।
(ii) प्रतिबल, तनाव ह्रास तथा पुनर्बलन - मनोवैज्ञानिकों के एक समूह की प्राक्कल्पना यह है कि कुछ लोग इसलिए मद्यपानता को अपना लेते हैं क्योंकि मद्यपान करने से उनकी जिन्दगी का तनाव, चिंता आदि में कमी आ जाती है। मद्यपान करके अपनी जिन्दगी की तनावपूर्ण परिस्थितियों में बिना किसी तरह के चिंता दिखलाए वे उत्तम निष्पादन बनाए रखने में सक्षम हो जाते हैं। लेभेनसन एवं उनके सहयोगियों ( 1980) तथा मूलानी (1999) द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि मद्यपानता व्यक्ति के तात्कालिक तनाव की स्थिति को कम कर देती है और व्यक्ति थोड़ी देर के लिए काफी अच्छा महसूस करने लगता है, जबकि इसका परिणाम बुरा हो सकता है।
(iii) वैवाहिक एवं अन्य घनिष्ठ सम्बन्ध - कॉक्स तथा क्लिंगर (1988) ने मद्यपानता की व्याख्या करने के लिए एक अभिप्रेरणात्मक मॉडल का प्रतिपादन किया है। इस मॉडल में मद्यपानता का उत्तरदायित्व स्वयं व्यक्ति पर ही लादा गया है। व्यक्ति द्वारा मद्यपान किए जाने का कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं ही चेतनं या अचेतन रूप से मद्यपान करने का निर्णय करता है क्योंकि इससे उसमें भावात्मक अर्थात् उसके मनोदशा में परिवर्तन आ जाता है तथा साथ ही साथ इससे उसे कुछ हद तक अपने साथियों का समर्थन भी मिलता है।
(3) सामाजिक-सांस्कृतिक कारक - मद्यपान के लिए किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि व्यक्ति को मद्यपान व्यसनी बनने में समाज की संस्कृति का भी योगदान होता है। वेल्स (1946), हार्टोन (1943), सुलकुनेन (1976) द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि निम्नांकित तीन ऐसे कारक हैं जो मद्यपान की ओर व्यक्तियों में उन्मुखता उत्पन्न करते हैं-
(i) हार्टोन (1943) - ने 56 ऐसे ही समाज की संस्कृतियों की समीक्षा की है और पाया है कि जिन सामाजिक संस्कृतियों में असुरक्षा का स्तर अधिक होता है, उनमें एलकोहल या मद्यपान करने की उन्मुखता अधिक देखी गयी है।
(ii) कुछ अध्ययनों में देखा गया है कि द्रुत सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक विघटन से भी मद्यपान के प्रति लोगों की उन्मुखता में वृद्धि होती है। मैककार्ड, मैककार्ड तथा गुडेमैन (1960) द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि शैक्षिक स्तर तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर गंदा होने से व्यक्तियों में मद्यपानता की प्रबलता भी अधिक होती है।
(iii) सामाजिक-सांस्कृतिक द्वारा मद्यपानता के प्रति लोगों में उत्पन्न मनोवृत्ति तथा प्रबलता निर्भर करती है। सुलकुनेन (1976) ने एक अध्ययन किया जिसके परिणाम में पाया कि यूरोपियन तथा यूरोपियन संस्कृति से प्रभावित छह देशों अर्थात् अर्जेन्टाइना, कनाडा, चिली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा न्यूजीलैण्ड द्वारा पूरे संसार का करीब 80% मद्यपान पिया जाता है। हालाँकि इन सभी देशों में पूरे संसार की जनसंख्या के मात्र 20% ही लोग रहते हैं।
स्पष्ट हुआ कि कई कारण एवं कई अवस्थाएँ ऐसी हैं जो व्यक्ति में मद्यपानता की ओर झुकाव उत्पन्न करती हैं।
|
|||||