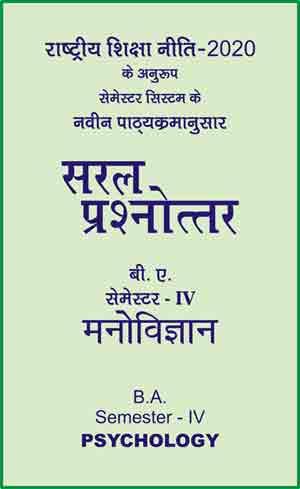|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञानसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 मनोविज्ञान - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- दुर्भीति से आप क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
अथवा
विशिष्ट दुर्भीति क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
अथवा
प्रश्न- सामाजिक दुर्भीति विशिष्ट दुर्भीतियों से किस प्रकार भिन्न है? इसके कारण तथा उपचार विस्तार से समझाइये।
अथवा
सामाजिक दुर्भीति से आप क्या समझते हैं? इसके कारणों तथा उपचारों की व्याख्या कीजिए।
सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-
1. सामाजिक दुर्भीति।
2. एगोराफोबिया।
3. एगोराफोबिया के प्रमुख लक्षण एवं कारणों का वर्णन कीजिए।
4. सामाजिक दुर्भीति (Social Phobia) विशिष्ट भीतियों (Specific Phobias) से किस प्रकार भिन्न हैं?
5. दुर्भीत के प्रमुख कारण बताइए।
उत्तर-
(Phobia)
दुर्भीति एक बहुत सामान्य चिन्ता विकृति है जिसमें व्यक्ति किसी ऐसी विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से सतत् तथा असन्तुलित मात्रा में डरता है, जिससे वास्तव में दौरा भी उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति यह समझता है कि उसका डर अत्यधिक है। व्यक्ति दुर्भीति उत्पन्न करने वाले कारकों से दूर रहना पसंद करता है।
डेविसन एवं नील (1996) के अनुसार - "मनोरोगविज्ञानियों द्वारा दुर्भीति को एक विघटनकारी डर-व्यवहृत परिहार जो किसी खास वस्तु या परिस्थिति से उत्पन्न खतरा के अनुपात- से अधिक होता है तथा जिसे प्रभावित व्यक्ति द्वारा आधारहीन समझा जाता है, के रूप में परिभाषित किया गया है।"
दुर्भीति के लक्षण (Symptoms of Phobia) - अमेरिकन मनोचिकित्सक संघ (American Psychiatric Association or APA, 1994) ने दुर्भीति के निम्नलिखित लक्षण- बताये हैं-
1. किसी विशेष परिस्थिति या उद्दीपक से इतना अधिक डर जो वास्तविक खतरे के अनुपात से कहीं अधिक हो।
2. व्यक्ति को उस विशेष परिस्थिति या उद्दीपक का सामना करने पर अत्यधिक चिन्ता या विभीषका का होना।
(Types of Phobia)
दुर्भीति के सामान्यया तीन प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं-
1. विशिष्ट दुर्भीति (Specific Phobia ) - विशिष्ट दुर्भीति एक ऐसा असंगत डर है जो विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति की उपस्थिति या उसके अनुमान से उत्पन्न होता है। जैसे- छिपकली से डरना या बिल्ली से डरना । सम्पूर्ण दुर्भीति का 4% विशिष्ट दुर्भीति है। इसके चार प्रमुख प्रकार हैं-
(i) पशु दुर्भीति (Animal Phobia) - इसमें रोगी विशेष तरह के पशु से कुछ कारणों से असंगत रूप से डरने लगता है। यह महिलाओं में अधिक होती है तथा इसका प्रारम्भ बाल्यावस्था में होता है।
(ii) निर्जीव वस्तु से उत्पन्न दुर्भीति (Inanimate Object Phobia) - इसमें व्यक्ति अजीवित वस्तुओं से असंगत डर दिखाता है, जैसे-अंधेरे से डर, गंदगी से डर। यह पुरुषों तथा महिलाओं में लगभग सामान रूप से होती है और यह किसी भी उम्र के व्यक्तियों में हो सकती है।
(iii) बीमारी तथा चोट से सम्बद्ध दुर्भीति (Illness and Injury Phobia) - इसमें व्यक्ति में चोट, जख्म या अन्य तरह की बीमारी से असंगत डर उत्पन्न हो जाता है, परन्तु उस बीमारी से डरने की बात नहीं होती है। इस तरह को दुर्भीति की शुरूआत मध्य आयु में होती है तथा इसे नोसोफोबिया (Nosophobia ) कहते हैं।
(iv) रक्त दुर्भीति (Blood Phobia ) - इसमें रोगी को उन परिस्थितियों में असंगत डर उत्पन्न हो जाता है जिसमें उन्हें रक्त देखने को मिलता है चाहे फिर सूई चुभने से रक्त निकल रहा हो। जीव संख्या के करीब 4% लोगों में यह दुर्भीति होती है। यह महिलाओं में अधिक होता है तथा उसकी शुरूआत उत्तर बाल्यावस्था में होती है।
2. एगोराफोबिया (Agoraphobia) - एगोराफोबिया का शाब्दिक अर्थ भीड़-भाड़ या बाजार स्थलों से डर होता है । परन्तु वास्तविकता में एगोराफोबिया में कई तरह के डर शामिल होते हैं जिनका केन्द्र बिन्दु सार्वजनिक स्थान होता है। खरीदारी करने के लिये जाने से डर, यात्रा करने का डर, भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने का डर इसके उदाहरण हैं।
3. सामाजिक दुर्भीति (Social Phobia) - इसमें व्यक्ति को अन्य व्यक्ति की उपस्थिति का सामना करने का डर होता है। उसे यह डर होता है कि लोग उसका मूल्यांकन करेंगे। इसलिये वह ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहता है तथा वह चिन्तित रहता है।
(Etiology of Phobia)
दुर्भीति के चार प्रमुख सिद्धान्त या कारक निम्नलिखित हैं-
1. जैविक सिद्धान्त या कारक (Biological Theory or Factors) - इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं-
(i) स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र (Autonomic Nervous System) - दुर्भीति उन व्यक्तियों में अधिक उत्पन्न होती है जिनका स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र कई तरह के पर्यावरणीय उद्दीपकों द्वारा बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाता है। लेसी (Lessy, 1967) ने इस तरह के स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र को स्वायत्त अस्थिरता (Autonomic Destability) कहा है।
(ii) आनुवंशिक कारक (Genetic Factors) - अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि दुर्भीति होने की संभावना उन व्यक्तियों में अधिक होती है जिनके माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों को यह रोग हुआ हो।
2. मनोविश्लेषणात्मक सिद्धान्त या कारक (Psychoanalytical Theory or Factors) - फ्रायड के अनुसार दमित उपाह आवेगों (Depressed impulses) से उत्पन्न चिन्ता के प्रति रोगी द्वारा अपनायी गयी सुरक्षा दुर्भीति है।
3. व्यवहारात्मक सिद्धान्त या कारक (Behavioural Theory or Factors) - इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कारक आते हैं-
(i) धनात्मक पुनर्बलन (Positive Reinforcement)- दुर्भीति का विकास धनात्मक पुनर्बलन के आधार पर भी होता है जैसे कोई बच्चा स्कूल जाने से डरकर माता-पिता से बहाना बनाता है कि उसे स्कूल न जाना पड़े।
(ii) मॉडलिंग (Modeling) - मॉडलिंग के अनुसार व्यक्ति दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण करके दुर्भीति विकसित करता है।
(iii) परिहार अनुबन्धन (Avoidance Conditioning) - दुर्भीति का विकास परिहार अनुबन्धन द्वारा भी होता है। इस तथ्य को वाटसन तथा उनकी शिष्या रेनर ने अलबर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके दिखाया।
4. संज्ञानात्मक सिद्धान्त या कारक (Cognitive Theory or Factors) - दुर्भीति में संज्ञानात्मक कारकों की प्रमुख भूमिका होती है। दुर्भीति से ग्रसित व्यक्ति जानबूझकर सूचनाओं को इस ढंग से संग्रहित करता है कि उससे दुर्भीति और भी मजबूत हो जाती है। इसे संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह (Cognitive bias) कहते हैं।
(Treatment of Phobia)
दुर्भीति के उपचार को निम्नांकित प्रमुख भागों में बांट सकते हैं-
1. जैविक उपचार (Biological Treatment) - दुर्भीति के रोगियों की चिन्ता कम करने के लिये चिन्ता विरोधी औषधि जैसे प्रोपेनेडियोल्स (Propanediols) तथा बेनजोडियाजेपाइन्स (Benzodiazepines) आदि का प्रयोग करते हैं। परन्तु इनका प्रमुख दोष यह है कि इस औषधि को बन्द करते ही दुर्भीति के लक्षण लौट आते हैं।
2. मनोविश्लेषणात्मक उपचार (Psychoanalytic Treatment) - इसमें चिकित्सक रोगी के दमित मानसिक संघर्ष की पहचान कर उसे असंगत डर की वस्तुओं या परिस्थिति से दूर ले जाता है। इस संघर्ष को पहचान करने के लिये वह स्वतन्त्र साहचर्य स्वप्न- विश्लेषण आदि का सहारा लेता है।
3. व्यवहारपरक उपचार (Behavioural Treatment) - व्यवहार उपचार पद्धति की इस प्रविधि का प्रतिपादन और विकास वुल्पे (Woolphe, 1950, 58, 61) ने किया था। दुर्भीति के उपचार के लिए यह पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय रही है। चिन्ता या दुर्भीत को कम करनें के लिए यह एक सफल उपचार पद्धति है। वुल्पे के अनुसार इस उपचार पद्धति में रोगी को दुर्भीति उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में पूर्णतः शान्त और शिथिल (Relaxed) रहने को कहा जाता है। इस प्रकार रोगी को शान्त एवं शिथिल रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जब रोगी यह प्रशिक्षण पूर्ण कर लेता है तब उसे दुर्भीति उत्पन्न करने वाली परिस्थिति में शान्त रहने का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. इम्प्लोसिव एवं फ्लडिंग चिकित्सा पद्धति ( Implosive and Flooding Therapy) - यह दोनों उपचार पद्धतियाँ विलोपन (Extinction) के नियम से सम्बन्धित हैं। इन उपचार पद्धतियों की प्रमुख मान्यता यह है कि रोगी जब तक यह नहीं सीख पाता है कि दुर्भीति उत्पन्न करने वाले उद्दीपक या परिस्थितियाँ रोगी के लिए हानिकारक नहीं हैं तब तक वह दुर्भीति को समाप्त नहीं कर पाता है। जब रोगी में दुर्भीति के लक्षण उत्पन्न होते हैं और उन्हें यह अनुभव कराया जाता है कि उनकी चिन्ता या भय निराधार है तो उनमें दुर्भीति के लक्षण समाप्त होने लगते हैं। इस पद्धति के मुख्य समर्थक स्टाम्फ एवं लेविस (Stamph and Levis, 1997) हैं।
5. संज्ञानात्मक उपचार पद्धति (Cognitive Therapy) - संज्ञानात्मक उपचार पद्धति द्वारा भी दुर्भीति का उपचार किया जाता है। संज्ञानात्मक उपाचर पद्धति को संज्ञानात्मक व्यवहार उपचार पद्धति भी कहा जाता है। इस उपचार पद्धति में रोगी की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर उपचार किया जाता है। इस पद्धति से उपचार करने पर संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस उपाचर पद्धति में मानसिक रोगों का कारण चिन्तन या संज्ञान को माना जाता है। इस उपाचर में रोगी की संज्ञानात्मक पुनर्रचना (Cognitive restructuring) को ठीक किया जाता है जिससे रोगी का चिन्तन और विश्वास उपयुक्त बन सके और रोगी समायोजित व्यवहार करने में समर्थ हो सके।
|
|||||