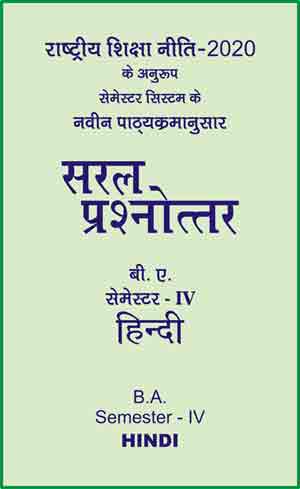|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 हिन्दी बीए सेमेस्टर-4 हिन्दीसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 हिन्दी - सरल प्रश्नोत्तर
स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य
अनुवाद कला में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यास ही किसी अनुवादक को पारंगत कर सकता है, परन्तु कभी-कभी अभ्यास भी किन्हीं अनुचित अनुवाद क्रियाओं का हो जाता है, इसलिये पहले यह समझ लेना चाहिए कि अनुवाद कार्य का दायित्व लेने वाले विद्वानों को किन दोषों से बचना चाहिए तथा उसे किन गुणों को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए।
अनुवाद कार्य के लिए प्रयोजित रचना या उसके विषय के प्रति यदि अनुवादक किसी प्रकार के पूर्वाग्रहों से युक्त हो, जैसा कि प्रायः होता है, तो वह रचना मूल रचनाकार की रचना में अभिव्यक्ति दोष का सृजन कर देता है। यह दोष अनुवाद कार्य का सबसे बड़ा दोष है।
अनुवादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अनुवाद करते समय अभिव्यक्ति में स्वतंत्र नहीं है, अतः उसे स्वयं को मूल रचना के भावों तथा विचारों को दूसरी भाषा में अन्तरण करने से अधिक कुछ नहीं करना है।
कभी-कभी अनुवाद रचना के विषय सम्बन्धी ज्ञान में मूल रचनाकार के ज्ञान से अधिक ज्ञान हो सकता है तथा यह भी संभव है कि कभी-कभी अनुवादक मूल रचना के अनेक भाव- विचारों के विपरीत भाव-विचार रखता है अर्थात् मूल रचना के भाव विचारों के प्रति वह किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है या विषय सम्बन्धी उसकी पूर्वाग्रही धारणा सिद्धान्त संकल्पना में मूल रचनाकार की संकल्पना में, अपनी धारणा को प्रच्छन्न रूप से अनुबद्ध हुई समझ लेता है, तो वह ऐसी धारणा का स्वरूप ही अनुवाद करते समय बदल डालेगा।
अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है। अतः अनुवादक के लिए दोनों - स्रोत और लक्ष्य भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य भी है परन्तु अनुवादशास्त्री इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दोनों भाषाओं के ज्ञान मात्र से बात नहीं बनती है।
अनुवाद कार्य की कठिनता के सम्बन्ध में स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का मन्तव्य अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में, “एक प्रकार से मौलिक लेख लिखना जितना आसान है, किसी दूसरी भाषा से अनुवाद करना उतना ही कठिन है। मेरा निजी अनुभव है कि मैं अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में उतनी आसानी से अनुवाद नहीं कर सकता जितनी आसानी से बोल या लिख सकता हूँ। गहन विषयों का अनुवाद तो और भी अधिक कठिन हो जाता है।
अनुवादक को केवल उन दोनों भाषाओं का जिनमें से कि एक से दूसरी में अनुवाद करना है, अच्छा ज्ञान होना ही अनिवार्य नहीं बल्कि उस विषय पर अच्छा अधिकार भी होना चाहिए जिस विषय से वह अनुवाद किये जाने वाला ग्रन्थ सम्बन्ध रखता है। इसीलिए किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि अगर वह दो भाषाओं को मामूली तौर से जानता है तो वह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर सकता है।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के इस उद्धरण से यह बात प्रकट होती है कि प्रायः विद्वान लोग भी जितनी आसानी से वह स्रोत या लक्ष्य भाषा में स्वाभाविक रूप से कोई विचार प्रकट कर सकते हैं, वह अनुवाद कार्य में ऐसा कर पाना कठिन महसूस करते हैं। इसका भी मूल कारण अभ्यास का अभाव ही होता है।
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के ही अनुसार अनुवादक का स्रोत तथा लक्ष्य भाषानुसार विद्व-ज्ञान से ही काम नहीं चलता, वरन् उसे अपेक्षित अनुवाद के विषय का भी ज्ञान होना आवश्यक है। यह गुण भी अनुवादक द्वारा विषय सम्बन्धी पुस्तकें पढ़ने के अभ्यास से सम्भव है।
आजकल अनेक विद्वान अनुवाद तो करते हैं, परन्तु उन्हें मूल रचना के विषय का ज्ञान नहीं होता । वास्तविक बात यह है कि विषय के ज्ञान से स्रोत कृति में प्रयुक्त अनेक संदर्भों को अनुवादक अनूदित कृति में विषय संदर्भों की पृष्ठभूमि के आधार पर अनुवाद करने में सक्षम हो सकता है।
वस्तुतः स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के शब्दों के अर्थ की सम्यक् जानकारी से काम नहीं चल सकता। सफल अनुवाद के लिये शब्दों की प्रकृति और उनके परिवेश की सूक्ष्म और यथार्थ जानकारी का होना भी अनिवार्य है। अन्यथा अनुवादक स्रोत भाषा के साथ न्याय कर ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ-अशोक के लिए ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त 'देवानां प्रियः' संस्कृत शब्द का प्रयोग किया गया है। कई अनुवादक इस शब्द का प्रयोग ब्राह्मणों के दुर्वचन रूप में मानते हैं और इसी संदर्भ को लेकर वह अशोक को वैदिक धर्म का विद्वेषी सिद्ध करने के लिए 'देवानां प्रियः' शब्द का अनुवाद करते हैं।
यह अनुवादकों के विषय ज्ञान की कमी का तो परिचायक है ही, संस्कृत भाषा की प्रकृति से अपरिचय का भी द्योतक है। यही स्थिति अंग्रेजी के यू (you) और डियर (Dear) शब्दों की है । इन दोनों शब्दों का प्रयोग छोटो-बड़ों और समान स्तर तथा आयु के व्यक्तियों के लिये एक समान किया जाता है। अनुवादक को देखना होगा कि कहाँ यू का अनुवाद तू करना है, कहाँ तुम और कहाँ आप इसी प्रकार डियर का अनुवाद कहाँ प्रिय, कहाँ सम्मान्य और कहाँ आदरणीय करना उपयुक्त होगा-अनुवादक के लिए यह देखना अनिवार्य हो जाता है।
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों -स्रोत और लक्ष्य भाषाओं की जानकारी का अर्थ यह कदापि नहीं है कि केवल शब्द कोश में निहित अर्थ की अथवा व्याकरणिक रूप की जानकारी होनी चाहिए। यह तो सतही ज्ञान कहलायेगा।
सत्य तो यह है कि दोनों भाषाओं की प्रकृति परम्परा और उनके सांस्कृतिक परिवेश के मर्म को समझे बिना अनुवादक गहराई में उतर ही नहीं पायेगा। उदाहरणार्थ - नर्स के लिए प्रयुक्त 'मिडवाइफ' शब्द का हिन्दी में 'आधी पत्नी' अनुवाद तो कभी सही नहीं माना जायेगा । वस्तुतः स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की प्रकृति और परम्पराओं का ज्ञान इन भाषाओं के निरन्तर सम्पर्क अभ्यास से ही सम्भव है। अंग्रेजी समाचार-पत्रों में निरन्तर नये शब्दों का प्रयोग होते हुये देखा जाता है।
अनुवादक को यदि अंग्रेजी समाचार-पत्रों के प्रति लगाव नहीं होता और वह अपनी विद्वता के आधार पर ही अनुवाद में प्रवृत्त होता है, तो यह उसकी भूल है । अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रायः नई तरह की वाक्य रचनाएँ भी आती हैं, जिनका अनुकरण अंग्रेजी के विद्वान अपनी पुस्तकों में भी करने लगते हैं।
प्रायः अंग्रेजी के कुछ शब्दों के प्रयोग तो इस तरह किये जाने लगे हैं, जिन्हें हम सदा से एकार्थक रूप में ही जानते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग की परम्परा का ज्ञान अभ्यास से ही संज्ञानित रह सकता है।
इसके अतिरिक्त अनुवादक के लिये दोनों स्रोत और लक्ष्य भाषाओं के वक्ताओं की सामाजिक मर्यादाओं और परम्पराओं की जानकारी का भी होना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ किसी अपरिचित अथवा सम्मानित महिला के लिये अंग्रेजी भाषा के 'डियर मैडम' का हिन्दी अनुवाद 'प्रिय श्रीमती जी' सही नहीं होगा।
भारतीय समाज में सामान्यतया महिलाओं को विशेष आदर देने की प्रथा एवं परम्परा है। अतः यहाँ 'डियर मैडम' का सही अनुवाद 'आरणीया महोदया' या सुश्री' ही होगा ।
अनुवादक के लिये संदर्भ और प्रसंग की जानकारी का होना भी सर्वथा अपेक्षित है। इसके अभाव में वह अनुवाद कार्य में न्याय कर ही नहीं सकता। उदाहरणार्थ अंग्रेजी के सन् (Son) का अर्थ सभी स्थानों पर पुत्र ही करना उचित नहीं होगा। 'सन् ऑफ इण्डिया' का सही अनुवाद 'भारत का सपूत होगा न कि भारत का पुत्र । इसी प्रकार कहीं आत्मज, कहीं बेटा, लड़का तो कहीं कुलदीपक प्रयोग में आएगा।
इस सम्बन्ध में एक विद्वान का यह कथन बड़ा ही उपयुक्त है-" शब्द भाव अथवा विचार की पोशाक नहीं है जो इच्छानुसार बदली जा सके अर्थात् पैंट-कमीज के स्थान पर धोती-कुर्ता पहना दिया जाये।" यह तो भाव या विचार का मांस अथवा उसकी त्वचा है। अतः भाव विचार के अनुकूल एवं अनुरूप शब्दों का प्रयोग करने वाला अनुवादक ही अनुवाद को सफल एवं सजीव बना सकता है।
इसी संदर्भ में उमर खय्याम की रुबाइयों के अनुवादक फिट्ज जेराल्ड के अनुवाद कार्य की समीक्षा करते हुए डॉ. हरिवंशराय बच्चन का वक्तव्य बड़ा ही सटीक है। उन्होंने सजीवता को ही अनुवाद की सफलता का मूल तत्त्व स्वीकार करते हुए कहा है- “यदि अनुवाद का अर्थ यह है कि एक भाषा के शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा का शब्द लाकर रख दिया जाये तो फिट्ज जेराल्ड सफल अनुवादक नहीं हैं और अगर अनुवाद का अर्थ यह है कि मूलभावों को दूसरी भाषा के माध्यम से जमानत किया जाये तो फिट्ज जेराल्ड आदर्श अनुवादक हैं।'
वस्तुतः यदि अनुवाद मूल भाषा में अभिव्यक्त संवेदना को सम्प्रेष्य नही बना पाता तो वह सर्वथा निष्फल और निरर्थक है। अनुवाद का सजीव होना आवश्यक है यदि उसमें किसी कारणवश मूल प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती तो उसमें अपनी ही सांसों का संचार कर देना चाहिए।
"अपनी ही सांसों का संचार' शब्द भी बहुत वृहत् भावी शब्द है। अवश्य ही अनुवादक को यह अधिकार है कि वह स्रोत भाषा के भाव और मूल यथार्थ की रक्षा करे, लेकिन कैसे ? ऐसे नहीं कि जहाँ स्रोत भाषा की मूल सांसों का भी अतिक्रमण न हो, 'अतिक्रमण हो' या 'अतिक्रमण हो रहा है' इसकी प्रकृति का ज्ञान भी अभ्यास के क्षेत्र की ही बात है ।
प्रत्येक भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों के रूप में कुछ मुहावरों और जीवन के किसी सत्य को सजीव रूप देने के लिये लोकोक्तियों की रचना तथा उनका प्रचलन हो जाता है। उनका शब्दानुवाद करना न तो संभव होता है और न ही वांछनीय। उदाहरणार्थ - हिन्दी में पुत्र को 'बुढ़ापे की लकड़ी' कहा जाता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद 'A stick of old age' कभी उस अर्थ को सूचित नहीं कर पायेगा।
इसी तरह भारत की भाषाओं में 'मुंह में तिनका दबाना' का भावार्थ अधीनता स्वीकार करना ही लेना होगा। ऐसी लोकोक्तियों तथा मुहावरों के अनुवाद के लिए लक्ष्य-भाषा में, स्रोत भाषा में प्रयुक्त लोकोक्तियों तथा मुहावरों की ही खोज करनी पड़ सकती है, परन्तु यह तब तक सहज रूप में सम्भव नहीं है जब तक गहनपूर्वक किये गये अभ्यास द्वारा उनका संकलन अनुवादक के पास नहीं हो। इसके लिये केवल कोशों से काम नहीं चलता ।
बहुत -सी लोकोक्तियाँ और मुहावरे की समकक्ष लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे कोशों में होते ही नहीं। कभी-कभी ऐसे मुहावरों आदि के समकक्ष मुहावरे आदि गढ़ लेने के अनुवादक के अधिकार को भी अमान्य नहीं क्रिया जा सकता, परन्तु ऐसे अधिकार का प्रयोग अनुवादक तभी कर सकता है जब इस प्रकार के सृजन को अपने अभ्यास में लाता रहा हो ।
अनुवादक के लिये जहाँ स्रोत भाषा और लक्ष्य-भाषा का पर्याप्त और गहन ज्ञान अपेक्षित है, दोनों भाषाओं के शब्दों की प्रवृत्ति और परिवेश की जानकारी अपेक्षित है, वहाँ उसके लिये अनूदित की जाने वाली रचना में निरूपित समय, स्थान, विषय और समाज आदि की भी सही, पूरी और गहरी जानकारी का होना आवश्यक है अन्यथा वह अनुवाद कार्य के लिए न्याय कर ही नहीं सकता।
अनुवादशास्त्रियों ने अनुवाद कार्य में इसे परम उपयोगी माना है, लेकिन ऐसा प्रायः अनुवादकों के लिये संभव नहीं होता। फिर भी स्रोत रचना में इनकी जानकारी कराने वाले तत्व अवश्य होते हैं। यह स्रोत भाषा की सांस्कृतिक और सामाजिक परम्पराओं के होते हैं जिनकी जानकारी अनुवादक को कम-से-कम उस सीमा तक होनी चाहिए कि वह उनके वर्णन को उनकी यथार्थता का प्रसंग प्रदान कर सके। यह सामान्य ज्ञान की भी बात है और सामान्य ज्ञानं सामान्य अभ्यास के बिना नहीं होता ।
वस्तुतः अनुवाद की सभी समस्याओं का निदान अनुवाद करते रहने के अभ्यास में हो सकता है। जिनको अपने भाषा प्रवाह को आकर्षक और रुचिपूर्ण बनाने की इच्छा होती है, वह इसके लिए निरन्तर अभ्यास करते हैं।
प्रायः स्रोत भाषा की मूल रचना और लक्ष्य भाषा के विभिन्न अनुवादों को पढ़ने का अभ्यास तो आवश्यक है ही, परन्तु इसके लिये सर्वोत्कृष्ट क्रिया है, स्वयं अनुवाद करते रहने का अभ्यास।
|
|||||