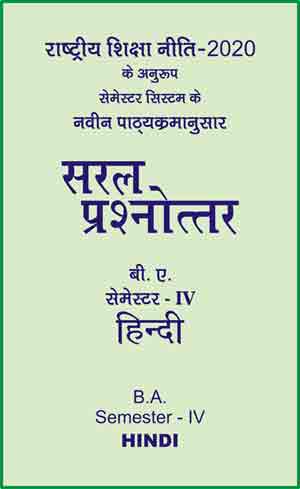|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 हिन्दी बीए सेमेस्टर-4 हिन्दीसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-4 हिन्दी - सरल प्रश्नोत्तर
स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य
जिस प्रकार कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि को हम नितान्त सृजनात्मक साहित्य | मानते हैं, उसी प्रकार अन्य गद्य-विधाएँ भी सृजनात्मक साहित्य के ही विभिन्न आयाम हैं और इसलिए इनका अनुवाद न तो अन्य विधाओं से बिल्कुल भिन्न है और न ही इनके अनुवाद की समस्याएँ भी पहले से कम हैं।
इन गद्य विधाओं में विचार एवं अनुभूति की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुआ करती है। इसके अनुवादक को विचार एवं अनुभूति की इसी प्रामाणिकता को सुरक्षित रखते हुए अनुवाद करना होता है। इन विधाओं में एक ओर विचारों की तथ्यपरता और दूसरी ओर अनुभूति की। कलात्मकता विद्यमान होती है और इन दोनों के समन्वित रूप को लक्ष्य भाषा में उतारना ही अनुवाद की सफलता की कसौटी है।
सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल होती है, क्योंकि साहित्य में, विशेष रूप से काव्यभाषा में, अनेक काव्यशास्त्रीय तत्त्व निहित होते हैं। ये तत्त्व कभी बिम्बों और प्रतीकों के रूप में तो कभी अलंकारों के रूप में प्रस्तुत होते हैं।
काव्यशास्त्रीय तत्त्वों की ये जटिलता एक ओर तो काव्य की सौंदर्य वृद्धि करती है और दूसरी ओर उसकी रसास्वादन में बाधक भी बनती है।
कविता की भाषा अन्य साहित्यिक विधाओं से कई कारणों से भिन्न होती है। कवि के शब्दों के चयन के विशेष चमत्कारिक प्रभाव निहित होता है, क्योंकि इन शब्दों में सामान्य अर्थ के साथ-साथ कुछ विशिष्ट अर्थ छवियाँ भी संश्लिष्ट रूप में विद्यमान रहती हैं। इस प्रकार के चुने हुये विशेष शब्दों के सामान्य अर्थ को तो अनुवादक आसानी से स्थानान्तरित कर देता है, किन्तु उसकी विशिष्ट अर्थ छवियों में सुरक्षित रख पाना इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि प्रत्येक भाषा में इस प्रकार के शब्द होते ही नहीं ।
कोई भी काव्य-भाषा काव्यशास्त्रीय तत्वों के संदर्भ में जितनी ही जटिल होगी उसका अनुवाद. उतना ही कठिन होगा। स्रोत भाषा के काव्यशास्त्रीय तत्त्वों को लक्ष्य भाषा में अवतरित करते समय अनुवादक एक साथ पाठक और सृजक की भूमिका निभाता है।
सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और दार्शनिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों का अनुवाद इस चुनौती के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत कर देता है। समकालीन संदर्भ में प्रत्येक रचनाकार को कितनी ही समस्याओं के स्पष्टीकरण के लिए दार्शनिक एवं सांस्कृतिक उदाहरणों को सादृश्य रूप में अपनाना ही पड़ता है । साहित्य में तो ये तत्व अनुभूति को गहनता और विचार को विस्तार प्रदान करने का महत्त्वपूर्ण साधन होते हैं।
दार्शनिक एवं सांस्कृतिक चरित्र, नाम, घटनाएँ, अभिव्यक्तियाँ कभी प्रत्यक्ष रूप में और कभी मुहावरों के रूप में अपनाई जाकर स्थिति को अपेक्षित अर्थ प्रदान करती हैं। इसलिए अनुवादक दार्शनिक एवं सांस्कृतिक तत्त्वों के अनुवाद के उत्तरदायित्व से बच नहीं सकता । इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अनुवादक के लिए आवश्यक है कि उसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की दार्शनिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विशेष ज्ञान हो ।
इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक को एक साथ दो प्रकार की वास्तविकताओं का साक्षात्कार करते हुए दोनों का संयोजन करना होता है जिसके लिए उसे इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही उसे ध्यान में रखना होता है कि वह दार्शनिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति से संदर्भ विशेष में सार्थकता भी रखें और उसके द्वारा उत्पन्न किया गया प्रभाव भी सुरक्षित रखें।
सृजनात्मक साहित्य में शब्दों की अभिव्यंजना-शक्ति एक महत्त्वपूर्ण तत्व होती है जिसे बिम्बों, प्रतीकों, व्यंग्य, ध्वनि, अलंकार, सांस्कृतिक तत्त्व आदि के प्रयोग द्वारा लेखक अपने साहित्य में उत्पन्न करता है। इसके साथ-साथ वह मुहावरों और लोकोक्तियों द्वारा भी भाषा की अभिव्यंजना में वृद्धि करता है।
मुहावरों एवं लोकोक्तियों का मूल स्रोत उस देश अथवा भाषा की संस्कृति विशेष हुआ करतीहै। ये उस देश अथवा भाषा की सांस्कृतिक चेतना के वाहक होते हैं और भाषा की अभिव्यक्ति को एक विशिष्टता प्रदान करते हुए उसे सशक्त रूप प्रदान करते हैं। साथ ही ये उस भाषा को सहजता और स्वाभाविकता भी प्रदान करते हैं।
मुहावरों एवं लोकोक्तियों जैसी लोकाश्रित तत्त्व युग-युगांत के लोकानुभव को हमारे सामने रखते हैं, यह लोकानुभव हमारे नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन पर ही आधारित होते हैं।
इन लोकाश्रित अभिव्यक्तियों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजना जितनी अधिक होगी, उसका अनुवाद भी उतना ही कठिन होता जाएगा।
अनुवाद एक भाषा की सामग्री का दूसरी भाषा में रूपान्तरण है। इसलिए अनुवाद का संबंध भाषाविज्ञान से स्वतः ही स्थापित हो जाता है। वास्तव में, भाषा कुछ ऐसे ध्वनि-प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपनी विचार-संपदा को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं।
भाषा के ध्वनि प्रतीकों की यह व्यवस्था अर्थगत, शैलीगत एवं व्याकरणिक संरचनाओं के नियमों के रूप में हमारे सामने आती है जो उस भाषा को नियंत्रित करती है। इन्हीं अर्थगत, शैलीगत और व्याकरणिक संरचनाओं के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकने में सक्षम होते हैं।
एक भाषा के शब्दों तथा उसकी व्यवस्था के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्दों तथा उसकी व्यवस्था लाने के लिए दोनों भाषाओं की तुलना आवश्यक है। इस तरह अनुवाद मूलतः दो भाषाओं की तुलना पर आधारित होता है, अतः उसका सीधा सम्बन्ध भाषा विज्ञान के तुलनात्मक रूप से है। यह तुलना शब्द समूह तथा भाषा की व्यवस्था दोनों की होती है।
शब्द- समूह की तुलना से अभिप्राय शब्दों की अर्थगत तुलना से है, और व्यवस्था से अभिप्राय भाषा की शैलीगत एवं व्याकरणिक संरचनाओं की तुलना से है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का शैली एवं व्याकरण के स्तर पर अध्ययन किया जाता है और अनुवादक को इस संदर्भ में आने वाली अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। सृजनात्मक साहित्य का अनुवाद निश्चित रूप से एक कठिन प्रक्रिया है और इसी कारण किसी ने अनुवादक को प्रबंधक कहा और किसी ने अनुवाद प्रक्रिया को ही असंभव घोषित । कर डाला। इस प्रकार के अनुवाद के भावपक्ष में यह कठिनाई शैलीपक्ष की अपेक्षा कम ही होती है।
डॉ. सुरेश सिंहल के शब्दों में - “सफल अनुवाद के लिए आवश्यक है कि भाव के साथ- साथ मूल कृति की शैलीपरक विशेषताओं को भी लक्ष्य भाषा में अवतरित किया जाए। ये विशेषताएँ प्रायः काव्यशास्त्रीय, लोकाश्रित, दार्शनिक, सांस्कृतिक, शैलीवैज्ञानिक, व्याकरणिक आदि तत्त्वों के रूप में प्रस्तुत होती हैं। सफल अनुवाद का मूल तंत्र यह है कि अनुवादक में ऐसी क्षमता होनी चाहिए जिससे वह इन सभी प्रकार की विशेषताओं को लक्ष्य भाषा में सुरक्षित रख सके। किन्तु अनुवाद में प्रायः ऐसा हो नहीं पाता है । अनुवादक को कई कारणों से इनका अनुपात बदलना पड़ता है। कई बार मूल अभिव्यक्ति व्याकरणिक अभिधा के सहारे करनी पड़ती है। बहुत से अनुवादों में ऐसा देखने में आता है कि उनमें शैलीपरक तत्त्व मूल की अपेक्षा अधिक नहीं होते हैं। फिर भी वस्तुस्थिति यही है कि साहित्यिक अनुवाद में यह एक आवश्यक गुण है जो अनुवादक से सृजनात्मकता की माँग करता है।"
अनुवादक से सृजनात्मक की यह माँग मूल रचना की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति-भंगिमा पर निर्भर करती है। भाव एवं शैली के स्तर पर अभिव्यक्ति का यह सौंदर्य जितना अधिक होगा अनुवाद उतना ही कठिन हो जाएगा। इसलिए कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबन्ध आदि का अनुवाद क्रमशः कठिन से आसान हो जाएगा।
कहा जा सकता है कि सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में विधा कोई भी हो, यह मूल लेखक की व उसकी कृति की मानसिकता से और उसकी पृष्ठभूमि से आत्मसात् होने की एक सृजनात्मक प्रक्रिया है।
मूल कृति के प्रति उसे अपनी निष्ठता को सहेजना-सँवारना पड़ता है। साहित्य के अनुवाद को सृजन के शब्दों की स्थूल डोर उस अदृश्य सूक्ष्म प्रक्रिया से जोड़ती है जो सृजन के क्षणों में मूल लेखक के मानस में घटित हुई होगी। यह संपूर्ण प्रक्रिया अपने आप में एक सृजनात्मक प्रक्रिया है और अनुवादक को इसके विविध आयामों से होकर गुजरना पड़ता है
|
|||||