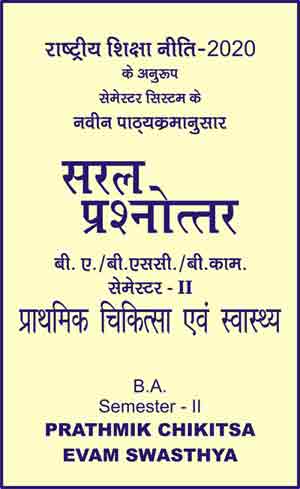|
बी ए - एम ए >> बीए बीएससी बीकाम सेमेस्टर-2 प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीए बीएससी बीकाम सेमेस्टर-2 प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्यसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए बीएससी बीकाम सेमेस्टर-2 प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य - सरल प्रश्नोत्तर
महत्वपूर्ण तथ्य
संवेदी अंग या ज्ञानेंद्रियां सेंसरी न्यूरान के बने वे विशिष्ट अंग हैं जो हमारे आस-पास के वातावरण या पर्यावरण में घटित होने वाली घटनाओं को प्राप्त करते हैं और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करके मस्तिष्क को सूचनायें भेजते हैं। जिससे उनके बारे में हम जान पाते हैं और उसके प्रत्युत्तर में उचित क्रिया कर पाते हैं।
मानव में पाँच संवेदी अंग पाये जाते हैं-
(1) आँख
(2) कान
(3) नाक
(4) जिह्वा तथा
(5) त्वचा
हमारी पहली ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग आँख है जो प्रकृति की अनोखी देन है जो हमें संसार के रंग-बिरंगे चित्र दिखलाती है और जीवन को परिपूर्ण बनाती है।
मानव नेत्र अनेक भागों में विभाजित होता है जिनमें रक्तक पटल, कार्निया, आयरिस, पुतली, नेत्र लेंस रेटिना, पीत बिन्दु तथा अन्ध बिन्दु मुख्य हैं।
रक्तक पटल काले रंग की एक झिल्ली होती है। काला रंग होने के कारण यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और आन्तरिक परावर्तन की संभावना को समाप्त कर देती है।
कार्निया से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है।
कार्निया के पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे आइरिस कहा जाता है।
आयरिस कैमरे के डायफ्राम की भांति कार्य करता है।
आँख का रंग आयरिस के रंग पर ही निर्भर करता है।
पुतली अथवा नेत्र तारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियमन करता है जबकि पुतली के आकार को आइरिस या परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
आयरिस के पीछे प्रोटीन का बना पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का बना एक द्वि- उत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहा जाता है।
इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है।
रेटिना, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे आन्तरिक भाग में दृष्टिनाड़ी से बना एक पर्दा होता है। इसी रेटिना पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिम्ब बनता है। इस प्रतिबिम्ब के बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुँचता है जिससे मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिम्ब सीधा दिखाई देता है।
जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब वस्तुयें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इस दशा में वस्तु का प्रतिबिम्ब रेटिना के आगे या पीछे कहीं पर भी बन जाता है। इसी को दृष्टि दोष कहा जाता है।
निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखायी देती हैं, परन्तु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखायी देती। इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूर दृष्टि दोष या Hypermetropia में दूर की वस्तुयें स्पष्ट दिखायी देती हैं परन्तु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखायी देती। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है।
वर्णान्धता रोग से पीड़ित व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अन्तर नहीं कर पाता। यह एक आनुवांशिक दोष है। जिसका अभी तक कोई इलाज ज्ञात नहीं है।
कभी-कभी अधिक आयु के व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, इसी दशा को मोतियाबिन्द कहा जाता है। इसका निवारण आपरेशन द्वारा कृत्रिम लेंस लगाकर किया जाता है।
कान मानव शरीर की दूसरी ज्ञानेंद्रिय है। इसका कार्य सुनना तथा शरीर का संतुलन बनाये रखना है।
कान के तीन भाग होते हैं-
(1) बाहय कर्ण
(2) मध्य कर्ण तथा
(3) अन्तर कर्ण (Internal Ear)
कान का बाहरी भाग कर्णपाली या पिन्ना कहलाता है। यह कान की रक्षा करने के साथ ध्वनि तरंगों को पकड़ने में भी मदद करता है।
बाह्य कर्ण 2.5 सेमी लम्बी एक घुमावदार नली के रूप में होती है। इसमें कुछ ग्रंथियां पायी जाती हैं, जिसका स्राव कीटाणुओं तथा धूल के कणों आदि को कान के अन्दर जाने से रोकता है। मध्य कर्ण के तीन भाग होते हैं-
(1) कान का पर्दा
(2) श्रवणीय अस्थिकायें तथा
(3) श्रवणीय नली।
अन्तर कर्ण के भीतर सुनने के उपकरण और संतुलन बनाये रखने वाले पदार्थ होते हैं।
कान की अर्द्ध वृत्ताकार नलिकायें शरीर की साम्यावस्था एवं संतुलन बनाये रखने में सहायक होती हैं।
नाक का कार्य श्वसन के साथ-साथ वस्तुओं की गंध का ज्ञान कराना होता है।
नाक की गुहा में ऊपर की अन्तः त्वचा के नीचे Ol factory Nerves के छोड़ फैले होते हैं।
गंधयुक्त वस्तुओं से अत्यंत सूक्ष्म रासायनिक कण निकलते हैं, जो सांस के माध्यम से नासिका में पहुँचते हैं और वहाँ स्नायु तन्तुओं के छोर को उद्दीप्त कर प्रेरणा उत्पन्न करते हैं। यह प्रेरणा नासिका के स्नायु तंत्र द्वारा मस्तिष्क को जाती है जिसके कारण हमें गंध का ज्ञान होता है। जीभ पर पाये जाने वाले कवक रूप अंकुरक आकार में छोटे परन्तु संख्या में बहुत अधिक होते हैं जो मुख्यतः जीभ के किनारे एवं छोर पर पाये जाते हैं और ये ही अंकुरक स्वाद का पता लगने हेतु जिम्मेदार होते हैं।
जीभ की नोंक पर मीठेपन की स्वाद कलिकायें पायी जाती हैं जबकि दोनों किनारों पर खट्टेपन की स्वाद कलिकायें, जीभ के पिछले भाग पर कड़वेपन का स्वाद बताने वाली कलिकायें होती हैं।
त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे लम्बा तथा बड़ा भाग है जो संवेदी अंग का कार्य करने के साथ शरीर को खुलने से बचाने का कार्य एवं उत्सर्जन का कार्य भी करती है।
|
|||||