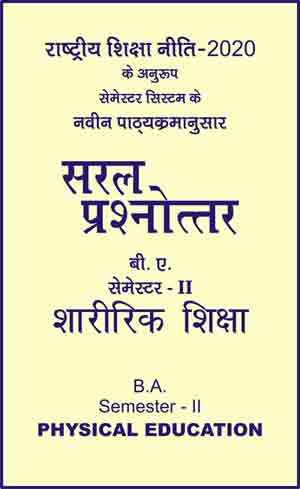|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-2 शारीरिक शिक्षा - खेल संगठन एवं प्रबन्धन बीए सेमेस्टर-2 शारीरिक शिक्षा - खेल संगठन एवं प्रबन्धनसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बीए सेमेस्टर-2 शारीरिक शिक्षा - खेल संगठन एवं प्रबन्धन - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- वित्तीय प्रबन्ध की अवधारणा की व्याख्या कीजिये। इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर -
(Financial Managment )
सामान्य अर्थ में वित्तीय प्रबन्ध, सामान्य प्रबन्ध की वह शाखा है, जिसके द्वारा किसी व्यवसाय के कोषों के स्रोतों, कोषों के आवण्टन तथा नियन्त्रण का अध्ययन किया जाता है। व्यापक रूप में वित्तीय प्रबन्ध से आशय व्यावसायिक संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उचित स्रोतों से आवश्यक वित्त प्राप्त करना, इसे व्यवसाय में सही ढंग से विनियोजित करना तथा इसका कुशल उपयोग करना है तथा इससे प्राप्त आय को सही ढंग से नियोजित एवं नियन्त्रित करना है ताकि संस्था को अधिकतम लाभ हो सके, उसकी साख उज्ज्वल बने तथा संस्था सतत् उन्नति कर सके। यह व्यावसायिक प्रबन्ध का एक कार्यात्मक क्षेत्र है तथा सम्पूर्ण प्रबन्ध का ही एक भाग है, जिसमें निम्नलिखित चार बातें सम्मिलित की जाती हैं-
(i) वित्तीय नियोजन,
(ii) वित्त एकत्रित करना तथा विनियोग करना,
(iii) आय का प्रबन्ध,
(iv) वित्तीय नियन्त्रण।
(Definitions of Financial Management)
वित्तीय प्रबन्ध की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं-
(i) सोलोमन के अनुसार, - “वित्तीय प्रबन्ध का सम्बन्ध एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत अर्थात् पूँजी निधियों के कुशल उपयोग से है।"
(ii) जे० एफ० ब्रेडले के अनुसार, - “वित्तीय प्रबन्ध शैक्षिक प्रबन्ध का वह क्षेत्र है, जिसका सम्पूर्ण पूँजी का सम्यक् प्रयोग एवं पूँजी के साधनों के सतर्कतापूर्ण चयन से है ताकि शिक्षा को इसके उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में निर्देशित किया जा सके।"
(iii) वैस्टन एवं ब्राइगम के अनुसार,- “वित्तीय प्रबन्ध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है, जो व्यक्तिगत उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है।"
उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है - वित्तीय प्रबन्ध शैक्षिक प्रबन्ध का एक वह क्षेत्र है, जिसके अन्तर्गत संगठन की वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियन्त्रण के कार्य किये जाते हैं।
वित्तीय प्रबन्ध विभाग का क्षेत्राधिकार अन्य विभागों की तुलना में कुछ अधिक व्यापक होता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वित्तीय प्रबन्ध के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नितान्त आवश्यक हो गयी है, क्योंकि "शैक्षिक वित्त का प्रबन्ध एक कला होने के साथ-साथ एक विज्ञान भी है। इसके लिए परिस्थिति की सही पकड़ एवं विश्लेषणात्मक दक्षता की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही वित्तीय विश्लेषण की विधियों और तकनीकों के प्रचुर ज्ञान तथा उनके व्यावहारिक उपयोग एवं प्राप्त परिणामों की सही समीक्षा करने की भी अपेक्षा होती है। "
उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वित्तीय प्रबन्ध शिक्षा - प्रबन्ध के अन्य क्षेत्रों की भाँति ही इसका एक क्षेत्र है, जो आधुनिक सन्दर्भों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में कदाचित् अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। अपनी केन्द्रीय प्रकृति, नियोजन, समन्वय एवं नियन्त्रण स्थापित करने की उसकी शक्ति एवं विचाराधीन प्रत्येक प्रश्न के साथ जुड़े हुए वित्तीय पक्ष पर भली प्रकार विचार किये बिना निर्णय न लिये जा सकने की विवशता के कारण वित्तीय प्रबन्ध अब एक सतत् प्रशासनिक कार्य बन गया।
(Characteristics of Financial Management)
वित्तीय प्रबन्ध विचारधारा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं-
(1) व्यावसायिक प्रबन्ध का एक अभिन्न प्रमुख अंग - वित्तीय प्रबन्ध की परम्परागत . विचारधारा के प्रचलन के समय वित्तीय प्रबन्धक को शिक्षा के प्रबन्ध में महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था, परन्तु आधुनिक शैक्षिक प्रबन्ध में वित्तीय प्रबन्ध व्यावसायिक प्रबन्ध का एक प्रमुख अंग है तथा वित्तीय प्रबन्धक उच्च प्रबन्ध टोली के सक्रिय सदस्यों में से एक होता है। शिक्षा की गतिविधि के साथ वित्त का प्रश्न जुड़ा हुआ है, अतः वित्तीय प्रबन्धक सभी महत्त्वपूर्ण शैक्षिक निर्णयों में आधारभूत भूमिका निभाता है।
(2) लेखांकन कार्य से भिन्न - बहुत से लोग वित्त कार्य तथा लेखांकन कार्य को एक ही मानते हैं, क्योंकि दोनों में बहुत-सी शर्तें एवं अभिलेख एक समान ही होते हैं परन्तु वित्त कार्य लेखांकन कार्य से भिन्न होता है। लेखांकन कार्य में वित्तीय एवं सम्बन्धित समकों का संग्रहण किया जाता है, जबकि वित्त कार्य में इनका निर्णयों के लिए विश्लेषण एवं उपयोग किया जाता है।
(3) केन्द्रीयकृत स्वभाव - आधुनिक शैक्षिक प्रबन्ध के विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय प्रबन्ध का स्वभाव केन्द्रीयकृत है। जहाँ उत्पादन, विपणन तथा कर्मचारी प्रबन्ध के कार्यों का अत्यधिक विकेन्द्रीकरण सम्भव है, वहाँ वित्त कार्य का व्यावहारिक दृष्टि से विकेन्द्रीयकरण वांछनीय नहीं है तथा वित्त कार्य के केन्द्रीयकरण द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।
(4) वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक - परम्परागत वित्तीय प्रबन्ध वर्णनात्मक अधिक तथा विश्लेषणात्मक कम था, जबकि आधुनिक वित्तीय प्रबन्ध वर्णनात्मकं कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक है। आज वित्तीय विश्लेषण की सांख्यिकीय तथा गणितात्मक विधियाँ विकसित हो गई हैं, जिनके द्वारा किन्हीं दी हुई आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितियों के सन्दर्भ में सम्भावित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुना जा सकता है।
(5) सतत् प्रक्रिया - परम्परागत वित्तीय प्रबन्ध की धारणा के अन्तर्गत वित्तीय प्रबन्ध की प्रक्रिया निरन्तर नहीं चलती थी, बल्कि यह प्रक्रिया कुछ विशिष्ट घटनाओं के घटित होने पर जाग्रत होती थी तथा उनसे उत्पन्न वित्त प्राप्ति की समस्याओं के समाधान होने पर मन्द हो जाती थी। परन्तु आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबन्ध की प्रक्रिया सतत् चलने वाली प्रक्रिया है तथा शिक्षा की सफलता के लिए वित्तीय प्रबन्धक को निरन्तर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है।
(6) कार्य निष्पत्ति का मापक - आधुनिक युग में शैक्षिक संस्था में विभिन्न कार्यों की निष्पत्ति (Performance ) को वित्तीय परिमाणों में मापा जाता है। यदि एक उपक्रम पूर्व निर्धारित मात्रा में आगम प्राप्त कर सका है। तथा लागतों को उचित स्तर पर रख सका है तो वह अपने लाभ उद्देश्य अथवा सम्पदा के मूल्य को अधिक करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में : सफल होता है। वित्तीय प्रबन्धक को संस्था के लिए तरलता तथा लाभदायकता के कार्यों को पूरा करना होता है। इन कार्यों के लिए उसे जोखिम तथा लाभदायकता का सही विभाजन करना होता है। ऐसा करने पर ही वांछित निष्पत्ति का स्तर प्राप्त किया जा सकता है।
(7) व्यापक क्षेत्र - वित्तीय प्रबन्ध का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। वित्तीय प्रबन्ध का कार्य संस्था की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं के लिए साधनों को प्राप्त करना, उनका आवंटन करना तथा अनुकूलतम उपयोग करना है। वित्तीय प्रबन्ध लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन, शैक्षिक बजटन, रोकड़ व साख प्रबन्ध, सामग्री प्रबन्ध आदि के लिए भी उत्तरदायी है।
(8) वित्तीय नियोजन, नियन्त्रण एवं अनुवर्तन - आधुनिक विचारधारा के अनुसार वित्तीय प्रबन्ध के साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए योजना बनाना, उनके अनुसार साधन प्राप्त करना, प्रभावी उपयोग करना, बजट के अनुसार नियन्त्रित करना, विचलनों की खोज करना तथा अनुवर्तन द्वारा सुधारात्मक कार्य करना शामिल होता है।
|
|||||