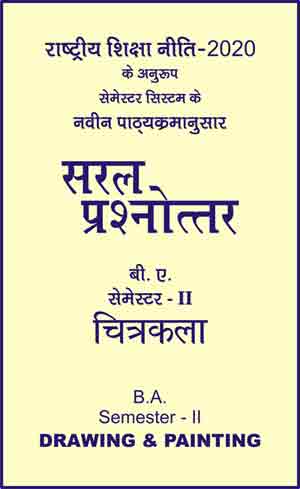|
बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-2 चित्रकला - कला के मूल तत्व बीए सेमेस्टर-2 चित्रकला - कला के मूल तत्वसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
|||||||
बीए सेमेस्टर-2 चित्रकला - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- चित्र में प्रवाह उत्पन्न करने वाली विधियों पर प्रकाश डालिये।
अथवा
चित्रण में प्रवाह उत्पन्न करने की विधि क्या है?
अथवा
चित्रण में प्रवाह किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है? उदाहरण सहित समझाइये।
उत्तर -
प्रवाह सृजन की विधियाँ
कला रचना में प्रवाह - सृजन के लिए निम्न विधियाँ अपनायी जाती है-
1. पुनरावृत्ति ( Repetition ) - जब एक ही आकृति की उचित अन्तर से आवृत्ति की जाती है तो दृष्टि एक आकृति से दूसरी आकृति तक चलती जाती है। इस प्रकार के उदाहरण प्रकृति में साधारणतया देखने को मिलते हैं भारतीय लघु चित्रों में इस प्राकृतिक गुण का खुलकर प्रयोग किया गया है। जैसाकि भारतीय लघु चित्रों में अंकित वृक्ष और वस्तुओं के आलेखनों में दिखाई पड़ते है। इस विधि को प्रयोग करने के तीन प्रकार है-
(i) लम्बवत् - इसमें आकृति की आवृति लम्बाई में की जाती है।

(ii) क्षैतिजवत् - आकृतियों की आवृत्ति क्षैतिज के समानान्तर चौड़ाई में की जाती है।

(iii) कर्णवत् - इसमें आकृति की आवृत्ति एक कर्ण से दूसरे कर्ण के क्रम में की जाती है। तो आवृत्ति द्वारा प्रवाहिता प्राप्त करने के लिए इकाइयों के बीच की दूरी उचित अनुपात में समान होनी चाहिये।

लम्बवत् तथा क्षितिजवत् आवृति को समानान्तरवाद भी कहा जा सकता है। कभी-कभी. ऐसे रूप जिन्हें डिजाइन की इकाई के रूप में प्रयोग करना कठिन होता है पास-पास आवृत्ति करने पर सुख की अनुभूति प्रकट करते है जैसे वर्ग तथा आयत।
2. वैकल्पिक अनुक्रम - जब किसी आकृति को विभिन्न आकारों में आवृत्त किया जाता है तो अनुक्रम होता है और प्रवाह का सृजन होता है। अनुक्रम द्वारा उत्पन्न प्रवाह, आवृत्ति द्वारा उत्पन्न प्रवाह से अधिक आर्कषक एवं मधुर होता है। यह अनुक्रम दो प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है-
(i) स्पष्ट अनुक्रम - इसमें आकृतियों का अनुक्रम स्पष्ट दिखाई पड़ता हैं उसे स्पष्ट अनुक्रम कहते है।

(ii) जटिल अनुक्रम - आकृतियों का अनुक्रम स्पष्ट नहीं होता है रेखा के समान अनुक्रम भी दृष्टि की दिशा-निर्देशक का कार्य करता है। दृष्टि के ऊपर नीचे, आगे पीछे और चित्र फलक के भीतर और बाहर भी खींच ले जाता है। अनुक्रम का बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग संयोजन की अत्यन्त आकर्षक और प्रवाह युक्त बना सकता है।

3. लम्बी एवं घुमावदार रेखाओं द्वारा प्रवाह उत्पन्न करना या निरन्तरता (Continuity) - यदि किसी रेखा अथवा आकृति में वर्तुल घुमाव देते हुए उसे आगे बढ़ाया जाए तो उसमें सुन्दर लय की अनुभूति होती है। शंख के मुख्य भाग में इसी तरह की लय होती है। उसमें रेखा भी घूमती जाती है और उसके साथ-साथ रेखाओं के बीच की चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। इससे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजन्ता के चित्र है।

अजन्ता में रेखा का लयात्मक अंकन इतना सुन्दर हुआ है कि सभी रूपरेखा के अनुरूप ढले हुये दिखाई पड़ते है। चाहे वो मानव आकृति हो, वृक्ष, लतायें अथवा हाथी इत्यादि पशु आकृति सशक्त प्रवाहयुक्त रेखांकन के कारण लावण्यमय हो गये है।
4. विकीर्णन (Radiation) - आवृत्ति और अनुक्रम से सम्बन्धित एक और व्यवस्था भी संयोजन में साधारणतया प्रयुक्त होती है इसे प्रसारण कहते है। इस पद्धति में एक आकर्षक बिन्दु केन्द्र होता है। तथा अन्य निर्देशक रेखायें इस केन्द्र में फैलती प्रतीत होती है। अथवा दूसरे शब्दों में कह सकते है कि प्रत्येक निर्देशन रेखाचित्र में आकर्षण केन्द्र की ओर दृष्टि को ले जाती है। इन निर्देशक रेखाओं को किंचित कर्णवत् झुका देने से जो गति उत्पन्न होती है वह पानी में घूमने वाली भवर की गति का आभास देती है। जैसे- सूर्य, चन्द्र आदि। किसी प्रकाश पुंज से चारों ओर आभा विकण होती है अथवा पुष्प की पंखुड़ियाँ केन्द्र से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार की सुन्दर लय का आभास विकीर्णन पद्धति द्वारा किया जा सकता है। इसके दो स्वरूप है-
(i) वाह्योन्मुख - जब गति की अनुभूति केन्द्र से बाहर की ओर हो तो लय वाह्योन्मुख होती है।

(ii) केन्द्रोन्मुख - जब गति की अनुभूति बाहर से केन्द्र की ओर हो तो लय की अनुभूति केन्द्रोन्मूख होती है।

|
|||||