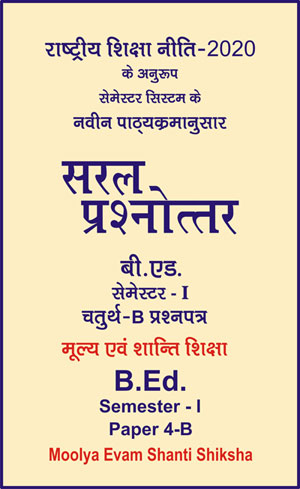|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा
प्रश्न- वर्तमान मूल्यों के प्रकारों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
मानव जीवन की मूलभूतस्थित रहने हेतु आज कुछ मूल्य अविस्मरणीय हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएँ दो प्रकार की होती हैं। एक वैयक्तिक, द्वितीय सामाजिक एवं आध्यात्मिक। इनके अंतर्गत वे आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं, जिनमें संबंध मानवता सहायक पारिवारिक जीवन, आर्थिक सुरक्षा, नागरिक सुविधा, मनोरंजन एवं दैनिक सूचना से दायित्वबोध होता है। मनुष्य की रचना एवं प्रकृति ऐसी है कि वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना जीवित नहीं रह सकता है। मनुष्य इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न क्रियाएँ किया करता है। इन क्रियाओं एवं वस्तुओं के प्रयोग से मानव जीवन में कुछ 'मूल्य' बनते हैं। 'मूल्य' वस्तुतः मानव जीवन एवं उसकी प्रवृत्त क्रियाओं एवं व्यवहार से संबंधित होता है। मूल्यों का व्यापक निम्न प्रकार से है-
-
शारीरिक मूल्य - शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति स्वास्थ्य, शक्ति, तंदुरुस्ती, सौंदर्य एवं चुस्ती जैसे गुणों अथवा मूल्यों को प्राप्त करता है। अतः शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बालकों का शरीर स्वच्छ एवं बलवान हो सके। प्राचीन काल में छात्र का शारीरिक शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया जाता था एवं व्यायाम एवं योग को विशेष रूप से अनिवार्य माना जाता था। शारीरिक मूल्यों के विकास से व्यक्ति में उत्साह, स्फूर्ति, मानसिक एवं चारित्रिक गुणों में वृद्धि एवं विकास संभव होता है। अतः शिक्षा में शारीरिकता एवं शारीरिक विकास का उद्देश्य व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के लिए लाभदायक है। खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक श्रम की पाठ्यचर्या क्रियाओं का नियमित संचालन आवश्यक है। इसके द्वारा मनुष्य में अनुशासन, सहिष्णुता, संघर्षशीलता, आत्म-निर्भरता, सुप्रभु, ईमानदारी, निर्णय क्षमता, शारीरिक शुद्धता आदि का विकास होता है।
-
नैतिक मूल्य - चरित्र व्यक्ति के गुणों का बाह्य स्वरूप को उजागर करता है एवं नैतिकता उसमेंसआंतरिक स्वभाव है। अतः चरित्र को आदतों का समूह भी कहा जाता है। चरित्र के अनंत कार्यों में नियम पालन, कर्तव्य परायणता, इत्यादि आचरण, सौंदर्यशास्त्र के गुण पाए जाते हैं। नैतिकता नीति शब्द से निकट है। नीति का अर्थ है "जिसे व्यवहार एवं समाज स्वीकार करता है तथा यह व्यक्ति एवं समाज दोनों पर प्रभावी करते हैं। अतः नैतिकता का संबंध स्वाभाविकता से होता है। चरित्रवान व्यक्ति बुद्धिमान माना जाता है। उसे उच्च, हित, अहिंसा, सत्याचार, अनुशासन, सद्भाव, निर्देशता आदि के गुणों का ध्यान रहता है।
गांधीजी के अनुसार - "एक व्यक्ति उच्च आदर्शों के बिना नैतिक स्वाभाव को प्राप्त नहीं कर सकता है।" उदाहरण, अहिंसा, दया एवं जीवन आदर्शों के गुणों बेवजह स्वाभाव को निर्धारित देते हैं। चारित्रिक मूल्यों के अंतर्गत समाज के लिए कष्ट सहन करना, जीवों पर दया, क्षमा, अहिंसा आदि आते हैं। आधुनिक समय में विद्यालय में नैतिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है तथा पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों का प्रमुख स्थान प्रदान किया है। नैतिक शिक्षा में समस्त छात्रों के पाठ्यक्रम को एक समान रूप से पालन किया जाता है। नैतिकता के सभी गुणों को उदाहरण एवं कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। -
सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्य - ई.बी. टेलर के अनुसार - सांस्कृतिक मूल्यों के अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, न्याय, नीति-विधान, अन्य व्यवस्थाएं तथा आदतें आती हैं। इसे व्यक्ति समाज के उत्तरदायी सदस्य के रूप में ग्रहण करता है। अतः समाज की संस्कृति का अर्थ है - समाज में जीवन जीने की कला। अतः शिक्षकों को सभ्यता एवं संस्कृति की विशेष महत्व होता है, जो हमारी विरासत की परिपाटी हुआ करती है।
-
बौद्धिक मूल्य - शैक्षिक मूल्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालयों का विषय समझना व्यापक, व्यावहारिक, उपयोगी, बुद्धिवर्धक अनुकूलन बढ़ाने वाला एवं व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होना उचित रूप से प्रदान किया जाना चाहिए। विषयों की साक्षात्कार आध्यात्मिक कक्षा में नमी मानी जाती है कि वे व्यावहारिक जीवन से संबंधित किए जाएं। इसके अलावा ज्ञान वृद्धि हेतु पुस्तकालय, रेडियो, टेलीविजन, सेमिनार, चर्चाएं एवं शोध का सहारा लिया जाए। शिक्षकों में बाल-विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद, प्रश्न उत्तर अभियान में शिक्षार्थियों के शिक्षण की दक्षता बढ़ाई जाए एवं सभी अध्यापकों को स्वतंत्रतापूर्वक पाठ्यक्रम चलाने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अतः विद्यालय एवं विद्यार्थी तथा विद्यार्थी के परस्पर संबंधों में प्रेम, सहयोग, सेवा, सद्भाव, आचरण पालन, मानवता, सौहार्द आदि भाव एवं मूल्यों का विकास होता है। यह सब विद्यालयीय वातावरण पर निर्भर करता है।
-
व्यावसायिक मूल्य - प्रत्येक व्यक्ति जीवन को व्यवस्थित करने हेतु जीविका के साधन को ढूंढता है। जीविकोपार्जन, धनोपार्जन आदि व्यावसायिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। जीवन में व्यक्ति अपने लिंग के अनुसार एवं परिस्थितियों के अनुसार कोई न कोई व्यवसाय चुनता पड़ता है अन्यथा वह अपना, अपनों का तथा समाज का हित नहीं कर सकता। इसलिए इस मूल्य हेतु व्यक्ति को किसी विशेष व्यवसाय में शिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह कुशल एवं निपुण होकर धनोपार्जन कर सके।
-
सामाजिक-राजनीतिक मूल्य - व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने समाज के लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मूल्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता, नागरिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी, जनता के योग्य बनाना आदि गुण सम्मिलित हैं। यह मूल्य भी व्यापक हैं इसके अंतर्गत कई अन्य मूल्य एवं लक्ष्य भी आ जाते हैं। सामाजिक मूल्यों को व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों से खोजता है एवं अपना मन बढ़ाता है जिससे राष्ट्र की महत्ता बढ़ती है। शिक्षा का उद्देश्य समाज को ऐसे समाज का विकास करना है, जिससे वह समाज का कल्याण कर सके जो शिक्षा बालक को समाजोपयोगी विकास नहीं कराती, वह शिक्षा व्यर्थ है।
-
अंतर्राष्ट्रीय मूल्य - वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व एकता में जुड़ा है। विश्व के सभी राष्ट्र मिल जुलकर उन्नति करें तो समाज का विकास होगा। समाज के सभी नागरिकों द्वारा विश्व के प्रति प्रेम तथा विश्वबंधुत्व की भावना स्थापना हेतु प्रयास करने चाहिए। विश्वविद्यालयों स्तर तक सभी संस्थाओं में स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करके विश्वबंधुत्व की भावना छात्रों में जागृत की जा सकती है।
-
जनतंत्रीय मूल्य - भारत एक जनतंत्रीय देश है। अतः शिक्षा के माध्यम से जनतंत्रीय मूल्यों का विकास करना अत्यावश्यक है। जनतंत्रीय मूल्य में स्वतंत्रता, भ्रातृत्व तथा समानता। स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार, भाषा एवं विचार, संचालन आदि की स्वतंत्रता आती है। भ्रातृत्व के अंतर्गत जाति, रंग, धर्म का भेद-भाव न होकर एक राष्ट्र के सभी लोग भाई-भाई हैं। समानता के अनुसार सब दृष्टिकोण से सबको समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व एवं सामाजिक न्याय मिलेगा। शिक्षा, नवन एवं मतदान प्रभावशाली बनें, जिससे जनतंत्र की शक्ति एवं सफलता सिद्ध हो। अतः विद्यालय में शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास एवं सामाजिक व्यवहार की सुविधा मिल सके।
-
नागरिकता के मूल्य - व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति को योग्य नागरिक बनाने का प्रयत्न शिक्षा द्वारा होता है। जैसे राज्य होता है, वैसे ही नागरिकता की शिक्षा भी जाती है।
यहां के नागरिकों को भी स्वतंत्रता, समानता एवं सामाजिक न्याय का अधिकार है। ईमानदारी, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता, उच्च शिक्षा, आत्मज्ञान, राजनीतिक कार्यों के प्रति रुचि एवं सक्रियता आदि उसके गुण उत्तम नागरिक के लिए अनिवार्य हैं।
जनता की सफलता सुधारात्मक पद्धति में ही है। इस मूल्य से व्यक्ति में जिम्मेदारी तथा अनुशासन की भावना बढ़ती है, इसके साथ-साथ निर्माण भी होता है। -
परिस्थितियों के अनुकूल मूल्य - यह प्रकृति का नियम है- कि जीवन संघर्ष में वही जीवित रह सकता है जो परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ हो। डार्विनवाद के अनुसार भी- जीवन के विकास परिस्थितियों के अनुकूलन से होते हैं। अतः शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों में ऐसी रूचि डालनी हो जिससे वे अपने वातावरण को अनुकूल बनाने में समर्थ हों अर्थात शिक्षा व्यक्ति को दृढ़ तथा शक्तिशाली बनाएं, जिससे वह अपने अनुकूलन को सभी तरह से रख सके। व्यक्ति अपनी बुद्धि, प्रवृत्तियों, भावनाओं, इच्छाओं आदि पर नियंत्रण रखें और जहां पर जिसकी जरूरत हो, उसका उचित प्रयोग समय-दशा और स्थिति के अनुसार करें।
व्यक्तित्व विकास के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार निर्धारित हो ताकि ऐसी सुविधा दी जाए जिससे बालकों में बौद्धिकता के विकास हो। ज्ञान, प्राकृतिक निरीक्षण, पिकनिक, कला-प्रदर्शनी, संगीत, नृत्य का प्रदर्शन, अभिनय, रेडियो, के कलात्मक कार्यक्रम आदि ऐसे साधन हैं, जिसमें भाग लेकर छात्र सौंदर्यबोधि का विकास कर सकते हैं।
|
|||||