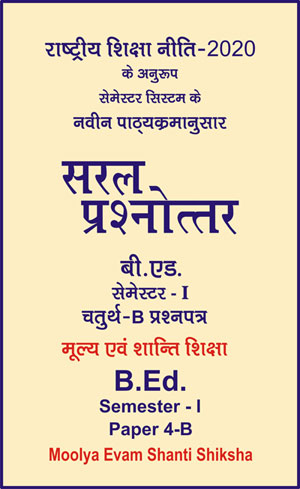|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-B - मूल्य एवं शान्ति शिक्षा
प्रश्न- भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं कौन-सी हैं? शिक्षा तथा संस्कृति के सम्बन्धों की व्याख्या कीजिए।
उत्तर-
संस्कृति का आधार - सामान्यतः संस्कृति शब्द प्रयोग संस्कार अथवा सुसंस्कृत के लिए किया जाता है। संस्कृति का अर्थ है - कुछ तत्वों की पूर्ति करना अथवा उन्हें संपन्न करना। अर्थात् विभिन्न संस्कृतियों द्वारा सामाजिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना।
संस्कृति की खोज संबंध मनुष्य से होता है, जिसके अन्तर्गत उसके रीति-रिवाज, परम्पराएं, मान्यताएं, धार्मिक, नैतिक, आर्थिक, विज्ञान, धर्म, विश्वास, सामाजिक संगठन, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था - सभी कुछ आ जाते हैं।
संस्कृति की परिभाषाएं - विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई संस्कृति की परिभाषाएं निम्नलिखित हैं -
सर्वेस्व एवं बुक्कन के अनुसार - "संस्कृति में वह शक्ति आ सकती है, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जा सकता है। किसी राष्ट्र की संस्कृति उसकी सामाजिक विरासत होती है।"
टेलर के अनुसार - "संस्कृति की सामान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी विशेष समाज एवं स्थान में निवास करने वाले विभिन्न व्यक्तियों के जीवन व्याख्य करने की सामाजिक विधि।"
टायलर के अनुसार - "संस्कृति वह जटिल पूंजी है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, कानून, परम्पराएं, वे योग्यताएं सम्मिलित होती हैं जो किसी समाज के सदस्य द्वारा अर्जित की जाती रहती हैं।"
भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं - भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं -
(1) पुरुषार्थ - पुरुषार्थ भारतीय जीवन एवं हिंदू दर्शन का एक अन्य प्रमुख तत्व रहा है। व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को सुव्यवस्थित ढंग से सीढ़ी प्रति सीढ़ी प्राप्त किया जाता है। पुरुषार्थ में भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है - धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष।
(A) धर्म - व्यक्ति का कर्तव्य के माध्यम से कार्यों की पूर्णता की जाना ही धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपने वर्ण, आश्रम, वंश, आयु एवं सामाजिक स्थिति से सम्बंधित धर्म अर्थात कर्तव्यों का पालन करें।
(B) अर्थ - अर्थ व्यक्ति का आर्थिक क्रियाओं एवं धन के अर्जन एवं संग्रह से संबंधित है, किंतु यह भौतिकतावादी दृष्टि नहीं बल्कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात् अपने आचारों की पालन-पोषण एवं विभिन्न ऋणों से मुक्त होने के लिए समर्पित किया जाने वाले पंच यज्ञों को करने के लिए होता है।
(C) काम - काम का तात्पर्य व्यक्ति के अपने वंश को समाज में उत्तराधिकार पीढ़ी-दर-पीढ़ी निरंतरता को बनाए रखना होता है। व्यक्ति की कामेच्छा नियंत्रित होती है। वह अपने सौंदर्यदृष्टि से अपने जीवन को संतुष्टि प्रदान करता है।
(D) मोक्ष - मोक्ष को साध्य एवं अंतिम लक्ष्य एवं पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया। जब व्यक्ति धर्म, अर्थ एवं काम के पुरुषार्थों के अनुरूप व्यवहार करता है, तब वह मोक्ष का अधिकारी हो सकता है।
(2) धर्म पर आस्था - धर्म का अर्थ होता है धारण करना - "धारयते इति धर्मः"। जो धारण करने योग्य हो उसे ही धर्म कहा जाता है। भारतीय समाज अपनी जीवन ज्योति, कला-कला ज्ञान, सामाजिक भावनाओं एवं राजनीतिक व्यवस्था के लिए मूल्यों को आधार मानता है। धर्म को भारतीय समाज को धर्म प्रधान समाज की संज्ञा दी जाती है। भारतीय दर्शन में कर्म की व्याख्या, पुरुषार्थों का विवेचन, पांच गुणों का उल्लेख एवं पंच महायज्ञों के सम्बन्ध के अतिरिक्त आश्रम, अर्थ एवं विवाह की संरचना भी धर्म द्वारा अनुमोदित एवं नियंत्रित रही है। कोई भी व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को अधिकार से प्राप्त कर सकता है, जब वह धर्म से युक्त हो। आश्रम एवं कर्तव्यों का पालन करता हो।
(3) आश्रम व्यवस्था - भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विशेषता से उसकी आश्रम व्यवस्था। भारतीय दर्शन में उल्लेखित श्लोक - शान्ति व्यक्तित्व के रूप में चार वर्षों के जीवन की आशा की गई है। व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन को नियमित करके उसके चार रही अर्थों में पुरुषार्थों की पूर्ति के लिए आश्रम व्यवस्था का विधान बनाया गया। चार प्रमुख आश्रम माने गए हैं - ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम।
(4) वर्ण व्यवस्था - प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार समाज चार वर्णों में यथा- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के रूप में विभक्त था। इसका आधार समाज के लोगों की योग्यताओं के आधार पर किया जाता था। सभी वर्णों के अपने-अपने कर्तव्य व धर्म हुए हैं।
(5) जाति प्रथा - प्राचीन श्रमण भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है। जाति एक ऐसा समूह है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिकता के आधार पर निर्धारित होती है। बाद में यही वर्ण की व्यवस्था जन्म आश्रित होने लगी।
(6) संयुक्त परिवार की प्रथा - भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण प्रथा संयुक्त परिवार की थी। इसमें कई पीढ़ी की व्यक्ति एक साथ रहते थे एवं सभी एकत्रित होकर समाज का विकास करते थे। संयुक्त परिवार संस्था का कार्य करता था, अज्ञान शिक्षा-दीक्षा, पाठ-पाठन एवं मनोरंजन आदि सभी की व्याख्या का कार्य करता था। नवीनता के कारण इस प्रथा का ह्रास हो रहा है।
(7) पुनर्जन्म में विश्वास - हिन्दू धर्मग्रंथों आत्मा को अमर-अजर एवं अविनाशी तत्व माना जाता है। साधारण हिन्दू धर्म की संस्कृति पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास करती है।
(8) संस्कार विधायन - संस्कार का शुद्धिकरण को कहते हैं। जिसका अर्थ है मनुष्य को शुभ बनाना, सुसंस्कृत, योग्य एवं शुद्ध करता। प्रमुख रूप से सोलह संस्कारों की व्यवस्था बनाई गई थी जो जीवन के शुभ शुद्धिकरण है। संस्कार के हिन्दू धर्म में एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान के रूप में माना गया है।
(9) विविधता में एकता - भारत एक बहुभाषी देश है। यहां पर विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। भिन्न संस्कृतियों के होते हुए भी वे सभी अपने को भारत का नागरिक मानते हैं। सभी मिल-जुलकर रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत की विविधता में एकता है।
शिक्षा एवं संस्कृति में सम्बन्ध - शिक्षा एवं संस्कृति का अन्योन्याश्रित संबंध है। संस्कृति के प्रभाव में शिक्षा निहित एवं निर्भरशास्र है। यदि किसी समाज की शिक्षा में कोई विशेषता मिलती है, तो उसका परिमाण अक्सर उस समाज की संस्कृति है। वस्तुतः प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षा का प्रचार करता है। शिक्षा निम्नलिखित प्रकार से संस्कृति की सहायक सिद्ध होती है -
(1) संस्कृति के संरक्षण में सहायक।
(2) संस्कृति के विकास में सहयोगी।
(3) संस्कृति की निरंतरता में सहायता के रूप में।
(4) संस्कृति के परिवर्तन में सहायता प्रदान करती है।
(5) संस्कृति से शिक्षा सामायोजन होती है।
(6) संस्कृति से सामाजिक परिवर्तनों का निर्वाह होती है।
(7) संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास करने में सक्षम होती है।
(8) संस्कृति का शिक्षण प्रणालियों एवं पद्धतियों पर प्रभाव पड़ता है।
(9) संस्कृति का शिक्षण अनुकूलन पर भी पड़ता है।
(10) संस्कृति का शिक्षा के उद्देश्यों पर भी प्रभाव पड़ता है।
(11) संस्कृति का अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है।
(12) संस्कृति विद्यालयों को भी प्रभावित करती है।
(13) संस्कृति बालक के एवं उसके जीवन के अमिट छाप के रूप में प्रभावित करती है।
|
|||||