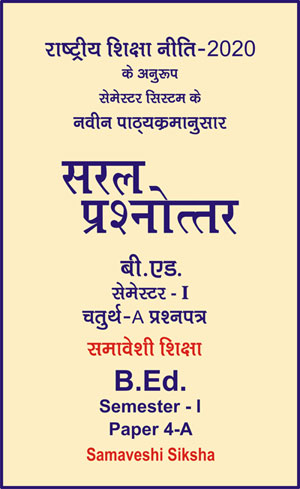|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों को बताइये और शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
उत्तर—
मंद अधिगामी बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधान
(Educational Provision for Slow Learner Children)
इन बालकों की सहायता के लिए वर्तमान समय में अधिक प्रयोग किये जा रहे हैं तथा सुधारात्मक अनुदेशन की निर्माण किया जा रहा है। इनके सम्बन्ध में शोध अध्ययन भी किये गये हैं, जिनसे मंद अधिगामी बालकों के लिए दिशा-निर्देशन मिला है।
(I) मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण विधियाँ
(Special Method of Teacher for Slow Learner Children)
शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने मंद अधिगामी बालकों के शिक्षण के लिए शिक्षण विधियों का विकास शोध अध्ययनों के आधार पर किया है। इन अध्ययनों से सिद्ध हुआ है कि मंद अधिगामी बालक सरल एवं प्रायोगिक शिक्षण विधियों से अधिक सीखते हैं जिनके अन्तर्गत मूर्त अधिगम अनुभव प्रदान किया जाये और सार्थक बनाया जाये।
अर्थात शिक्षण पद्धति में, गणित, इतिहास, विज्ञान तथा सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन के शिक्षण में शिक्षण पर्यटन का आयोजन अधिक उपयोगी होता है। जिन शिक्षण विधियों में चित्र, मानचित्र, चार्ट, मॉडल का प्रयोग किया जाता है उनसे यह बालक अधिक सीखते हैं। मंद अधिगामी बालकों के लिए निम्नलिखित तीन विधियाँ अधिक उपयोगी होती हैं—
(1) प्रगति आलेख तैयार व्यवस्था— विद्यालय के अन्तर्गत मंद अधिगामी बालकों की शैक्षिक प्रवृत्ति का आलेख तैयार करना चाहिए और इसका सामान्य परीक्षा एवं आकलन। संहित आलेख से बालक की समस्या का निदान होता है और उसकी प्रवृत्ति का भी पता चलता है। बालक के व्यावहारिक उपचार के लिए यह आलेख निर्माण आवश्यक है। इससे बालक का एकल इतिहास भी तैयार होता है, जिससे भविष्य में सहायता मिलती है। इस आलेख के आधार पर शिक्षक बालक को समुचित सुविधा तथा सहायता प्रदान कर सकता है।
(2) शिक्षक द्वारा बालकों का अवलोकन— शिक्षक द्वारा मंद अधिगामी बालकों के घर का अवलोकन करने से शिक्षक को परिवार के वातावरण का बोध होता है कि माता-पिता और अन्य सदस्य बालक के साथ किस प्रकार का व्यवहार एवं प्रोत्साहन देते हैं। यदि घर का वातावरण प्रतिकूल नहीं है तो शिक्षक का कर्तव्य होता है कि घर का वातावरण सुधारने के लिए उसके माता-पिता को सुझाव दें जिससे बालक का समुचित विकास हो सके।
(3) अधिगमगत अनुदेशन आवश्यकता— उपर्युक्त विवरण से विदित होता है कि इन बालकों के सीखने की गति धीमी होती है जिसके अनेक कारण होते हैं। इनके निवारण के कारणों का सही बोध होता है और सुधार हेतु अनुदेशन की आवश्यकता होती है। इसकी प्रक्रिया के अनुसार अधिगमगत अनुदेशन अधिक उपयोगी होता है क्योंकि इसके अन्तर्गत पाठ्यवस्तु को छोटे-छोटे खण्डों में प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक खण्ड के बाद उसे अनुग्रही कार्य होता है। भाषा अधिगम अनुभूति की जाँच करता है जिसके सही होने पर उसे पुनर्बल मिलता है। इस प्रकार यह विधि मंद अधिगामी बालकों के लिए उत्तम है क्योंकि इससे प्रत्येक बालक को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है।
(II) मंद अधिगामी बालकों के लिए पाठ्यक्रम की भूमिका
(Organization of Curriculum for Slow Learner Children)
यदि इन बालकों को विशिष्ट विद्यालयों तथा विशिष्ट कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तब इस परिस्थिति में इनका पाठ्यक्रम भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यवस्तु का रूप आयु वर्ग के अनुसार बदलता रहना चाहिए और आयु वर्ग के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का प्रारूप ऐसा रखा जाये जिससे ऐसे बालकों का सम्पूर्ण विकास हो सके। इसका स्वरूप सामान्य विद्यालयों से भिन्न होना चाहिए। इनकी शिक्षण व्यवस्था भी विशेष प्रकार की होनी चाहिए।
ऐसे बालकों के पाठ्यक्रम के लिए निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करना चाहिए—
(1) पाठ्यक्रम का केन्द्र केवल भाषा और अंकों का ज्ञान।
(2) सामान्य ज्ञान सम्बन्धी विषय जैसे— पर्यावरण, योजनात्मक क्रियाएँ तथा सौन्दर्यानुभूति क्रियाओं को सम्मिलित किया जाये।
कुछ व्यावहारिक क्रियाओं को भी महत्व दिया जाये जिससे उनमें रुचि विकसित हो सके। समय विभाजन की क्रियाओं को कठिनाई में ध्यान में रखते हुए रखा जाना चाहिए। छोटे विद्यालयों में छोटे बालकों के लिए पाठ्य-सहायक क्रियाओं और सुधारात्मक कक्षाओं की व्यवस्था की जाये।
(III) पाठ्यक्रम का लचीलाीकरण
(Flexible Curriculum)
शिक्षाविदों को यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप ऐसा हो जिससे मंद अधिगामी अपना विकास कर सकें। मंद अधिगामी बालकों के विभाजन अधिक होते हैं तथा बालकों की अपनी समस्या और अधिगम आवश्यकताएँ होती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जितना सम्भव हो पाठ्यक्रम का स्वरूप लचीला हो। इसके अन्तर्गत मूर्त प्रस्तुतिकरण। अनुभवों को प्रोत्साहित किया जाये क्योंकि मंद अधिगामी बालक मूर्त वस्तुओं तथा दृश्य सामग्री से अधिक सीखते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वैज्ञानिक पाठ्यवस्तु और अमूर्त प्रक्रियाओं को कम महत्व दिया जाये क्योंकि इसे समझने में मंद अधिगामी बालकों को कठिनाई होती है। प्रयोगात्मक तथा योजना कार्यों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। इन बालकों के लिए मानसिक कार्य, लकड़ी के कार्य, चमड़े के कार्य, बुनने के कार्य, सिलाई तथा घर सजाने कार्यों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाये।
(IV) मंद अधिगामी बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियाँ
(Teaching Techniques for Slow Learner Children)
मंद अधिगामी बालकों के शिक्षण के लिए व्यक्तिगत उपचार विधि का उपयोग करना चाहिए। इनके लिए शिक्षण प्रविधियों का चयन इनकी आवश्यकताओं तथा मानसिक योग्यताओं के अनुरूप करना चाहिए जिससे इनका समुचित उपयोग किया जा सके। बालकों के विकास के अनेक शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक पक्ष होते हैं। बालकों की सम्प्रेषण प्रक्रिया में इनका अलग-अलग विचार करना चाहिए। यह पक्ष परिवर्तनशील होते हैं। इनमें परिवर्तन होता रहता है। इस लिए निम्नलिखित शिक्षण प्रविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए—
(1) व्यावहारिक आयाम— मंद अधिगामी बालकों के शिक्षण के लिए यह आयाम अधिक सार्थक तथा उपयोगी होता है। मंद अधिगामी बालक घर में अधिक रहते हैं और घर में देखते, सुनते तथा स्पर्श करने में अनुभव करते रहते हैं। यदि शिक्षण प्रक्रिया मानविकी व्यावहारिक आयाम में अमूर्त विषयों तथा सम्प्रेषणीय तत्व का सम्मिलन किया जाये तो बालकों को अधिक सफलता मिलती है।
(2) अभिप्रेरणा देना— मंद अधिगामी बालकों को अभिप्रेरणा देनी चाहिए जिससे इनमें सृजनशीलता का भाव उत्पन्न किया जा सके। इनके लिए ऐसी परिस्थित उत्पन्न की जाये जिससे उनमें सुरक्षा तथा आत्मविश्वास का भाव विकसित हो तथा वे अधिक सीखते हैं। शिक्षकों से इन बालकों के अच्छे सम्पर्क होने चाहिए।
(3) बालकों की प्रगति का आकलन— मंद अधिगामी बालकों के लिए यह सुझाव दिया गया है कि विद्यालय में इनके संचित प्रगति आलेख तैयार किए जायें। इसके आधार पर इनके व्यक्तिगत उपचार तथा सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(4) प्रत्यय की संरचना— मंद अधिगामी बालक सरल सामाजिकीकरण में सक्षम होते हैं। इन्हें योजना, प्रयोग, वाद-विवाद आदि के अधिक अवसर दिये जायें। इनके लिए ऐसी परिस्थित उत्पन्न की जाये जिससे वे स्वयं सामान्यीकृत जीवन पद्धति में वस्तुओं में समानता और सम्बन्ध को जान सकें। इनमें उत्सुकता एवं रुचि की उत्पत्ति का प्रयास किया जाये। इन्हें समय के अवसर दिया जाये जिससे इनमें प्रेरणा का विकास हो सके।
(5) अधिगम की निरन्तरता— शिक्षकों को ऐसी क्रिया करनी चाहिए जिससे बालकों सीखने हेतु प्रेरणा प्राप्त हो। शिक्षण में बालकों के मानसिक, भावात्मक, सामाजिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों को बालकों के पहचान कर लेने चाहिए कि वे बालकों सीखने हेतु तत्पर रहते हैं अथवा नहीं। इन बालकों की उपलब्धियों का निरन्तर अवलोकन करते रहना चाहिए।
(6) कार्य विधि/योजना विधि— मंद अधिगामी बालकों को सीखने के लिए कार्य करने के अवसर दिया जाये क्योंकि वे कार्य के तरीके सीखते हैं। ये मानसिक क्रियाओं में अच्छी तरह सीख पाते हैं क्योंकि इनके कल्पना रखने में कठिनाई होती है इन्हें अनुभव द्वारा सीखने की। वे कुछ प्रयोग करें, योजना विधि का उपयोग करें जिससे अनुभव करके सीख सकें।
(7) कार्य का स्तरीकरण— मंद अधिगामी बालकों की शिक्षण पाठ्यवस्तु का स्तरीकरण करना चाहिए। स्तरीकरण में इनकी आवश्यकताओं और मानसिक स्तर को ध्यान में रखा जाये। इन बालकों की कठिनाइयों तथा समस्याओं के अनुरूप पाठ्यवस्तु के स्तर का चयन किया जाये। इनके शिक्षकों को सही पाठ्यवस्तु विश्लेषण और स्तरीकरण किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाये कि इन बालकों के अधिगम हेतु विभिन्न स्तरों की पाठ्यवस्तु का उपयोग हो।
(8) एकीकरण करना— इन्हें शिक्षण की पाठ्यवस्तु का पर्याप्त अभ्यास कराया जाये तथा पुनरावृत्ति कराई जाये। इनके अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे ये पाठ्यवस्तु उत्तम ढंग से एकीकृत कर सकें।
मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं के विशेषज्ञों के सहयोग की आवश्यकता होती है जैसे— शिक्षक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासक आदि। मंद अधिगामी बालकों की सम्पूर्ण जानकारी मनोवैज्ञानिकों द्वारा ही की जाती है। ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रियात्मक तथा विकास की कठिनाइयों को भी पता लगाते हैं। डॉक्टरी परीक्षण द्वारा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं, ज्ञानेन्द्रियों तथा शारीरिक बाधिता का पता चलता है।
शिक्षक की भूमिका
(Role of Teacher)
गिलफॉर्ड तथा टैक्सले ने (1971) में मंद अधिगामी बालकों के शिक्षण के लिए ठोस सुझाव दिये हैं जो इस प्रकार हैं—
(1) इन बालकों के अध्ययन हेतु व्यापक सुविधाओं का आयोजन करता तथा इन्हें बालकों की पहुँच के अन्तर्गत ले रखना।
(2) इनके शिक्षण में योग्य तथा प्रतिभावान बालकों की सहायता लेनी चाहिए जिससे वह इनकी व्यक्तिगत सहायता कर सकें।
(3) शिक्षकों को ऐसे बालकों के लिये छोटी कक्षा अथवा अनुवर्ग शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
(4) पाठ्यवस्तु के अनुदेशन निर्माण तथा इनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
(5) इन बालकों के सुझावों के प्रति शिक्षकों को संवेदनशील रहना चाहिए।
(6) इन बालकों को सतत् शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
(7) इन बालकों के माता-पिता की सहायता लेने का प्रयास करना चाहिए।
(8) शिक्षकों को पाठ्यवस्तु को छोटे-छोटे खण्डों में प्रस्तुत करना चाहिए और मूर्त सहायक सामग्री का उपयोग अधिक करना चाहिए। इनके लिए सुधारात्मक शिक्षण को तथा अनुवर्ती शिक्षण की सुव्यवस्थित व्यवस्था करनी चाहिए।
(9) जितना सम्भव हो इन बालकों को स्वतंत्रता देनी चाहिए।
(10) इन बालकों को अवसर देना चाहिए न कि प्रवेश देना चाहिए क्योंकि ये बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के समान गति में नहीं सीख सकते हैं।
(11) इन बालकों के सुझाव को मानना चाहिए और सम्भव हो तो अनुसरण करना चाहिए।
(12) कक्षा में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये जिससे सभी बालक क्रियाशील रह सकें, जैसे— कहानी कथन, नाटक, संगीत आदि।
|
|||||