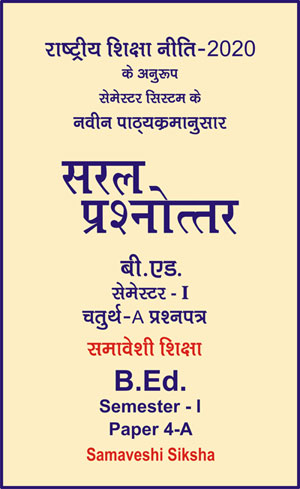|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- समावेशी शिक्षा के विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए।
अथवा
भारत में समावेशी शिक्षा के विभिन्न मुद्दों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
उत्तर -
समावेशी का तात्पर्य
समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करने का कार्य करती है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक असहाय या विकलांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षा के समावेशीकरण के अन्तर्गत एक सामान्य छात्र एक असहाय या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना केवल विशिष्ट छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक शिक्षक को इस सिद्धांत या व्यवस्था को अपनी कक्षा में व्यवस्थित रूप से लाना होता है।
समावेशी शिक्षा का एकीकरण के सिद्धांत का जन्म कनाडा और अमेरिका में हुआ था। इसकी शुरुआत कनाडा व अमेरिका से प्रारंभ हुई। प्राचीन शिक्षा पद्धति के बजाय नई शिक्षा नीति का प्रयोग आधुनिक समय में होने लगा है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या विशेष कक्षाओं को स्वीकार नहीं करता। असहाय छात्रों को सामान्य छात्रों से अलग शिक्षा देना यह तक स्वीकार नहीं है तथा मान्य भी नहीं है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा नैतिक एवं कानूनी दृष्टि से भी इसे सही नहीं माना जा सकता। असहाय छात्रों को भी सामान्य छात्रों की भांति शिक्षा प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है।
समावेशी शिक्षा और शिक्षण
एक शिक्षण-एक सहयोग अर्थात् यह शिक्षण प्रतिमान में एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो दूसरा प्रशिक्षित शिक्षण में पहले शिक्षक द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्य को प्रभावी तथा उपयोगी बनाने हेतु कक्षा में अनुशासन, कक्षा को सुव्यवस्थित रखने तथा छात्रों की तात्कालिक समस्याओं के निराकरण में सहयोग करता है।
एक शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो दूसरा शिक्षक कक्षा में सूक्ष्म-दृष्टि निरीक्षण करता है। इस शिक्षा के कई रूप हैं:
(i) एक शिक्षा एक निरीक्षण - मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, सहायक शिक्षक कक्षा का निरीक्षण करता है।
(ii) स्थिर और घूर्णीय शिक्षा - इसमें कक्षा को अनेक भागों में बाँट दिया जाता है। मुख्य शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, दूसरा विशेष शिक्षक दूसरे फ्लैग पर इसकी जाँच करता है।
(iii) समानतर शिक्षण - इसमें आधे कक्षा में मुख्य शिक्षक तथा आधे कक्षा में विशेष शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रदान किया जाता है। दोनों समूहों को एक जैसा पाठ पढ़ाया जाता है।
(iv) वैकल्पिक शिक्षण - मुख्य शिक्षक अधिक छात्रों को पाठ पढ़ाता है जबकि विशेष शिक्षक दूसरे समूह के दूसरे पाठ पढ़ाता है।
(v) टीचिंग टीम - यह पारस्परिक शिक्षण पद्धति है। दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षण देते हैं। यह काफी सहज शिक्षण पद्धति है।
समावेशी शिक्षा का महत्व
समावेशी शिक्षा का महत्व निम्नवत है—
-
समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करती है।
-
समावेशी शिक्षा अन्य छात्रों को अपनी उम्र के साथ कक्षा के जीवन में काम लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने हेतु प्रेरित करती है।
-
समावेशी शिक्षा बच्चों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में और उनके स्थानीय स्कूलों की गतिविधियों में उनके माता-पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है।
-
समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनपन की स्कूल संस्कृति के साथ-साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहन और अवसर प्रदान करती है।
-
समावेशी शिक्षा शिक्षक/विद्यार्थियों को अपने स्वयं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के साथ-साथ प्रत्येक को व्यापक विद्यालय के साथ मैत्रीभाव का विकास करने की क्षमता विकसित करती है।
इस प्रकार समावेशी शिक्षा समाज के सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की बात का समर्थन करती है। समावेशी शिक्षा का आशय विकलांग विद्यार्थियों/विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ बैठकर सामान्य रूप से समान शिक्षा देना है ताकि सामान्य छात्रों और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले छात्रों में कोई भेदभाव न रहे तथा दोनों तरह के विद्यार्थी एक-दूसरे को ठीक ढंग से समझते हुए आपसी सहयोग के साथ पठन-पाठन के कार्य को निष्पादित कर सकें।
समावेशी शिक्षा से सम्बन्ध कुछ चुनौतियाँ/मुद्दे
समावेशी शिक्षा के सम्बन्ध कुछ चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ या मुद्दे निम्नवत हैं—
1. सामाजिक विद्यालयी वातावरण - बालकों की शिक्षा चाहे वह किसी भी स्तर की हो, उसमें विद्यालय वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। विद्यालय का वातावरण ही औपचारिक रूप से कुछ शिक्षाएँ स्वयं ही दे देता है। समावेशी शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण सुखद एवं प्रेरणात्मक होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों, विशिष्ट शैक्षिक क्रियाकलापों इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आधुनिक साजो-सामान, शैक्षिक सहायक उपकरण, सहायकताएँ, संसाधन, भवन की बनावट इत्यादि का प्रबन्ध आवश्यक है। बिना इसके विद्यालय में समावेशी वातावरण का निर्माण सम्भव नहीं है।
2. सबके लिए विद्यालय की उपलब्धता - समावेशी शिक्षा की मूल भावना है कि एक ऐसा विद्यालय हो जहाँ सभी बालक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। परन्तु सामान्यत: यह तरह की बातें देखने और सुनने में आती हैं कि किसी बालक को उसकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया जाता है।
समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को सभी बालकों तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में बाधित नीतियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए।
शिक्षा के अधिकरण अधिनियम 2009, इस दिशा में एक प्रभावी संवैधानिक कदम है परन्तु भारत में इसका बाधारहित कार्यान्वयन अभी भी शेष है।
3. बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम - बालकों को शिक्षित करने का सबसे प्रभावी तरीका है कि उनके खेलने के तरीकों तथा गतिविधियों के माध्यम से सीखने-सिखाने का प्रयास किया जाए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम बालकों की अभिरुचियों, मनोविज्ञान, आकांक्षाओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रुचि के अनुसार अनुकूल बनाया जा सके। बालकों में विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास हो सके। उसे विद्यालय के बाहर बालक के सामाजिक जीवन से जोड़ा जा सके।
4. मार्ग निर्देशन व मार्गदर्शन की व्यवस्था - शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सत्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के साथ भी लागू होती है। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक और परिवार सामुदायिक अधिकारियों के साथ विद्यालय कर्मचारियों के बीच सहयोग और सहकारिता की आवश्यकता है।
समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत घर से विद्यालय जाते समय बालकों को आस-पास के माहौल में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालयों में सीखने की प्रक्रिया में यह एक महत्वपूर्ण कारक होता है। मार्गदर्शन और निर्देश के अभाव में कठिनाइयाँ बढ़ सकती हैं, जिससे आत्मविश्वास में कमी होने की संभावना रहती है।
5. सहायक तकनीकी उपकरणों का उपयोग - आज के युग में तकनीकी उपयोग से मानव जीवन काफी हद तक सुगम हो गया है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आज तकनीक का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए और उसके प्रचार-प्रसार के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जाना भी आवश्यक है।
- दूरदर्शन,
- कम्प्यूटर,
- रेडियो,
- इंटरनेट,
- मोबाइल फोन,
शिक्षण तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा सामाजिकरण, मनोरंजन आदि में प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है।
6. समुदाय की सक्रिय भागीदारी - विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा की पूरी बुनियाद प्रतिभागिता/सहभागिता पर टिकी है। एक अकेले व्यक्ति प्रयासों से उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।
समावेशी शिक्षा हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक की सामाजिक जीवन की स्थितियों को समाज के साथ जोड़ने से ही उसे शिक्षा ग्रहण करने में सहायता मिलेगी।
7. शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण - शिक्षक की ही शिक्षा पद्धति को वास्तविक गतिशील शक्ति तथा शैक्षिक संस्थानों की आधारशिला माना गया है। यह सत्य है कि बालक मात्र पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों क्रियाएँ, सहायक शिक्षण अधिगम सामग्री आदि सभी वस्तुओं का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान तथा योगदान होता है। परन्तु शिक्षक ही वह शक्ति एवं स्रोत होता है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आपको शिक्षण कार्य तक ही सीमित नहीं रखता है अपितु विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित रूप से समायोजन करने हेतु विशेष प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करता, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अभिभावकों तथा विशेष अध्यापकों से बालक की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहयोग व सहकार पूर्ण व्यवहार करता, बालक को मिलने वाली शैक्षिक सुविधाओं की व्याख्या करता इसलिए कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण के साथ-साथ उपर्युक्त कार्यों से पूर्णतया निपुण हो एवं इस हेतु उन्हें सामान्य बालकों, विशेष बालकों एवं विद्यालयों की पर्याप्त जानकारी हो। वह बालकों के प्रति स्वभाव व सकारात्मक अभिवृत्तियों रखता हो, उनके मानसिकता को समझता हो।
|
|||||