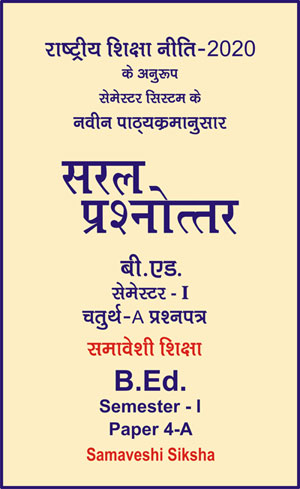|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- असमर्थ व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति का उल्लेख कीजिए।
उत्तर -
असमर्थ व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा के लिए 10 फरवरी, 2006 को एक व्यापक नीति लागू की गई।
इसका मुख्य उद्देश्य संविधान में निहित सभी व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा प्रतिष्ठा का अधिकार प्रदान करना था, तथा एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना था, जिसमें असमर्थ बच्चों एवं व्यक्तियों को स्थान सुरक्षित हो।
आधुनिक समाज में समावेशी शिक्षा की धारा ने असमर्थ बालकों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर दिया है। आज समाज में मानसिकता परिवर्तन होने के कारण समाज इन बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार है और इसे सहज माना जा रहा है।
असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए कुछ प्रयास
2006 से पूर्व भी इन बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास किए गए, जिन प्रयासों में कुछ सफलता मिली। इन प्रयासों से विशिष्ट शिक्षा धारा को बल मिला।
2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ असमर्थ व्यक्ति हैं,
जबकि 2011 के आंकड़ों में बाकी बचे हुए असमर्थ व्यक्तियों में अलग-अलग प्रकार के कुछ दृष्टिहीन, कुछ शारीरिक, कुछ श्रवण, कुछ वाणी व भाषा, कुछ अन्य बाधा से असमर्थ हैं।
75 प्रतिशत असमर्थ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनमें से 49 प्रतिशत शिक्षा से वंचित तथा 34 प्रतिशत रोजगार में हैं।
ऐसे में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके पूर्व इनके लिए व्यावसायिक पुनर्वास पर बल दिया जाता था, जिससे वे अपना रोजगार कर सकें व आत्मनिर्भर बन सकें।
असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए कुछ कानून
असमर्थ बालकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता व अधिकारों से संबंधित कुछ नियम एवं कानून बनाए गए हैं।
2006 की शिक्षा नीति से पूर्व प्रमुख कानून निम्न हैं—
-
Rehabilitation Council of India, Act 1992:
- 1992 के इस एक्ट का सम्बन्ध मानव संसाधनों का विकास करने तथा असमर्थ बालकों के पुनर्वास के सम्बंध में सुविधाएँ प्रदान करने से संबंधित है।
-
Persons with Disabilities, Act 1995:
- यह एक्ट असमर्थ व्यक्तियों को शिक्षा तथा नौकरी का अधिकार प्रदान करता है तथा इसमें बाधारहित वातावरण तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान भी है।
-
National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability Act, 1999:
- इस एक्ट के द्वारा असमर्थ बालकों के अभिभावक बनने की कानूनी प्रक्रिया निर्धारित की गई है
- इसका उद्देश्य स्वतंत्र तथा सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है, जिससे असमर्थ व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जीवनयापन कर सकें।
उपर्युक्त कानून के साथ-साथ अब सरकार ने कई ऐसी संस्थाएँ स्थापित की हैं जो इन असमर्थ व्यक्तियों की सुरक्षा, शिक्षा, व्यवसाय, पुनर्वास के लिए कार्य कर रही हैं। ये संस्थाएँ केंद्र, राज्य, जिला तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यरत हैं।
इसके साथ-साथ लगभग 250 प्राइवेट संस्थाएँ इनकी शिक्षा, व्यवसाय के लिए कार्य कर रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज व ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर इन बच्चों की शिक्षा व व्यवसायिक पुनर्वास के लिए कार्यरत हैं।
साथ ही राष्ट्रीय विकलांग निगम (NHFDC) का विशेष योगदान है जो अपने अंग व बाह्य व्यक्तियों को कम ब्याज पर धन उपलब्ध कराता है जिससे वे व्यक्तिगत रोजगार कर सकें।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति अधिनियम, 2006 को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत कर लेते हैं, ताकि इसे समझने में आसानी हो—
राष्ट्रीय अधिनियम 2006
| राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष | हस्तक्षेप के प्रमुख तत्व |
|---|---|
| हस्तक्षेप से बचाव तथा पुनर्वास माध्यम | बचाव, शीघ्र पहचान व हस्तक्षेप |
| असमर्थ स्त्रियाँ | पुनर्वास सहायता कार्यक्रम |
| अवरोध रहित वातावरण | मानव संसाधन विकास |
| असमर्थता प्रमाणपत्र देना | असमर्थ व्यक्तियों की शिक्षा |
| सामाजिक सुरक्षा | रोजगार |
| गैर-सरकारी संस्थानों को प्रोत्साहन देना | अवरोधरहित वातावरण |
| माता-पिता को सामाजिक-आर्थिक स्तर सम्बंधी सूचनाएँ | सामाजिक सुरक्षा |
| अनुसंधान | अनुसंधान |
| खेलकूद व सांस्कृतिक जीवन | खेल क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रियाएँ |
| वर्तमान अधिनियम में परिवर्तन | कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व |
असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति अधिनियम 2006
इस नीति में जो सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं, उपरोक्त चित्र उसका सारांश है।
इस नीति में उपरोक्त बिंदुओं के लिए सुझाव व कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, जिनका विवेचन इस प्रकार है—
1. असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति तथा मौलिक पक्ष
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2006 में यह माना गया कि असमर्थ एवं बाधित व्यक्ति भी समाज का अभिन्न अंग हैं। उन्हें भी समाज में चलने हेतु समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसीलिए राष्ट्र उनको जीवनयापन करने तथा समान अधिकार प्रदान करने के लिए बचनबद्ध है।
इस शिक्षा नीति के मौलिक पक्ष इस प्रकार हैं —
(i) असमर्थता से बचाव एवं पुनर्वास - इस नीति पर बल दिया जाता है कि सामान्य जनता को जागरूक बनाया जाए जिससे वे रिश्तों से इस बात की जानकारी लें कि समाज में किसी भी प्रक्रिया में कोई बाधा हो तो ध्यान रखा जाए कि समाज में बाधित बच्चे पैदा न हों। पुनर्वास के सम्बंध में नीति तीन प्रकार से विषयक किया गया है —
पुनर्वास
| वैहिक पुनर्वास | शैक्षिक पुनर्वास | आर्थिक पुनर्वास |
|---|---|---|
| शीघ्र पहचान | उपस्थिति व सत्ता | नौकरी |
| परामर्श एवं मेडिकल | छात्रवृत्ति | प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी की व्यवस्था |
| सहयोगी साधन | तकनीकी व व्यावसायिक | स्व-व्यवसाय शिक्षा |
| - | विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच | - |
पुनर्वास के सम्बन्ध में शिक्षा नीति, 2006 में निम्न बातें स्पष्ट हैं जो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।
a. शीघ्र पहचान - शीघ्र पहचान के लिए सरकार द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि ग्रामीण जनता तक भी ये सुविधाएँ पहुँच सकें।
b. परामर्श व मेडिकल - इस नीति में सुझाव दिया गया है कि असमर्थ बालकों की पहचान कर उनके उपचार के लिए परामर्श व चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसमें वैद्यकीय चिकित्सा, मनोचिकित्सा, श्रव्य चिकित्सा तथा हस्ताक्षर को अन्य प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा।
- इस कार्य के लिए राज्य तथा अन्य सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।
- असमर्थ व्यक्तियों का 75 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, इसलिए विशेष ध्यान देते हुए राज्य सरकार की सहायता से जिला असमर्थ पुनर्वास केंद्र (District Rehabilitation Disability Center - DDRC) की स्थापना की जाएगी।
- ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इनके स्वास्थ्य की देख-रेख का कार्य ASHA (Accredit Social Health Activities) के द्वारा सम्पन्न किया जाएगा।
c. सहयोगी साधन - राष्ट्रीय नीति 2006 में वैद्यिक पुनर्वास के अन्तर्गत सहयोगी साधन की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाएगा।
- असमर्थ बालकों के लिए पीछे वाली कुर्सी, साइकिल, बैसाखी।
- इन बच्चों को पढ़ने-लिखने में सहायक उपकरण जैसे ब्रेल पुस्तकें, टेप रिकॉर्डर, अन्य उपकरण की व्यवस्था की जाएगी।
- असमर्थ बच्चों के लिए सहयोगी साधनों की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं गैर-सरकारी संस्थाएँ सहायता करेंगी।
(ii) शैक्षिक पुनर्वास -
असमर्थ बच्चों को शिक्षा के लिए संविधान की धारा 21 सभी को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करती है।
- असमर्थ व्यक्तियों के लिए असमर्थता एक्ट 1995 के भाग 26 में असमर्थ बालकों को 13 वर्ष तक की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है।
- सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6-14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क गुणवत्तायुक्त शिक्षा देना है।
- इस अभियान में बाधित एवं असमर्थ बालकों की शिक्षा के लिए वैद्यकीय शिक्षा, सहयोगी सामग्री की व्यवस्था, समुदाय आधारित पुनर्वास, पाठ्य सामग्री की व्यवस्था, अनुकूलन आदि की व्यवस्था का सरकार को उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।
a. उपस्थिति व सत्ता - असमर्थ बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार उन बच्चों का पता लगाएगी जो असमर्थ हैं व विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसके लिए सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके आधार पर इन बच्चों को विद्यालय में नामांकन किया जाएगा ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष उपकरण, पुस्तकें आदि की व्यवस्था की जाएगी।
b. छात्रवृत्ति - इस नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि असमर्थ एवं बाधित बालकों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। लेकिन इसका भविष्य में विस्तार किया जाएगा जिससे सभी असमर्थ बालक अपनी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।
c. तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा - यह सुझाव दिया गया है कि असमर्थ एवं बाधित बालकों को विशेष प्रशिक्षण तथा माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- व्यावसायिक शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाएगा।
- इसके लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा।
d. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच - असमर्थ बालक जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थान व विश्वविद्यालयों में विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
iii. असमर्थ व्यक्तियों का आर्थिक पुनर्वास
आर्थिक पुनर्वास से अर्थ है कि असमर्थ व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए दो प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है— प्रथम: नौकरियाँ तथा द्वितीय: स्वरोजगार।
a. सरकारी नौकरियाँ - इसके अनुसार सरकार की नौकरियों में असमर्थ व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।
- केंद्र तथा राज्य के सरकारी कार्यालयों, संस्थानों में A, B, C तथा D समूह में आरक्षण
- A - 3.07%
- B - 4.41%
- C - 3.76%
- D - 3.18%
b. गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी की व्यवस्था - गैर-सरकारी क्षेत्र में भी असमर्थ व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस वर्ग में नौकरी में समावेशी असमर्थ व्यक्तियों के टैक्स में छूट तथा प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- जिससे वे अपनी व्यावसायिक कुशलता का विकास कर सकें।
c. स्व-रोजगार - व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण के द्वारा असमर्थ व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- असमर्थ व्यक्तियों को आसान शर्तों पर NHFDC के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाएगा।
- यह कम ब्याज दर पर दिया जाएगा तथा टैक्स में छूट भी दी जाएगी।
- स्वयं सहायता समूह योजना के अंतर्गत विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
2. असमर्थ स्त्रियाँ
भारत में बालकों के साथ-साथ अधिकतर स्त्रियाँ भी असमर्थता से बाधित हैं।
- 2001 की जनगणना के अनुसार 93.01% लाख असमर्थ स्त्रियाँ हैं।
- यह कुल समूची असमर्थ जनसंख्या का 42.46% है।
- असमर्थ स्त्रियों को व्यावसायिक पुनर्वास, नौकरी से रक्षा, उत्पादन से सुरक्षा की आवश्यकता है।
असमर्थ स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान - राष्ट्रीय नीति में इनके लिए रोजगार व आवास स्थान बनाने का प्रावधान रखा गया है। इस नीति में असमर्थ स्त्रियों के लिए निम्न बातें कही गई—
-
- असमर्थ स्त्रियों के लिए आवास व रोजगार।
- रोजगारकर्मी स्त्रियों हेतु होस्टल बनाने का प्रावधान।
- असमर्थ स्त्रियों के बच्चों की देखभाल के लिए अतिरिक्त भत्ता देने का प्रावधान।
- यह सहायता केवल उन्हीं स्त्रियों को ही प्रदान की जाएगी जिनके बच्चे भी असमर्थ हैं।
3. असमर्थी बालक :-
भारत में असमर्थी व्यक्तियों का अधिकांश समूह बालकों का है, जिनके लिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इस नीति में असमर्थी बालकों के लिए निम्न सुझाव दिए गए हैं:-
- देखभाल एवं प्रतिकर से विकास का अधिकार।
- समानता एवं प्रतिकर से विकास का अधिकार।
- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण में समानता के अवसर।
- विकास का अधिकार तथा विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान।
इस प्रकार की नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि असमर्थी बालकों की देखभाल, समानता, स्वास्थ्य एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण में समानता की आवश्यकता है।
4. अवरोधरहित वातावरण :-
राष्ट्रीय नीति में इस बात पर ध्यान दिया गया है कि असमर्थी बालकों एवं व्यक्तियों के लिए अवरोधरहित वातावरण का निर्माण किया जाएगा। ताकि असमर्थी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चल-फिर सकें। इसके लिए शिक्षा संस्थानों में आने-जाने के लिए सुविधा, सहायक उपकरणों की उपलब्धता आदि की व्यवस्था की जाएगी।
5. असमर्थ प्रमाण पत्र प्रदान करना :-
सरकार इस बात के लिए दृढ़ है कि असमर्थी व्यक्तियों को असमर्थता का प्रमाण पत्र दिया जाए।
- इस प्रक्रिया के लिए सरल, पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।
- इस सर्टिफिकेट से इन्हें रोजगार के अवसरों में लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।
6. सामाजिक सुरक्षा :-
सरकार असमर्थी व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बचनवद्ध है। इसके लिए सरकार ने निम्न उपाय अपनाये हैं:-
- (क) राज्य सरकार इन असमर्थी व्यक्तियों को असमर्थ भत्ता या असमर्थता पेंशन प्रदान करती है।
- (ख) केंद्र सरकार असमर्थ बालकों के अभिभावकों को टैक्स पर छूट देती है।
- (ग) सहायक अभिभावक योजना के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा बहु-विकलांग बालकों की देख-रेख के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस प्रकार इस नीति में असमर्थी बालकों की सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है ताकि वे बच्चे व व्यक्ति समाज में आसानी से सुरक्षित जीवनयापन कर सकें।
7. गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन :-
विकलांग एवं असमर्थी बालकों व व्यक्तियों को रोजगार देने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- जैसा कि अभी तक कई गैर-सरकारी संस्थाएँ इस हेतु कार्य कर रही हैं।
- इस संस्थानों के साथ सम्पर्क बढ़ाया जाएगा व उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस नीति में निम्न बातें पर ध्यान दिया गया:-
(अ) पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा इन संस्थाओं के व्यवहार तथा नैतिकता के नियमों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
(ब) गैर-सरकारी संस्थाओं की एक डायरेक्टरी बनाई जाएगी जिसमें इन संस्थाओं का विवरण दर्ज होगा। इसका उद्देश्य:-
असमर्थ बालकों एवं असमर्थ व्यक्तियों के संगठन, माता-पिता की मानसिकता आदि को समझने वाली बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, उनका नाम इस डायरेक्टरी में होगा जिससे उनके कार्यों का पता आसानी से लगाया जा सके।
(स) गैर-सरकारी संगठनों को मानव संसाधनों के विषय में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान किये जायेंगे। इन संगठनों द्वारा पहले से दिये जा रहे प्रबंधन प्रशिक्षण को और मजबूत बनाया जायेगा।
(द) गैर-सरकारी संस्थाओं को अनुदान के लिए सरकार पर कम निर्भर होने तथा स्वयं अपने संस्थानों को अधिक विकास करने पर बल दिया जायेगा।
|
|||||