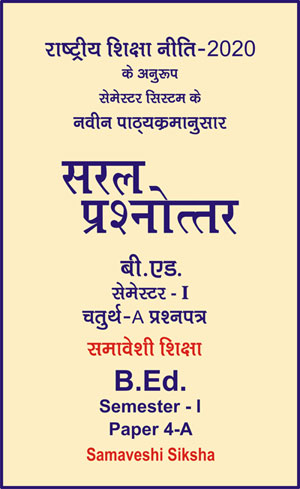|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
5 पाठक हैं |
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- समावेशी शिक्षा की अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व को उल्लिखित कीजिए।
उत्तर -
समावेशी शिक्षा की अवधारणा में निम्नलिखित तथ्य दिखाए देते हैं—
- शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।
- यह सहअवसर के सिद्धांत पर आधारित है।
- यह विविधतापूर्ण शिक्षण पद्धति की आवश्यकता है।
- सामायोजन की कला का विकास करना।
- इसमें सामान्य, विशिष्ट, अपंग सभी बच्चे मिलकर शैक्षिक अनुभव प्राप्त करते हैं।
- इसका उद्देश्य सामान्य शिक्षा में सभी को एक साथ शिक्षण करना है।
- विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना।
- प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता होती है। उसका विकास करना और उसे आगे बढ़ाना।
- विशिष्ट व सामान्य बालकों में सामाजिक कुशलता व व्यवहार का विकास करना।
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व
वर्तमान में जनसंख्या विस्फोट से बालकों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ उनकी बढ़ती हुई विविधताएं भी महत्वपूर्ण रूप से देखी जा रही हैं। इन सभी प्रकार की विविधताओं के साथ लेकर सभी को समान शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है।
यह शिक्षा भाषा, धर्म, लिंग, संस्कृति एवं सामाजिक तत्त्व शारीरिक, मानसिक गुणों की विविधता वाले बालकों को एक-दूसरे से सीखने, सामाजिक रूप से समायोजित होने तथा सामायोजन हेतु बहुगुणी अवसर प्रदान करने में सहायक है। वर्तमान में समावेशी शिक्षा अपरिहार्य आवश्यकता बन गई है।
वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व इस प्रकार है।
1. शिक्षा के स्तर को बढ़ाना - समावेशी शिक्षा "सबके लिए शिक्षा की अवधारणा" पर ही नहीं बल्कि सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा पर आधारित है। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में शिक्षण प्रक्रिया ऐसे नियोजित की जाती है जैसे कि हर बच्चा अपना समुचित विकास कर सके और अपनी योग्यता एवं क्षमता का विकास कर सके।
2. संवैधानिक उत्तरदायित्व का निवर्हन - भारत के संविधान में भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जाति, धर्म, भाषा, शारीरिक अक्षमता, लिंग आदि के कारण शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका निवर्हन करने तथा इसकी प्रवृत्ति रोकने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून भी बनाया गया है। जिसके अनुसार शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। उसे कोई भी शिक्षण संस्थान शिक्षा देने से इनकार नहीं कर सकता। समावेशी शिक्षा भी सभी को शिक्षा प्रदान करने का आह्वान करती है।
3. सामाजिक समानता - समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत का अनुसरण करती है। यूनेस्को के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया कि "स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी बच्चे अध्ययन करते हैं साथ में खेलते हैं।"
समाज व्यवहार की कला सीखने का सबसे अच्छा माध्यम स्कूल ही है। यह सिद्धांत "स्कूल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी बच्चों को अध्ययन द्वारा एक समान शिक्षा कराई जाती है।"
जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, भाषा, मानसिक गुणों की विविधता वाले बच्चों को एक साथ समान शिक्षा कराई जाती है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक रूप से बाधित बालकों को सभी के साथ शिक्षा प्रदान करने पर बल देती है।
4. व्यक्तिगत जीवन का विकास - यह शिक्षा व्यक्तिगत जीवन के विकास में लाभकारी होती है। बच्चों को मानसिकता व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। इस शिक्षा के तहत बालकों में संचारात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक व मानसिक विकास के लिए इसका विशेष महत्व है।
5. समाज के विकास के लिए - व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं। व्यक्तियों के संगठनों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि सम्पूर्ण समाज का विकास करना है तो सभी को शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।
व्यक्ति के परिश्रम, समझदारी व प्रयासों से ही उसका जीवन संवरता है और शिक्षा की भूमिका इसमें सर्वोपरि रहती है। इस प्रकार समाज का विकास उसके सुयोग्य नागरिकों पर निर्भर करता है।
वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि शिक्षा संस्थान प्रत्येक व्यक्ति को समाज बनाए तथा उसे प्रदान की जाने की जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी-अपनी योग्यताओं व कुशलता का विकास करे। समावेशी शिक्षा में समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है जिससे कि वे सभी शिक्षित होकर रोजगार प्राप्त कर सकें व अच्छे समाज की निर्माण में सहायता कर सकें।
6. लोकतांत्रिक गुणों का विकास - समावेशी शिक्षा बच्चों के लोकतांत्रिक गुणों के विकास में सहायक होती है। लोकतांत्रिक गुणों के अंतर्गत न्याय, सहिष्णुता, सहअस्तित्व, सहभागिता, सहनशीलता, एक-दूसरे का सम्मान आदि आते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षण करने से इन गुणों का विकास संभव है। ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहिए क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली अन्य पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, स्कूल तथा बच्चों में, या कक्षा से बाहर पारस्परिक क्रिया तथा व्यवहार में गतिशीलता व समायोजन को बढ़ावा देती है।
7. उचित समायोजन - समावेशी शिक्षा से छात्र विभिन्न परिस्थितियों व वातावरण में समायोजन कला सीखते हैं, अनेक अध्ययननों से पता चलता है कि नियमित रूप से मिल-जुलकर कार्य करने से छात्र में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है।
8. राष्ट्र की प्रगति - शिक्षा किसी भी देश के विकास एवं प्रगति के लिए आवश्यक है। यूनेस्को ने जेनेवा में समावेशी शिक्षा पर 2008 में एक रिपोर्ट दी और स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति विस्तार के बावजूद भी अभी 72 मिलियन बच्चे निर्धनता या सामाजिक स्तर के कारण विद्यालय नहीं जा पाते हैं।
राष्ट्र के विकास एवं प्रगति के लिए मानवीय समानता का पक्षधर होना आवश्यक है और यह कुपोषित शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई असमर्थ बालक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसमें उन सभी गुणों का बाह्यिक विकास होता है जिसका समाज से अपेक्षा रहती है। यदि व्यक्ति या बालक शिक्षित है तो वह किसी क्षेत्र में निपुण बन सकता है और राष्ट्र की भावनाओं का समर्थन करता है। इसलिए समावेशी शिक्षा में सभी को शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे देश का प्रत्येक बालक शिक्षा प्राप्त कर जो कि राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है।
9. आधुनिक तकनीकों का प्रयोग - वर्तमान में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरनेट आदि का प्रयोग साधारण-सी बात हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होने लगा है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को इन उपकरणों का ज्ञान कराया जाता है। इस ज्ञान से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग कर उचित ज्ञान प्राप्त कर सकता है तथा ज्ञान का विकास कर सकता है।
10. शिक्षा की सार्वभौमिकता - सरकार शिक्षा की सार्वभौमिकता के लिए अनेक योजनाएं बनाती है, जब तक इन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है तब तक इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा (विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा) को तभी सार्वभौमिक बनाया जा सकता है जब तक प्रत्येक बालक के गुणों, स्तर तथा आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें शिक्षा का विकास किया जाए। समावेशी शिक्षा सरकार की योजनाओं को सही रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें महिला, जाति, भाषा व शारीरिक रूप से असमर्थ बालकों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाती है।
11. माता-पिता के लिए स्तुत्यजनक प्रभाव - अधिग्रहण: "देखा जाता है कि असहाय, अपंग बालकों के जन्म के साथ-साथ उनके अभिभावकों को चिंता यह बनी रहती है कि बालक की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होगी?"
इस प्रकार की निराशा व हताशा बनी रहती है। लोग प्रारंभ से ही ऐसे बच्चों को दया की दृष्टि से देखते हैं। पहले इन बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजना पड़ता था, माता-पिता अधिक चिंतित रहते थे।
किन्तु अब समावेशी शिक्षा के कारण वे कारण अब ऐसे बालक अपने परिवार के साथ ही रहकर सामान्य विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो कि माता-पिता व अभिभावकों के लिए स्तुत्यजनक प्रभाव है।
12. रोजगार के अवसरों में वृद्धि - शिक्षा को जीविकोपार्जन में सहायक यंत्र के रूप में माना जाता है। प्रत्येक देश में शिक्षा एक अंग और ज्ञान संग्रह में सहायक है। दूसरी ओर शिक्षा रोजगार के साधन से शिक्षित व्यक्ति किसी भी रोजगार की कुशलता के साथ कर सकता है, वहीं अशिक्षित व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण लाचार होता है। परिणामस्वरूप निर्धनता का एक चक्र चलता रहता है।
शिक्षा का प्रसार करना हमारी आवश्यकता है और समावेशी शिक्षा इस दृष्टि से एक प्रयास है।
|
|||||