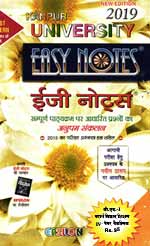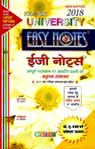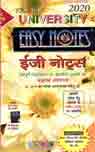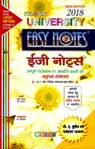|
शिक्षाशास्त्र >> ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षण ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षणईजी नोट्स
|
|
||||||
बी.एड.-I प्रश्नपत्र-4 (वैकल्पिक) पदार्थ विज्ञान शिक्षण के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
प्रश्न 6. आर. सी. ई. एम. उपागम के विभिन्न सोपान क्या है? इसके अनुसार
पाठ-योजना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।
अथवा
आर. सी. ई. एम. उपागम के विभिन्न पदों को बताते हुये पाठ-योजना का प्रारूप
प्रस्तुत कीजिए।
1. आर. सी. ई. एम. उपागम के चरण बताइये।
2. आर. सी. ई. एम. के अनुसार पाठ-योजना का प्रारूप बताइये।
उत्तर=आर.सी. ई. एम. उपागम
(R.C.E.M Approach)
शिक्षण लक्ष्यों को व्यावहारपरक रूप में लिखने का यह उपागम रीजनल कॉलेज ऑफ
एजूकेशन, मैसूर के डॉ. दबे द्वारा सन् 1967 ई. में विकसित किया गया। इसमें
लक्ष्यों के निर्धारण में ब्लूम की टेक्सानोमी को ही प्रयुक्त किया गया। परन्तु
संज्ञानात्मक क्षेत्र के छ: वर्गों के स्थान पर चार वर्गों-ज्ञान, बोध, प्रयोग
और सृजनात्मक को ही लिया गया।
आर.सी.ई.एम. के अनुसार, उद्देश्यों का वर्गीकरण
(1) ज्ञान प्रत्यास्मरण करना
(2) बोध अभिज्ञान करना
सम्बन्ध देखना
उदाहरण देना
भेद करना
वर्गीकरण करना
अर्थापन करना
(3) प्रयोगतर्क करना परिकल्पना का प्रतिपादन करना
परिकल्पना की स्थापना करना
निष्कर्ष निकालना
पूर्व कथन करना
(4) सजनात्मक विश्लेषण करना -संश्लेषण करना
मूल्यांकन करना
इस उपागम में शिक्षण लक्ष्यों को निर्धारित कर लिया जाता है। तत्पश्चात् पढ़ाए
जाने वाले पाठ की विषय-वस्तु के तथ्यों को प्रयुक्त करते हुए अपेक्षित
व्यावहारिक परिवर्तन के रूप में लिखा जाता है—
ज्ञानात्मक-1.1 विद्यार्थी ......" का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
1.2 विद्यार्थी ...... प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे।
अवबोधात्मक-2.1 विद्यार्थी ......' तथा ....." में सम्बन्ध देख सकेंगे।
2.2 विद्यार्थी ..." का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे।
2.3 विद्यार्थी ......" एवं ....... में अन्तर कर सकेंगे।
2.4 विद्यार्थी ......" की व्याख्या कर सकेंगे।
2.5 विद्यार्थी ......" को वर्गीकृत कर सकेंगे।
2.6 विद्यार्थी ......" की जाँच कर सकेंगे।
2.7 विद्यार्थी ....." को सामान्यीकृत कर सकेंगे।
प्रयोगात्मक-3.1 विद्यार्थी ....... के कारण बता सकेंगे।
3.2 विद्यार्थी ...... की परिकल्पना सिद्ध कर सकेंगे।
3.3 विद्यार्थी ...... को निर्मित परिकल्पना सिद्ध कर सकेंगे।
3.4 विद्यार्थी ....... के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाल सकेंगे।
3.5 विद्यार्थी....... के विषय में भविष्यवाणी कर सकेंगे।
सृजनात्मक 4.1 विद्यार्थी .....' को विश्लेषित कर सकेंगे।
4.2 विद्यार्थी ......" को संश्लेषित कर सकेंगे।
4.3 विद्यार्थी ....... का मूल्यांकन कर सकेंगे।
प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षण अभ्यास में आर.जी.ई.एम. का प्रयोग शिक्षण
उद्देश्यों का उपरोक्त विश्लेषण शिक्षण क्रियाओं के स्तर को तो प्रदर्शित करता
है। किन्तु उनका विशिष्ट रूप स्पष्ट नहीं करता। जब उद्देश्यों की परिभाषा
छात्रों के व्यवहारों के परिवर्तन से कर दी जाती है तो वह स्पष्ट व प्राप्त
करने योग्य हो जाते हैं।
इस कारण इन उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है।
अन्यथा यह स्पष्ट नहीं हो पायेगा कि निर्धारित उद्देश्यों के दृष्टिकोण से
छात्रों में किस क्षेत्र में कौन-से विकास सम्बन्धी व्यावहारिक परिवर्तन हुए
हैं।
शिक्षण व अधिगम में प्रत्यक्ष सजीव सम्बन्ध हेतु उन्हें व्यावहारिक रूप में
लिखना आवश्यक हो जाता है।
इसके फलस्वरूप शिक्षण क्रियायें सीमित व सुनिश्चित हो जाती हैं एवं सभी प्रकार
की अस्पष्टतायें दूर हो जाती हैं इससे मापन व विधि निर्धारण में सहायता मिलती
है।
आर. सी. ई. एम. उपागम के सोपान
(Steps of R.C.E.M Approach)
आर.सी.ई.एम. उपागम के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं-
(1) अदा (Input)-इसके अन्तर्गत अपेक्षित व्यावहारिक परिवर्तनों को निर्धारित
किया जाता है। तत्पश्चात् ज्ञान, बोध प्रयोग तथा सृजनात्मक लक्ष्यों के 17
मानसिक योग्यताओं में वर्गीकृत करके उनकी सहायता से शिक्षण लक्ष्यों को
व्यावहारिक रूप में लिखा जाता है।
(2) प्रक्रिया (Process) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण की
प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। शिक्षक प्रस्तुत प्रकरण की विषय-वस्तु के
अनुरूप शिक्षण युक्तियों एवं विधियों का चयन करते हैं ताकि उपर्युक्त अधिगम
परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकें, विद्यार्थी प्रेरित किए जा सकें उन्हें
शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रखा जा सके।
(3) प्रदा (Out Put) इसके अन्तर्गत विद्यार्थियों के वास्तविक व्यावहारिक
परिवर्तन अंकित होते हैं। इन्हें वास्तविक अधिगम प्रदा (Real Learning Out
comes R.L.O.S.) कहा जाता है। इसके लिए शिक्षक विविध प्रकार की मापन प्रविधियों
का उपयोग करता है। मापन की प्रविधियाँ अकथित परिवर्तन पर आधारित होती हैं।
इसमें शिक्षक लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं।
इसमें शिक्षक अपने शिक्षण के साथ ही शिक्षण लक्ष्यों की जानकारी भी रखता है।
शिक्षण-प्रशिक्षण अभ्यास हेतु पाठयोजना का प्रारूप
पाठ-योजना संख्या ......
दिनांक............ विषय......... चक्र
कक्षा....प्रकरण..........अवधि
शिक्षण लक्ष्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन
सहायक सामग्री-
शिक्षण विधि-
पूर्वज्ञान-
प्रस्तावना-
शिक्षक क्रियाएँ-छात्र क्रियाएँ-श्यामपट कार्य
उद्देश्य कथन....
प्रस्तुतीकरण-
शिक्षण -अदा अनुदेशन - प्रक्रिया शिक्षण-प्रदा मूल्यांकन वास्तविक व्यवहार
परिवर्तन
बिन्दु-अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन-सम्प्रेषण विधि अधिगम के अनुभव शिक्षण
क्रियाएँ-
1. ज्ञान- व्याख्यान, चार्ट- सूचना, निरीक्षण, लिखना, अन्तः प्रक्रिया करना
2. बोध - छात्र क्रियाएँ पुनरावृत्ति प्रश्न करना, प्रदर्शन
परिभाषा देना, कथन स्पष्टीकरण - देना, व्याख्या करना वाद-विवाद, तथ्य
अधिनियमों व्याख्यात्मक
प्रश्न समस्या, समाधान को पहचानना, अपने शब्दों में
अर्थ प्रदर्शन सहित
-सम्बन्ध देखना, व्यक्त करना, वाद-विवाद भिन्नता देखना समस्या का समाधान करना।
- समस्या समाधान - प्रयोग करने का प्रयोगशाला परीक्षा -अवसर देना।
देना। प्रयोगशाला कार्य | सीखे हुए ज्ञान का | परिस्थितियाँ उत्पन्न प्रयोग
करना। करना। नई समस्या का | तत्वों का विश्लेषण| आलोचनात्मक प्रश्न समाधान,
करना सम्बन्ध पूछना व्यक्तिगत कार्य स्थापित करना, नई समस्या उत्पन्न पर बल
दिया निर्णय लेना करना जाना।
समस्या का समाधान निकलवाना।
3. प्रयोग
4. सृजनात्मक
श्यामपट सारांश ...
मूल्यांकन ...
गृह कार्य....
सन्दर्भ ग्रन्थ...
|
|||||