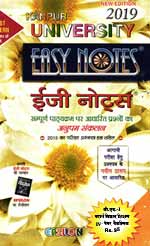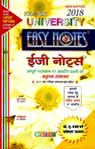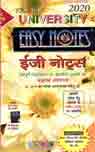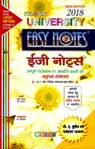प्रश्न 3. पाठ-योजना के विभिन्न प्रारूपों का उल्लेख कीजिए। किसी एक के
अनुसार, कक्षा आठ हेतु कोई पाठ-योजना तैयार कीजिए।
अथवा
आठवीं कक्षा के लिए विज्ञान विषय के किसी प्रकरण पर एकपाठ-योजना निर्मित
कीजिए।
1. पाठ-योजना के प्रारूपों को समझाइये।
2. किसी एक विषय की पाठ-योजना के प्रारूप को बताइये।
3. विभिन्न विषयों की पाठ योजनाओं के प्रारूप को समझाइये।
4. कक्षा आठ हेतु कोई एक पाठ योजना बताइये।
उत्तर-पाठ-योजना बनाने हेतु अपनाये जाने वाले प्रारूप
(Forms to be Followed to Prepare Lesson Plan)
1. परिचयात्मक विवरण (Identifying Data)- पाठ-योजना का यह प्रारम्भिक सोपान है।
इसके अन्तर्गत एक शिष्य-अध्यापक द्वारा अपनी पाठ-योजना पुस्तिका तथा पुन: कक्षा
में अध्ययन करते हुए श्यामपट पर निम्न बातें लिखी जाती हैं-
(i) अध्यापक का नाम और उसका रोल नम्बर।
(ii) कक्षा और श्रेणी जिसे पढ़ाना है।
(iii) विषय का नाम (जैसे भौतिक विज्ञान शिक्षण हेतु "भौतिक विज्ञान" लिखा
जाएगा)
(iv) उप-विषय या प्रकरण का नाम (जिस पर पाठ-योजना तैयार की गई है) प्रकरण
(Topic) का नाम पहले से ही नहीं लिखा जाता, बल्कि प्रस्तावना स्तर पर प्रश्न
पूछकर या अन्य किसी तरह से अपने पाठ को प्रस्तावित करते हुए जब अध्यापक द्वारा
पाठ को पढ़ाने का प्रयोजन बता दिया जाता है तो उसके साथ ही फिर पढ़ाए जाने वाले
पाठ या प्रकरण की घोषणा की जाती है, जैसे “विद्यार्थियों आज हम ऊर्जा के स्रोत
के बारे में अध्ययन करेंगे।" ऐसी घोषणा कर चुकने के पश्चात् ही उप-विषय या
प्रकरण के आगे"ऊर्जा के स्रोत" लिखा जाता है।
(v) पाठ के शिक्षण की तिथि (जब पाठ-योजना तैयार की जाए वह तारीख यहाँ नहीं लिखी
जाती पर जिस तारीख को कक्षा में पाठ प्रस्तुत किया जा रहा हो वह लिखी जाती है)।
(vi) अवधि (Duration) : जितने समय के शिक्षण अधिगम हेतु पाठ-योजना तैयार की गई
है। प्रायः यह अवधि कक्षा पीरियड यानी 35-40 मिनट की ही होती है।
2. सहायक सामग्री (Aid Material)-पाठ को पढ़ाने के लिए जिस तरह की शिक्षण अधिगम
सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसका संक्षिप्त विवरण ही यहाँ दिया जाता है।
पाठ-योजना बनाते समय ही अध्यापक को यह लिखना पड़ता है। कक्षा में अध्यापक
द्वारा इस तरह के विवरण को न तो मौखिक रूप से और न ही श्यामपट पर लिखकर कभी भी
नहीं दिया जाता। अपनी पाठ योजना पुस्तिका में अध्यापक द्वारा निम्न प्रकार की
सहायक सामग्री का विवरण दिया जा सकता है—
(i) श्यामपट, चाक, झाड़न, संकेतक और (ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसकी आवश्यकता
सभी प्रकार के भौतिक विज्ञान पाठों के लिए पड़ती है)।
(ii) स्थूल सामग्री या वास्तविक वस्तुएँ।
(iii) चार्ट, चित्र, ग्राफ तथा मॉडल आदि।
(iv) स्लाइड, फिल्म, ट्रांसपेरेंसीज (Transparencies) तथा कम्प्यूटर
प्रस्तुतीकरण।
3. अनुदेशनात्मक उद्देश्य (Instructional Objectives)–इन्हें भी पाठ-योजना
पुस्तिका में ही लिखा जाता है तथा कभी भी विद्यार्थियों के सामने कक्षा में
मौखिक रूप से या श्यामपट लेखन के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किया जाता।
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण कार्य तथा उनकी उचित व्यवहारजन्य शब्दावली
में अभिव्यक्ति, ये दोनों ही काफी महत्त्वपूर्ण तथा पेचीदा कार्य हैं जिनके लिए
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की वर्गीकरण प्रणालियों (व्यवहार के सभी अनुक्षेत्रों
हेतु) तथा इन उद्देश्यों को व्यवहारजन्य शब्दावली में व्यक्त करने की विधियों
तथा पढ़ाए जाने वाली विषय-वस्तु का प्रकृति आदि की पूरी-की-पूरी समझ तथा
उद्देश्य निर्माण एंव लेखन हेतु अपेक्षित कौशल की जरूरत होती है।
अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण करके उन्हें व्यवहारजन्य शब्दावली में कैसे
लिखा जाता है, इससे सम्बन्धित ज्ञान एवं कौशल के अर्जन के लिए पाठक इस पुस्तक
के तीसरे अध्याय में वर्णित पाठ्य सामग्री की पूरी-पूरी सहायता ले सकते
हैं।
4. पूर्व ज्ञान (Previous Knowledge)-यहाँ छात्र अध्यापकों द्वारा अपनी पाठ
योजना पुस्तिका में पाठ को बढ़ाने हेतु जिस तरह के पूर्व ज्ञान तथा अनुभवों का
अर्जन विद्यार्थियों से अपेक्षित है। उसका संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करते
हैं। इस विवरण को भी केवल मात्र पाठ योजना पुस्तिका में लिखा ही जाता है,
अध्यापक द्वारा कक्षा में इसका किसी रूप में प्रस्तुतीकरण नहीं होता।
5. पूर्व ज्ञान परीक्षा एवं प्रस्तावना (Testing of Previous and
Introduction)पहले सोपान में जिस प्रकार के पूर्व ज्ञान के विद्यमान होने की
कल्पना विद्यार्थियों में की गई है उसी का परीक्षण करने की बात इस सोपान में
उठती है। यह कार्य या तो विद्यार्थियों से उचित प्रश्न पूछकर किया
जाता है या उनसे कुछ कार्य या क्रियाएँ सम्पादित करने के लिए कहा जाता है, या
उनसे कोई समस्या हल कराई जाती है अथवा उन्हें किसी ऐसी समस्यात्मक परिस्थिति
में रखने का प्रयत्न किया जाता है जिसकी वजह से उन्हें प्रस्तुत पाठ को पढ़ाने
की आवश्यकता का अनुभव हो। जिस तरह से पूर्व ज्ञान की परीक्षा लेनी हो तथा पाठ
को पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव कराना हो वह सब कुछ पाठ योजना पुस्तिका में लिखा
जाता है और उसी को आधार बनाकर अध्यापक कक्षा में पूर्व ज्ञान की परीक्षा तथा
पाठ के लिए प्रस्तावना का कार्य सम्पन्न करता है। पाठ प्रस्तावना का उद्देश्य
इस तरह प्रस्तुत पाठ के लिए पर्याप्त आधारभूमि तैयार करना है ताकि विद्यार्थी
पाठ शिक्षण हेतु अधिक-से-अधिक अभिप्रेरित हो सकें।
6. उद्देश्य घोषणा (Announcement of the Aim)-इस सोपान के अन्तर्गत अध्यापक
कक्षा में यह स्पष्ट रूप से बताता है कि आज किस प्रकरण विशेष का अध्ययन करना है
जैसे- विद्यार्थियों आज यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि "प्रकाश किस प्रकार गति
करता है?" आओ विद्यार्थियों आज हम जानें कि "प्रकाश सीधी रेखा में कैसे गमन
करता है?" आदि-आदि। इस तरह की घोषणा करने के पश्चात् छात्र-अध्यापक को उप-विषय
या प्रकरण का नाम उसके निर्धारित स्थान में श्यामपट पर लिख देना चाहिए।
7. प्रस्तुतीकरण (Presentation) अभी तक उपरोक्त सोपानों के अन्तर्गत जो कुछ भी
कहा गया है वह पाठ शिक्षण की प्रथम अवस्था यानी तैयारी से ही अपना सम्बन्ध रखता
है। वास्तविक क्रियात्मक रूप से शिक्षण करने की मंजिल तो प्रस्तुतीकरण नामक इसी
सोपान के माध्यम से ही तय की जाती हैं। क्या पढ़ाया जाएगा तथा कैसे पढ़ाया
जाएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या स्वरूप होगा तथा विद्यार्थी और
अध्यापकों के बीच कैसी अंत:क्रिया चलेगी? किस तरह की विधियाँ, तकनीक और व्यूह
रचनाओं का प्रयोग होगा, कैसी शिक्षण सामग्री किस रूप में प्रयोग में लाई जाएगी
इन सब बातों का नियोजन इसी सोपान के अन्तर्गत किया जाता है। वैसे तो जैसाकि हम
चर्चा कर चुके हैं, प्रस्तुतीकरण के लिए शिक्षण बिन्दु, शिक्षक गतिविधियाँ तथा
विद्यार्थी गतिविधियाँ नाम से तीन कॉलमों को बनाने का प्रचलन है, परन्तु स्थिति
अनुसार हम पहले कॉलम शिक्षण बिन्दु को भी हटा सकते हैं और क्या शिक्षण करना है
उससे सम्बन्धित सामग्री को बिना कॉलमों में बाँटे हुए पहले विषय-वस्तु (Subject
matter) के रूप में पहले ही लिखकर फिर शिक्षक और विद्यार्थियों की क्रियाएँ
हेतु दो कॉलमों में विभक्त कर आवश्यक कक्षा-कक्ष अन्त:क्रिया की प्रस्तुति कर
सकते हैं। जहाँ ऐसे काम न चले वहाँ हम प्रस्तुतीकरण हेतु तीन अलग-अलग कॉलम भी
बना सकते हैं।
8. सामान्यीकरण (Generalization)-भौतिक विज्ञानों के अधिकांश पाठों में किसी
नियम, सिद्धान्त तथा कार्यप्रणाली की खोज तथा स्थापना की बात सामने आती है।
भौतिक विज्ञानों में इस बात हेतु हम कई तरह के उदाहरण बालकों के सामने रखते
हैं, बहुत-सी वस्तुओं तथा उनके गुण एवं कार्य व्यापार का प्रदर्शन करते हैं,
उनके परीक्षण एवं प्रयोगों के परिणामों को सावधानी से नोट करने के लिए कहते
हैं। इन सभी बातों के आधार पर ही सामान्यीकरण कराया जाता है। इस तरह का
सामान्यीकरण करने में प्राप्त परिणामों को आधार बनाकर अध्यापक द्वारा ऐसे
प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी अनुक्रियाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को कोई
नियम, सिद्धान्त तथा कार्यपरक पद्धति के सामान्यीकरण में ज्यादा-से-ज्यादा
सहायता मिले जिसकी सहायता से सामान्यीकरण होगा तथा सामान्यीकरण के रूप में जो
कुछ भी प्राप्त होगा वह सभी कुछ छात्र-अध्यापकों द्वारा अपनी पाठ योजना
पुस्तिका में लिखा जाता है ताकि उसी को आधार बनाकर वे कक्षा में सामान्यीकरण के
लिए आवश्यक गतिविधियों का संचालन कर सकें।
9. पुनरावृत्ति (Recepitulation)-पाठ योजना हेतु यह काफी महत्त्वपूर्ण सोपान है
और इसका सम्बन्ध शिक्षण की उत्तर क्रियात्मक अवस्था (Post active phase of
teaching) से है। जब
पाठ का प्रस्तुतीकरण हो जाता है तो जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसे
विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ठीक तरह बिठाने के लिए पुनरावृत्ति कार्य का
सहारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पढ़ाने के दौरान जो कुछ अपूर्णता या गैप रह
जाते हैं या विद्यार्थियों के द्वारा अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने में जो
कमियाँ रह जाती हैं उनका मूल्यांकन तथा निवारण का उद्देश्य भी इस सोपान द्वारा
पूरा हो सकता है।
(10) गृह कार्य (Home Work)-पाठ-योजना का यह अन्तिम सोपान है। यहाँ
विद्यार्थियों को घर पर करके लाने हेतु कुछ कार्य सौंपा जाता है। इसका उद्देश्य
कक्षा में बालकों ने जो कुछ भी पढ़ा और सीखा है उसको ठीक तरह से उनके मस्तिष्क
में बिठाना तथा उपयोग करना सिखना होता है। भौतिक विज्ञान में इस प्रकार का गृह
कार्य निम्न रूपों में दिया जा सकता है-
(i) पढ़ाये गये प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों, सिद्धान्तों तथा प्रक्रियाओं आदि
को घर से याद करके लाने के लिए कहा जा सकता है।
(ii) प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों, सिद्धान्तों, प्रक्रियाओं तथा अनुप्रयोगों का
उन्हें कितनी अच्छी तरह से बोध हुआ है यह जानने के लिए उन्हें कुछ प्रश्नों के
उत्तर घर से अपनी उत्तर-पुस्तिकाओं में लिखने को कहा जा सकता है।
(iii) जो कार्य प्रयोगशाला में इनके द्वारा किया जाता है उसे अपनी प्रैक्टीकल
कॉपियों में लिखकर लाने के लिए कहा जा सकता है।
(iv) छात्रों को उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री या अनुप्रयोग आधारित वस्तु या
परीक्षण तथा प्रयोग करने के लिए जा सकता है जिससे स्पष्ट हो कि उन्होंने
कक्षा/प्रयोगशाला में कुछ अधिगम अनुभव कार्य किया है।
पाठ-योजना-1
विद्यालय-कृषक इन्टर कॉलेज मवाना, मेरठ - विषय विज्ञान कक्षा-VIII A
दिनाँक 4 सितम्बर, 2015 - उपविषय-भौतिक विज्ञान क्लाश—द्वितीय प्रकरण—ठोस
पदार्थों के गुण समय-35 मिनट
प्रमुख धारण (Major Concept)-प्रत्यावस्था, सुघट्यता व भंगुरता
विशिष्ट उद्देश्य (Specific Objective) –
1. प्रत्यावस्था की परिभाषा एवं उदाहरण सहित व्याख्या
2. सुघट्यता की परिभाषा व उदाहरण
3. भंगुरता की परिभाषा व उदाहरण
सामान्य उद्देश्य
1. छात्रों को विज्ञान के तथ्यों से अवगत कराना तथा विज्ञान का व्यावहारिक
उपयोग सिखाना।
2. छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
3. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
4. छात्रों की विचार शक्ति एवं तर्क शक्ति को उत्पन्न करना।
5. छात्रों में आत्म-निर्भरता एवं आत्म-विश्वास की भावना पैदा करना।
पूर्वज्ञान (Previous Knowledge)- छात्रों को यह पता है कि स्प्रिंग को खींचकर
छोड़ने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है, एल्युमिनियम का तार बल लगाने
पर मुड़ जाता है और चाक बल लगाना।
सहायक सामग्री (Material Aids)-चाक,श्यामपट, स्प्रिंग, चार्ट आदि।
पाठ योजना-3
कक्षा-VIII
विषय-रसायन विज्ञान
प्रकरण—पदार्थ की अवस्थायें
दिनांक-2 जनवरी, 2016
अवधि-40 मिनट
सामान्य उद्देश्य-
1. छात्रों में रसायन विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
2. छात्रों में विषय से सम्बन्धित आत्म विश्वास पैदा करना।
3. छात्रों में निरीक्षण एवं निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना।
4. छात्रों को नई तकनीकी जानकारियों से अवगत कराना।
5. छात्रों को स्वावम्बी बनाना।
विशिष्ट उद्देश्य छात्रों को पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं एवं उनके गुणों के
बारे में ज्ञान प्रदान करना।
सहायक सामग्री-
1. कांच की प्लेट,
2. पानी,
3. गैसे से भरा गुब्बारा,
4. चॉक, डस्टर व, श्यामपट आदि
पूर्व ज्ञान - छात्रों को ठोस, द्रव तथा गैस के बारे में सामान्य जानकारी है।
प्रश्न
सम्भावित उत्तर
1. पानी को ठण्डा करने पर क्या बनेगा? -बर्फ।
2. बर्फ को छूने पर क्या अहसास होता है?-ठण्डा लगता है।
3. बर्फ को पिघलने देने पर क्या होता है?-द्रव बनता है।
4. द्रव को गर्म करें तो क्या बनेगा?-भाप बनेगी।
5. जो वस्तु स्थान घेरती है तथा भार होता है, वह क्या है? - पदार्थ।
6. पदार्थ की कितनी अवस्थायें होती हैं?-उतर नहीं दे पाते।
उद्देश्य कथन आज हम ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में जानेंगे।
प्रकरण-पदार्थ की अवस्थायें।
प्रश्न
सम्भावित उत्तर
1. पदार्थ किन-किन अवस्थाओं में पाया जाता है? - ठोस, द्रव तथा गैस में।
2. ठोस का आकार एवं आयतन कैसा होता है? - निश्चित।
3. ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है?-क्योंकि ठोस के अणु पास होने के कारण
उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल अधिक होता है।
4. द्रवों का आयतन एवं आकार कैसा होता है? - द्रवों का आयतन निश्चित तथा आकार
अनिश्चित होता है।
5. ऐसा किस कारण होता है? - द्रव के अणु ठोस की तुलना में दूर-दूर होते हैं तथा
इनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान भी कम होता है।
6. गैसों का आयतन तथा आकार कैसा होता है? - गैसों का आयतन तथा आकार अनिश्चित
होता है।
7. यह अनिश्चित क्यों होता है?- क्योंकि गैस के अणु ठोस व द्रव की अपेक्षा
दूर-दूर होते हैं तथा उनके मध्य लगने वाला आकर्षण
बल का मान बहुत कम होता है।
सारांश
ठोस-इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं तथा इसके अणुओं के बीच लगने
वाला आकर्षण बल का मान भी अधिक होता है।
द्रव-इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है इसके अणुओं के मध्य लगने
वाला आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है।
गैस—इसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं इनके अणुओं के बीच लगने वाला
आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है।
पुनरावृत्ति प्रश्न -
1. मेज किस अवस्था में पायी जाती है?
2. पानी की कौन-सी अवस्था है?
3. गैस के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का मान कैसा होता है?
4. गैस का आयतन निश्चित क्यों होता है?
5. बल किस अवस्था में पाया जाता है?
6. द्रव का आयतन एवं आकार कैसा होता है?
निरीक्षण कार्य शिक्षक कक्षा में छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करेगा तथा
उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा।
...Prev | Next...