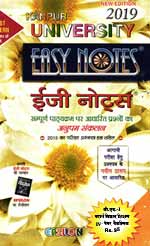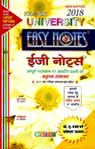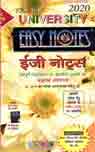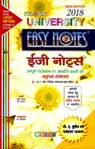|
शिक्षाशास्त्र >> ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षण ईजी नोट्स-2019 बी.एड. - I प्रश्नपत्र-4 वैकल्पिक पदार्थ विज्ञान शिक्षणईजी नोट्स
|
|
||||||
बी.एड.-I प्रश्नपत्र-4 (वैकल्पिक) पदार्थ विज्ञान शिक्षण के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार हिन्दी माध्यम में सहायक-पुस्तक।
प्रश्न 2. पाठ्य-पुस्तक से आप क्या समझते हैं? इनकी विशेषताएँ बताते हुए
इनमें होने वाले सुधार हेतु सुझाव दीजिए।
अथवा
पाठ्य-पुस्तक का अर्थ बताते हुए इनकी विशेषताएँ तथा सुझावों को वर्णन कीजिये।
1. पाठ्य-पुस्तक का क्या अर्थ है?
2. पाठ्य-पुस्तक की विशेषताओं को बताइये।
अथवा
विज्ञान पाठ्य-पुस्तक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए?
3. माध्यमिक स्तर पर पदार्थ विज्ञान पाठ्य-पुस्तकों में सुधार हेतु सुझाव
दीजिए।
उत्तर-पाठ्य-पुस्तक
(Text-Book)
सहायक साधनों के रूप में पाठ्य-पुस्तकों का अपना एक विशेष स्थान है। सभी विषयों
के शिक्षण कार्य में पाठ्य-पुस्तकें एक सफल सहायक और उचित मार्ग-निर्देशन के
रूप में कार्य करती आ रही हैं। यह विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए ही समान
रूप से उपयोगी हैं। पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी प्रकार का उपयोगी ज्ञान अच्छी
तरह सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में बिना किसी विशेष परिश्रम एवं खर्चे के
आसानी से उपलब्ध कराने, विषय को रोचक एवं उपयोगी बनाने में तथा सभी विद्यालयों
के कार्यों में समानता लाने में पाठ्य-पुस्तकों की बराबरी कोई भी सहायक साधन
नहीं कर सकता। विज्ञान जैसे विषय में जिसमें तथ्यों की वास्तविकता, यथार्थता और
संक्षिप्तता पर बल दिया जाता है। यही कारण है कि पाठ्य-पुस्तकों की उपयोगिता को
विज्ञान शिक्षण में निर्विवाद स्वीकार कर लिया गया है।
परन्तु एक पाठ्य-पुस्तक से ये सभी लाभ तभी उठाये जा सकते हैं जबकि वह कुछ
आवश्यक गुणों से युक्त हो। साधारण तौर पर विज्ञान शिक्षण की एक अच्छी
पाठ्य-पुस्तक में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए-
1. पाठ्यक्रम के अनुसार - पाठ्य-पुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण
पाठ्यक्रम पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के सभी अंगों पर इसमें उचित ध्यान
दिया जाना चाहिए।
2. विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति - पाठ्य-पुस्तक जिस श्रेणी के लिए
लिखी गई हो, उस श्रेणी में विज्ञान-शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके,
इसका ध्यान रखा जाना चाहिए।
3. पुस्तक का लेखक - पुस्तक विषय को अच्छी तरह जानने वाले योग्य एवं अनुभवी
लेखक द्वारा 'लिखी होनी चाहिए। अच्छा यही है कि उसे उन श्रेणियों को पढ़ाने का
अनुभव हो जिनके लिए वह पुस्तक लिखी गई है। लेखक का भाषा पर भी पूर्ण अधिकार
होना आवश्यक है।
4. पाठ्य-पुस्तक का चयन -
(i) पाठ्य-वस्तु जिस श्रेणी के लिए पुस्तक लिखी गई हो, उसके स्तर के अनुकूल
होनी चाहिए।
(ii) पाठ्य-पुस्तक में पाठ्य-सामग्री का चयन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए।
अच्छा तो यही है कि अनुभवी अध्यापकों के निजी अनुभव तथा वैज्ञानिक तथ्यों की
यथार्थता पर जोर दिया जाये।
(iii) पाठ्य-सामग्री विज्ञान-शिक्षण की आधुनिक उपयोगी विधियों की आवश्यकताओं को
ध्यान में रखकर लिखी होनी चाहिए।
(iv) पाठ्य-सामग्री अब तक विज्ञान तथा विज्ञान-शिक्षण के क्षेत्र में की गई सभी
खोजों को ध्यान में रखकर विज्ञान के परिवर्तित स्वरूप के अनुकूल ही होनी चाहिए।
(v) विषय-वस्तु का छात्रों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं, उनके सामाजिक एवं
प्राकृतिक 'परिवेश से सम्बन्धित होना आवश्यक है।
(vi) उस श्रेणी में विज्ञान के अतिरिक्त जो विषय पढ़ाये जा रहे हैं, उनको ध्यान
में रखते हुए पाठ्य-सामग्री ऐसी होनी चाहिए जिससे विज्ञान का स्वाभाविक रूप से
सभी विषयों के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सके।
(vii) अध्यापक के लिए उचित सुझाव और निर्देश भी दिये जाने चाहिए जैसे प्रयोग और
प्रदर्शन सम्बन्धी, सहायक सामग्री और स्वनिर्मित यन्त्रों के निर्माण एवं उपयोग
सम्बन्धी सुझाव तथा कुछ वैज्ञानिक रुचिकर कार्यों, संग्रहालय, भ्रमण आदि
कार्यों से सम्बन्धित निर्देश आदि।
(viii) प्रत्येक पाठ के अन्त में सारांश के रूप में मुख्य-मुख्य बातें दोहराई
हुई होनी चाहिए।
(ix) प्रत्येक पाठ के अन्त में अभ्यास एवं पुनरावृत्ति के लिए प्रश्न तथा
उपयुक्त समस्याएँ होनी चाहिए। नवीन प्रकार के प्रश्नों को उचित स्थान दिया जाना
चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो सके प्रश्न व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर होने
चाहिए। आगे पढ़ने के लिए तथा सीखे हुए सिद्धान्तों एवं तथ्यों को परखने एवं
व्यावहारिक प्रयोग में लाने के लिए अधिन्यास (Assignment) भी होने चाहिए।
5. शैली एवं भाषा-
(i) पुस्तक रुचिकर और मनमोहक शैली में लिखी होनी चाहिए, जिसे पढ़ने में बच्चों
का अच्छी तरह मन लग सके। अधिकतर बच्चों को वार्तालाप, कहानी, यात्रा अथवा दृश्य
वर्णन आदि से सम्बन्धित संवाद या शैली ही अच्छी लगती है।
(ii) पुस्तक की भाषा बहुत ही सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जहाँ तक हो सके
विद्यार्थियों से जितनी भाषा सम्बन्धी योग्यता की आशा की जा सकती है, उसके
अनुकूल ही होनी चाहिए।
(iii) वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धान्तों को क्रियात्मक कार्यों,
प्रयोगों,आकर्षक एवं स्पष्ट चित्रों से पूरी तरह स्पष्ट किया जाना चाहिए। इनसे
एक ओर तो विषय के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है तथा दूसरी ओर शिक्षण में
रोचकता आती है।
(iv) विभिन्न तथ्य एवं सिद्धान्त अलग पैराग्राफों (गद्यांश) में बतलाए जाने
चाहिए। एक साथ रखने से समझने में कठिनाई हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए वाक्य
भी अधिक लम्बे-लम्बे नहीं होने चाहिए।
(v) पुस्तक में भाषा सम्बन्धी अथवा मुद्रण (Printing) सम्बन्धी भूलों की ओर
विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विज्ञान जैसे विषय में ऐसी तनिक-सी गलती से
शब्दों का अर्थ उलट-पलट हो जाता है। बहुत-सी अशुद्ध बातें बच्चों के मन में घर
कर लेती है, क्योंकि बच्चे छपे हुए पृष्ठों पर अध्यापक के कथन से कहीं अधिक
विश्वास करते हैं।
(vi) वैज्ञानिक सूत्र, संकेत तथा पारिभाषिक शब्द और नामावली वही होनी चाहिए जो
अधिक -से-अधिक प्रयोग में आती हो तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर
मान्य हो।
6. पाठ्य-वस्तु का आयोजन -
(i) पाठ्य-पुस्तक में पाठ्य-वस्तु के आयोजन सम्बन्धी सूचना देने के लिए आरम्भ
में अच्छी तरह विषय-सूची दी जानी चाहिए।
(ii) विषय-सामग्री का आयोजन इस प्रकार का होता है कि प्रकरणों तथा पाठों में
परस्पर सम्बन्ध बना रहे।
(iii) विभिन्न प्रकरण "सरल से कठिन की ओर" नामक सिद्धान्त के अनुसार क्रमबद्ध
होने चाहिए। पहले सरल प्रकरण के लिए जाए, बाद में कठिन।
(iv) विषय-वस्तु का आयोजन प्रकरण के अंश (Concentric) के सिद्धान्त पर होना
चाहिए। किसी भी श्रेणी में पढ़ाए जा रहे अंशों का पिछली तथा बाद की कक्षाओं में
पूर्ण सम्बन्ध होना चाहिए।
(v) विषय-सामग्री की व्यवस्था में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक क्रम को भी स्थान
दिया जाना चाहिए।
7. पुस्तक की छपाई तथा गैट-अप-
(i) पाठ्य-पुस्तक में प्रयोग किया जाने वाला कागज अच्छे स्तर का होना चाहिए।
(ii) पाठ्य-पुस्तक की छपाई छात्रों की आय के अनुकल होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं
में अक्षरों एवं चित्रों का आकार अधिकतर बड़ा ही रखना चाहिए। शीर्षक बड़े तथा
छोटे टाइप में आवश्यकतानुसार दिये जाने चाहिए।
(iii) छपाई सीधे अक्षरों में पूरी तरह स्पष्ट एवं अच्छी तरह पढ़ी जाने वाली
होनी चाहिए।
(iv) पाठ्य-पुस्तक की जिल्द बहुत आकर्षक तथा मजबूत होनी चाहिए। उसकी सिलाई ऐसी
हो कि पुस्तक आसानी से खोलकर सुविधापूर्वक पढ़ी जा सके।
(v) पुस्तक उचित आकार की होनी चाहिए। यह न तो अधिक लम्बी ही होनी चाहिए और न
अधिक भारी हो, जिससे छात्र सरलता से इसे प्रयोग में ला सकें।
8. कुछ अन्य उपयोगी बातें-
(i) संस्करण अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो उसी साल का हो अथवा उसमें
आवश्यक सुधार कर दिये गये हों।
(ii) पाठ्य-पुस्तक बाजार में आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
(iii) इतनी सब विशेषताओं के साथ-साथ उनका मूल्य भी अधिक नहीं होना चाहिए।
|
|||||